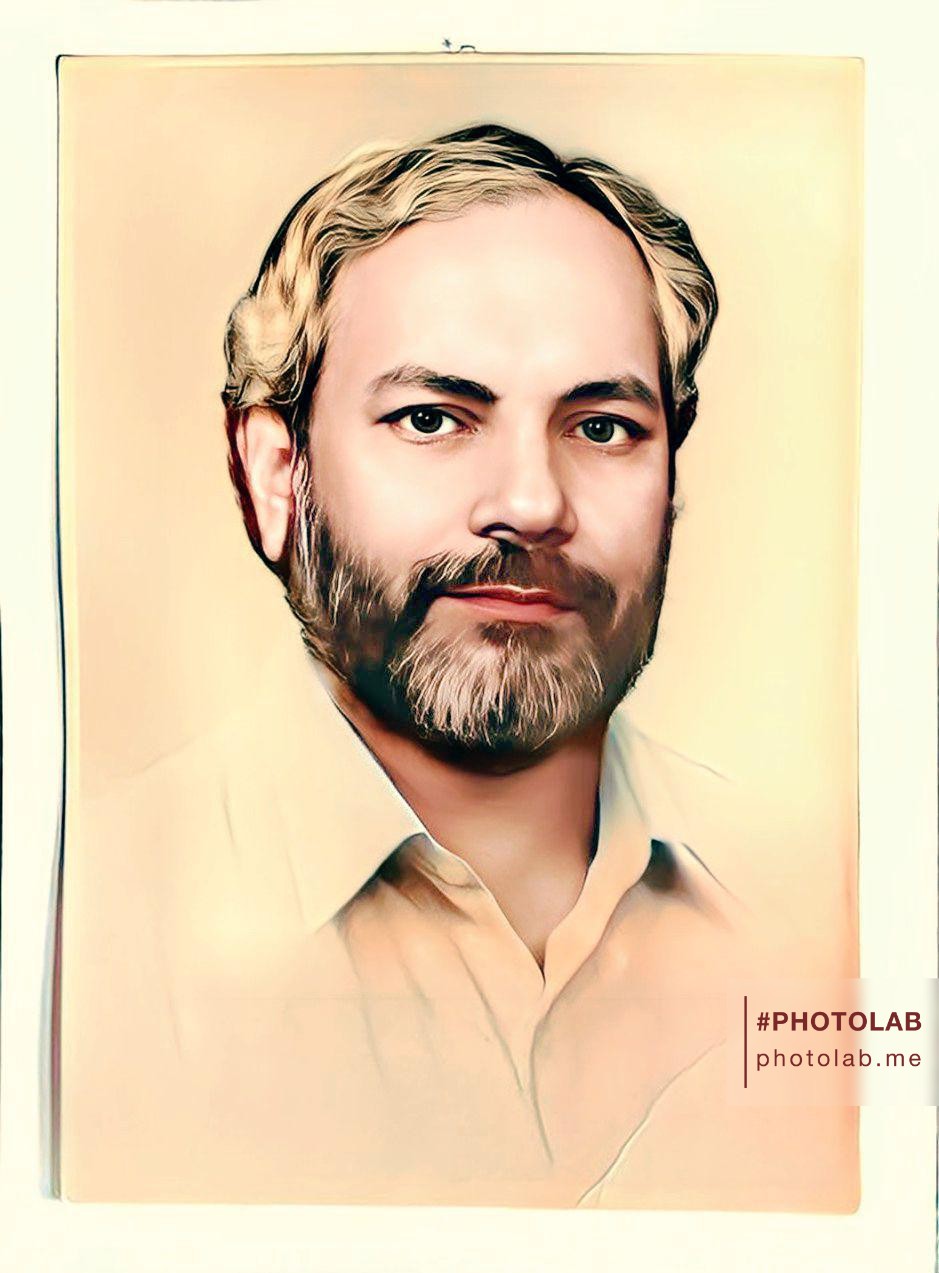तेजपाल सिंह ‘तेज’ : तथाकथित बाबाओं, पूंजीपतियों और राजनेताओं के बीच गठबंधन: लोकतंत्र पर एक त्रिकोणीय संकट
तथाकथित बाबाओं, पूंजीपतियों और राजनेताओं के बीच गठबंधन: लोकतंत्र पर एक त्रिकोणीय संकट
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता, बहुलता और धर्मनिरपेक्षता रही है। लेकिन बीते कुछ दशकों में लोकतंत्र का यह आधारभूत ढांचा धीरे-धीरे कमजोर होता गया है। आज हम एक ऐसे त्रिकोणीय गठबंधन को उभरते देख रहे हैं, जिसमें तथाकथित ‘धार्मिक बाबा’, कार्पोरेट पूंजीपति और सत्ता के गलियारों में बैठे राजनेता एक साझा मंच पर आ खड़े हुए हैं। यह गठबंधन न केवल जनता की चेतना को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, और संवैधानिक मूल्यों को भी निगलता जा रहा है।
1. तथाकथित बाबाओं की राजनीति में दखलअंदाज़ी : धर्म से सत्ता तक की यात्रा
भारत में संतों और महात्माओं की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन आज के तथाकथित बाबाओं की भूमिका भक्ति या अध्यात्म से अधिक सत्ता-संरचना के भीतर है। ये बाबा अब केवल आश्रमों में नहीं रहते, बल्कि टीवी चैनलों, चुनावी मंचों और कंपनियों के बोर्ड रूम में भी देखे जाते हैं। इनमें से कई बाबा न सिर्फ राजनीतिक दलों के प्रचारक बन गए हैं, बल्कि खुद चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, और नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। धर्म का नाम लेकर वे एक खास विचारधारा को जनता पर थोपने का काम कर रहे हैं। उदाहरणार्थ –
-बाबा रामदेव, जो योगगुरु से सीधे-सीधे एक व्यावसायिक साम्राज्य (पतंजलि) के निर्माता बने, और जिन्होंने खुलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया।
-आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद जैसे बाबाओं पर यौन शोषण से लेकर हिंसा तक के गंभीर आरोप लगे, लेकिन वे लंबे समय तक सत्ता संरचना का संरक्षण पाते रहे।
2. पूंजीपतियों की सांठगांठ और राजनीतिक निवेश : विकास का झूठा नैरेटिव
भारतीय पूंजीपति वर्ग ने 1991 के उदारीकरण के बाद से राज्य के भीतर गहरी पैठ बना ली। लेकिन आज हालात इस स्तर पर पहुँच चुके हैं कि वे केवल आर्थिक नीतियों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि सरकारों की संरचना और प्राथमिकताएं भी तय करते हैं। चुनावी चंदे से लेकर मीडिया की खरीद तक, सब कुछ इस गठजोड़ का हिस्सा है।
कॉर्पोरेट पूंजी और बाबाओं का संबंध : बाबाओं के विशाल साम्राज्य (जैसे रामदेव की पतंजलि, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग) में पूंजीपतियों का भारी निवेश होता है। बदले में ये बाबा धार्मिक नैरेटिव और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर उन आर्थिक नीतियों को वैधता प्रदान करते हैं जो कॉर्पोरेट हितों को पोषित करती हैं। यह एक दोतरफा लाभ का सौदा है।
3. राजनेताओं की भूमिका और रणनीति : धर्म और विकास का दोहरा खेल
राजनीतिक दल विशेषकर दक्षिणपंथी दलों ने बाबाओं और पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ करके सत्ता की एक अजेय मशीनरी बना दी है। एक ओर बाबा लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, दूसरी ओर पूंजीपति मीडिया और प्रचार तंत्र को नियंत्रित करते हैं। राजनेता इस पूरी संरचना के नियंता और लाभार्थी बन जाते हैं। यथा --
- राजनीति में बाबाओं का इस्तेमाल
- मंचों पर बाबाओं की उपस्थिति
-‘धर्म संसद’ जैसे मंचों से चुनावी निर्देश
- को साधने के लिए साधुओं के जरिए वोट बैंक पर असर
- द्वारा एक विशेष विचारधारा का सांस्कृतिक प्रचार
4. यह गठबंधन क्यों है खतरनाक?
(क) लोकतंत्र का हरण : जब धर्म, पूंजी और राजनीति एकत्र होते हैं, तो आम जनता के अधिकार, आलोचना की स्वतंत्रता, और संविधान के सिद्धांत सबसे पहले कुचले जाते हैं। लोकतंत्र केवल एक औपचारिक ढांचा रह जाता है, जहां असली शक्ति इस त्रिकोणीय गठबंधन के हाथ में होती है।
(ख) सामाजिक न्याय का पतन : बाबा जातिवाद को धार्मिक वैधता देते हैं, पूंजीपति सामाजिक असमानता को आर्थिक अनिवार्यता बताते हैं, और राजनेता इसे 'परंपरा' बताकर संविधान विरोधी नीतियों को लागू करते हैं।
(ग) विचार और चेतना का हरण : बाबा टीवी और यूट्यूब पर आध्यात्मिक भाषा में धार्मिक राष्ट्रवाद फैलाते हैं, पूंजीपति उसे प्रायोजित करते हैं, और राजनेता उसे कानून और पुलिस के जरिए लागू करते हैं।
5. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गठबंधन का मूल्यांकन:
अंबेडकर की चेतावनी : डॉ. आंबेडकर ने कहा था: "धर्म अगर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विरुद्ध जाता है, तो वह धर्म नहीं, गुलामी है।" बाबाओं और राजनेताओं का यह गठबंधन ठीक उसी तरह धर्म का उपयोग कर रहा है, जैसा मनु-प्रधान वर्णव्यवस्था करती थी।
गांधी और नेहरू की दृष्टि : जहां गांधी ने धार्मिकता को आत्मानुशासन के रूप में देखा, वहीं नेहरू ने धर्म को राजनीति से बाहर रखने की वकालत की। लेकिन आज धार्मिक प्रवचन, राजनैतिक घोषणापत्र बनते जा रहे हैं।
6. मीडिया और न्यायपालिका पर असर :
मीडिया का धार्मिक पूंजीकरण : निजी मीडिया संस्थानों में पूंजीपतियों का सीधा निवेश है, और अब बाबा भी टीवी चैनलों और डिजिटल मंचों के मालिक या भागीदार हैं। परिणामस्वरूप जनता के वास्तविक मुद्दे (बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य) गायब हो जाते हैं और उनकी जगह “धर्म खतरे में है” जैसे जुमले छा जाते हैं।
न्यायपालिका पर दबाव : कुछ मामलों में बाबाओं के खिलाफ मामले वर्षों तक खिंचते हैं, और कई बार सत्ता के प्रभाव में निर्णय भी पक्षपातपूर्ण दिखाई देते हैं। इससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।
7. वर्तमान उदाहरण
- मंदिर आंदोलन: एक धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया और पूंजीपतियों ने उसमें जमकर निवेश किया।
- और अन्य धार्मिक मेलों में सरकार की सहभागिता: सरकारी धन और संसाधनों को खुलेआम बाबाओं के प्रभाव क्षेत्र में लगाया गया।
- और आयुर्वेदिक व्यवसाय: बाबा रामदेव की कंपनी को सरकार ने कर छूट, जमीन और प्रचार में भारी समर्थन दिया।
- मोदी का तथाकथित 'संतों के आशीर्वाद' का प्रदर्शन: चुनावी जनसभाओं और टीवी इंटरव्यू में बाबाओं के साथ तस्वीरें और मंच साझा कर जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया गया।
8. वैकल्पिक रास्ता और जनजागरण की आवश्यकता :
बुद्ध-अंबेडकर की राह : अंबेडकर और बुद्ध दोनों ने 'विवेक' और 'चेतना' पर ज़ोर दिया। आज जब धर्म, पूंजी और राजनीति का गठजोड़ जनचेतना का हरण कर रहा है, तो नागरिकों को विवेक का सहारा लेना ही होगा।
जन आंदोलनों की भूमिका : चाहे वह किसान आंदोलन हो, सीएए विरोध हो या दलित-अधिकार आंदोलन — ये सब इस त्रिकोणीय गठजोड़ के खिलाफ जन शक्ति का प्रतीक हैं।
शिक्षा और संवाद की आवश्यकता : धर्म का ज्ञान, पूंजी का उपयोग और राजनीति की समझ — इन तीनों को विवेक और संवैधानिक चेतना से जोड़ना ही एकमात्र समाधान है।
तथाकथित बाबाओं, पूंजीपतियों और राजनेताओं के बीच बना यह त्रिकोणीय गठबंधन लोकतंत्र के लिए एक धीमा ज़हर है। यह गठजोड़ धर्म की आड़ में सामाजिक विषमता को वैधता देता है, पूंजी की ताकत से जनता की चेतना को नियंत्रित करता है, और सत्ता के माध्यम से संविधान के मूल्यों को दरकिनार करता है। अब समय आ गया है कि जनता खुद तय करे कि उसे लोकतंत्र चाहिए या धर्मोपजीवी गठबंधन। क्योंकि अगर धर्म का बाजार, पूंजी का मीडिया और राजनीति की सत्ता मिल जाए, तो जनता के पास केवल भ्रम और भक्तिभाव ही बचता है — अधिकार नहीं।
इस गठबंधन का इतिहास क्या है?
“तथाकथित बाबाओं, पूंजीपतियों और राजनेताओं के बीच गठबंधन” का इतिहास कोई हालिया घटना नहीं है; इसकी जड़ें भारत के औपनिवेशिक काल से भी पहले की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में देखी जा सकती हैं, जब धर्म, धन और सत्ता तीनों मिलकर सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख औजार हुआ करते थे। आइए हम इस गठबंधन के ऐतिहासिक विकास को कालक्रमानुसार समझें:
1.प्राचीन भारत: धर्म और सत्ता का जन्मजात गठबंधन
- की संधि: वैदिक युग से ही भारतीय समाज में ब्राह्मण (धार्मिक सत्ता) और क्षत्रिय (राजनीतिक सत्ता) के बीच एक मौन समझौता था।
- 'राजा को देवत्व' देते थे, और राजा ब्राह्मणों को विशेषाधिकार। धर्मग्रंथों में वर्णित ‘राजधर्म’ और ‘मनुस्मृति’ जैसे ग्रंथ इसी गठजोड़ की वैचारिक नींव बनते हैं।
- को राज्यशक्ति का औचित्य देने वाला उपकरण बनाया गया – जैसे ‘राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है’।
अर्थ और धर्म का संतुलन: पूंजीवाद उस समय अपने आधुनिक रूप में नहीं था, लेकिन व्यापारियों (वैश्य वर्ग) को भी धार्मिक वैधता और सत्ता संरक्षण मिलते रहे।
2. मध्यकाल: सूफी-संत बनाम शाही बाबागीरी
सूफी-संत परंपरा ने जहां राज्य सत्ता से दूरी बनाई, वहीं कई हिंदू और मुस्लिम संतों ने राजाश्रय को प्राप्त किया और धार्मिक ताकत को राजनीतिक वैधता में बदला। जैसे:
- महाप्रभु के अनुयायी बंगाल के नवाबों से संबंध रखते थे।
- जैसे कवियों को मुगल शासकों ने संरक्षण दिया।
- और राजाओं के बीच संबंध भी कभी सहयोगी, कभी टकरावपूर्ण रहे (जैसे गुरु तेग बहादुर और औरंगज़ेब के बीच)।
- वर्ग भी धार्मिक संस्थाओं को दान देकर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहा।
3. औपनिवेशिक भारत: धार्मिक नेताओं की राजनीतिक भूमिका :
- शासन में धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल बहुत ही रणनीतिक रहा।
- ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नेताओं और पोंगापंथियों को प्रोत्साहित किया।
- की क्रांति में कई धार्मिक नेताओं की भागीदारी ने उन्हें जनता के नायक बना दिया, जिसका लाभ बाद में राजनीतिक दलों ने उठाया।
-आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, देवबंदी और बरेलवी आंदोलन – सभी धर्म आधारित संस्थाओं ने सामाजिक सुधार के नाम पर राजनीति में दखल देना शुरू किया।