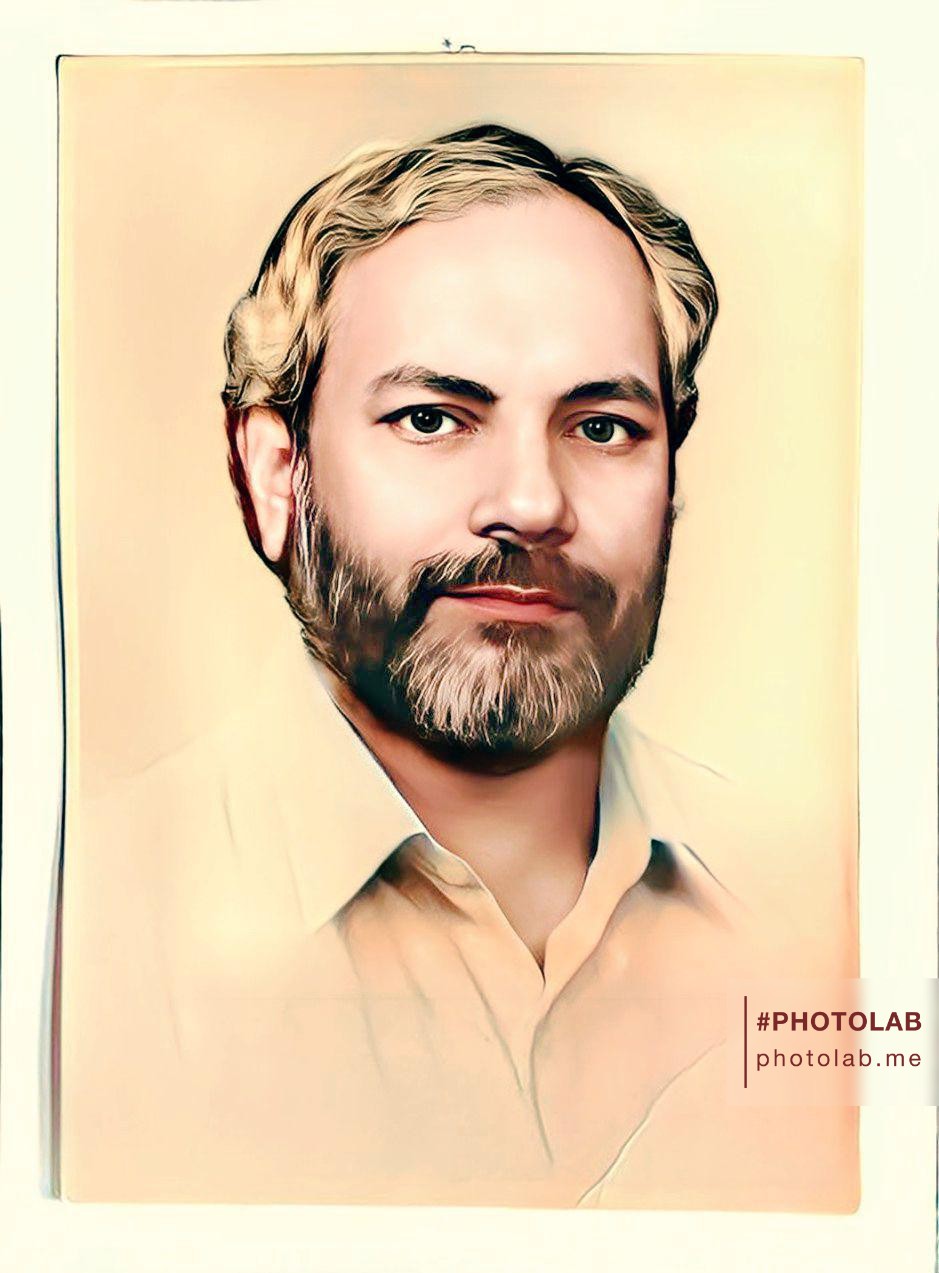तेजपाल सिंह ‘तेज’ (प्रस्तोता) : कवि, कविता और वो -ईश कुमार गंगानिया
प्रस्तुति : तेजपाल सिंह ‘तेज’
कवि, कविता और वो
-ईश कुमार गंगानिया
मौजूदा अंक नए साल यानी जनवरी-मार्च 2024 का है। लेकिन नए साल के पटाखों की गूंज, दावतों और बधाइयों का दौर कभी का नेपथ्य में चला गया हैं। इसलिए नए साल की बात करना ठीक नहीं लग रहा। इसके विपरीत वर्तमान दौर चुनाव का दौर है। इसलिए हर कोई चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई आदि की तर्ज पर लोकतंत्र की पीठ पर सवार हो, मनचाही उड़ान भर रहा है। चुनावी माहौल में इलेक्टोरल बांड की फुलझडि़यां और राजनीतिक मंचों से रंगबिरंगी रेवडियों की गारंटी ने सारे आकाश को गर्द-ओ-गुबार से भर दिया है। ऐसी अफरातफरी के माहौल से परे, सोचा क्यों न कवि, कविता और वो को लेकर कुछ गुफ्तगू की जाए।
शीर्षक को देख कर पाठक के मन मस्तिष्क में पति, पत्नी और ‘वो’ फिल्म जैसी कोई छवि उभर सकती है। लेकिन आधुनिक कवि और कविता का संबंध पति-पत्नी जैसा नहीं है। कवि और कविता का रिश्ता प्रेमी और प्रेयसी जैसा भी नहीं है, क्योंकि प्रेमी और प्रेयसी की दुनिया बहुत छोटी होती है और दोनों के बीच सिमटी रहती है। इस संबंध में दुख-सुख, मिलन-विछोह, नफा-नुकसान आदि दोनों तक सिमटा रहता है। लेकिन कवि और कविता के रिश्ते में ‘वो’ की भूमिका एक के प्रति वफादारी और दूसरे के प्रति गद्दारी यानी विलेन जैसी विवादित व संदिग्ध भी नहीं है। कवि और कविता के संबंध में यह रिश्ता, दोनों के प्रति वफादारी का रिश्ता है, जिम्मेदारी का रिश्ता है। यह रिश्ता विवाद से परे सकारात्मक व अनुकरणीय है। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें, ‘वो’ उन परिस्थितियों का नाम है जो शब्दों की झाड़-पोंछ और श्रृंगार करने वाले शिल्पी को कवि और श्रृंगारित शब्दों को कविता की संज्ञा का हकदार बनाता है। इसलिए ‘वो’ पर बात करना जरूरी महसूस हो रहा है।
मौजूदा संपादकीय में ‘वो’ पर बात करने की एक दूसरी वजह भी है। संपादक मंडल और उससे बाहर भी एक सुगबुगाहट बनी है कि साहित्य आलोचना की पत्रिका के संपादकीय में साहित्य पर भी बात होनी चाहिए। मुझे भी यह मांग काफी हद तक जायज लगी, इसलिए मैंने सोचा- क्यों न इस बार एक नए प्रयोग की तरह कविता पर बात की जाए। जब कविता पर बात होगी तो निस्संदेह कवि पर भी बात होगी। इन दोनों पर बात होने का मतलब है, कवि और कविता के वजूद के लिए अनिवार्य ‘वो’ यानी नियामक क्रियाकलापों व परिस्थितियों पर बात होना। यदि इन नियामक तत्वों पर बात न हो तो सारी कवायद ही बे-मायने हो जाती है। मेरा मानना है- ‘वो’ को समझे बगैर कवि और कविता को समझने की कोशिश धूल में लट्ठ भांजने जैसा उपक्रम होगा। ऐसे में हमारे हाथ धूल का साम्राज्य लगेगा, जिसमें कवि और कविता को ढूंढ पाना दुर्लभ काम होगा।
‘वो’ को समझने की इस कड़ी में मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद करना चाहता हूं। उनकी मान्यता है- ‘कविता लिखने की कला को अभ्यास से अर्जित नहीं किया जा सकता। यह ईश्वरदत्त है और जो चीज ईश्वरदत्त है, वह अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती।’ मैं इस पूरी स्थापना से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे यह स्थापना वर्णवाद के पहाड़े का नया संस्करण जैसी लगती है, जिसमें विद्वता ब्राह्मण की जन्मजात बपौती है। माना कि कुछ व्यक्तियों में मुश्किल कार्य को सहजता और सरलता से करने की क्षमता होती है। किसी को आसान कार्य करने में भी कुछ ज्यादा ही कठिनाई हो सकती है। यह प्रकृति प्रदत्त हो सकता है लेकिन मैं इस मिथक को कवि वृंद के दोहे- 'करत-करत अभ्यास के जड़मतिहोतसुजान। रसरीआवत-जात ते सिल पर पड़त निशान॥' की रोशनी में देखना चाहता हूं। कहना चाहता हूं कि अभ्यास से कवित्व ही नहीं जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ न कुछ उल्लेखनीय हासिल किया जा सकता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है।
कोई भी व्यक्ति यदि अपने परिवेश के प्रति जागरुक व संवेदनशील है और उसमें कविता जैसा कुछ करने की ललक है, कीड़ा है तो उसकी यथार्थपरक दृष्टि उससे कविता लिखवा सकती है। यह कविता प्यार, करुणा, दया, दुख, सुख, संघर्ष, क्रोध, प्रतिरोध आदि अनेक भाव पैदा कर सकती है। ये भाव किसी भी व्यक्ति के मन में हलचल पैदा कर सकते हैं और उसे सम्मोहित कर कविता के उस रचना संसार की यात्रा करा सकते हैं जो कवि ने अपने शब्दों के शिल्प और संवेदना के स्तर पर रचा है। कविता व्यक्ति को अपने वशीभूत के दम पर जितने अधिक समय के लिए उसकी दुनिया से दूर, अपने आगोश में मुग्ध रख सकती है, वह कवि और कविता की ताकत होती है। इस ताकत का कभी न सूखने वाला स्त्रोत ‘वो’ है, जो निरंतर कुछ न कुछ नए की मांग करता है; और इसे बासी कुछ भी पसंद नहीं है। इसके लिए किसी ईश्वर या ईश्वरदत्त किसी वरदान की जरूरत नहीं है। जैसी कि द्विवेदी की मान्यता है कि ईश्वरदत्त के बगैर कविता नहीं होती तो नास्तिक, अम्बेडकरवादी कविता और इनके कवियों की दुनिया कभी की वीरान हो गई होती। ऐसा न होना बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आज की कविता के सरोकार परंपरागत सरोकारों से भिन्न हैं।
पहले कविता ही क्यों, भारत के संदर्भ में, सम्पूर्ण साहित्य ही जाति विशेष की बपौती हुआ करता था। जाहिर है ‘वो’ भी इनकी बपौती रहा है। इसलिए संवेदनाओं का स्तर भी वर्ग/जाति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवेश का ही प्रतिनिधित्व करता था, पूरे समाज का नहीं। वैसे आज भी नहीं करता है, क्या करता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर ‘हां’ में होता तो दलित यानी अम्बेडकरवादी विमर्श, स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, बहुजन विमर्श आदि विमर्श को अस्तित्व में आने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन सवाल अस्मिता का है, वजूद का है, प्रतिनिधित्व का है और सवाल समाज की सामाजिक विश्वसनीयता का भी है। वीर भारत तलवार दलित यानी अम्बेडकरवादी चेतना के संबंध में इसकी पुष्टि कुछ इस प्रकार करते हैं-‘दलितों की हमारे समाज में एक खास स्थिति है। अपनी इसी स्थिति के कारण वे सच्चाई के उन पहलुओं को देख पाते हैं, जिन्हें हम सवर्ण, अपनी सवर्ण स्थिति के कारण ही, नहीं देख पाते। यही कारण कि आज जब दलित जाग रहे हैं और समाज को, इतिहास और हर चीज को अपनी जगह से, अपने नजरिए से देख रहे हैं तो सच्चाई के कई ऐसे पक्ष सामने आ रहे हैं जिससे हमारे पूरे सामाजिक इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत महसूस हो रही है।’
दलित साहित्यकार हमेशा से ही अपने साहित्य के बारे में दावा करते रहे है कि स्वानुभूति के चलते दलित समाज से जुड़ा व्यक्ति ही दलित साहित्य लिख सकता है, आज भी यह दावा बरकरार है। कविता इस दावे से बाहर नहीं है, यानी दलित साहित्य का ‘वो’ स्वानुभूति के वशीभूत है। काफी हद तक यह ठीक भी है, लेकिन इसे अंतिम सत्य जैसा मानकर चलना कविता के हित में नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नामवर सिंह (?) ने इस तर्क को काटते हुए किसी मंच से टिप्पणी की थी-क्या घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना जरूरी है? यह तर्क भी अजीब है लेकिन फिर भी इस पर विचार होना चाहिए कि साहित्य/कविता की दृष्टि समावेशी होनी चाहिए। इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि साहित्य और कविता भी राजनीति के शिकार रहे हैं। आधुनिक कविता को साहित्य की राजनीति और अवसरवाद से मुक्त होना चाहिए तभी अपने समय के इतिहास में अपनी भरोसेमंद उपस्थिति दर्ज करा सकेगी, जिसका जिक्र वीर भारत तलवार कर रहे हैं।
आधुनिक कविता का ‘वो’ इसकी भूमिका मनोरंजन, सौंदर्य, दुख-दर्द की काव्यमय अभिव्यक्ति, नए-नए कल्पना संसार रचना आदि से बड़ी है। कविता की जो बहुआयामी छवि हमारे सामने है, वह अपने समय का इतिहास बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसकी सशक्त विषयवस्तु है। जाहिर है, इसे अपने काल की एक सच्ची गवाह होना चाहिए। इसलिए इसे सच्चाई व विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए; यानी इसे बेबुनियाद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना, कविता के हक में नहीं होता। आज उपस्थित सभी विमर्श इसी मांग की पूर्ति करते नजर आते हैं। इसका श्रेय हिन्दी साहित्य जगत की अपेक्षा दुनिया के ग्लोबल विलेज में तब्दील हो जाने और इसके चलते अस्तित्व में आए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों को जाता है, जिसमें विभिन्न भाषाओं का अन्य भाषाओं में अनुवादित साहित्य उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है।
आधुनिक कविता यथार्थवादी है। ऐसा कहना शायद स्थितिप्रज्ञ होने का प्रमाण है। कविता आदिकाल की दरबारी यानी चारण कविता से अलग है। इसके सरोकार शासक के महिमामंडन, मनोरंजन और कवि की रोजी-रोटी के सवाल के समाधान तक सीमित नहीं हैं। उद्देश्य की दृष्टि से इसे मुजरे और कैबरे जैसे किसी मनोरंजन के समकक्ष रखकर भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन यकीन के साथ ऐसा दावा भाट व चारण संस्कृति के विषय में नहीं किया जा सकता। आधुनिक कविता का ‘वो’ भाषा के आविष्कारी धर्म, संकेतों के प्रयोग, स्वरों के स्तरीकरण, काव्य परंपरा को तोड़ने, और कविताओं में नई लय और मुहावरों को स्थापित करने की वकालत करता है। यह अलग बात है कि आज भी साहित्य/कविता इस भाट व चारण संस्कृति से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। कई बार पद, पुरस्कार, पारितोषिक आदि का पलड़ा इतना भारी होता है कि कवि अपने उद्देश्य से भटक जाता है। यदि वर्तमान काल को भटकाववाद, समझौतावाद या अवसरवाद काल की संज्ञा दी जाए, अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए।
आजकल ‘डर’ के परिवेश ने कवि और कविता को काफी प्रभावित किया है और अधिकांश कवि परिस्थितियों से पलायन करते नजर आते हैं। उनका ‘वो’ के मदारियों की बंदरिया बनना और उसके अनुरूप ही उछल कूद करना होकर रह गया है। कितने लोग हैं जो राहत इंदौरी की तरह कह पा रहे हैं ‘अगर ख़िलाफ़ हैं होने दो, जान थोड़ी है/ ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है...सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में/ किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी का ही एक अन्य किस्सा है जिसका सार कुछ इस प्रकार है। किसी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत कर दी कि राहत इंदौरी ने सरकार को बेईमान कहा है। राहत ने पूछताछ के दौरान अपने शब्दों की जादूगरी दिखाते हुए कहा-मैंने सरकार को बेईमान कहा है, अपने देश की सरकार को थोड़े ही बेईमान कहा है। पुलिस कहती है-अच्छा, खुद को ज्यादा अक्लमंद समझते हो, क्या हमें नहीं पता कि कौन से देश की सरकार बेईमान है?
आजकल हम ऐसे ही लोकतंत्र (?) में रह रहे है, जहां जन्नत की हकीकत सब जानते हैं मगर अधिकतर लोग ऐसी ही पुलिस बने हैं और समाज के राहत इंदौरियों को कठघरे में खड़ा किए जा रहे हैं। लेकिन कवि और कविता को, भले ही राहत इंदौरी के अंदाज में ही सही, मुखर होना चाहिए। आज ‘वो’ को तुलसी, सूर, मीरा की अपेक्षा कबीर-रैदास की जरूरत है। इन्होंने जो देखा, अनुभव किया उसे निडरता से अभिव्यक्त किया। अगर ये किसी डर से नियंत्रित होते, न तो ये अपने काल के इतिहास का प्रतिनिधित्व कर पाते और न ही इतने प्रासंगिक होते, जितने ये हर परिस्थिति में नजर आते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि कविता साहित्य का अभिन्न अंग है। इसे भी अपने काल के इतिहास की एक सशक्त कड़ी बनना है, इसलिए इसे वर्तमान के प्रति ईमानदार व जवाबदेह होना चाहिए, जैसे माखन लाल चतुर्वेदी की कविता ‘पुष्प की अभिलाषा’ भी अपने समय का सशक्त प्रतिनिधित्व करती है।
जाहिर है यथार्थवादी कविता में यथार्थ होना चाहिए मगर इसका चित्रण प्रभावोत्पादक रीति से होना चाहिए। कुछ कविताएं अखबार की कतरनों तक सिमट कर रह जाती है। उनमें यथार्थ जरूर हो सकता है, मगर प्रभावोत्पादकता के अभाव में उन्हें कविता कहना, कविता के साथ नाइंसाफी होगी। प्रमाण की जरूरत नहीं, आजकल दलित यानी अम्बेडकरवादी कविता की विषयवस्तु ऐसी हो गई कि मराठी के कुछ जिम्मेदार साहित्यकार इसे ‘गाली कविता’ कहने पर मजबूर हैं, यानी इस कविता का ‘वो’ गाली हो गया है। मैं ऐसी कविता को कविता की श्रेणी में रखने का पक्षधर नहीं हूं। अखबार की कतरनों का जबरन अतिशयोक्ति से अलंकरण करना भी इसे कविता नहीं बना सकता। लेकिन आजकल फेसबुक पर ऐसी कविताओं का चलन काफी बढ़ गया है और इसकी तारीफ में वाह! वाह! की बाढ़ बनी रहती है। ऐसी कविता लिखने वालों और तारीफ के पुल बांधने वाले निस्संदेह कविता के भविष्य के लिए खतरा हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है-‘गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। तुकबंदी और अनुप्रास कविता के लिए अपरिहार्य नहीं। किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है...। पद्य के लिए क़ाफ़िए वग़ैरह की ज़रूरत है, कविता के लिए नहीं। कविता के लिए तो ये बातें एक प्रकार से उल्टा हानिकारक हैं।’ वे पद्य और कविता को एक अद्भुत अंदाज में अलग करते हैं। मौजूदा संदर्भ में मुझे देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविता ‘लिफाफा’ की याद ताजा हो आती है, जिसे मुझे उनसे आमने-सामने सुनने का अवसर मिला। यह कुछ इस प्रकार है- ‘पैगाम तुम्हारा और पता उनका; दोनों के बीच फाड़ा मैं ही जाऊंगा।’ निस्संदेह इस कविता के ‘वो’ की प्रभावोत्पादकता गजब की है और अनूठी भी। इसलिए यह कविता आज भी मेरी स्मृति का अटूट हिस्सा बनी हुई है।
मैं इसे एक संस्मरण के माध्यम से कदम आगे बढ़ाकर देखना चाहता हूं। एक छात्र दिल्ली के नेहरू विहार में आईएएस की तैयारी कर रहा था और उसका पिता अपनी जमीन तक बेचकर उसके सपने को साकार करने में जुटा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके पिता का एक पत्र आया, उसमें सिर्फ तीन शब्द लिखे थे-‘और कब तक?’ शब्दों की प्रभावोत्पादकता ऐसी कि इन तीन शब्दों को पढ़कर पुत्र बेचैन हो उठा। उसके पास न कुछ कहने को बचा था और न ही कुछ अधिक सुनने को। इन तीन शब्दों को फैलाने की जरूरत समझें तो तीन लाइनों में तोड़ सकते हैं। क्या इन तीन शब्दों को कविता नहीं कहा जाना चाहिए? बेशक ये तीन शब्द विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविता की तरह मुकम्मल चित्र/ घटना नहीं हैं। अगर आप इन तीन शब्दों के वजूद में आने के पीछे छिपी वजह और कहानी से अवगत हैं तो आप इसे कविता कह सकते हैं। इसे मुकम्मल कविता बनने के इसके पीछे छिपी वजह को कविता का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे में ये तीन शब्द कविता की पंच लाइन ‘वो’ हो सकते हैं, जो कविता की एक महत्वपूर्ण शर्त, प्रभावोत्पादकता पर खरे उतरते हैं। ये मनोरंजन न सही मगर दर्द की पराकाष्ठा का सबब अवश्य बन सकते हैं। द्विवेदी जी के हिसाब से इसे कविता होना चाहिए, आप क्या कहते हैं?