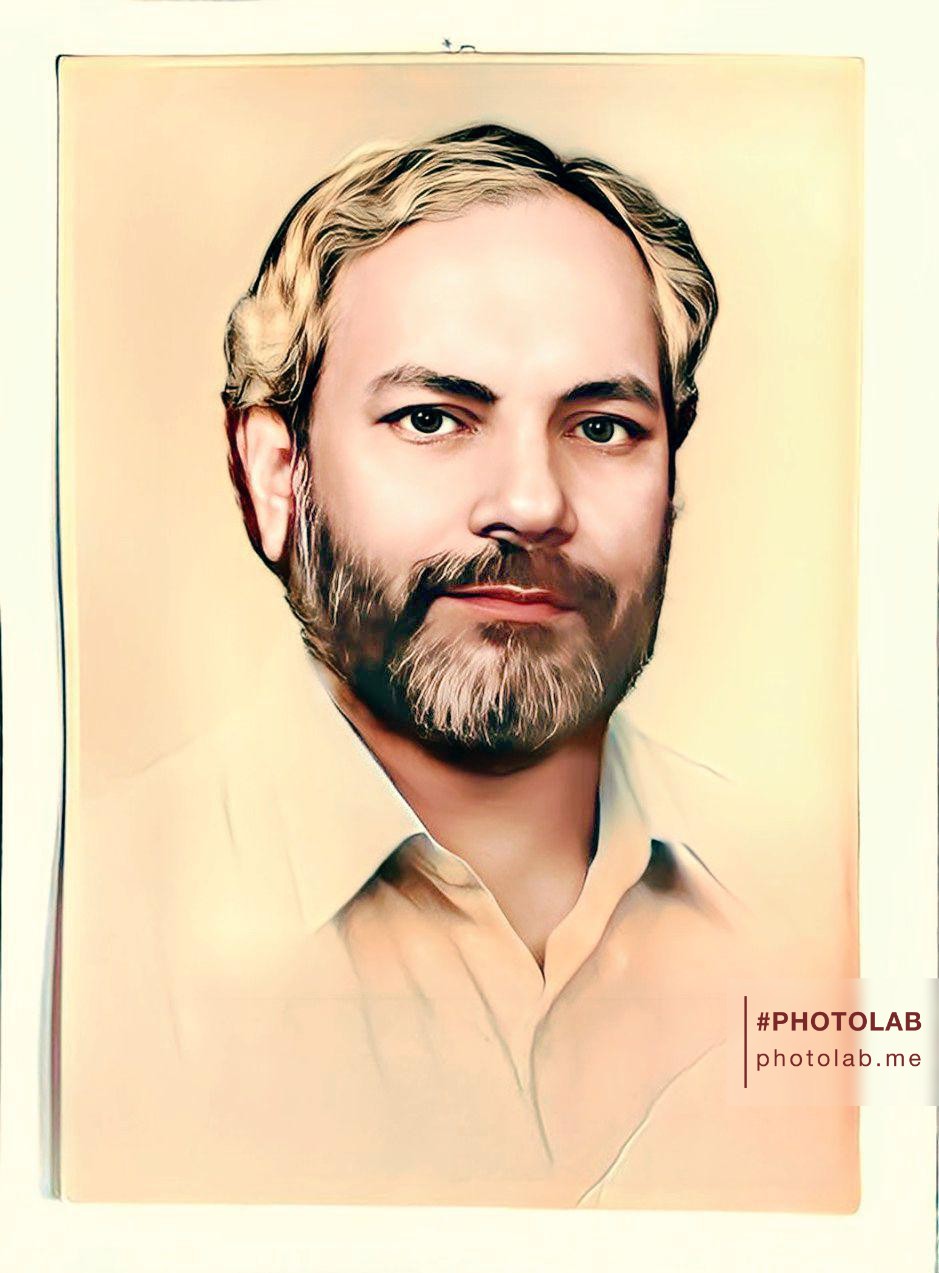तेजपाल सिंह ‘तेज’ (प्रस्तोता) : दोहरी गुलामी के उन्मूलन का विमर्श -ईश कुमार गंगानिया
प्रस्तुति : तेजपाल सिंह ‘तेज’
दोहरी गुलामी के उन्मूलन का विमर्श
-ईश कुमार गंगानिया
अप्रैल 2024 में दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसका विषय था- ‘विमर्शों का वैश्विक परिप्रेक्ष्य: पुनर्विचार की आवश्यकता, कुछ प्रश्न कुछ प्रवृत्तियाँ.’ इसमें प्रो. वीर भारत तलवार, प्रो. आशुतोष कुमार, डॉ. कवितेंद्र इंदु आदि ने प्रमुखता से अपने विचार व्यक्त किए. टीम समय संज्ञान ने महसूस किया कि संपादकीय में इस प्रकार के विषयों पर भी बात होनी चाहिए. विमर्श पर बात करने से पहले मुझे लगा कि उन परिस्थितियों पर थोड़ा ठहर कर बात की जाए, जो प्रतिद्वंद्वी बाइनरी बनाती हैं और विमर्श के लिए ज़मीन तैयार करती हैं. मैं इन परिस्थितियों की तलाश रूसो के सामाजिक संविदा (Social Contract) के पहले वाक्य से करना चाहता हूं. रूसो कहते हैं—‘मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है.’ (Man is born free and everywhere he is in chains.)
ज़ाहिर है, रूसो व्यक्ति की नैसर्गिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति के बहुआयामी विकास, आपसी भाईचारे और अमन-चैन को सुनिश्चित करती है. इस संविदा में व्यक्तियों के समूह की सामान्य इच्छा (General Will) और सामान्य हित (Common Good) संकल्पित हैं. सामान्य इच्छा और सामान्य हित की सामूहिक स्वीकार्यता के चलते संगठित समाज अस्तित्व में आया. राज्य और इसका व्यापक ढाँचा भी इसी संगठित समाज की बुनियाद पर खड़ा है. लोभ, मोह, वासना, अहंकार, श्रेष्ठता जैसी अनेक प्रकार की जंजीरों में कैद व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब इस ढाँचे को चुनौती देता है तो समाज में असंतोष और आपसी टकराव की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं. रूसो जिन ज़जीरों की बात कर रहे हैं, वे अदृश्य हैं मगर क़दम -दर-क़दम गुलामी की अद्भुत नजीर पेश करती हैं. एक बड़ी नजीर यह भी है कि भारतीय समाज ऐसी ही जंजीरों की बदौलत वैचारिकी की नवीनता/आधुनिकता, आविष्कार और वैज्ञानिक टेंपरामेंट के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में पिछड़ा है; मगर व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुश्मन धर्म यानी धर्म के नाम पर धंधा/षडयंत्र, जाति व लिंग आधारित शोषण-उत्पीड़न की रूढि़वादी परंपराओं व रीति-रिवाजों की जंजीरों/गुलामी के मामले में विश्वगुरु है.
रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विस्तृत, परिष्कृत और बखूबी परिभाषित दस्तावेज को स्वतंत्र भारत का संविधान कह सकते हैं. यह संविधान उस प्रारूप समिति की बदौलत अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे. भारतीय संविधान में व्यक्तियों के समूह की सामान्य इच्छा और हितों की सुरक्षा इसकी उद्देशिका में ‘जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा,’ के रूप में सुनिश्चित की गई हैं. लेकिन आज हर गली-कूचे में शोर है कि संविधान की संप्रभुता खतरे में है. कह सकते हैं कि निरंकुशता/कायरता की जंजीरों में कैद कोई भ्रमित व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह समाज व राज्य की स्वतंत्रता और इनके स्वाभाविक सामान्य हितों को चुनौती दे रहा है. कहने की ज़रूरत नहीं, खोखली परंपराओं और रीति-रिवाजों में कैद मुट्ठीभर लोगों का यह कुचक्र नया नहीं है. यह धर्म, जाति, लिंग और न जाने कितने स्तर पर भारतीय अस्मिता को निरंतर खोखला करता रहा है और आज भी कर रहा है. हम इनकी श्रेष्ठता व स्वतंत्रता के भ्रम के इस जश्न को जश्न-ए-गुलामी कह सकते हैं, क्योंकि यह खोखली परंपराओं और रीति-रिवाजों में कैद मुट्ठीभर लोगों की मानसिक विकृति/गुलामी का एक अद्भुत नमूना होकर रह गया है.
श्रेष्ठता का यह भ्रम गुलामी का एक पक्ष है. इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे हम पीडि़त पक्ष कह सकते हैं. महामना जोतिबा फुले अपने ग्रंथ ‘गुलामगिरी’ की प्रस्तावना में पीडि़त पक्ष की गुलामी को होमर के कथन के माध्यम से सूत्रबद्ध करते हैं—‘जिस दिन मनुष्य गुलाम होता है, उस दिन उसकी आधी अच्छाइयाँ छीन ली जाती हैं.’ (The day that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtues.) लेकिन फुले राजनीतिक और सामाजिक गुलामी को अलग-अलग करके देखते हैं और सामाजिक गुलामी को अधिक खतरनाक मानते हुए बताते हैं—‘इस देश में राजनीतिक रूप से हम कई बार गुलाम बने और स्वतंत्र भी हुए. लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर युगों-युगों से चली आ रही सामाजिक गुलामी नष्ट नहीं हुई.’ बाबा साहब डॉ. अंबेडकर इस गुलामी के उन्मूलन का सूत्र देते हैं—गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वह अपनी गुलामी की जंजीरें ख़ुद -ब-ख़ुद तोड़ डालेगा.
बाबा साहब ने पीडि़त पक्ष की गुलामी तोड़ने का सूत्र दिया है. लेकिन बड़ी समस्या पीडि़त पक्ष की गुलामी की जनक दूसरी गुलामी यानी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि की श्रेष्ठता के भ्रम की गुलामी के उन्मूलन की है. गौरतलब है, जिस राजनीतिक गुलामी पर विजय की बात फुले कर रहे हैं, वह विदेशी ताकतों की गुलामी से आजादी का मसला है. इसके विरुद्ध पूरा देश लड़ता है, इसलिए आजादी सुलभ हो जाती है. लेकिन जिस खतरनाक सामाजिक गुलामीकी बात फुले कर रहे हैं, वह अपने देश के तथाकथित धर्म की देन है. इसके उन्मूलन के लिए अलग-अलग समुदाय जैसे दलित, आदिवासी, स्त्री आदि सदियों से अलग-अलग लड़ते आए हैं. इस लड़ाई के विरुद्ध जिस दिन पूरा समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा, इस पर विजय पाना भी आसान हो जाएगा. लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं क्योंकि इस गुलामी से ग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ख़ुद को आजाद, श्रेष्ठ और निरंकुश समझता है. परिणामस्वरूप, वह ख़ुद की अस्मिता को सार्वभौमिक और अन्य की अस्मिता को पारिवेशिक बनाने का षडयंत्र निरंतर करता रहता है.
सरल शब्दों में कहें तो यह अपने कद को बड़ा और प्रतिपक्ष के कद को काट छांटकर छोटा करने का षडयंत्र है. दलित-शोषित, पिछड़ा व आदिवासी समाज यानी पीडि़त पक्ष, जिसमें महिला स्वाभाविक रूप में हर स्तर पर शामिल हैं, इसी षडयंत्र के जीते-जागते उदाहरण हैं. हमें पीडि़त पक्ष की पारिवेशिक कर दी गई सामाजिक अस्मिता को पुनर्स्थापित करने व तथाकथित सार्वभौमिक सामाजिक अस्मिता को भी श्रेष्ठता के भ्रम की गुलामी से मुक्ति के लिए संवाद करना है. मौजूदा कवायद को मैं ‘दोहरी गुलामी के उन्मूलन का विमर्श’ कहना चाहता हूं. इसका मकसद दोनों के बीच की दूरियाँ पाट कर अमन-चैन व आपसी सौहार्द की एक ऐसी बस्ती बसाना है जहाँ दोनों प्रतिद्वंद्वी अस्मिताओं के बीच सहज हुक्का-पानी सुनिश्चित हो सके. ज़ाहिर है, यह नैतिक वैधता के बगैर संभव नहीं है.
हम जानते हैं कि परंपरावादी साहित्य में नैतिक वैधता का अभाव रहा है, इसके चलते इन्होंने हाशियाकृत समाज को अपने समाज और साहित्य की परिधि के करीब फटकने तक नहीं दिया. मौजूदा अमृत काल ने तो जैसे नैतिक वैधता की उम्मीदों के दरवाजे भी लगभग बंद ही कर दिए हैं. प्रो. आशुतोष विमर्श को सार्वजनिक संवाद के रूप में देखते हैं और कवितेन्द्र का कहना है—‘विभिन्न विमर्शों के चलते साहित्य और आलोचना का लोकतंत्रीकरण हुआ है.’ हमें लगता है, यह लोकतंत्रीकरण सिर्फ मंचों पर हुआ है, व्यवहार में होना अभी बाक़ी है. इन विमर्शों के बहाने जो ज्ञान बाँटने की प्रक्रिया व प्रवृत्ति सामने आती है उससे आभास होता है जैसे परंपरावादी/प्रगतिशील साहित्य के कर्णधार इन विमर्शों के बहाने भी अपनी श्रेष्ठता का ही प्रदर्शन करते हैं.
ये हाशियाकृत कर दी गई अस्मिताओं के संघर्ष में अनेक प्रकार की खामियाँ निकालते हैं ताकि हाशियाकृत समाज का चूल्हा-चौका अलग होने के बावजूद भी इनकी वर्चस्ववादी चौधराहट की धमक पीडि़त समाज के दिलो-दिमाग पर बनी रहे. ये संघर्षरत अस्मिता आंदोलन को उन आदर्शों की कसौटी पर परखते हैं जिनका पालन करना इनकी ख़ुद की फितरत में नहीं है. ऐसा नहीं है कि पारिवेशिक कर दी गई अस्मिताओं की पुनर्स्थापना के आंदोलन के तौर-तरीकों में खामियाँ नहीं हैं, अनेक खामियाँ हैं और उन पर बात हो भी रही है. हम यह भी मानते हैं कि इन्हें निरंतर आत्ममंथन, मूल्यांकन और बेशक अन्य विमर्शों के साथ तालमेल, वैचारिक आदान-प्रदान व आपसी सहयोग की निरंतर ज़रूरत है. लेकिन मेरा सवाल है—पीडि़त विमर्श के हमदर्द जब यह जानते हैं कि समाज के बड़े वर्ग के साथ जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर सदियों से अन्याय हुआ है और आज भी हो रहा है, तो इस अन्याय के विरुद्ध साथ खड़े होने से दूर क्यों भागते हैं? इनके विमर्श दूर खड़े होकर ज्ञान बाँटने या हतोत्साहित करने की फतवेबाजी तक सीमित क्यों है?
ये सवाल बेवजह नहीं हैं, इनके पुख्ता आधार की लंबी श्रृंखला है. इसे समझने के लिए हाशियाकृत अस्मिता आंदोलन के सबसे बड़े सिम्पथाइज़र राजेंद्र यादव का उल्लेख करना चाहूंगा. एक तरफ राजेंद्र यादव स्वीकार करते हैं—‘दलित केवल सुविधा से वंचित नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से बराबरी के सम्मान से भी वंचित रहे हैं. वे दलित इसलिए हैं कि हमने उन्हें न ज्ञान दिया, न सम्मान. इससे अधिक अमानवीयता और क्या होगी. हमें ख़ुद को सहनशील बनाते हुए दलित-विमर्श को मुख्य धारा में स्थान देना चाहिए. ऐसा करके हम उन पर कृपा नहीं करेंगे. यदि हमें ख़ुद को बचाना है तो उन्हें साथ लेना होगा.’ लेकिन दूसरी तरफ वे अपनी बात से मुकर जाते हैं और टिप्पणी करते हैं—‘हंस साहित्य हवाई हमला करता है, क़ब्ज़ा करने वाली फ़ौजें क़ब्ज़ा करती हैं, जो ज़मीन पर लड़ती हैं. साहित्य में ज़मीन की फ़ौज ही वह सब करेगी और इस ज़मीनी फ़ौज का नायक आप दलित लेखक होंगे, ग़ैर-दलित लेखक नहीं.’ क्या आपको यादव जी की यह कवायद सवर्ण मानसिकता से ग्रसित व वर्चस्ववादी चौधराहट क़ायम रखने की मुहिम का हिस्सा नहीं लगती? क्या ऐसा ईमानदारी से विमुख विमर्श कोई भेदभाव रहित अमन-चैन की ज़मीन तैयार कर सकता है? क्या आपको नहीं लगता हैं—यादव जी सवर्ण और अवर्ण दोनों नावों में पैर रखकर चलते रहे हैं? ऐसे प्रश्नों पर खुले मन से विचार होना चाहिए, मगर दुखद है कि साहित्य व समाज के लंबरदार ऐसा कुछ करने का साहस नहीं दिखाते.
डॉ. अंबेडकर ऐसे रीढ़-विहीन आचरण को निजद्वैतवाद (fissiparous) की संज्ञा देते हैं. इस कड़ी में महान आलोचक नामवर जी के ख़ुद के दलित होने की परिभाषा को समझते हैं—‘वैसे मैं अपनी गणना दलितों में कर सकता हूं. मेरे गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी दृष्टि में और जैसाकि मैं लिख चुका हूं, काशी के पंडितों के बीच ‘ब्राह्मण समाज में ‘अछूत की तरह बहुत दिनों तक रहे, कुछ उनके कारण, कुछ अपने कर्मों के कारण. मैं भी एक अरसे तक हिन्दी वालों के बीच अछूत ही रहा हूं.’ नामवर जी के इस अछूतपन/दलितपन पर ख़ुद टिप्पणी करने से बेहतर है कि मुद्राराक्षस की टिप्पणी की मदद से इसे समझा जाए—‘राम विलास शर्मा, नामवर सिंह, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र यादव जैसे अनेक लेखक लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने बड़े कष्ट उठाए. दरिद्रता झेली. उनकी दरिद्रता का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि हमने तीन रोज मुर्गा नहीं खाया, दो दिन विलायती शराब नहीं पी, एक जगह से दूसरी जगह पैदल चले. हम दुकान की खिड़की पर खड़े देखते रहे कि एक नई तरह का आवरण आया है जिसे खरीद न सका, पंच सितारा होटल में न जा सका.’
सवाल उठता है—‘क्या हाशियाकृत समाज की पीड़ा इतनी भर है जितनी महान आलोचक नामवर जी बतला रहे हैं?’ दरअसल इस प्रकार के क्रियाकलाप ही मुद्राराक्षस जैसे व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि वे मुखौटों की हक़ीकत को सार्वजनिक करें. चलिए नामवर जी के व्यक्तित्व को थोड़ा और परखते हैं. वे डॉ. धर्मवीर के कबीर पर किए गए काम के संदर्भ में एक टिप्पणी करते हैं—‘मैं धर्मवीर की आलोचना कर ब्राह्मणों को सुख नहीं पहुँचना चाहता.’ नामवर जी स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि वे डॉ. धर्मवीर की आलोचना कर सकते हैं, मगर करना नहीं चाहते. अगर वे ऐसा करते हैं तो यह डॉ. धर्मवीर से भिड़ रहे ब्राह्मणों की मदद होगी और उन्हें सुख पहुँचेगा. ऐसा वे इसलिए कर रहे कि उन्हें ब्राह्मणों से अपना हिसाब चुकता करना है. सुख तो वे डॉ. धर्मवीर को भी नहीं पहुँचना चाहते थे, मगर यह अनायास हो जाता है. ज़ाहिर है, ब्राह्मण साहित्यकारों ने भी नामवर जी को जातिगत आधार पर आघात पहुंचाया होगा तभी वे दो दुश्मनों यानी दलित और ब्राह्मण में से दलित के साथ खड़े होने में सुकून पाते हैं. क्या नामवर जी का यह स्टेटमेंट उनके जातिवादी चरित्र और उनकी सारी प्रगतिशीलता की कलई खोलकर नहीं रख देता?
ऐसा भी नहीं लगता कि नामवर जी दलित की पीड़ा समझते थे. अगर उन्हें दलितों की पीड़ा का एहसास होता तो वे जोतिबा फुले और डॉ. अम्बेडकर को अंग्रेज समर्थक न कहते. दूसरे शब्दों में वे इन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हुए यह संदेश देने का प्रयास नहीं करते कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ़ लड़ता दलित राष्ट्र विरोधी और साम्राज्यवादी ताकतों की ओर देखता है और उनसे संचालित होता है.’ यह घटनाक्रम बताता है कि नामवर जी और इन जैसे महान साहित्यकारों की सारी प्रगतिशीलता जातिवाद से पराजित है. इसने जातिवाद के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया हुआ है. अगर ऐसा न होता तो सदियों से हाशियाकृत समाज की अस्मिता का प्रश्न कभी का हल हो गया होता. लेकिन प्रगतिशीलता के पैरोकारों में इतना साहस नहीं कि इस हक़ीकत को स्वीकार सकें. प्रो. आशुतोष भी प्रगतिशीलता का कुछ ऐसा ही ख्याली पुलाव बनाते हुए कहते हैं—‘हाथ से हाथ जोड़कर ही विमर्श होगा, उसी से बदलाव की संभावनाएं हैं. जहाँ वह खड़ा है और दुनिया देख रहा है, इसमें काफ़ी फासला है. यह फासला मिटा कर ही विमर्श कारगर हो सकता है.’ तथ्यात्मक रूप से हम आशुतोष से सहमत हैं और अंबेडकरवाद इस सार्वभौमिक सत्य से इंकार नहीं करता है. लेकिन सवाल तो बनता है—‘सदियों से सारी बागडोर आशुतोष जैसे ज्ञान बाँटने वाले तथाकथित श्रेष्ठ जनों के हाथ में रही है, इन्हें हाथ से हाथ जोड़कर विमर्श करने से किसने रोका है? ये हाथ से हाथ न जोड़ने का ठीकरा हाशियाकृत समाज के सिर पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? अजीब तर्क है भाई कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और....
अंबेडकरवाद भी इसी सोच का पैरोकार है. कुछ ऐसा तो करो जिसमें कुछ दम हो और भरोसा जगे. अब कवितेन्द्र को ही ले लीजिए वे चिंता जताते हैं—‘आजकल अनुभव के चलते दूसरों से कम्यूनिकेट करने से इंकार करते हैं, यह मात्र एक आधार बन गया है और एकांकी लिखते हैं और इसी के आधार पर बात करते हैं. यह एक अजीब तरह का कैदखाना है.’ निस्संदेह, यह चिंता अंबेडकरवादी लेखन की भी चिंता है, जिसके बैनर तले हर कोई मठाधीश बना बैठा है और मनमर्जी के फतवे जारी कर रहा है. यह संवादहीनता साहित्य के आपसी संबंधों के लिए भी खतरा है. हमारी एप्रोच समावेशी है और अपेक्षा है कि अन्य की एप्रोच ऐसी ही हो. लेकिन अविश्वसनीयता के ऐसे गर्दोगुबार में प्रश्न पैदा होता है—कहीं ये सारी चिंताएं अस्मितावादी विमर्श के विरुद्ध आत्मरक्षा यानी अपनी प्रगतिशीलता के प्रदर्शन की रणनीति तक तो सीमित नहीं? सवाल कड़वा जरूर है मगर क्या करें यह मानसिक विकृति की जंजीरों में कैद भारतीय समाज की देन है और यह विवश करता है कि हर क़दमफूंक-फूंक कर रखा जाए. खैर, यह जो कुछ भी है, दोनों पक्ष से अतिरिक्त धैर्य, भरोसे और स्वानुभूति की माँग करता है.
दयाल सिंह कॉलेज के कार्यक्रम में प्रो. आशुतोष सवाल उठाते हैं—‘हिन्दी में विमर्श ठहरे हुए क्यों लगते हैं? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इसकी वजह विमर्श के कैनवास का संकीर्ण व संकुचित होना है, जो पूरे समाज का नहीं, मुट्ठीभर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें स्वानुभूति जैसे तत्वों का अभाव है, जो अविश्वसनीयता की जननी है. इस अविश्वसनीयता को डर भी कह सकते हैं, जो मोहनदास नैमिशराय की प्रतिक्रिया में झलकता है—‘गै़र-दलित साहित्य में घुसपैठ करते हैं और आगे चलकर दिक्कत करते हैं. दिक्कत तब बढ़ जाती है जब ये दलित साहित्य की परिभाषा करने लग जाते हैं और आगे बढ़कर यह भी दुस्साहस करते हैं—‘दलितों ऐसे लिखो, वैसे लिखो.’ यह संकट कब्जे़ का संकट है. पहले भी साहित्य और समाज दोनों ही जातीय वर्चस्व के कैदी रहे हैं और आज भी इससे मुक्त नहीं हैं. अब अंबेडकरवादियों ने जब अपना घर अपने दम पर बनाया है तो उनका डर है—कहीं जातीय दबंगई व षडयंत्र फिर से उनके खून-पसीने से बनाए घर पर भी कब्जा न कर लें और ये फिर से बेघर न हो जाएं? सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो मुद्राराक्षस बताते हैं—‘भारतेन्दुहरिश्चन्द्र से लेकर आज तक किसी सवर्ण लेखक ने ख़ुद को दलित लेखक नहीं कहा. आज भी श्रीलाल शुक्ल या किसी अन्य सवर्ण लेखक की हिम्मत नहीं है कि वे दलित सवालों का सामना कर सकें. अगर कोई सवर्ण लेखक दलितों के बारे में लिख रहा है तो वह दलित राजनीति की सत्ता में अपनी जगह बनाना चाहता है.’
हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि कोई सवर्ण अपने को दलित लेखक कहने का साहस दिखाए. मगर हां, हमारा इतना आग्रह ज़रूर है कोई भी लेखक सवर्ण होने की ताल भी ठोकने की जरूरत महसूस न करे. प्रगतिशीलता के मुखौटे में भी सवर्णवाद कतई सामने नहीं आना चाहिए. एक लेखक का परिचय लेखक के रूप में होना चाहिए, न कि किसी भी वर्ण या जाति के रूप में. परेशानी यही है कि राजेंद्र यादव भले ही ओबीसी समाज से थे, मगर सवर्ण मानसिकता के विकार से मुक्त नहीं थे. इसी के चलते वे अपने को सवर्णों के साथ जोड़ कर ‘हम’ और अस्मिता संघर्ष के पैरोकारों को ‘वो’ के खांचे में रखकर बात करते रहे हैं. इसलिए विमर्श अभी तक कोई सम्मानजनक मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं. इस कड़ी में पुन: कवितेन्द्र की एक अन्य चिंता पर लौटते हैं—‘हमारा कैनवास ग्लोबल व सार्वभौमिक स्वीकार्यता से परिपूर्ण होना चाहिए. दलित व स्त्री विमर्श के बंद बक्से की तरह नहीं. विभिन्न विमर्शों को मिलाकर निष्कर्ष निकाले जाने की ज़रूरत है.’
कवितेन्द्र की चिंता जायज़ है और अंबेडकरवाद भी इसका पक्षधर है. इसी के चलते डॉ. अंबेडकर ने जातियों और धर्मों की जंजीरों में कैद भारतीय विद्वानों (जो कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं बाद में कुछ और; इस ‘कुछ और’ का संबंध धर्म और जातियों के लबादे से है, जिसके बगैर ये ख़ुद को निर्वस्त्र जैसा कुछ समझते दिखते हैं) को भारतीयता का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि हम पहले भी भारतीय हो, बाद में भी भारतीय और भारतीय के अतिरिक्त कुछ और न हों. हमारा प्रश्न है—‘क्या आज भी भारतीयता हमारी प्राथमिकता बन पाई है? कवितेन्द्र को यह भी बताना चाहिए—आज समाज और राजनीति में कितनी भारतीयता बची है? उन्हें यह भी बताना चाहिए आज साहित्य और समाज में कितने ऐसे मूल्य बचे हैं जो सार्वभौमिकता को सींचने का काम करते हैं? जिन बक्सों की बात कवितेन्द्र कर रहे हैं, उन्हें इस पर भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि इन बक्सों के अस्तित्व में आने के लिए जिम्मेदार कौन हैं? हमें लगता है कि उन्हें पहले अपने हिस्से की जि़म्मेदारी का परिचय देना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर सार्वभौमिकता की इमारत बुलंद हो सके.
बाबा साहब से पहले भी जोतिबा फुले ने बाबा साहब से एक क़दम आगे बढ़कर थॉमस पेन के संकल्प—‘विश्व ही मेरा देश है, सभी का कल्याण करना मेरा धर्म है.’ से प्रेरित होकर ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ यानी विश्व परिवारवाद का घोषणा पत्र जारी कर विश्व स्तर पर मानवता यानी समता, स्वतंत्रता व बंधुता की स्थापना का संकल्प लिया और सत्यशोधक समाज के निर्माण की मुहिम चलाई. लेकिन भारतीय समाज में गु़लामी की मजबूत ज़ंजीरों के चलते परिणाम क्या, वही ढाक के तीन पात. हम कवितेन्द्र की चिंता से सहमत हैं—‘विमर्शों ने अपने-अपने दायरे बना लिए हैं, सीमा बना ली है. जैसे अनुभववाद के चलते जो देखा, भोगा, वही सही है, यह सामान्यीकरण का कमजोर तर्क है. इसका मतलब दूसरे के अनुभवों से वंचित हो जाना है. दूसरों के अनुभव भी विमर्श में शामिल किए जाने की जरूरत है, समग्रता में देखने की जरूरत है. यह मसला इससे भी जुड़ा है कि ‘दलित साहित्य कौन लिख सकता है’, को भी रीडिफाइन करने की जरूरत है.’
जहाँ तक अनुभववाद के चलते जो देखा, भोगा, वही सही, का जो मसला है, वह जातिवादी जंजीरों में कैद परंपरावादी साहित्यकारों के विरुद्ध आक्रोश की अभिव्यक्ति है. लेकिन दीगर हक़ीकत यह भी है कि यह आक्रोश की अभिव्यक्ति भी ग़ुलामी की ज़ंजीरों से मुक्त नहीं है. दरअसल, सदियों से चले आ रही उपेक्षा और शोषण-उत्पीड़न की आंधी ने अस्मितावादी आंदोलनकारियों की आंखों को भी धूल से पाट दिया है. ये अपनी बनाई घास-फूंस की झोपड़ी में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से आशंकित हैं, डरते हैं. यह नए प्रकार के अछूतपन की पहल जैसा कुछ है. मुझे लगता है देवेन्द्र दीपक इसे समझने में हमारी मदद कर सकते हैं—‘अस्पृश्यता एक अंधा कुआँ है. कुएँ में गिरे व्यक्ति को लेकर चिंता के दो स्तर हैं. एक-चिंता उस व्यक्ति की चिंता है जो कुएँ में गिरा हुआ है और कुएँ के बाहर निकलने की कोशिश में हलकान और लहूलुहान हो रहा है. दूसरी चिंता उस व्यक्ति की है जो कुएँ की जगत पर खड़ा होकर कुएँ में गिरे व्यक्ति को बचाने की गुहार लगा रहा है. कुएँ में गिरा व्यक्ति अछूत है और कुएँ की जगत पर खड़ा व्यक्ति सवर्ण है. अछूत की चिंता आहत की चिंता है, सवर्ण की चिंता सदाशयी की चिंता है. यक़ीनन दोनों चिंताओं के आयाम भिन्न हैं.’ अनुभववाद पर उंगली उठाने वालों को पहले सदाशयी की चिंता के फलक को बड़ा करने और थोड़ा ईमानदार होने की जरूरत है तभी वे आहत की चिंता को समझ सकते हैं. इस समझ के चलते दो प्रतिद्वंद्वी अस्मिताओं के घर्षण से राहत की संभावनाएं प्रबल होंगी, वरना...
यह सदाशयी की चिंता है कि राजेंद्र यादव पीडि़त अस्मिता के समर्थन में परंपरागत साहित्य पर सवाल उठाते हैं—‘पहले एक ख़ास किस्म का, शास्त्रीय किस्म का साहित्य था, जो आज भी विश्वविद्यालयों में होता है, वह अतीत की तरफ देखता था, जिसका समाज सुनिश्चित था, वह स्थिर व गतिहीन साहित्य था, वह अपने ही बनाए पाठों से बाहर नहीं देखता था.’...‘अगर साहित्य को समझना है तो उन शक्तियों को समझना होगा जो हाशियाकृत हैं, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिन्हें महान साहित्य व रचनाओं में अनदेखा कर दिया गया. जैसे कि दलित का सवाल है, स्त्री मुक्ति का सवाल है, अल्पसंख्यकों का सवाल है.’ इतना ही नहीं दलित आत्मकथाओं के समर्थन में तो यादव जी हद से गुज़र जाते हैं, जब वे कहते हैं—‘दलित आत्मकथाओं के पढ़ने के बाद मुझे तथाकथित सवर्णों द्वारा लिखे साहित्य को पढ़ने का मन ही नहीं करता.’ यादव जी की सदाशयता के पोषक उपरोक्त कथन निस्संदेह स्वागत योग्य हैं. इसी के चलते यादव जी के योगदान को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है.
लेकिन जब हम उनकी इस सदाशयता को उनके यथार्थ, और उनके व्यवहार के धरातल पर उतरकर देखते हैं तो उनकी सदाशयता खोखलेपन की ज़ंजीरों में कैद नज़र आती है. जब यादव जी से पूछा जाता है—‘यादव जी, आपने किसी दलित को अपनी किसी कहानी का पात्र बनाया? इसके जवाब में यादव जी कहते हैं, ‘जिन क्षेत्रों में मेरा अनुभव नहीं है, कहानी में मैंने उधर जाने की कोशिश नहीं की. मेरा संपर्क गाँवों से किताबों के माध्यम से ज्यादा है, वहाँ की जिन्दगी को वहीं जाकर अनुभव का नहीं है. इसके लिए मैंने कोई कहानी गांव पर नहीं लिखी, कोई कहानी दलित पर नहीं लिखी, मुसलमान की जिन्दगी पर नहीं लिखी. मुसलमान एकाध पात्र आ गया हो, अलग बात है. स्त्रियों पर लिखी हैं क्योंकि वे हमारा हिस्सा हैं.’ हिंदी जगत की सबसे लोकप्रिय पत्रिका ‘हंस’ के संपादक की सदाशयता ग़ज़ब की है.
हमें लगता है कि यादव जी को यह भी बताना चाहिए था कि स्त्री उनका हिस्सा कैसे हैं? क्या वे स्त्रियों के किसी महाविद्यालय के बड़े आचार्य रहे हैं या किसी महिला आश्रम के संचालक, जिसके कारण स्त्री उनका हिस्सा हो गई. क्या राजेंद्र यादव ने स्त्रियों को अपना हिस्सा इसलिए बनाया कि वे बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर अपनी भाषा व बौद्धिक श्रेष्ठता का परिचय देते हुए कह सकें—‘धर्म की दिग्विजय का झंडा औरत की योनि में गाड़ा जाता है?’ काश! दलित, मुसलमान आदि यादव जी के जीवन का हिस्सा हो पाते. ऐसे सवाल कवितेन्द्र सरीखे अन्य विद्वानों से भी पूछे जाने चाहिए और उन्हें उसी सदाशयता से इन सवालों के जवाब भी देना चाहिए. कवितेन्द्र को स्पष्ट करना चाहिए—‘क्या उनकी सदाशयता यादव जी जैसी ज़ंजीरों में कैद है या उनके अनुभव कुछ अलग हैं यानी ज़ंजीरों से मुक्त?
राजेंद्र यादव की उपरोक्त टिप्पणी से सवाल पैदा होता है—‘क्या राजेंद्र यादव अंबेडकरवादी साहित्य को समुदाय विशेष तक सीमित कर देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो डॉ. अंबेडकर की भारतीयता की, और फुले की विश्व परिवारवाद की अवधारणा के साथ-साथ कवितेन्द्र की अनुभववाद और दलित साहित्य कौन लिख सकता है, की रीडिफाइन करने की माँग स्वत: ख़ारिज हो जाती है. लेकिन अंबेडकरवादी साहित्य इसे ख़ारिज होने देने का पक्षधर नहीं है, भले ही राजेंद्र यादव हमें ‘उद्भावना’ के संपादक से साक्षात्कार में आरोपों से लादते हुए कहें—‘दलित अपनी समस्याएं अपने-अपने ढंग से ख़ुद ही हल कर रहे हैं. जैसाकि मैंने पहले कहा कि उनके यहाँ एक विचारहीनता है, इसलिए उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लड़ाया जा सकता है, और इस्तेमाल किया जा सकता है.’
हमें नहीं मालूम कि राजेंद्र यादव ने किस मनस्थिति में दलितों में विचारहीनता, बिकाऊपन, अवसरवादी व इस्तेमाल की सामग्री कहा है, लेकिन अंबेडकरवादियों को इन आरोपों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और यह उनके गंभीर आत्ममंथन की विषयवस्तु होनी चाहिए; न कि इसे आरोप-प्रत्यारोप की सामग्री बना, अपनी ऊर्जा जाया करने की. सदाशयता की जंजीरों को समझने के लिए मैनेजर पांडेय को चर्चा में लाना ज़रूरी महसूस हो रहा है. वे दलित साहित्य के संबंध में टिप्पणी करते हैं—‘मैंने दलित साहित्य के उभार और आगमन का स्वागत तथा समर्थन बुनियादी तौर पर मार्क्सवादी दृष्टि के तहत किया था.’ संभवत: मार्क्सवाद उनके प्रगतिशील होने की दृष्टि है. जब वे हिन्दूवादी दृष्टि के प्रभाव में होते हैं तो धर्म परिवर्तन के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं-‘मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि अम्बेडकर के आखिरी दिनों की राजनीति की निराशा का परिणाम था उनका बौद्ध-धर्म ग्रहण करना.’…वे अम्बेडकरवादी साहित्य के अलग अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं और टिप्पणी करते हैं—‘यह ठीक है कि दलितों का रचनात्मक उद्देश्य अलग है और इसका स्वरूप भी प्रचलित साहित्य से अलग है. इसलिए उसके अस्तित्व की बात समझ आती है, लेकिन पूरे साहित्य का वह हिस्सा है.’ इसी दृष्टि के तहत वे इसे पूरे साहित्य का हिस्सा बनाने की वकालत करते हैं, लेकिन इन्हें अपने साहित्य में जगह देने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाते, क्या चलाते हैं?
पुन: जब मैनेजर पांडेय मार्क्सवादी होते हैं तो टिप्पणी करते हैं—‘अब लगता है कि आने वाले समय में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व अगर दलित साहित्य करने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.’ हमें नहीं मालूम पांडेय की कितनी दृष्टियां हैं और कौन-सी दृष्टि उनकी वास्तविक है. कहीं मैने