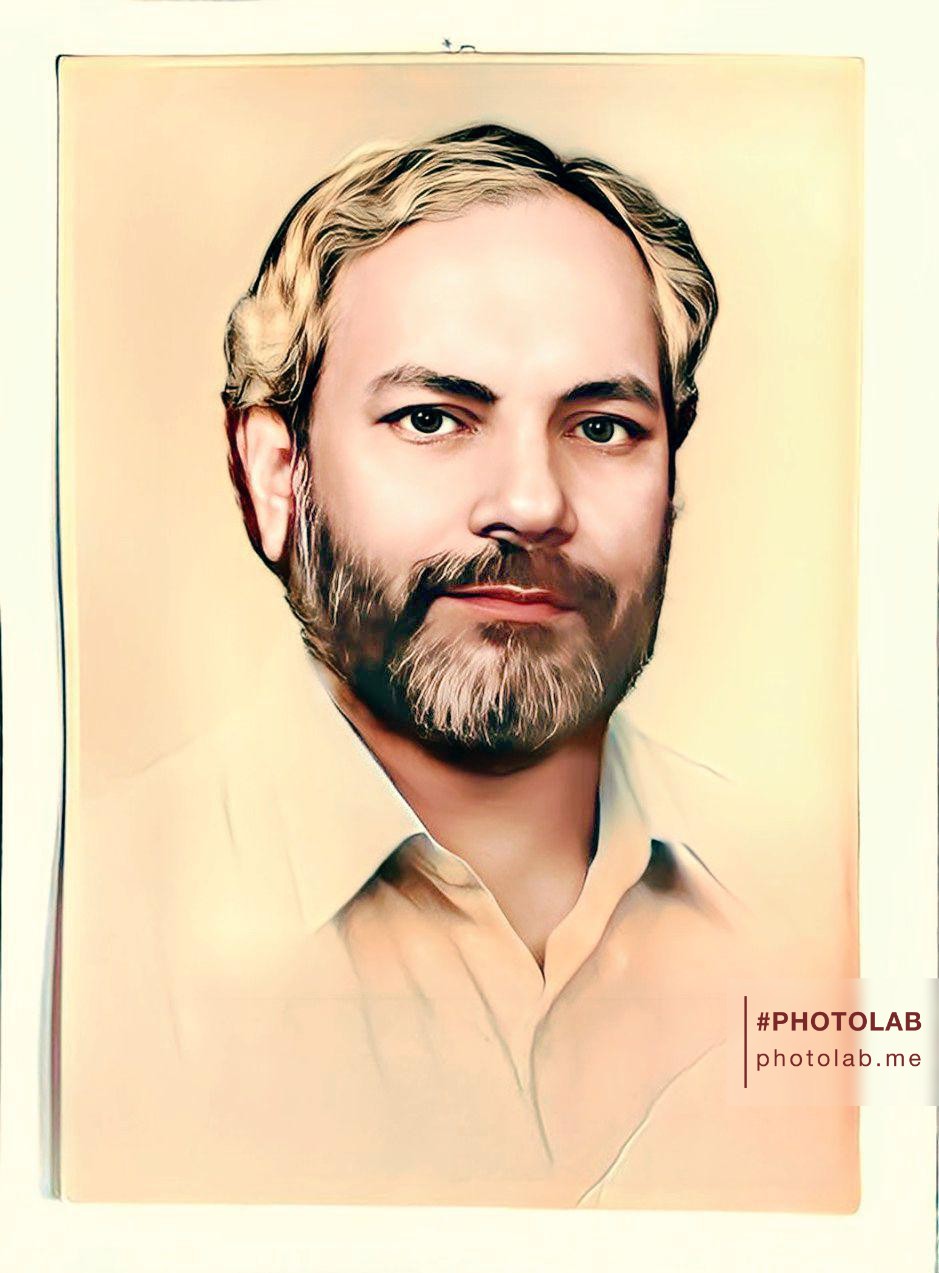तेजपाल सिंह 'तेज' (प्रस्तोता) : भारतीय ज्ञान परंपरा और आजीवक संस्कृति - ईश कुमार गंगानिया
प्रस्तुति - तेजपाल सिंह 'तेज'
भारतीय ज्ञान परंपरा और आजीवक संस्कृति
- ईश कुमार गंगानिया
भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा तात्पर्य उस ज्ञान-विज्ञान की परंपरा से है जो प्राचीन काल से शुरु होती है और वर्तमान से होते हुए भविष्य की ओर सतत अग्रसर रहती है। इस परंपरा के अनुसरण के दौरान हम लौकिक, अलौकिक, धर्म-कर्म, भोग-उपभोग, त्याग-तपस्या, जीवन-मृत्यु आदि से जुड़े अनेक अध्ययनों के साथ-साथ विभिन्न संस्कृतियों के रूबरू होते हैं। ऐसा प्रचलित है कि ज्ञान परंपरा की यात्रा प्राचीन काल में मौजूद ऋषि और गुरुकुल से शुरु होती है; यह तक्षशिला, नालंदा, विक्रम शिला, उज्जयिनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा और शोध के प्रमुख केंद्रों से होते हुए आधुनिक विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के माध्यम से निर्बाध रूप से जारी है। ज्ञान के संवर्धन की इस परंपरा में देश-विदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाएं सदैव गौण रहती हैं; और ज्ञान परंपरा का कारवां ज्ञान के आपसी आदान-प्रदान के साथ निरंतर चलता रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के ‘भाषा शिक्षा विभाग’ द्वारा आयोजित वर्तमान संगोष्ठी ‘भारतीय ज्ञान परंपरा का सातत्य’ भी इसी परंपरा का स्वाभाविक अंग है।
मुझे ‘भारतीय ज्ञान परंपरा में आजीवक संस्कृति’ पर बात करना है, जिसका किसी ऋषि या गुरुकुल परंपरा से कोई वास्ता नजर नहीं आता। यह कार्य एक अंधेरी कोठरी (अंधेरी कोठरी ही नहीं, बल्कि एक अंधकारयुक्त जंगल) में काली बिल्ली की तलाश करने जैसा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आजीवक से संबंधित कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो कुछ भी इस संस्कृति के विषय में उपलब्ध है, वह बेहद भ्रामक, छितराई व विरोधाभासी है। दूसरे, हम पाते हैं कि यह सारी जानकारी इस संस्कृति को नष्ट करने और इसे बदनाम करने वालों के साहित्य में उपलब्ध है, जो इस स्थिति को करेला और ऊपर से नीम चढ़ा जैसा बनाती है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का वह काला अध्याय है, जिसमें ज्ञान की एक परंपरा ने, ज्ञान की एक दूसरी यानी चार्वाक/लोकायत/आजीवक परंपरा का नामोनिशान मिटाने में मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। कहने की जरूरत नहीं कि नामोनिशान मिटाने की यह परंपरा आज भी जारी है।
इसके विपरीत एकलव्य का अंगूठा न रहने का यह अर्थ नहीं निकाल लिया जाना चाहिए कि एकलव्यों ने अपने आपको तीरंदाजी यानी ज्ञान की परंपरा से डिसोन कर लिया है। आज ये हाथ से ही नहीं, बल्कि मुंह और पैरों से भी तीरंदाजी करने की क्षमता रखते हैं। आजीवक को लेकर मौजूदा कवायद यही है कि हमें विरोधियों के साहित्य में उपलब्ध छिन्न–भिन्न कर दिए गए बेहद सीमित यानी ना के बराबर अवशेषों की मदद से इस संस्कृति को पुन: अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमारे लिए यह किसी प्रतिद्वंद्विता या प्रतिशोध का विषय नहीं है, बल्कि पतन की दिशा में अग्रसर वर्तमान समाज को इस पतन से रोकना है। यह किसी से छिपा नहीं हैं कि प्राचीन काल में आजीवक संस्कृति के विलुप्तिकरण के पीछे जो तथाकथित धार्मिक व राजनीतिक ताकतें मौजूद थीं, कमोबेश उसी मानसिकता की पोषक ताकतें आज भी सक्रिय हैं; और समाज को भ्रमजाल में फंसाकर, अपने संकीर्ण हितों को साधने के लिए समाज का दोहन कर रही हैं। मानवता को खंडित करने वाला यह अपराध किसी देशद्रोह से कम बड़ा अपराध है। इस आलेख का मकसद समाज को आजीवक संस्कृति से रूबरू कराना है; एक बेहतर नागरिक और बेहतर समाज के निर्माण की प्रक्रिया में सार्वभौमिक वैज्ञानिकता, व्यवहारिकता और नैतिकता को सुनिश्चित करना है।
आजीवक संस्कृति को समझने से पहले ‘आजीवक’ और इसके चार्वाक यानी लोकायत दर्शन से संबंध को समझना जरूरी है। आनंद झा के अनुसार—‘चार्वाक’ यही एक ऐसा नाम है जो कि सर्वथा ‘अनुच्छिष्ट’ (शुद्ध, जिसमें मिलावट नहीं) है। सर्वथा अनुच्छिष्ट कहने से तात्पर्य यह है कि न यह किसी का उच्छिष्ट (जूठन) है और न इसका कोई लोक प्रस्तुति के कारण ‘लोकायत’, कहलाने वाले दर्शन के सर्वप्रथम आचार्य का नाम इतना अप्रसिद्ध हो, यह कम आश्चर्य की बात नहीं।’1 आनंद झा ने यह बात चार्वाक दर्शन के विलुप्तिकरण की नाकाम साजिशों को बेनकाब करने की गरज से कही लगती है। इस एक टिप्पणी से कई बातें स्पष्ट होती हैं, एक- यह दर्शन ‘प्राचीन’ है, दो- ‘मौलिक’ है और तीन-यही ‘लोकायत’ दर्शन है।
इस कड़ी में अगला प्रश्न है-‘आजीवक’ कौन? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में पुन: आनंद झा से रूबरू होना हमारी जरूरत है; बाध्यता है। इसके अनुसार-‘लोकायत-सिद्धान्त अनुगामी जन ही ‘आजीवक’ नाम से इसलिए अभिहित होते थे कि शरीरात्मवादी होने के कारण शरीर के सदुपयोगार्थ, उसकी रक्षा के लिए आजीवक को, अर्थात श्रमात्मक आजीविका को, वे मुख्य कर्तव्य के रूप में अपनाते थे। एतदतिरिक्त यह भी कारण था आजीवक नाम से उनके पुकारे जाने का, कि वे श्रमोपयोगी स्वास्थ्य के लिए सदा सचेष्ट रहते थे। क्योंकि आजीवक का दूसरा अर्थ, पूर्ण रूप से जीवन का, अर्थात स्वास्थ्य जीवन का संपादन भी होता है। शरीर को आत्मा मानने वाले अपने स्वास्थ्य-स्वरूप जीवन के संपादन में सर्वथा सचेष्ट हों, यह सर्वथा युक्तिसंगत ही है। इन सारी बातों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दर्शन जन-जीवन से घनिष्ठता रखने वाले कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि, राजनीति-स्वरूप दण्डनीति और स्वास्थ्यप्रद आयुर्वेद इन तीनों से पूर्ण रूप से सम्बद्ध था।’2
जहां तक इसकी उपयोगिता का प्रश्न है, कहने की जरूरत नहीं कि जो इस दर्शन में मौजूद है, वह अपने प्राचीन काल का ही नहीं, बल्कि वर्तमान का बेहतर प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। अगर इसे शिक्षा जगत की वर्तमान चर्चित शख्सियतों में से एक डा. विकास दिव्यकीर्ति के शब्दों में समझें तो हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है, वह उल्लेखनीय है-‘अगर चार्वाक ग्रंथों को जलाया नहीं गया होता तो दुनिया में सबसे अधिक वैज्ञानिक भारत में होते, क्योंकि वे तर्कवादी थे। अगर चार्वाक दर्शन को बचाया गया होता तो यूनिवर्सिटी के हर विभागाध्यक्ष के नाम के सामने चार्वाक लिखा होता।’3जाहिर है कि यह चिंतन-दर्शन तर्क-विवेक और वैज्ञानिकता पर आधारित था। निस्संदेह, यह प्रकृति के नियम, न्याय व नैतिकता की सार्वभौमिकता पर आधारित था। लेकिन यह भी जग जाहिर है कि ‘आजीवक संस्कृति’ के पोषक साहित्य को जलाया गया है, नष्ट किया गया है।
यहाँ प्रश्न उठता है, इस संस्कृति और इससे जुड़े चिंतन-दर्शन को नष्ट करने वाले कौन थे? डा. एल. डी. बार्नेटके अनुसार-इस अपरिष्कृत पंथ से असहमति सबसे पहले उपनिषदों में दिखाई दी, जिसमें कुछ उदारवादी ब्राह्मणों ने, शायद कुछ सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा समर्थित, एक प्राथमिक अद्वैतवादी आदर्शवाद की अटकलों को आगे बढ़ाया, जबकि वेदवाद के किले को अज्ञानी लोगों के उपयोग के लिए बरकरार रखा। लेकिन इस समय के आसपास ब्राह्मणवादी कर्मकांड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, और दूर-दूर तक फैल गया, जिससे कुछ ब्राह्मण खुद भी प्रभावित हुए; अब तक, ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद की बुनियाद को पूरी तरह से नकार दिया गया था, और जो लोग नए और सच्चे सिद्धांत का दावा करते थे, उनके प्रचारक कई तरफ से उठ खड़े हुए। इस क्रांतिकारी आंदोलन ने कई चरण धारण किए। कुछ हलकों में, ब्राह्मणवादी और गैर-ब्राह्मणवादी, यह चार्वाक के नाम से जुड़े एक मोटे नास्तिक भौतिकवाद के रूप में सामने आया।’4
बार्नेट की उपरोक्त टिप्पणी स्पष्ट संकेत देती है कि सबसे पहले आजीवकों का विरोध उपनिषदों में मिलता है जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड और इसके रूढ़िवाद लिए खतरा बनता है। यह क्रांतिकारी आंदोलन कई चरणों में हुआ और चार्वाक के नाम से जुड़े एक मोटे नास्तिक भौतिकवाद के रूप में सामने आया। गौरतलब है, चार्वाक अपने समय का इकलौता नास्तिक धर्म-दर्शन था; और नास्तिकता का पैमाना वेदों, जिसे बार्नेट के अनुसार ‘अज्ञानी लोगों के उपयोग के लिए बरकरार रखा’, को न मानना और वेदों की निंदा करना था। यदि यह कहा जाए कि चार्वाक यानी आजीवक का विरोध उपनिषदों से भी पहले का है तो इसे गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस कड़ी में ए. एल. बाशम आजीवकवाद के उदय पर और रोशनी डालते प्रतीत होते है, जब वे कहते हैं–‘प्राचीन भारत में दार्शनिक चिंतन की सीमा हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे थी, और यहां तक कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महान विधर्मी संप्रदायों द्वारा निर्धारित सीमाओं से भी परे थी। पूर्ण भौतिकवादी समूहों, चार्वाक या लोकायत की उपस्थिति, जो आत्मा, देवताओं और भविष्य के जीवन के अस्तित्व को नकारते थे, बहुत प्रसिद्ध है।’5स्पष्ट है कि आजीवकवाद का हिंदू धर्म से टकराव बुद्ध और महावीर से भी पुराना है। मौजूदा संदर्भ में इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैन, बौद्ध और आजीवक संप्रदाय का उदय हिंदू धर्म के विरोध में हुआ था। बहुत संभव है कि यह पुराना टकराव आजीवकवाद की अपेक्षा चार्वाक/लोकायत नाम से मौजूद रहा हो।
बाशम आगे बताते हैं-‘ऐसे कई शिक्षकों (जो हिंदूवाद के प्रतिरोध में थे) ने अनुयायियों के समूहों को इकट्ठा किया और संघों की स्थापना की, शायद कुछ मामलों में एक दूसरे से शिथिल रूप से जुड़े हुए थे; और इनमें से कुछ से आजीवकवाद विकसित हुआ…जो अपने संस्थापक की मृत्यु के लगभग दो हजार वर्षों तक जीवित रहा।’6 इस टिप्पणी से साफ है कि पहले समूहों और संघों (जो आपस में थोड़ा कम सक्रिय रूप से जड़े थे) की तुलना में मक्खलि गोसाल के नेतृत्व में उनका संघ अपनी गतिविधियों के कारण काफी सक्रिय हो गया हो, जिसके चलते ‘आजीवक’ और ‘आजीवकवाद’ जैसे पद चर्चा के केंद्र आ गए। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आजीवकवाद की शुरुआत या आजीवकवाद के जनक मक्खलि गोसाल हैं, जो महावीर और बुद्ध के लगभग समकालीन (छठी सदी ई.पू.) हैं। इस संबंध में विकास दिव्यकीर्ति की टिप्पणी-श्रमण यानी सीकर्स, जो वेदों से असंतुष्ट थे (यानी वेदों की आलोचना करते थे) , उनकी संस्थाओं (आंदोलनकारी) की संख्या 63 थी।7काबिल-ए- गौर है।
बहुत संभव है कि गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बनाना यानी लोकायत/चार्वाक को आजीवक से अलगाना, उसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिस साजिश के तहत इस संस्कृति के साहित्य को प्रक्षिप्त किया गया, जलाया गया और अंतत: विलुप्त करने का प्रयास किया गया। ऐसा भी नहीं है कि यह प्रक्षिप्तिकरण प्राचीन काल तक सीमित था। कबीर-रैदास के साथ भी अनेक प्रकार के किस्से कहानियां इसी प्रकार के प्रक्षिप्तिकरण का परिणाम हैं। आज पाठ्यक्रमों में अनेक प्रकार के बदलाव, नेताओं के भाषणों में इतिहास के संबंध में ऊल-जुलूल, शरारतपूर्ण व गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी भी इसी श्रेणी में आते हैं। शहरों और सड़कों के नाम बदलना आदि भी कमोबेश इसी प्रक्षिप्तिकरण का हिस्सा हैं। विश्वसनीयता की परख के लिए पुन: बाशम की पुस्तक में उपलब्ध टिप्पणी काबिल-ए-गौर है-‘धार्मिक सुधारक शायद ही कभी किसी पुराने विश्वास के आधार के बिना अपने नए विश्वास के केंद्रीय सिद्धांतों को तैयार करता है, जिस पर निर्माण किया जा सके; इसके बजाय वह पहले की शिक्षाओं को दोहराता है, संशोधित करता है, या उन पर नया प्रकाश डालता है, और यह दोहराना उसके समकालीनों के लिए एक नए रहस्योद्घाटन की ताकत और नवीनता है।’8 कहा जा सकता है कि चार्वाक और हिंदू धर्म के आपसी संघर्ष के परिणामस्वरूप ही बुद्ध का धम्म और महावीर का जैन धर्म अस्तित्व में आया। इन्होंने अपने-अपने धर्म-दर्शन की बुनियाद एकदम नए सिरे से नहीं रखी। धर्म के संबंध जो आपसी टकराव की परिस्थितियां थी, उन्हीं को संशोधित कर नए धर्म की स्थापना की। इन दोनों धर्मों के संस्थापकों द्वारा चार्वाक/आजीवक का विरोध और प्रतिद्वंद्विता इसी का परिणाम हो सकता है। विकास दिव्यकीर्ति इस हकीकत को पुख्ता करते नजर आते हैं, जब वे टिप्पणी करते है-‘बौद्ध, महावीर और अद्वैत सभी चार्वाक निंदक थे। कहावत है कि हम अपने मामले में अच्छे वकील और दूसरों के मामलों में अच्छे जज होते हैं।’9 मौजूदा संदर्भ में हिंदुत्ववादियों की तरह बौद्ध और जैन भी अपने मामले में अच्छे वकील और आजीवकों के मामले में अच्छे जज बने बैठे हैं। ये दिल खोलकर आजीवकों की आलोचना/निंदा करने में एक दूसरे से पीछे नहीं हैं।
हम जानते हैं कि मौजूदा विवाद का कोई अंत नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हम यह भी अच्छे से जानते है कि भौतिकवादी दार्शनिकों यानी आजीवकों का जिन आर्यों के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन था, वे तो आज भी अपने वेदों, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म आदि अवधारणाओं और मान्यताओं के साथ के साथ हिंदू, हिंदुत्व, सनातनी और न जाने कितनी प्रकार की जातिवादी व वर्चस्ववादी पहचान के साथ मौजूद हैं। लेकिन दीगर सवाल है-चार्वाक/लोकायत यानी आजीवक कौन थे और अब वे कहां है? यह सवाल बहुत ही पेचीदा है और विस्तृत विचार की मांग करता है। इस पेचीदगी को समझने के लिए पहले डा. धर्मवीर से रूबरू होते हैं, उनके अनुसार-‘मौर्य साम्राज्य में भी आजीवक धर्म का दबदबा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन हो गए थे, पर उनके बेटे बिन्दुसार आजीवक ही रहे थे। बिन्दुसार के बेटे अशोक, आजीवक माता-पिता की सन्तान थे। अशोक आजीवक भी रहे और बाद में बौद्ध की तरफ झुक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मौर्य साम्राज्य का कोई सम्राट ब्राह्मण धर्म का अनुयायी नहीं रहा। तब मौर्य को भी शूद्र कहना उचित नहीं है-इसका मतलब केवल यह है कि अवर्ण आजीवक समाज का विरोधी खेमों की चतुर्वर्ण समाज व्यवस्थाओं से महायुद्ध चल रहा है। इस बारे में इसके सिवा कुछ और न समझा जाए कि पूरा और एकजुट आजीवक समाज, वर्ण व्यवस्थाओं के चारों वर्णों- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-से लड़ रहा है। इस का मतलब यह भी है कि आजीवक समाज के लिए-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों शब्द विदेशी उच्चारण और बाहरी मूल के हैं।’10
हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं; और वर्णव्यवस्था में हिंदू यानी सनातनियों जान बसती है। ये वर्ण और जातियों के समूह हैं। बानगी के रूप में इस वर्ण और जाति के खेल को 1921-1922 में गुजराती के "नव जीवन' अखबार में व्यक्त गांधी जी यानी राष्ट्रपिता के विचार के माध्यम से समझते हैं-‘मेरे विचार से अब तक हिन्दू समाज अपनी जाति प्रथा के कारण जीवित है। जाति प्रथा में स्वराज के बीज मौजूद हैं। जाति प्रणाली विकसित करने वाले समाज में आश्चर्यजनक संगठन क्षमता होती है। जातियों के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होता है। एकता के लिए अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति न देने से ही इसे बुरा नहीं माना जा सकता। नियंत्रित व मर्यादित जीवन का दूसरा नाम जाति प्रथा है। जाति को नष्ट करने का अर्थ पैतृक पेशों को नष्ट करना होगा। अपने पैतृक पेशे छोड़कर यदि ब्राह्मण शुद्ध और शूद्र ब्राह्मण बनने लगेंगे तो समाज का काम ही ठप्प हो जाएगा। जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है।’11
लेकिन डा. धर्मवीर अपनी टिप्पणी के माध्यम से बता रहे हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था से जो बाहर हैं, वे आजीवक हैं। स्पष्ट है, इन्हें सरकारी भाषा में अनुसूचित जाति-जनजाति कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में ये खुद को दलित कहते हैं। लेकिन डा. धर्मवीर उन दलितों से बेहद खफा हैं जो धर्मांतरण कर बुद्धिज्म या अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। वे टिप्पणी करते हैं-‘आज दलित लोग अपनी पहचान खोने के लिए लड़ रहे हैं जबकि अन्यत्र संसार में लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो समाज अपनी पहचान खोने के लिए लड़ता है वह कभी जीत नहीं सकता। किसी भी धर्मान्तरण में दलित समाज अपनी पहचान ही खोता है।’12
सवाल है-अपनी पहचान खोने के लिए कौन लड़ता है?इसके जवाब में बशीर बद्र का शेर-कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता, काफी हद तक सटीक बैठता है। ये मजबूरियां ही तो हैं, जो इतिहास का आजीवक अपनी सम्मानजनक अस्मिता की तलाश में आज भी कभी मुसलमान, तो कभी ईसाई; कभी सिख, तो कभी बौद्ध; और न जाने कितने तथाकथित अस्मितामूलक संप्रदायों और धर्मगुरुओं की चौखट पर माथा रगड़ रहा है, लेकिन उसकी अस्मितामूलक पहचान की यात्रा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसी कदम ताल के चलते आज इस देश का मूल निवासी सैंधव यानी आजीवक संभवत: उससे भी बद्तर हालत में है, जो इस संस्कृति के विनाशकों ने चाहा था। भले ही आज संविधान का शासन है, लेकिन आजीवक संस्कृति के संवाहकों के विरुद्ध, सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरु हुई जंग आज भी विभिन्न मुखौटों की आड़ में बराबर जारी है। इतिहास का आर्य जो पहले घुसपैठिया था, आज वह स्वामी है और पहले से अधिक ताकतवर हो गया है; क्योंकि आज सत्ता, शासन-प्रशासन, प्रचार तंत्र सब उसके नियंत्रण में हैं; और तथाकथित न्याय भी उसकी चौखट पर हाजिरी देकर ही आगे बढ़ता है। साहित्य और इतिहास उसके घर के दास बनकर रह गए हैं; इसलिए इतिहास के चार्वाक/लोकायत संस्कृति के संवाहक आजीवक के अवशेष मिलना भी दुर्लभ हो रहा है। परिणामस्वरूप, आजीवक खुद अपनी संस्कृति का नाम तक भूल गए हैं। आज ये जातियों की जंग में उलझ कर रह गए हैं। कभी ये जाति उन्मूलन की बात करते हैं तो कभी जातियां मजबूत करने की। ऐसे विवादों का न आदि है और न अंत; बस एक अजीब-सा जुनून है, जिसने आजीवकों को सुकून छीन लिया है।
इस सब के बावजूद, इसी इतिहास, जिसकी विश्वसनीयता के विषय में डा. अम्बेडकर, डब्लू एण्ड एस के हवाले से बताते हैं-‘प्राचीन इतिहास मूलतः कोई इतिहास ही नहीं है। उस प्राचीन भारत का कोई एक इतिहास नहीं है। इसके बहुत सारे इतिहास हैं। लेकिन ये अपना चरित्र खो चुके हैं। इसे महिलाओं और बच्चों के मनोरंजन का साधन मात्र बना दिया गया।’13लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हम मानते है कि इतिहास में जैसे भी उपलब्ध अवशेष हैं, हमें उन्हीं से तलाश करना है-आजीवक कौन थे?इस कड़ी में सबसे पहले हम इतिहासकार कश्यप की टिप्पणी का उल्लेख करना चाहते हैं। इसके अनुसार-‘अनार्य दुर्गों और नगरों में रहते थे। आर्यों ने उनका उन्मूलन किया, उनके दुर्गों और पुरों का विध्वंस करके अनार्यों को दक्षिण के पर्वतों की ओर ढकेल दिया। कहा जाता है कि उनमें से बहुतों ने पर्वतों में शरण ली और उनमें से बहुतेरे गोंड, खांड, कोल, भील, संथाल, औराव, भुण्डादि उन्हीं के वंशज हैं। उनमें से बहुत से पकड़ लिए गए और दास घोषित कर दिए गए। इन्हीं में से आज हिन्दुओं की वर्ण व्यवस्था के अन्तिम स्तर के शूद्र हैं।’14जो बात कश्यप कह रहे हैं, आदिवासियों के बारे में ठीक ऐसे ही निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ‘द वायर’ के यू-ट्यब चेनल पर 16 नवम्बर 2024 अपने साक्षात्कार में, साक्षात्कारकर्ता जाने माने वकील कपिल सिब्बल के समक्ष पेश करते हैं।
गौरतलब है कि उपरोक्त टिप्पणी में अन्तिम स्तर के शूद्र का सीधा-सा संबंध हिन्दूवादी वर्णव्यवस्था से बाहर मौजूदा दलितों से है। कोसम्बी के अनुसार-‘इस सिलसिले में निश्चित ही लिखित सामग्री और पुरातत्व खोज से मिलने वाली जानकारी दोनों एक दूसरे से मेल खाती हैं। इसलिए विश्वास करने के कई आधार हैं कि कम से कम कुछ बातों में असुर शब्द का अर्थ था: सिंधु घाटी की स्थापना करने वाले।’15 यहां कोसम्बी स्पष्ट करते हैं कि सिंधु घाटी के वारिसों को ‘असुर’ कहा गया। ‘असुर’ यानी दलितों को अपमानित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अनेक संज्ञाओं में से ‘एक संज्ञा’। कहने की जरूरत नहीं कि अंतिम स्तर के शूद्र, दास, दस्यु, दलित, हरिजन चाण्डाल, अस्पृश्य, अनार्य, असुर आदि वे अपमानजनक अलंकरण हैं जो इस देश के सभ्य और सुसंस्कृत समाज के द्वारा इस देश के मूलनिवासी सैंधव/चार्वाक/लोकायत यानी आजीवकों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
इस हकीकत को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखने के लिए कंवल भारती, जिन्होंने आजीवक पर एक पुस्तक भी लिखी है, की टिप्पणी से रूबरू होना अनिवार्य महसूस हो रहा है, इसके अनुसार-‘आर्य जब भारत में आए, तो विचार के स्तर पर उनका संघर्ष लोकायत से हुआ। आर्यों द्वारा अनार्यों को दास, दस्यु कहकर अपमानित करना और भारी संख्या में उनको मौत के घाट उतारना आकस्मिक नहीं था। उसके मूल में संस्कृति विरोध ही था। ऋग्वेद की एक ऋचा इसकी साक्षी है, जिसमें कहा गया है-अकर्मा दस्युरयिनो अमंतुन्यव्रतीः अमानुषाः।, तस्या मित्रहन्वधदसिस्य दंभय।। (ऋग्वेद 10-22-8) ‘अर्थात हम चारों ओर दस्यु जाति से घिरे हैं। ये यज्ञ नहीं करते, उनके कर्मकाण्ड भिन्न हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। हे शत्रुहंता, उन्हें मारो। दस्यु जाति का विनाश करो।’16इस मारने और विनाश करने की इंटेंसिटी को इतिहासकार डा. दीनानाथ के शब्दों में समझें अगर, तो तस्वीर कुछ इस प्रकार की बनती है-‘कुछ लोगों का अनुमान है कि बार-बार आग लगने से यह सभ्यता बरबाद हो गई। सिंधु की खुदाई की राख की एक दूसरे के बाद सात तह मिली हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि सिंधु घाटी के नगर सात बार बसे और सात बार उजड़े। इसी लिए मोहनजोदड़ो को ’मुर्दों का टीला’ भी कहा जाता है।’17
कंवल भारती की उपरोक्त टिप्पणी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आर्यों ने जिस सभ्यता/संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया था, वे लोकायत/चार्वाक यानी अनार्य, दास, दस्यु आदि सभी आजीवक संस्कृति के संवाहक हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें ऋग्वेद में यज्ञ न करने वाले, अलग कर्मकाण्ड करने वाले हैं, जो मनुष्य नहीं हैं, कहा गया है और इनका विनाश (सिंधु घाटी के नगरों का सात बार तक उजड़ना या उजाड़ा जाना) करने का आह्वान किया गया है। सत्य के परीक्षण की इस यात्रा में हम एम. व्हीलर की टिप्पणी का उल्लेख करना जरूरी समझते हैं, इसके अनुसार-‘मौजूदा दलित, अस्पृश्य आदिवासी आदि ही सिंधु घाटी के मूल निवासी हैं जिनका विनाश आर्यों ने किया था।...‘आज के विद्वान ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपिया को सिंधु घाटी का हड़प्पा नामक स्थान मानना चाहते हैं।’18 यद्यपि वर्तमान अनुसूचित जाति-जनजाति के मूलनिवासी यानी आजीवक होने के और भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, हमें लगता है कि उपरोक्त प्रमाण ही पर्याप्त हैं, वरना विषयांतर का खतरा पैदा हो जाएगा।
अब हम आजीवक संस्कृति की कुछ परिचयात्मक प्रमुख विशेषताओं पर बात करते हैं जिनकी वजह से आजीवक संस्कृति को विलुप्तिकरण का शिकार होना पड़ा। इस संदर्भ में हम शुरु से ही रेखांकित करके चलना अनिवार्य समझते हैं कि हम इस संस्कृति पर चर्चा इस नजरिए से कर रहे हैं कि ‘यह वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में हमारी किस प्रकार मदद कर सकती है।’ यह कैसे एक तर्क-विवेक व वैज्ञानिक टेंपरामेंट, जिसकी वर्तमान समाज को नितांत आवश्यकता है, को हमारे जीवन का अंग बनाने में सहायक हो सकती है। कैसे यह अंधी आस्था के अंधकार में दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला ला सकती है; और कैसे यह समाज और देश ही नहीं, बल्कि मानवता के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकती है।
इस कड़ी में हमारा आग्रह है कि जहां भी चार्वाक/लोकायत शब्द का प्रयोग है, उसे आजीवक और उसकी संस्कृति के रूप में ही समझा जाए; क्योंकि जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि लोकायत-सिद्धान्त अनुगामी जन ही ‘आजीवक’ है। शरीर और आत्मा अलग नहीं, एक ही है। शरीर के सदुपयोग, स्वास्थ्य और श्रमात्मक आजीविका ही आजीवक नाम से पुकारे जाने का प्रमाण है। इसमें जन-जीवन से घनिष्ठता रखने वाले कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि, राजनीति-स्वरूप दण्डनीति और स्वास्थ्यप्रद आयुर्वेद, इन तीनों से पूर्ण रूप से सम्बद्ध रहे हैं।’ आजीवक संस्कृति की यह तस्वीर कुछ अधूरी लगती है। हमें लगता है कि डा. दीनानाथ वर्मा इसे पूरा करने में सहायक हो सकते हैं, उनके अनुसार-‘सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह सभ्यता शांतिप्रधान सभ्यता थी और इसका विकास अत्यंत शान्तिमय वातावरण में हुआ था। बड़े मार्के की बात है कि उत्खनन में कवच, ढाल, तलवार, शिरस्त्राण आदि युद्धोपयोगी सामान नहीं मिले हैं। यहां धनुष-बाण, कुल्हाड़ी, माला आदि आखेटीय प्रवृत्ति के द्योतक हो सकते हैं ...अन्य प्राचीन सभ्यताओं की अपेक्षा सैन्धव सभ्यता का नैतिक स्तर ऊंचा था और वहां के निवासी वाणिज्य, व्यापार, कला कौशल की उन्नति पर अपने देश को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते थे ।’19
उपरोक्त सभी कार्यों का संपादन स्वस्थ्य शरीर द्वारा ही संभव है। इसलिए शरीर आजीवकों की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस लिए इनके विषय में कहा गया है-यावत जीवेत्, सुखम जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत:।। इस कथन को लेकर आजीवकों के निंदकों द्वारा इनकी निंदा की यही वजह है कि आजीवक संस्कृति के अनुयायी आम आदमियों की तरह श्रम आधारित आजीविका के संवाहक थे। वे किसान, कारीगर थे, व्यापारी सब थे और इसी तरह के अन्य लोग थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो ‘क्या आम और क्या खास, आजीवक संस्कृति में सभी श्रम आधारित आजीविका का निर्वहन करते थे’। यह इनकी संस्कृति को खास बनाती है, क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम का भरपूर सम्मान रहा है। लेकिन अपने यहां आज स्थिति इसके एकदम उलट है। श्रम आधारित आजीविका को हेय दृष्टि से देखा जाता है और पारिश्रमिक भी बहुत मामूली दिया जाता है। इस कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं- ‘उनकी संख्या भी बौद्धों से ज्यादा थी। कारण यही था कि आजीवकों द्वारा समाज सुधार पर अत्यधिक बल दिया जाता था। बौद्ध लोग मक्खलि गोसाल की आलोचना किया करते थे। समय-समय पर आजीवकों और बौद्धों के बीच खुली मुठभेड़ हुआ करती थी।’20इस कड़ी में भगवती सूत्र के हिन्दी भाष्यकार आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है-...'उस युग में भी जब स्वयं तीर्थंकर विद्यमान थे, गोशालक जैसा पाखण्डी व्यक्ति अधिक लोकप्रिय बन गया था। भगवान् महावीर के अनुयायियों की संख्या केवल एक लाख उनसठ हजार थी, जबकि गोशालक के अनुयायी ग्यारह लाख इकसठ हजार थे।’21 गौरतलब है, यह लोकप्रियता हवा में नहीं होती, लोकप्रियता के लिए ठोस आधार होता है; जाहिर है, आजीवकों के आधार के ठोस होने के प्रमाण रहे हैं, तभी यह लोकप्रिय था। यह पूर्वाग्रह नहीं तो क्या है, कि गोशालक को पाखंडी कहा जा रहा है।
हम जानते हैं कि इनकी तर्क-विवेक के आधार पर वेद निंदा करने के कारण आजीवकों को पाखंडी कह कर मजाक उड़ाया जाता है। इन्हें गैर-जिम्मेदार और इनकी दुनिया सिर्फ खाने-पीने तक सीमित बताई जाती है। लेकिन हम यह मानते हैं कि उस समय उत्तम स्वास्थ्य के लिए घी सर्वोत्तम आहार रहा होगा। संभवत: इसी गरज से आजीवक संस्कृति में ऋण लेकर भी घी पीने की बात कही गई है। यदि ऋण लेकर भी उत्तम स्वास्थ्य अर्जित किया जाता है और स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाता है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि स्वस्थ्य शरीर के माध्यम से जीवन के सारे क्रियाकलाप संभव है; और शरीर की बदौलत ही परिश्रम करके कोई भी ऋण चुकाया जा सकता है। कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के दम पर ही मानसिक और सामाजिक जीवन का आनंद लिया जा सकता है। यही इनके सुख का आधार है। यह भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसकी अंतिम परिणति मानसिक सुख और सुकून में होती है, जिसे परमानंद कहते हैं। आजीवक संस्कृति में शरीर और स्वास्थ्य की प्राथमिकता को समझने के लिए एक कहावत का उल्लेख जरूरी महसूस हो रहा है। इसके अनुसार-यदि धन की क्षति हुई है, तो कोई क्षति नहीं हुई है, अगर स्वास्थ्य की क्षति हुई है, तो कुछ की क्षति हुई है और यदि चारित्रिक क्षति हुई है, तो सब कुछ की क्षति हुई है। ऐसा लगता है कि यह कहावत आजीवक संस्कृति की बदौलत ही अस्तित्व में आई है।
दूसरे, आजीवकों का यह मानना कि इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद यानी उसके राख बन जाने के बाद कुछ हासिल होने वाला नहीं है; क्योंकि शरीर के अस्तित्व में आने के लिए जरूरी चारों तत्व अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी अपने-अपने मूल स्त्रोत में मिल जाते हैं। इसी लिए आजीवक संसार को किसी ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं मानते। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है, उसके अस्तित्व में आने के पीछे चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की थ्यौरी सबसे अधिक स्वीकार्य है; और आजीवक संस्कृति मोटा-मोटी इस थ्यौरी के करीब नजर आती है (यहां इस विषय पर इरादतन संकेत मात्र दिया जा रहा है)। दूसरे, आजीवक संस्कृति में दूसरा जन्म नहीं है। यही जन्म सब कुछ है और मृत्यु ही मोक्ष है। जीवन में सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक। इसे राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कुछ प्रकार समझा जा सकता है-’प्राचीन चार्वाक-ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं और परलोक नहीं। जीवन के भोग त्याज्य नहीं, ग्राह्य हैं। तजुर्बे (अनुभव) और बुद्धि को हमें सत्य के अन्वेषण के लिए अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए।’22इसे डा. धर्मवीर के शब्दों कुछ प्रकार समझा जा सकता है-‘आजीवक के विषय में ‘पहला सूत्र है-नो धम्मो 'त्ति । उनका दूसरा सूत्र है- नो तवो 'त्ति। उनका तीसरा सूत्र है-नत्थि पुरिस्कारे। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा; कोई ऐसा तप नहीं अमुक योनि में पैदा कर देगा; कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद पुनर्जन्म के रूप में मिलने वाला।’23
जाहिर है, शारीरिक श्रम आजीवकों के यहां काम एकैव: पुरुषार्थ की अवधारणा के चलते व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य ही जीवन में सुखों को सुनिश्चित कर सकते हैं। आजीवकों को अकर्मण्यवादी और भाग्यवादी कहने वालों की समझ दुरुस्त करने के लिए आजीवक संस्कृति के काम रूपी सर्वोच्च पुरुषार्थ को डा. हरिपाद चक्रबर्ती से समझते हैं। उनके अनुसार-‘बौद्ध ग्रंथों से प्रमाण दिए गए हैं कि राजगृह के पाण्डु पुत्र नाम के आजीवक साधु एक रथ निर्माता के पुत्र थे। जब उसने एक गाड़ी-निर्माता के काम का कमाल देखा तो वह खुशी में जोर-जोर से चिल्लाया था। कुछ आजीवक भविष्य वक्ताओं का काम करते थे। जनसान नाम आजीवक साधु राजा बिन्दुसार का दरबारी था। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि आजीवक साधु भीख पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे अपने जीवन में विभिन्न सामाजिक पेशों से जुड़े हुए होते थे।’24इस टिप्पणी में ‘भविष्य वक्ता’ का जिक्र आया है, यह आजीवक संस्कृति से मेल नहीं खाता है; क्योंकि इनका सब कुछ आज पर और अनुभवजन्य निष्कर्षों पर आधारित होता है, तो भविष्य वक्ता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, खैर...।
तस्वीर को और अधिक साफ करने के लिए पुन: डा. हरिपाद चक्रबर्ती को बीच में लाते हैं। उनके अनुसार-‘आजीविक" का उस व्यक्ति से सम्बन्ध है जो अपनी जीविका के लिए कुछ नियमों का पालन करता है। उन्होंने बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग में आए हुए शब्द "'सम्यग आजीव' की याद दिलाई है। लेकिन वहां यह आजीवकों से चुराया हुआ शब्द है। चक्रबर्ती ने यह संभावना जरूर जताई है कि पहले समय से ही कुछ साधु ऐसे होते थे जो जीविका के लिए पेशों को अपनाए रहते थे। मक्खलि गोसाल से जुड़े 'मंखत्व' के बारे में उन्होंने माना है कि यह चित्र प्रदर्शन का पेशा था और मक्खलि के पिता इसी पेशे को अपनाए हुए थे। बाण के 'हर्ष चरितम्' में 'यम पटिटका' का होना भी यही दर्शाता है। इसलिए यह संभव है कि आजीवक साधु भीख मांगने के बजाय चित्र प्रदर्शन के पेशे को अपनाए रहते थे।’25
आजीवकों में बिना किसी स्तरीकरण के ‘काम/कार्य’ की प्राथमिकता है। उनके यहां काम के बंटवारे के लिए न किसी वर्णव्यवस्था की जरूरत थी और न ही किसी जाति प्रथा की। लेकिन आज वर्ण और जाति प्रथा वर्तमान भारतीय समाज का ऐसा कोढ़ है, जिसका कोई इलाज यदि संभव है तो वह आजीवक संस्कृति में ही संभव है। आजीवक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की स्थिति समझने के लिए जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश की मदद ली जा सकती है। इसके अनुसार-‘सवाल है कि मक्खलि गोसाल आचार्यों और उपाध्यायों को अवर्णवादी क्यों बना रहे थे। उत्तर यह है कि आचार्य और उपाध्याय अपने आपको वर्णवादी घोषित कर रहे थे। यह आचार्यों और उपाध्यायों का घमंड था जो उनके वर्ण के रूप बोलता था। मक्खलि गोसाल ने उन के इसी घमंड पर चोट की थी।...जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश के अनुसार अवर्णवाद की परिभाषा–‘गुण वाले बडे़ पुरुषों में जो दोष नहीं हैं उनका उनमें उद्भावन करना अवर्णवाद है।’… ग्रन्थ 'राज वार्तिक' को उद्धृत करते हुए लिखा गया है-"ये श्रमण शूद्र हैं…इत्यादि संघ का अवर्णवाद है।’26 राम प्रताप त्रिपाठी शास्त्री इसे और स्पष्ट करते हुए बताते हैं-जो अधार्मिक जन हैं वर्णाश्रम की मर्यादा से वहिर्भूत (बाहर) हैं, वर्णसंकर हैं, कारीगरी या शिल्पकर्म करने वाले हैं, देवताओं ने उनको ही इन पिशाचों की आजीविका बनाई है|’27
ए एल बाशम इस कोढ़ को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं-‘गोशाल ने अपने मुख्यालय में कुम्हार की कार्यशाला का उपयोग किया होगा, और बर्तनों का उपयोग आजीवक तपस्या में किया जाता था, 'ये दोनों मिलकर यह संकेत देते हैं कि यह संप्रदाय किसी तरह से कुम्हार जाति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था, और अपने सदस्यों को विशेष रूप से आकर्षित करता था।’28 हमें लगता है कि यहां ‘कुम्हार’ जाति का परिचायक नहीं, बल्कि व्यवसाय का परिचायक है। डा. हरिपाद चक्रबर्ती आजीवक संस्कृति के गरिमामय इतिहास को कुछ इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं-‘गौरतलब है कि आजीवक धर्म के दरवाजे बिना जाति और लिंग का भेद किए कमाने वाले सभी पेशों के लोगों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। उदाहरण के लिए बिम्बिसार के एक सम्बन्धी आजीवक मत के अनुयायी हो गए थे। इस धर्म में औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग के लोग बहुतायत में जुड़े थे। हालाहला नाम की स्त्री जिन्होंने गोसाल के साथ 16 वर्ष गुजारे, एक कुम्हारी थीं। सद्दाल पुत्र भी कुम्हार थे। उन्होंने पोलासपुर में आजीवक संघ की सभा आयोजित की थी। लगता है, इस धर्म का कुम्हारों से विशेष सम्बन्ध था।’29
विश्लेषण की इस प्रक्रिया में जाति, धर्म और वर्ण से आगे यह देखना जरूरी हो जाता है-आजीवक संस्कृति में लिंग भेद की स्थिति क्या थी, कैसी थी? हम पाते हैं कि आजीवक संस्कृति में रामचरित मानस के सुंदर कांड में मौजूद 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी' जैसी अवधारणा नहीं है। यहां स्त्री की मान-मर्यादा व गरिमा मौजूद है। इसे डा. हरिपाद चक्रबर्ती की टिप्पणी से समझते हैं-‘किसी भी धार्मिक मामले में स्त्री का महत्व कम नहीं है। आजीवक धर्म में स्त्री पाप योनि नहीं है। वे नहीं मानते कि स्त्री के संसर्ग से पाप की सृष्टि होती है। विरोधियों के द्वारा की गई आलोचना से पता चलता है कि गोसाल के अनुयायियों को स्त्रियों का गुलाम कहा गया है।’30डा. हरिपाद चक्रबर्ती स्त्री के धार्मिक मामले तक सीमित न रहकर वे इसे जीवन की साधना से जोड़ते हुए टिप्पणी करते हैं-‘आजीवक धर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्त्री को छोड़ कर जीवन की साधना नहीं होती। यही नहीं, इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समानता के स्तर पर रहते हैं।’31 गौरतलब है कि यहां छठी सदी ई.पू. की बात हो रही है। कल्पना की जा सकती है कि सैंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यह कितनी गरिमामय रही होगी, जिसे रामचरित मानस, तथाकथित महान ग्रंथ में ताड़न की अधिकारी कह कर नारी के सारे तर्क-विवेक और स्वतंत्रता को बांझ बनाकर रख छोड़ा है। वर्तमान नारी उत्पीड़न की लगभग सभी घटनाओं के मूल में ‘ताड़न की अधिकारी’ वाली सोच काम करती है, जिसके तहत नारी पुरुष के हाथों की कठपुतली से अधिक कुछ नहींहै।
इस कड़ी में डा. धर्मवीर द्वारा व्यक्त स्थापना काबिल-ए-गौर है। इसके अनुसार-‘गोसाल ने हालाहला से विवाह किया था। इसी वजह से महावीर ने गोसाल को भ्रष्ट कहा था। महत्व अंजलि कम्म का है। महावीर और बुद्ध अंजलि कम्म के विरोधी थे। यह अंजलि कम्म क्या है? हाथ जोड़ कर स्त्री को प्रणाम करना है। गोसाल ने हाथ जोड़ कर स्त्री को प्रणाम किया था। अपने मरते समय भी उन्होंने अपनी पत्नी हालाहला को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया था जिसे ‘चरिमे अंजलि कम्म’ कहा जाता है।’32आजीवक परंपरा पर प्रकाश डालते हुए डा. धर्मवीर महावीर की सोच को जगजाहिर करते हुए बताते हैं-‘असल में, गोसाल और महावीर में बिगड़ी किस बात पर थी; जबकि ये दोनों छह सालों तक साथ-साथ रहे थे? बिगड़ी इस बात पर थी कि मक्खलि गोसाल ने स्त्री को साथ रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने ब्रह्मचर्य की इस परिभाषा को त्याग दिया था कि गृहस्थ और बाल-बच्चेदार आदमी होने से धर्म भंग होता है।’33
आजीवक संस्कृति के व्यापक कैनवास को समझने के लिए पुन: डा. धर्मवीर से रूबरू होते हैं। उनके अनुसार-‘आजीवक चिन्तन यह है कि राजा तो राजा, एक धर्म पुरुष को भी बिना परिवार और स्त्री के नहीं रहना चाहिए।…आजीवक लोग परिवार रखते हैं और कमा कर खाते हैं।…यह एक फैशन हो चला है कि जो जिस किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहता है, वह उसके लिए सबसे पहले स्त्री, बच्चे और परिवार को त्यागे। ऐसे तो किसी को विज्ञान में, किसी को सेना में, किसी को डॉक्टरी में, किसी को इंजीनियरी में, किसी को साहित्य, संगीत, नृत्य या कला में और किसी को अनन्य क्षेत्र में काम करना होता है, तो क्या वे सब यही कहने लगेंगे कि उन्हें स्त्री और परिवार का त्याग करना है?34
इस संस्कृति में स्त्री त्याग करने के लिए नहीं है। यह आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए है; क्योंकि यहां लिंग भेद नहीं है। इसलिए स्त्री आजीवक की परिभाषा से बाहर नहीं है, जो बताती है-'आजीवक' शब्द का अगला विकास 'आजीविका' में होता है। आजीविका को खाना-कमाना, रोजगार, कमाई आदि कहा जाता है। इससे आदमी की गुजर-बसर होती भी पेशा हो, यह वही है और इस में हुनर की आवश्यकता होती है। 'आजीविका" को छोटा कर के मात्र 'जीविका' भी कहा जाता है-जीविकोपार्जनI हेमचन्द्र की पुस्तक 'अभिधान चिन्तामणि' में भी इस शब्द के छह अर्थ दिए गए हैं।’35स्पष्ट है कि आजीवक संस्कृति में किसी भी प्रकार के काम, भले ही यह चिंतन-मनन व समाज सेवा से ही क्यों न जुड़ा हो, इसके लिए स्त्री और परिवार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यह संस्कृति इससे एक कदम आगे बढ़कर स्त्री को पुरुष की तरह काम करने को प्रेरित करती है। यह आजीवक संस्कृति जैसी सोच का ही परिणाम है कि स्त्री आज सेना तक में अनेक पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। कहने की जरूरत नहीं कि आजीवक संस्कृति में परिवार का हर सदस्य आजीवक है, जीविकोपार्जन की प्रक्रिया का हिस्सा है।
आजीवक के विषय में व्याप्त नकारात्मकता से संस्कृति के सकारात्मक व यथार्थपरक पक्ष को समझने लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसाकि हम पहले बता चुके हैं कि आर्यों ने इस देश के मूलनिवासियों यानी आजीवकों को नेस्तनाबूद करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा; और उन्हें अनेक निर्योग्यताओं से लादा। यद्यपि जैन धर्म और बौद्ध धम्म, आर्यों यानी हिंदू धर्म/सम्प्रदाय के विरुद्ध अस्तित्व में आए; लेकिन उन्होंने भी आजीवकों के साथ दुश्मन जैसी ही प्रतिद्वंद्वी व नकारात्मक भूमिका निभाई। भगवती सूत्र के हिन्दी भाष्यकार आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार-'उस युग में भी जब स्वयं तीर्थंकर विद्यमान थे, गोशालक जैसा पाखण्डी व्यक्ति अधिक लोकप्रिय बन गया था। भगवान् महावीर के अनुयायियों की संख्या केवल एक लाखउनसठ हजार) थी, जबकि गोशालक के अनुयायी ग्यारह लाख इकसठ हजार थे।36 यहां गोशाल को पाखंडी कहा जा रहा है जबकि गोशाल के विषय में जानकारी मिलती है कि वे स्वयं आजीवकों के चौबीसवें तीर्थंकर थे और उनके अनुयाइयों की संख्या जैन और बौद्ध दोनों से अधिक थी। सवाल उठता है-यदि गोशाल पाखण्डी थे तो उनके अनुयाइयों की संख्या जैन और बौद्धों से अधिक कैसे हो सकती है; और यह दो हजार से भी अधिक वर्षों तक कैसे अस्तित्व में रहा? लेकिन आलम है कि जैन और बौद्ध साहित्य में आजीवकों के खिलाफ पूर्वाग्रह की भरमार है।
इस कड़ी में लोमहंस जटाला में कहा गया है कि बोधिसत्व स्वयं एक बार आजीवक बन गए थे। नग्न और एकाकी, वे लोगों को देखते ही हिरण की तरह भाग जाते थे। वह कूड़ा-कचरा, छोटी मछलियाँ और गोबर खाता था।37यदि इस प्रकार की घटना को थोड़ी देर के लिए सच भी मान लिया जाए, तो यह इस समाज का सामूहिक यथार्थ नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक विकृति का परिणाम हो सकती है, समग्रता में किसी धर्म-सम्प्रदाय की स्थाई प्रवृत्ति नहीं। झूठ फैलाने की यह भेड़ा चाल यहीं नहीं रुकती, इस नासमझी को सच का जामा पहनाने के लिए हमारे सामने बालक जम्बूक की कहानी पेश की जाती है जिसमें बताया गया है-‘जम्बूक ने बहुत कम उम्र में ही नग्नता और मल खाने की प्रवृत्ति विकसित कर ली थी, और इसके लिए उसके माता-पिता ने उसे आजीवक संघ में शामिल कर लिया था। कारण चूंकि वह अपने घृणित आहार से पूरी तरह संतुष्ट था, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया।’38जम्बूक को मल खाने और नग्नता के चलते आजीवक संघ में शामिल करना, एक यह संकेत भी देता है वहां इस प्रकार के मानसिक विकारों के मुक्ति का मार्ग उपलब्ध हो। यह आजीवकों के उत्तम चरित्र और समस्या निवारण के कुशल प्रबंधन का द्योतक हो सकता है। इसके विपरीत, अगर इस टिप्पणी से यह संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि आजीवक मल खाते थे और नग्न रहते थे, तो इसे धूर्तता की पराकाष्ठा के अलावा कोई और नाम देना मेरे वश की बात नहीं है, खैर...।
आजीवकों के खानपान के नकारात्मक प्रचार से बाहर, सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। इस पहलू के अनुसार-‘बौद्धों और जैनों की तरह आजीविका अहिंसा में विश्वास करते थे, और आमतौर पर शाकाहारी थे। यह असंभव नहीं है जैसा कि वायु पुराण इंगित करता है, उनमें से कुछ ने जादुई अनुष्ठानों का अभ्यास किया, जिसमें रक्त बहाना शामिल था।…ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध और महावीर, दोनों ने धार्मिक नेताओं के रूप में अपने करियर के दौरान कम से कम एक बार मांस खाया था।’39भले ही जैनों और बौद्धों ने आजीवकों पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं लेकिन उपरोक्त उदाहरण के आधार पर हम बुद्ध, महावीर और इनके पूरे समाज पर मांसाहारी होने का आरोप नहीं सकते। यह अलग बात है कि आज विज्ञान और चिकित्सा ने मांसाहार को सामान्य आहार की तरह देखा है, कुछ मामले इसे बेहतर बताया है। इसके चलते आजकल मांसाहार को उस तरह से घृणित नजरिए से नहीं देखा जाता, जैसे बुद्ध और जैन के काल में देखा जाता रहा होगा।
ऐसे बिना हाथ-पैर के किस्सों से रूबरू होते हुए अचानक मुझे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की याद आती है। वे अपने चुनावी भाषण के दौरान अपने विरोधी राजनीतिक दलों के विरुद्ध नॉन-स्टॉप अनर्गल बयानबाजी के दौरान इंसानी जीवन के हर क्षेत्र को झूठ से ऐसे पाट देते हैं कि कुछ समय के लिए तो इसे सुनने वाला अंधभक्त भी शर्मसार होने से बच नहीं सकता। यहां उन घटनाओं और बयानबाजी का उल्लेख करना गैर-जरूरी महसूस हो रहा है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह को समझने के लिए हमें सिक्के के दूसरे पहलू यानी इस संस्कृति के सकारात्मक पक्ष से रूबरू होना जरूरी महसूस हो रहा है। ‘तीर्थंकरों की कुल संख्या चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि गोशाल को अपने अनुयायियों के बीच, जैनियों के बीच महावीर के बराबर दर्जा प्राप्त था, और उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया जाता था।’40 …भगवती सूत्र के अपने अंतिम दिनों के विवरण के दौरान गोशाल के बारे में दो बार कहा जाता है कि उन्होंने वर्तमान अवसर्पिणी युग के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर की स्थिति के लिए खुद दावा किया है।‘41 ये दोनों टिप्पणियां स्पष्ट संकेत देती है कि गोशाल महावीर से किसी भी रूप में कमतर नहीं हैं और समाज में उनकी स्वीकार्यता उल्लेखनीय है।
विश्लेषण की इस कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं-‘अभिजात्यों के वर्गीकरण से संकेत मिलता है कि आजीवक जैनों को पवित्रता में अपने से दूसरे स्थान पर मानते थे। बौद्ध भिक्षु तीसरे स्थान पर थे, और रूढ़िवादी ब्राह्मण को संभवतः काले वर्ग में दुष्ट कुरर-कम्मंत के साथ शामिल किया गया था, हालांकि, जैसा कि दिखाया गया है, 'कुछ संकेत हैं कि शुरुआती आजीवक अभ्यास और सिद्धांत कुछ मामलों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अभ्यास और सिद्धांतों की तुलना में रूढ़िवाद के करीब थे।’42उपरोक्त टिप्पणी एक अनूठे स्तरीकरण की ओर संकेत करती है जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, तीनों आजीवक से निचले पायदान पर मौजूद हैं। यह आजीवक को फिट फॉर नथिंग की श्रेणी में रखने वालों की आंखें खोलने वाला है।
गोशाल और आजीवक समाज पर नग्नता का आरोप लगा कर कठघरे में खड़ा करने वालों के लिए ए एल बाशाम की यह टिप्पणी काबिल-ए-गौर है। इसके अनुसार-‘भगवती सूत्र में कहा गया है कि उनकी मृत्यु पर गोसाल मंखलिपुत्त के शव को एक शानदार वस्त्र पहनाया गया था और आभूषणों से सुसज्जित किया गया था, जो यह सुझाव देता है कि किसी प्रकार का पोपीय ठाठ-बाट आजीवकवाद के नेताओं के लिए अज्ञात नहीं था।’43साफ है कि आजीवक समाज वस्त्र और ओढ़ने-पहनने के मामले में अपने समकालीन समाजों से किसी भी रूप में पिछड़ा नहीं था। स्पष्टता की गरज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं-‘भारत के बाहर भी आजीवकों के चित्रण मौजूद हैं। बोरोबुदुर में एक मूर्ति नव प्रबुद्ध बुद्ध की आजीवक उपका से मुलाकात को दर्शाती है; उपका के साथ यहां दो साथी आजीवक हैं, और तीनों ने एक अजीबोगरीब स्कर्ट जैसा परिधान पहना हुआ है और बालों को सावधानी से सजाया हुआ है (प्लेट II)।’44
इस संस्कृति में ओढ़ने-पहनने के अलावा भी आनंद और मौज-मस्ती और भी साधन उपलब्ध थे। अभयदेव द्वारा दो मार्गों (मग्ग) की परिभाषा से संदेह मजबूत होता है, जो छह दिसाचरों ने आठ महानिमित्तों के साथ पुव्वों से गोसाल की मृत्यु से कुछ समय पहले सम्मेलन में निकाला था। टिप्पणीकार के अनुसार, ये 'गीत और नृत्य हैं। आजीविकों की आठ अंतिमताओं में से दो को करिमगेये और करिमनट्टे, अंतिम गीत और नृत्य कहा जाता है,' और गोशाला ने स्वयं अपने अंतिम प्रलाप में गाया और नृत्य किया था।’45
वैसे भी आजीवक समाज कोई गया-बीता समाज नहीं था। इसमें कारीगर, व्यापारी और शासक, सभी रहे हैं। ये सामाजिक और आर्थिक मामले में किसी से कम नहीं थे। उस समय के समाज और आजीवकों की वेशभूषा के मसले को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पाते है-ब्राह्मणों ने जैनियों, बौद्धों और आजीवकों पर विशेष कर लगाए थे। कौटिल्य आजीवकों को अपना दुश्मन समझता था। उसने विधान किया है कि जो कोई आजीवकों और बौद्धों को भोजन खिलाता है, उस पर 100 पणों का जुर्माना लगाना चाहिए।…जैनियों और बौद्धों से प्रति परिवार के हिसाब से कर लिया जाता था, जबकि आजीवकों से यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता था।46 जाहिर है कि कर उन्हीं पर लगाया जाता है जो कर देने की कुव्वत रखते हैं। कर लगाने की दूसरी मंशा यह भी हो सकती है कि आजीवक अपने समकालीन शासक वर्ग के लिए चुनौती बने थे, जिसके कारण उन्हें शासक वर्ग के धर्म-संप्रदाय में शामिल होने के लिए का दबाव बनाने और हतोत्साहित करने के लिए उनपर टैक्स लगाए जाते थे। उल्लेखनीय है कि आजीवकों पर जैनों और बौद्धों की तर्ज पर परिवार के आधार पर टैक्स न लगाकर, प्रति व्यक्ति टैक्स लगाना, आजीवकों की प्रगतिशीलता और समृद्धि का द्योतक लगता है, न कि किसी पिछड़ेपन का।
आजीवकों का स्वतंत्रतावाद इस संस्कृति की एक अनूठी विरासत है जो रूसो के सामाजिक संविदा (