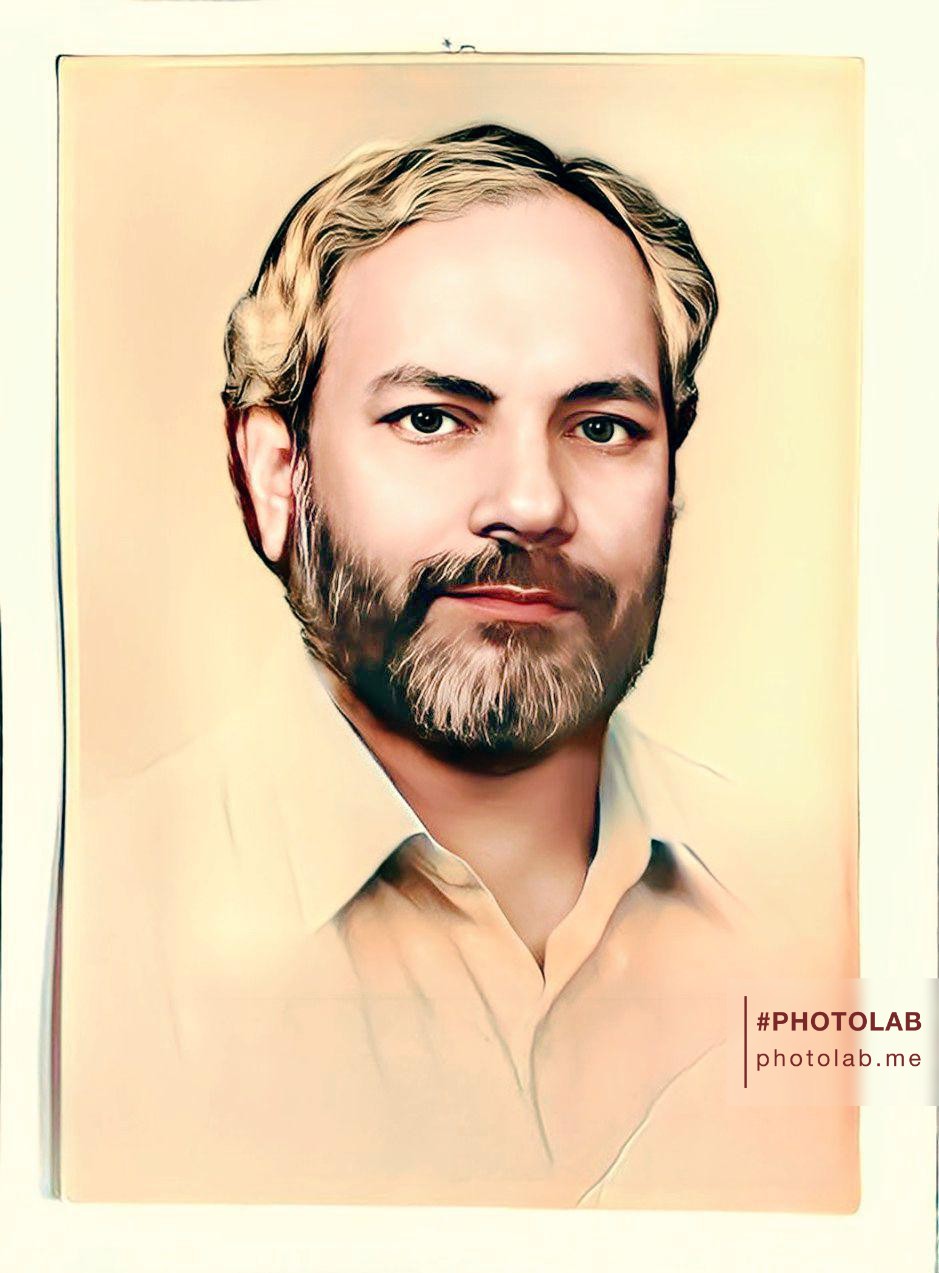तेजपाल सिंह 'तेज' (प्रस्तोता) : अम्बेडकरवादी आंदोलन का यथार्थ - ईश कुमार गंगानिया
- – तेजपाल सिंह ‘तेज’
- अम्बेडकरवादी आंदोलन का यथार्थ
- ईश कुमार गंगानिया
-
किसी भी प्रगतिशील समाज में व्यक्ति, उसके परिवेश और राष्ट्र की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने की आवश्यकता सदा बनी रहती है। इसके व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यत: आंदोलन की भी जरूरत होती है। समय, काल और परिस्थिति के अनुरूप इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं। किसी आंदोलन को समझना है तो आंदोलन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों से साक्षात्कार भी एक बेहतरीन साधन हो सकता है। विद्याभूषण रावत की साक्षात्कार की पुस्तक ‘अम्बेडकरवाद: विचारधारा और संघर्ष’ इसका एक सशक्त उदाहरण है। पुस्तक के लेखक यानी साक्षातकारकर्ता विद्याभूषण रावत इस अवधारणा को अमली जामा पहनाने वालों में से एक हैं। यदि उन्हीं के शब्दों में समझे तो भगवान दास के सान्निध्य ने उन्हें अम्बेडकरवाद और जातीय समस्या को समझने का अवसर दिया। वीटी राजशेखर की पत्रिका ‘दलित वॉयस’ ने उन्हें पेरियार और अस्मिता आंदोलनों से सशक्त परिचय कराया। एनजीऊके और एलआर बाली के सकारात्मक अनुभव, तर्कशीलता व समर्पण ने उन्हें अम्बेडकरवाद का एक जुझारू सिपाही बना दिया। परिणामस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों की अठारह बड़ी शख्सियतों के साक्षात्कार से अस्तित्व में आई पुस्तक ‘अम्बेडकरवाद: विचारधारा और संघर्ष’ के आकर्षण ने मुझे इस पर चर्चा करने को प्रेरित किया।
वजह साफ है कि डा. अम्बेडकर का चिंतन-दर्शन और उनका आंदोलन जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक रहा है और आज भी है। जहां एक ओर इसके समर्थकों का संगठित आंदोलन निरंतर अपनी जमीन मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जातिवादी शक्तियां अपने सांप्रदायिक चरित्र का परिचय देने से बाज नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो डा. अम्बेडकर का नाम तक लेना भी प्रसव पीड़ी से अधिक तकलीफदेह हो जाता है कि वे इसकी डिलीवरी देश की संसद तक में कर डालते हैं और माहौल में चारों तरफ गंदगी फैला देते हैं। यह पीड़ा से मुक्ति पाने का उनका तरीका है; लेकिन हमें भी अपनी पीड़ा से मुक्ति के विकल्प निरंतर तलाश करते रहना है। यह विकल्प अम्बेडकरवाद में निहित है। यह ऐसा विषय है जिसके लिए हमें निरंतर परिस्थितियों का पोस्टमार्टम करते रहना है। मौजूदा पुस्तक पर बात करना भी इसी पोस्टमार्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है।
हमारे कुछ विद्वान साथी अम्बेडकरवाद को जातियों की परिधि तक सीमित मानकर अम्बेडकरवाद को परिभाषित करते हैं; लेकिन हमारा मानना है कि इसका फलक ग्लोबल है। इसलिए मैं इस आलेख को दो भागों में विभाजित कर चर्चा करना चाहता हूं।पहले भाग में मैं जाति, राजनीति आदि अन्य मुद्दे और दूसरे भाग में समसामयिक अम्बेडकरवाद से जुड़े मसलों को रखने का पक्षधर हूं। कहने की जरूरत नहीं कि भारत में ‘जाति’ एक ऐसा दैत्य है जो कदम-दर-कदम इंसानियत की बलि लेने को सदैव आतुर रहता है। सवाल उठता है कि इस दैत्य का जनक कौन है? ‘इसका सबसे सरल जवाब ब्राह्मणवाद है, जिसका मतलब है तर्कहीन होना। ब्राह्मणवाद का मतलब है वर्चस्व।’1
दुखद है कि आज इसकी परवरिश ब्राह्मणवाद ही नहीं कर रहा है बल्कि इससे पीडि़त अनुसूचित जातियां भी धड़ल्ले से कर रही हैं। इनकी संख्या 800 से अधिक है। मूल समस्या है...‘आप उन चमारों को भी को एकजुट नहीं कर सकते जो 60 से अधिक जातियों में विभाजित हैं। आप वाल्मीकियों को भी एकजुट नहीं कर सकते, जो लगभग 12 जातियों में विभाजित हैं।’2 ‘पंजाब में 40 से अधिक जातियां हैं। इनमें दो प्रमुख समुदाय चूहड़ा और चमार हैं, जो एक साथ नहीं आना चाहते।’3 इस दैत्य के विरुद्ध ‘आंदोलन के लिए आदर्शवाद महत्वपूर्ण है, व्यवहारिकता महत्वपूर्ण है। लेकिन जातियों के आधार पर आंदोलन नहीं हो सकता।’4 माना कि जातियां बनाना और उनका पोषण करना वर्णवादियों का काम है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछने और विचार करने का भी है- क्या जातियों की इतनी बड़ी संख्या वर्णवादियों ने बनाई हैं? इनकी संख्या बढ़ाने में हमारे बीच मौजूद जातिवाद जिम्मेदार नहीं है? क्या हम हमारे बीच मौजूद ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उस शिद्दत से लड़ रहे हैं, जिसकी दरकार हम सबसे है? मैं इस अपराध के पक्ष में खड़े होने का पक्षधर नहीं हूं और न ही इसके पक्ष में सहानुभूति का कोई तर्क जुटाने की स्थिति में हूं, खैर...।
ऐसी हालत में दूसरा विकल्प क्या? धर्मांतरण। वहां भी स्थिति अच्छी नहीं रही; आखिर क्यों? इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं- ‘गुरुद्वारे' चोर-चमार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कररहे हैं। मैंने सिख धर्म का अध्ययन करके पाया कि उनके दसों गुरु खत्री जाति के थे।सबने अपनी पैतृक जाति में विवाह किया।...वहां स्वीपर मज़हबी सिख हो जाता है।...आपने जाति को सामने के दरवाज़े से फेंका और वह खिड़की से वापस आ गई।’5 ‘जब अछूत बड़ी संख्या में धर्मांतरित होकर ईसाईबन चर्च आने लगे तो समस्या उठ खड़ी हुई। अंत में उसका समाधान यह निकालागया कि कश्मीरी गेट चर्च में दो प्रार्थना सभाएं होने लगीं- एक सुबह, एक दोपहर। सुबह उच्च जाति के लोग आते थे, दोपहर में अछूत।’6 हमारे चारों ओर ऐसे अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद हैं जो जातिवाद को बराबर जिंदा रखने की मुहिम का हिस्सा मात्र बनकर रह गए हैं। क्या हमें स्वयं से सवाल करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम किसी निदान के लिए आंदोलित है? निदान के विकल्प तो दूर, आज के सांप्रदायिक माहौल में किसी समस्या पर बात तक करने के कोई मायने ही नहीं रह गए हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में मुद्दा ईसाइयत और सिखीज्म से हटकर बुद्धिज्म पर केंद्रित है। लेकिन यहां भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में एडवोकेट भगवानदास सवाल उठाते हैं—‘महाराष्ट्र में महार ही ऐसे लोग थे जो बौद्ध बनने के लिए आगे आए, लेकिन उनको भी अपनी 12 जातियों से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए मेरा मोह भी भंग हो गया।’7 बात पुरानी है मगर यह बुद्धिज्म के सबसे सशक्त गढ़ और बाबा साहब के प्रबल समर्थकों की हकीकत का आईना है। क्या इस हकीकत से आंख मूंद कर हम किसी बुद्धवाद या अम्बेडकरवाद को अमली जामा पहना सकते हैं? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट भगवानदास ने स्वयं बाबा साहब से सवाल किया—‘मैं अछूत समुदाय से आता हूं इसलिए मैं एक बौद्ध विहार में प्रवेश नहीं कर सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म किसी भी अन्य धर्म से बेहतर है?...बाबा साहब ने कहा—‘आपने क्या किया है? इतिहास या दर्शन में एम ए?...मैंने कहा नहीं, फिर उन्होंने सवाल पूछा—‘कहां तक शिक्षा प्राप्त की है? मैंने कहा स्वशिक्षा। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताया और कहा—‘अब और नहीं, अब इतना ही।’8 खैर, भगवानदास ने बाबा साहब की वजह से बुद्धिज्म ग्रहण कर लिया। कहने की जरूरत नहीं है, आज भी लोग अपने विवेक की अपेक्षा बाबा साहब की वजह से बुद्धिज्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिस दिन लोग अपने विवेक के दम पर बुद्धिज्म में प्रवेश करेंगे, तस्वीर ही अनूठी होगी, खैर...। सवाल है, वर्तमान बुद्धिज्म की जरूरत क्या हैं? संभवत:यह क्षेत्र अभी भी बंजर जमीन की तरह उपेक्षित है; इसे बाबा साहब के अतिरिक्त, खुद के खून-पसीने की दरकार है।
यह बंजर जमीन जैसी उपेक्षा सोचने पर विवश करती है कि दीक्षा भूमि पर धर्मांतरण करने वाले लोग ‘व्यक्ति/नायक पूजा’ के कारण अधिक और बुद्धिज्म के प्रति अपनी समझ के कारण कम समर्पित थे। ‘उस दौरान दीक्षा भूमि पर तो बाबा साहब के नाम पर धर्मांतरण का ऐसा जुनून चढ़ा कि बाजार में सफेद कपड़ा खत्म हो गया और अंतत: घोषणा करनी पड़ी कि किसी भी रंग के कपड़े पहन कर आ सकते हैं।’9 इस जुनून की अति तो तब नजर आती है, जब ‘कई लोग तीन दिनों के लिए घर से खाना पैक करके चले थे। घर के बने हुए ज्वार के आटे की रोटी और एक-दो प्याज।’10 धर्मांतरण की इस मुहिम से आज एक आम राय बन रही है कि ‘आज बौद्ध आंदोलन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज की मदद कर रहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। सांस्कृतिक आंदोलन राजनीतिक दल की तुलना में अधिक परिवर्तन लाएगा।’11 निस्संदेह, लोगों का जुनून काबिल ए तारीफ है और इससे असहमत होने की कोई वजह नहीं है कि सांस्कृतिक आंदोलन राजनीतिक दल की तुलना में अधिक परिवर्तन लाएगा। लेकिन दीगर हकीकत यह भी है कि सांस्कृतिक आंदोलन को किसी नारेबाजी, व्यक्ति पूजा या किसी अंधभक्ति की सीमाओं से परे यथार्थपरक व अग्रगामी होना चाहिए। जाहिर है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी ठोस रूपरेखा की दरकार है। अवसरवादी जीवनशैली और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस मामले में सबसे बड़ी बाधा है।मौजूदा परिस्थिति में सवाल तो बनता है-इस बाधा से मुक्ति के बगैर बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद थोथे कारतूस से अधिक कुछ और हो सकता है क्या?
उद्देश्य के प्रति जुनून की जरूरत है, जिसका अभाव है। इसकी पूर्ति करने वाले भी हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन कितने? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उनके अद्वितीय योगदान का उल्लेख करना निस्संदेह उनके योगदान को सैल्यूट करना और अनुकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। मसलन-लंदन में बसे वीटी राजशेखर के बेटे ने अम्बेडकरवादी आंदोलन से दूर लंदन में उनके साथ रहने की जिद की तो उनका जवाब काबिल-ए-तारीफ है—‘लंदन मेरा देश नहीं है। वहां आकर मैं क्या करूंगा? मैं एक सुअर की तरह ही जीऊंगा, जिसे तुम खिला-खिला कर मोटा कर दोगे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं ऐसी बातों में।’12 इतना ही नहीं जब उन्हें राज्यसभा के लिए दो-तीन बार ऑफर मिला। विधान परिषद के लिए भी ऑफर मिला तो उन्होंने सभी को नामंजूर करते हुए कहा—‘एक बार आप राजनीति में प्रवेश करते हैं तो आप बौद्धिक तौर पर बेईमान हो जाते हैं।’13 मेरा आग्रह है कि अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए और मूल्यांकन कीजिए कि जो अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद का झंडा उठाए हैं, क्या आपको उनकी प्रतिछाया के रूप में उनका कोई अवसरवादी समानांतर ऐजेंडा हुंकार भरता नजर आता है। यदि उत्तर नहीं, तो ये शख्सियत अनुकरणीय हैं।अगर उत्तर हां है तो बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद का कोई भविष्य नहीं है; लेकिन ऐसे व्यक्ति विशेष का समाज के हितों का सौदा कर अवसरवादी निजी हित साधने का मार्ग अवश्य प्रशस्त हो सकता है। मौजूदा संदर्भ में आंदोलन के प्रति वीटी राजशेखर जैसी ईमानदारी को लेकर एलआर बाली जैसे अन्य कई बुद्धिजीवियों का समर्पण भी काबिल-ए-गौर है।
जहां तक समर्पण और सहयोग का सवाल है, सछूतों के सहयोग को नजरअंदाज करना नाइंसाफी होगी जो आज कल अछूतों की तरफ से भी बराबर होती नजर आती है। एक-इस कड़ी में स्कूल में दाखिले के लिए गए भगवानदास के विषय में प्रधानाचार्य से जुड़े घटनाक्रम को याद करना चाहता हूं। उन्होंने उनके पिता से कहा—‘मैंने इसकी जांच कर ली है, यह एक अच्छा लड़का है और काफी प्रगति करेगा।’ पिता ने कहा भगवान की मर्जी होगी तो जरूर पड़ेगा। इस पर प्रधानाचार्य ने उग्रता से कहा—‘भगवान क्या है? वह क्या करता है? उसने आपके लिए क्या किया है?’14 इस घटना ने भगवानदास के जीवन को नया दृष्टिकोण और नई दिशा प्रदान की।
दो-‘कृष्ण कुमार ने मुझे पेपर शुरू करने के लिए प्रेरित किया।वे दलित नहीं थे। वे खत्री यानी उच्च जाति, आर्यसमाज के अध्यक्ष, जूते और कपड़े के एक बड़े व्यापारी से संबंधित थे। उनके परिवार की कई दुकानें थी। उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने उर्दू में भीम पत्रिका शुरू की।’15
तीन-‘मुल्कराज आनंद ने मुझे सलाह दी कि मुझे एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए। उन्होंने ही पत्रिका का नाम ‘दलित वॉइस’ रखने को कहा। फिर उन्होंने कुछ शुरूआती पैसा दिया ताकि पत्रिका शुरू हो सके। उन्होंने अपने लेख भी देने का वायदा किया। इस प्रकार ‘दलित वॉइस’ पत्रिका शुरू हुई।’16 (वे खत्री यानी क्षत्रिय थे)
चार-‘कुमुद पावड़े को पता चला कि बाबा साहब संस्कृत को प्यार करते हैं मगर नहीं पढ़ पाए। बस मैंने संस्कृत पढ़ने का निर्णय ले लिया।...टॉप किया। एक ब्राह्मण अध्यापक ने मेरी मदद की और प्रोत्साहित किया।...बाद में उन्होंने अंग्रेजी में भी एमए किया।’17
जिस प्रकार जातिवादी समाज ‘जाति’ देखकर व्यक्ति योग्यता व चरित्र तय करता है, अछूत भी इसी प्रवृत्ति के शिकार हैं और दुखद है कि उनका भी व्यक्ति के विषय में राय बनाने का पैमाना ‘जाति’ हो गई है। जैसे सविता अम्बेडकर के बाबा साहब और अछूत समाज के प्रति समर्पित होने के बावजूद उसे तथाकथित अम्बेडकरवादियों के घृणित आरोपों से दो-चार होना पड़ा। ‘कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब को छाछ में जहर दे दिया। अन्य ने कहा कि वह उसे धीमा जहर दे रही थी। लोखंडे ने कहा कि उसने उन्हें तकिया से दबाकर मार डाला।...बहुत सारे षडयंत्रों के आरोप थे। क्या बाबा साहब इतने छोटे बच्चे थे कि उनको इस बात का पता नहीं था कि उनके लिए अच्छा और बुरा क्या है?’18 निष्कर्ष क्या निकलता है-‘हम अंतत: बाबा साहब को धोखा दे रहे थे। उन पर आरोप लगाने वाले यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डा. अम्बेडकर मूर्ख थे। उनके बीच कई साल से मधुर संबंध थे। मेरी बेटी उस पर एक किताब लिख चुकी है।’19
ये तथाकथित अम्बेडकरवादियों और बुद्धवादी हैं जो डा. अम्बेडकर को जानने और शिक्षित होने का दावा करते हैं। पाठक स्वयं ही तय करें कि ये महान विभूतियां बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जातिवादी हैं या जातिवादियों की जूठन का हक अदा करने वाले अंधभक्त हैं? जातिवाद को परखने के लिए मौजूदा पुस्तक के बहाने थोड़ा और आगे बढ़ते हैं-‘एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपने और उनके बीच के सभी पत्र दिखाए। वे बहुत लंबे पत्र थे। बाबा साहब का उनके लिए हर एक पत्र 18 से लेकर 20-25 पृष्ठों तक का है। वे एक साल से रिलेशनशिप में भी थे। उनके पास बाबा साहब के साथ किए गए पत्र व्यवहार का विशाल संग्रह था, जिसे उन्होंने मुझे दिखाया। वह इन्हें ‘मोतियों की माला’ कहती थीं। बाबा साहब के हाथ की लिखावट बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा, बस एक नजर देख लो, पढ़ो मत।’20
यह कैसा बुद्धवाद है, कैसा अम्बेडकरवाद है जो डा. अम्बेडकर को इंसान नहीं रोबोट के रूप में स्वीकार करता है और रोबोट की तरह ही ट्रीट करता है। वह मानने को तैयार नहीं है कि डा. अम्बेडकर भी इंसान थे और उनके अंदर इंसानी अच्छाइयां और बुराइयां भी अवश्य रही हैं; उनके अंदर एक दिल भी था और वह दिल मानवता के हित के अलावा किसी महिला के प्रेम के लिए भी धड़क सकता है। एक ही क्यूं कई महिलाओं के प्रति भी धड़क सकता है। बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद का तकाजा है कि वे डा. अम्बेडकर को नॉन-बायोलॉजिकल बनाने की कोशिश न करें। नहीं भूलना चाहिए कि नॉन-बायोलॉजिकल होने की शुरुआत बीसवीं सदी से नहीं इक्कीसवीं सदी से होती है; यही विश्वगुरु के दर्शन की पहचान है। बाबा साहब नॉन-बायोलॉजिकल नहीं सुपर इंटेलेक्चुयल थे। नहीं भूलना चाहिए कि इंटेलेक्चुयल के चिंतन-दर्शन में खामियां भी हो सकती हैं और उनके निराकरण भी हो सकते हैं। लेकिन नॉन-बायोलॉजिकल में न कभी कोई कमी थी, न कोई है और न ही कोई कमी हो सकती है; किसी निराकरण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, खैर...। बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद की विश्वसनीयता और बेहतरी के लिए अंधभक्ति से मुक्ति जरूरी है-कृपया बाबा साहब को सुपर इंटेलेक्चुयल ही बने रहने दें।
सत्य के तलाश की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं-‘बाद में ढाले जी के साथ मेरी चर्चा हुई और हमें लगा कि बाबा साहब उनकी वजह से ही अपना काम पूरा कर पाए। यह असंभव होता यदि वह सहयोग न करतीं। उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनके साथ थीं। वह बाबा साहब को धम्म दीक्षा लेने से रोक भी सकती थीं। आर्य वंश के भंते द्वारा दिल्ली के बिड़ला महाबोधि विहार में माई और बाबा साहब ने 2 मई 1950 को ही धम्म दीक्षा ले ली थी। भदंत आनंद कौसल्यायन ने भी इस दीक्षा के बारे में लिखा था।’21…‘सोहन लाल ने उनके बारे में लिखा कि वह एक नर्स थी। लेकिन सौभाग्य से मुझे मूल प्रमाण पत्र मिल गया। मेरे पास माई का मूल प्रमाण पत्र है। वह डाक्टर थी।’22 माई से संबंधित इस कड़ी में कुमुद पावड़े को जोड़ दें तो साक्षात्कार हमारे सामने एक अलग ही तस्वीर पेश करता है-‘आज हम जातीय शोषण के लिए मनुवादियों को तो गाली देते हैं, लेकिन जब महिलाओं का प्रश्न आता है तो हम स्वयं मनुवादी हो जाते हैं।’23 कहना जरूरी है-अपने अंदर के जातिवाद और मनुवाद से मुक्ति बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद के ढोल-नगाड़े बजाने से नहीं, इन्हें जीवन में तर्क-विवेक और अग्रगामी सोच के दम पर जीने से पाई जा सकती है। ये दोनों वाद राजनीति के अखाड़े से बाहर इंसानियत की पाठशाला की विषयवस्तु हैं जो हमें कबीर, रैदास, फुले, पेरियार आदि के चिंतन-दर्शन में अपनी विश्वसनीयता के साथ मौजूद हैं।
साक्षात्कार के जरिए हम जान पाते हैं कि सविता अम्बेडकर सिर्फ बाबा साहब तक सीमित नहीं थी वे आंदोलन में सहयोगी भी थी-‘हम दलित शब्द नहीं चाहते, लेकिन एक आंदोलन के रूप में हमें आज दलित पैंथर की जरूरत थी। माई साहब कहती थी कि इसे भंग मत करो। इसे अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए एक आक्रामक विंग की तरह रहने दें। उन्होंने भाषण में कहा, इसे तीन भागों में बनाएं-राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक। जो लोग रुचि रखते हैं, उन्हें इसका नेतृत्व करना चाहिए, ताकि इसके खिलाफ लड़ाई न हो। इसलिए लिए यदि ढाले की रुचि धर्म में है तो उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। रामदास की राजनीति में दिलचस्पी है, इसलिए उन्हें इसका नेतृत्व करना चाहिए। यह वास्तव में एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी सलाह थी।’24 कहने की जरूरत नहीं कि हमारे चारों ओर बुद्धिमानी की सलाह चारों ओर बिखरी पड़ी हैं लेकिन असली मसला सलाह को मानने का है, इसे ईमानदारी से अपने क्रियाकलापों में शामिल करने का है और ईमानदारी से जीने का है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या सविता अम्बेडकर की सलाह यह थी जिसके कीर्तिमान माननीय रामदास जी स्थापित कर रहे हैं?
माई के व्यक्तित्व की परख के बाद पुन: बाबा साहब पर लौटते हैं-‘यह दो बिल्डरों की कहानी थी, जो बाबा साहब को प्रभावित करना चाहते थे, जब वह वाइस राय की परिषद में श्रम मंत्री थे और सीपीडब्लूडी उनके अधीन था। यह कुछ अनुबंध से संबंधित था और यशवंत दिल्ली आए थे। जैसे ही बाबा साहब को इस बारे में पता चला वह आग बबूला हो गए। उन्होंने यशवंत को तुरंत मुंबई के लिए रवाना होने को कह दिया। कहा कि उसे दिल्ली आने की जरूरत नहीं।’25 इसके विपरीत वर्तमान साक्षात्कार की पुस्तक में भरपूर सामग्री उपलब्ध है जो बताती है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन किस प्रकार दोगलेपन का शिकार रहा है। एक-‘मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो जीवन में आगे बढ़े लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कोई दलित आगे बढ़ जाता है, ब्राह्मण उसे खरीद लेता है।’26 दो-जमना दास ने बाबा साहब से कहा, हम छात्रवृत्ति के लिए चिंतित हैं। उनका जवाब था—‘हम कैसे आलसी छात्र हो गए हैं और अध्ययन के लिए अनिच्छुक हैं और कड़ी मेहनत से बचते हैं। सुविधाओं के बावजूद हम परीक्षाओं में अच्छी तरह से पास नहीं हो रहे हैं।’27 उपरोक्त की रोशनी में मेरे दिमाग में एक सवाल दस्तक देता है-क्या हमारा वर्तमान बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद ऐसे आदर्श की किसी जमीन पर खड़ा है? अगर नहीं तो क्यों? अगर हां, तो कहां है?
मौजूदा क्रम में मुझे लगता है कि साक्षात्कार के माध्यम से बाबा साहब की राजनीतिक दृष्टि को लेकर जो घालमेल नजर आती है, उसे समझा जाए। गौरतलब है कि किसी भी विचार को यदि उसके संदर्भ से काट दिया जाए तो अर्थ के अनर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। बाबा साहब ने अपने भाषण में कई मौकों पर कहा—‘हम सभी ने सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की तुलना में राजनीति को अधिक महत्व दिया है।’28 इसी कड़ी में एक दोस्त के बेटे के नेता बनने के संबंध में ढाले कहते हैं—‘नेता बनने के बारे में मत सोचो, सिर्फ एक अच्छा वकील बनने पर ध्यान दो।...दलितों के पास अच्छे वकील नहीं हैं।’29 लेकिन ‘जब बाबा साहब कहते हैं, राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है, इसे गलत समझा गया। जब वे यह बोल रहे थे तो एक राजनेता के रूप एससीएफ की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।’30 कहने का मतलब है कि हमें बाबा साहब के विचारों को समय और परिस्थितियों की रोशनी में समझने की जरूरत है। अर्थ को अनर्थ नहीं होने देना है, लेकिन हो क्या रहा है-जरा इसका उत्तर बाहर तलाशने से पहले, अपने अंदर भी तलाश करने का साहस दिखाएं। यह अम्बेडकरवाद के लिए संजीवनी जैसा कृत्य होगा।
जो अम्बेडकरवादी बाबा साहब को जातियों की दीवारों में कैद करने की मुहिम चलाए हैं, उन्हें समझने की जरूरत है-‘आजादी के बाद डा. अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की शुरूआत की, जो केवल अनुसूचित जाति के लोगों की नहीं थी। उनके पास अन्य जातियों के कई लोग थे। वह आधार को व्यापक बनाना चाहते थे और भारत की उन्नति के लिए आर्थिक और सामाजिक कारणों को शामिल करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने आरपीआई का नेतृत्व संभाला, वे उन्हें समझ नहीं पाए या उन्होंने बाबा साहेब के पीछे चलने की कोशिश नहीं की। इसलिए बाबा साहेब ने आरपीआई को एक अन्य अनुसूचित जाति संगठन में बदल दिया और फिर यह जाति और राज्य की सीमाओं पर विभाजित हो गया। आज हमारे पास आरपीआई के तीन भाग हैं, लेकिन वे कहीं नहीं पहुँचे।’31 यदि इस मसले को राजनीति की दीवारों में कैद कर दिया जाता है तो नाइंसाफी होगी। मेरा मानना है दलित साहित्य की नेतृत्वकारी महान शक्तियों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तभी यह जातिवाद के अंधेरे कुएं से मुक्ति पाकर वैश्विकता के समुद्र में गोते लगाने जैसा व्यापक उपक्रम हो सकता है और यह साहित्य वैश्विक नागरिकता के लिए सुपात्र होकर बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।
मौजूदा संदर्भ में यह भी समझने की जरूरत है-अपने अंतिम दिनों में बाबा साहब सभी महत्वपूर्ण नेताओं को साथ लाकर एक गैर-कांग्रेस, गैर-कम्युनिस्ट पार्टी बनाने पर विचार कर रहे थे। उन्होंने इसके संबंध में राम मनोहर लोहिया और एसएम जोशी जैसे समाजवादी नेताओं को प्रस्ताव भी भेजा था। इस प्रस्ताव प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन नागपुर के बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आयोजित धर्मांतरण समारोह के दौरान बाबा साहब ने एक नई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के बारे में चर्चा की थी। चूंकि 1957 के आम चुनाव नजदीक थे, इसलिए अम्बेडकर के बाद एससीएफ के नेतृत्व ने इसके बारे में निर्णय को भविष्य के लिए टाल दिया और सुरक्षित क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि वह हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना चुके थे और अब अनुसूचित जाति में शामिल नहीं थे। नेतृत्व के सवाल को हल करने के लिए सात सदस्यीय प्रेसिडियम का निर्माण किया गया, लेकिन यह जल्द ही यह टूट गया।’32 उपरोक्त टिप्पणी हमें आत्ममंथन को प्रेरित करती है कि धर्मांतरण के बाद राजनीतिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत क्यों हुई और आज के वर्तमान राजनीतिक अराजकता के चलते कौन से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जो शोषित-उत्पीडि़त समाज के हितों की रक्षा और उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।
साक्षात्कार के माध्यम से हमारे सामने बाबा साहब की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हो जाती है। ‘मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि बाबा साहब ने आरपीआईं की परिकल्पना में धर्मनिरपेक्षता को शामिल रखा था कि नहीं। धर्मनिरपेक्षता आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुरुपयोग में लाई जाने वाली अवधारणा है जिसे तथाकथित प्रगतिशीलों ने प्रचारित किया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आरपीआई की कल्पना प्रभुत्वशाली कांग्रेस के विरोध में खड़ी की गई थी।’…नवम्बर 1948 में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रो. केटी शाह ने एक संशोधन पेश किया था जिसमें कहा गया था कि 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष,समाजवादी राज्यों का संघ है।' स्वयं बाबा साहब ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि संविधान केवल राज्य के विभिन्न अंगों के कार्यों को नियमित करने की एक व्यवस्था थी और राज्य की नीति क्या होगी अथवा यह अपने आर्थिक तथा सामाजिक पक्षों को किस प्रकार व्यवस्थित करेगी, इसका निर्णय समय व परिस्थितियों के अनुरूप जनता के द्वारा किया जाना चाहिए।’33
गौरतलब है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें तय करना है कि कौन-सी पार्टी से दूरी बनानी है और कौन-सी पार्टी से नजदीकियां। मौजूदा संदर्भ में मेरा मानना है कि आज राजनीतिक पार्टियों की संख्या और उनके चारित्रिक पतन का पैमाना बदला है। इसलिए बाबा साहब के उनके समय के किसी भी आंकलन को आज के संदर्भ में अक्षरश: लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों के गहन अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर रणनीति बनाने की जरूरत हैं। यह साहित्य की जिम्मेदारी है कि वह राजनीति की दिशा और दशा के विषय में अपनी राय साझा करे, न कि खुद को गैर-राजनीतिक होने के टैग के साथ उदासीन बना ले।
इस कड़ी में महसूस हो रहा है कि साक्षात्कार के माध्यम से कांशीराम को अम्बेडकरवाद की रोशनी में परखा जाए। ‘बामसेफ वास्तव में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ था। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय नहीं थे और बामसेफ में शामिल होने वाले अधिकतर कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे। दुर्भाग्य से कांशीराम को भारत के समाजशास्त्र और राजनीति की बहुत समझ नहीं है। और उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और आरपीआई की विफलता के कारण पैदा हुए खालीपन का लाभ उठाया।...उन्होंने अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल किया था।’34 ‘बाबा साहब ने जाति के विश्लेषण के संबंध में जो कुछ लिखा था, उसका ठीक उल्टा कांशीराम ने अपनाया। जाति पर सवाल उठाने की बजाय, वह प्रत्येक जाति के एक टोकन व्यक्ति को ढूंढना चाहता था और विज्ञापन अभियानों में निवेश करता था। वे उसे बहुत नहीं पढ़ते थे, केवल उनके नाम का प्रयोग कर रहे थे।’35 यहां सवाल आग में घी डालने का नहीं, बल्कि परिस्थितियों के मूल्यांकन औरपुनर्मूल्यांकन की मांग की पूर्ति करना और भावी दिशा तय करने का है, इसलिए इसे अंधानुकरण की विषय वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए और पुनर्विचार की अनिवार्य सामग्री के रूप में अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है।
जहां तक आरपीआई का प्रश्न है-‘आज आरपीआई के 100 से अधिक समूह हैं। सब कुछ अवसरवादी हो गया है। उनके अनुसार नहीं चल रहा है। उन्हें एकजुट होना होगा। रिडिल्स के आंदोलन के दौरान, सभी लोग एकजुट हो गए। वे एक साथ रिडिल्स पर प्रतिबंध के खिलाफ लड़ रहे थे। मैंने कांशीराम को यह कहते हुए सुना कि तुम किसी की भी पूजा करो, लेकिन हमें वोट दो। मैंने इसे जबलपुर में सुना था जो मुझे पसंद नहीं आया।’36 हमें नहीं मालूम कि इस स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है लेकिन वर्तमान राजनीति मांग करती है कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता पाने के लिए अपने उन मूल्यों को तिलांजलि दे देनी चाहिए जिनके दम पर वे राजनीति में प्रवेश कर पाए। वर्तमान दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के वैचारिक और व्यवहारिक पतन के कारण जो परिणाम आए हैं, क्या उसे बसपा के पतन की वर्तमान दास्तान के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? हम मानते हैं कि इतना सहज निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए लेकिन जरूरत पार्टी के संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय व वैश्विक हितों के मद्देनजर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नैतिकता का इतना पतन नहीं होना चाहिए जितना आज हो रहा है। क्या राजनीति का मतलब नैतिक मूल्यों से शून्य हो जाना है? हम ऐसा नहीं मानते, क्या आप मानते हैं?
अधिकतर अम्बेडकरवादी मार्क्सवाद को ब्राह्मणवाद के बरअक्स रखकर इसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं लेकिन साक्षात्कार की यह पुस्तक कुछ अलग ही तस्वीर पेश करती है-‘बाबा साहब मार्क्सवाद के विरोधी दार्शनिक नहीं थे, लेकिन वे हठधर्मी लोगों के खिलाफ थे क्योंकि डांगे जैसे व्यक्ति साम्यवाद के बारे में लिखने वाले ज्यादातर लोग समाज के ऊपरी हिस्सों से थे और जाति से ब्राह्मण।...उन्होंने मार्क्सवाद का गंभीरता से अध्ययन किया। उनका झुकाव प्रगतिशील सोच की तरफ था।’37 लेकिन तब ‘बंगाल में समस्या यह थी कि गरीब केवल गरीब ‘वर्ग’ के रूप में गरीब हैं, न कि जाति के रूप में। वे ‘जाति के प्रसंग को समझदारी से अनदेखा करते हैं जैसे कि समाज में उसकी कोई भूमिका नहीं है।’38 ‘दलितों को अपनी जाति और पंथ के बावजूद, वाम आंदोलनों का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन व्यवहार में यह उल्टा था।’39 अम्बेडकर ने रिपब्लिकन की परिकल्पना कांग्रेस विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी संगठन के रूप में की थी, जाति की बात करने वाली पार्टी के रूप में नहीं।’40 यहां सवाल वैचारिक प्रतिबद्धता का है। बाबा साहब राजनीतिक पार्टी को जाति की बात करने तक सीमित नहीं मानते थे। क्या बाबा साहब का नाम लेकर राजनीतिक करने वाली हमारी पार्टियां उनके साथ उनकी वैचारिकी के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आप सहमत है-बाबा साहब को अवसरवादी नेताओं द्वारा चुनाव जीतने की सीढ़ी बनाने वाले समाज और राष्ट्र के मीत नहीं, सिर्फ दुश्मन हो सकते हैं।
सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है-‘कम्युनिस्ट मानते थे कि अम्बेडकर मजदूर वर्ग को विभाजित कर रहे हैं जबकि अम्बेडकर कम्युनिष्टों की आलोचना करते थे कि वह जाति आधारित भेदभाव को महत्व नहीं देते थे और उनके करीब रहने वाले दलित भी प्रताड़ना के शिकार थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट आधारभूत संरचना और उसकी बाहरी अभिव्यक्ति यानी बेस सुपर-स्ट्रक्चर के बारे में मार्क्सवादी विचार के बारे में सतही समझ रखते थे जिसके कारण वे मानते थे कि केवल जाति के खिलाफ संघर्ष से कुछ फायदा नहीं होगा।’41…‘ऐतिहासिक रूप से अम्बेडकर कम्युनिस्टों से आहत थे खासकर इसलिए कि उन्होंने 1952 के चुनावों में अम्बेडकर को हराया था। इसके बावजूद यह भी एक तथ्य था कि कांग्रेस से काफी पीछे होने के बावजूद कम्युनिस्ट उस समय की प्रमुख विरोधी पाटी थी।’42 गौरतलब है-निराशा के दौर में बाबा साहब ने गायकवाड़ को एक नोट भेजा था जो उनके छपे हुए संकलन में शामिल है। इस नोट में उन्होंने लिखा है-‘उन्हें लगता है कि उनके तरीके काम नहीं कर रहे और अगर साम्यवाद से दलितों को तत्काल राहत मिलती है तो उन्हें कम्युनिस्ट बन जाना चाहिए।’43 बाबा साहब का अंधानुकरण करने वाले महान चिंतकों को सोचने की जरूरत हैं कि कोई भी विचार, संस्था व विचारधारा सदैव एक तराजू पर नहीं तोले जा सकते। उन्हें समय, काल और परिस्थिति के अनुकूल विश्लेषण करने और उपयुक्त निर्णय लेने की जरूरत होती है। इस कसौटी के तहत कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी और कांग्रेसी सदैव दुश्मन नहीं, कभी मीत भी हो सकते हैं। जरूरत उपयुक्त मूल्यांकन की है, खैर...कोई भी पूर्णरूपेण सही या गलत नहीं होता।
जैसाकि पहले उल्लिखित है कि आलेख के दूसरे भाग में हम समसामयिक अम्बेडकरवाद से जुड़े मसलों पर बात करेंगे। इस कड़ी में कहना चाहता हूं कि आज अम्बेडकरवाद की साख दांव पर है। एक प्रकार से इसका हिंदूकरण जैसा कुछ हो गया है। इसकी शुरुआत 1960 से ही हो जाती है। मसलन-‘1960 के मध्य में अम्बेडकर के अंतिम संस्कार के स्थान पर एक स्मारक बनवाने के लिए पैसे जमा करने के वास्ते उनके बेटे को महू से लेकर मुम्बई तक पदयात्रा निकालनी पड़ी थी। अब इसी अम्बेडकर का स्मारक बनवाने की होड़ लग चुकी थी। भोली दलित जनता को शासक वर्ग के तिकड़म का कोई अंदाजा नहीं था और वे तेजी से इसके शिकार होने लगे। एक भयानक दुष्चक्र की शुरुआत हो गईं।’