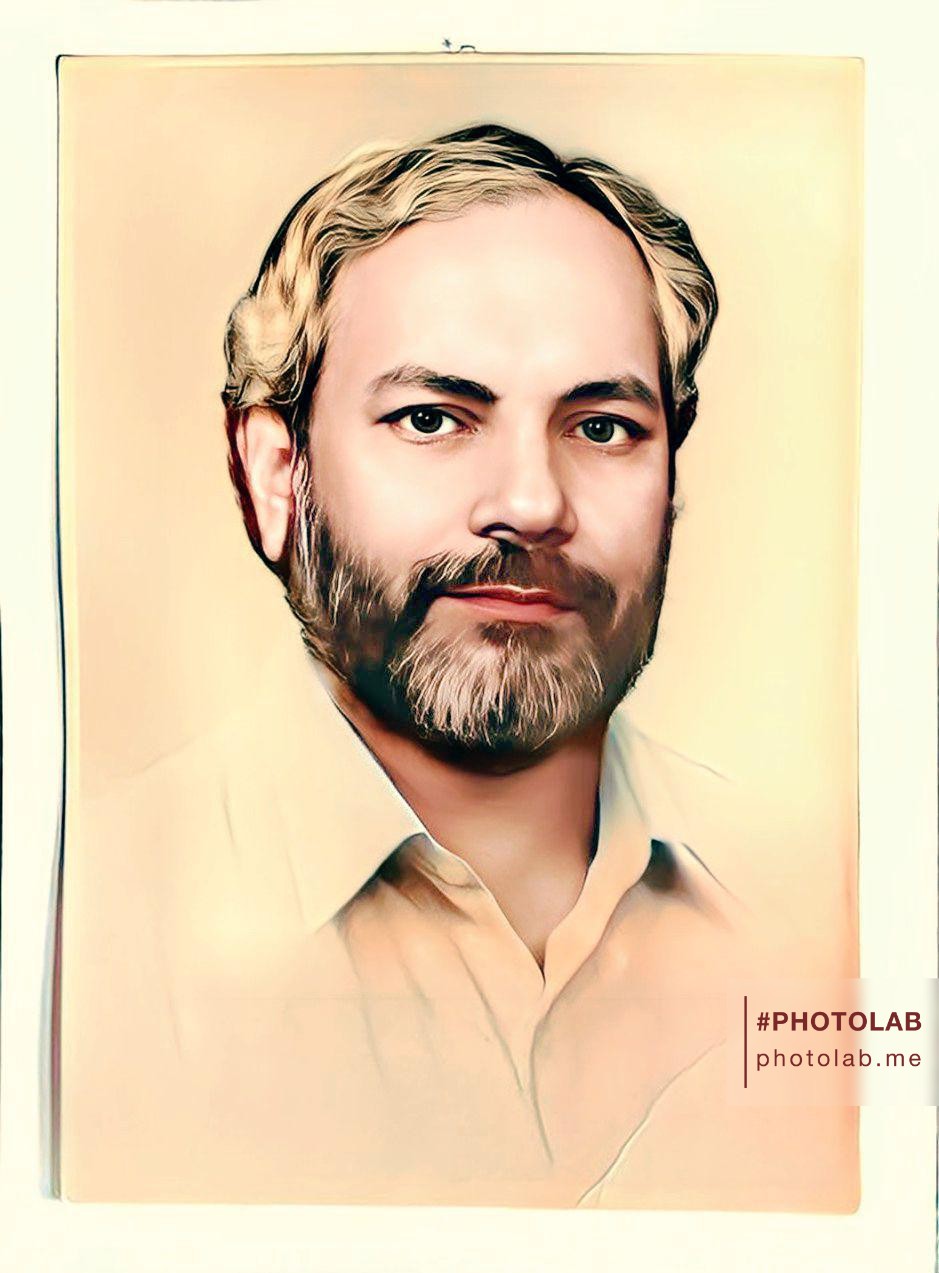मंंथन
मेरी अपनी रचना-प्रक्रिया
-तेजपाल सिंह 'तेज
कहा जाता है कि साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का सजीव होना जैसे संभव ही नहीं है। साहित्यकार का कर्म होना चाहिए कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व-बंधुत्व और सद्भाव के साथ हाशिये के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। यह तब ही संभव है जब कि साहित्यकार अपने जीवन व अपने परिवेश का हृदय से अवलोकन करे। यानी जीवन ही साहित्य का आधार है।
साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। यदि साहित्य समाज के लिए उपयोगी नहीं तो किसी को भी ग्राह्य नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। साहित्यकार के अंतस में युग-चेतना होती है और यही चेतना साहित्य सृजन का आधार बनती है। साहित्य की महत्ता को आँकने के लिए आत्मसंतुष्टि अथवा सुखानुभूति काफी नहीं, सहित्य में प्रेरणा या संदेश या जागृति का होना आवश्यक है। संवेदना ही एक ऐसी चीज है, जो साहित्य और समाज को जोड़ती है। संवेदनहीन साहित्य समाज को या तो नकारात्मक सोच के चूल्हे में झोंक देगा या फिर नापाक मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह जाएगा। ऐसे में साहित्य को जीवित रखना संभव नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि सहित्य सीमाबंदी नहीं की जा सकती। स्वतंत्र साहित्य ही साहित्य की व्यापक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब देखना यह है कि मेरा साहित्य किस करवट बैठता है। मैरा प्रयास रहा है कि मैं अपने देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने साहित्य कर्म को गति प्रदान की है । मेरे साहित्य पर दृश्टिपात करने से पूर्व मेरी रचना प्रक्रिया और रचना धर्मिता को जानना जरूरी है। अत: शुरुआत भी इस क्रम में की है।
मेरा जन्म एक अकृषक परिवार में सन 1949 में बुलन्दशहर उ.प्र.) के एक छोटे से गाँब अला बास बातरी में तब हुआ, जब भारत का संविधान रचा जा रहा था। दरअसल मैं बचपन से ही तमाम सामाजिक और पारिवारिक झंझावतों को झेलते हुए आगे बढ़ा हूँ।
मुझे गहरे से और ज्यादा जानने के भाव से यह उचित ही होगा कि मैं यहाँ उस वाकिये को भी जोड़ दूँ कि जब मैं भारतीय स्टेट बैंक में सहायक प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के प्रशिक्षण केंद्र आगरा में प्रशिक्षणार्थ गया हुआ था। प्रशिक्षिक माननीय राजेन्द्र कुमार जी थे। उन्होंने प्रशिणार्थियों से अपने और अपने बच्चों के विकास के विषय में कई सवाल किए। कुछ—कुछ अपनी रुचि के, कुछ प्रिशिक्षण प्राप्त करने वालों के। ज्यादातर ने परंपरागत मान्यताओं के हिसाब से ही उत्तर दिए । मैंने शांति से सबको सुना। अब ! राजेंद्र सर ने मेरी ओर उंगली उठा दी। यानी कि अब मेरी बारी थी। मैंने अपनी बात शुरु करने से पहले राजेन्द्र सर से कहा कि मुझ से पूर्व जिन-जिन भी प्रशिक्षणार्थी ने जो कुछ भी कहा, मेरी समझ से इसलिए परे है क्योंकि उन्होंने किस-किस आधार पर अपने विचार व्यक्त किए, उनका किसी ने भी खुलासा नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि अपनी बात आपके सामने अपने अन्दाज में रखूँ। राजेन्द सर ने बिना किसी हिचक के मुझे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान कर दी।
मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिभाषा देश, काल और परिस्थिति पर आधारित होती है। देश, काल और परिस्थिति को नकार कर जीवन की परिभाषा की ही नहीं जा सकती। फिर भी यदि कोई करता है तो वह शंका से परे नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं नितांत ग्रामीण हूँ। अकृषक परिवार से ही नहीं, अपितु एक दलित वर्ग के परिवार से भी हूँ। लगभग डेढ़ वर्ष की अल्पायु में मेरे पिता का देहांत हो गया था। सातवीं कक्षा में आते-आते माता का देहांत भी हो गया। आगे का भार बड़े भाई डालचन्द ने उठाया। मगर प्रथम श्रेणी में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद, मेरे बड़े भाई ने मुझे आगे पढ़ाने से हाथ खींच लिया। ये मेरे लिए एक त्रासदी से कम नहीं था। दिमाग का भी इतना विकास न था कि मैं आगे-पीछे का कुछ भी सोच सकूँ। ऐसे में निराशा की चादर समेटे, मैं अपने बहनोई माननीय श्रीराम के पास नौकरी पाने की लालसा से गया। उन्होंने कहा कि मैं चहाता हूँ कि तू आगे की पढ़ाई कर, इसके लिए जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं करूँगा। नौकरी तो मैं लगवा ही दूँगा। मैं उजास कम, हताशा कुछ ज्यादा लेकर अपने गाँव वापिस आ गया। सोचा, क्यों न पढ़ाई खुद ही कर लूँ? संसाधन तो न के बराबर थे ही । फिर भी मैंने जैसे-तैसे ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला ले लिया। इस पर भाई ने कुछ नाराजगी भी जाहिर की क्योंकि वो मेरी शादी कराकर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेना चाहते थे। किंतु मैं अपनी बात पर अडिग रहा और जैसे-तैसे मेहनत-मजदूरी करते हुए स्वतंत्र भारत इंटर कालेज, भवन बहादुर नगर, (बुलन्दशहर) उ.प्र. के प्रधानाध्यापक माननीय रामाश्रय शर्मा एवं अन्य ब्राह्मण अध्यापकों द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता के बल पर उत्तीर्ण की। वह भी प्रथम श्रेणी में। वस्तुत: सच तो ये है कि मैं दलित परिवार से होते हुए भी, ब्राह्मण अध्यापकों का घना चहेता रहा। कारण चाहे जो भी रहे हों।
बारहवीं करने के उपरांत, मैं 1969 में ही नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद, दिल्ली में रुके रहने के लिए मैंने जाने क्या-क्या न किया। अंतत: तीन-चार सरकारी नौकरी छोड़कर मैं अप्रैल 1974 को भारतीय स्टेट बैंक में बतौर टंकक-लिपिक भर्ती हो गया। अब दुविधा ये थी कि जिस शाखा मैं भर्ती हुआ था, उसमें मेरे साथ भर्ती हुए सभी कर्मचारी स्नातक या फिर स्तानकोत्तर थे। मैं केवल बारहवीं पास था। मेरे शैक्षिक स्तर को लेकर वो आपस में कुछ न कुछ अप्रिय बातें करने से बाज नहीं आते थे। उनकी ऊल-जलूल बातों का मुझे ये लाभ मिला कि 1975 में मैंने स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरठ यूनिवर्सिटी (अब : चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी) से पत्राचार पद्धति के तहत जरिए 1977 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। और अब मैं आपके एक अधिकारी के रूप में उपस्थित हूँ। तदंतर मैंने राजेन्द्र सर से ही सवाल कर दिया कि अब आप ही मेरे जीवन की परिभाषा तय करलें। उन्होंने और मेरे साथियों ने बड़े ही धर्य से मेरी बातें सुनीं। सभी प्रशिणार्थी शांत थे । राजेन्द्र सर भी। किंतु उन्होंने प्रत्युत्तर में, जीवन की परिभाषा तय करने का भार मुझ पर ही डाल दिया।
मैंने बिना कुछ देरी किए, उत्सुकता-वश सहज भाव से कहा कि महोदय! मुझे तो ‘जीवन’ संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं लगता। शेष आप स्वयं तय करें कि मेरी परिस्थितियों के अनुरूप आप जीवन को क्या संज्ञा प्रदान करेंगे। वे कुछ पल चुप रहे और अचानक तालियाँ बजाने लगे।…… बहुत खूब …..बहुत खूब। उनका इतना कहना था कि सभी प्रशिणार्थी भी तालियाँ बजाने लगे। ….. और सत्र के अंत तक मैं चर्चा का विषय बना रहा।
अपनी “रचना प्रक्रिया के विषय में कुछ लिखने से पूर्व यथोक्त सत्य व्यक्त करना, मैंने इसलिए आवश्यक समझा, क्योंकि किसी भी रचनाकार का परिवेश अक्सर उसकी रचना का किसी न किसी रूप में एक अभिन्न अंग होता है। या यूँ कहा जा सकता है कि किसी भी रचनाकार की रचना उसके परिवेश अक्सर किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। यह सत्य मेरी रचनाओं में उजागर होता है। है।
मैंने अपर्युक्त में दसवीं कक्षा पास करने के उपरांत अपने बड़े भाई के नकारात्मक व्यवहार का उल्लेख किया है। यह भी कहा है कि खुद मेहनत-मजदूरी करके बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की। दरअसल, मेरे बड़े भाई हेंड-पंप लगाने का कार्य करते थे। घरेलू काम होने के नाते, मैंने भी दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत हेंड-पंप लगाने का कार्य करना शुरू कर दिया। इसके चलते, मैंने अपने बलबूते पर ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला ले लिया था। ग्यारहवीं कक्षा के दिनों में इसी कारण से, मैं कालिज से अक्सर गायब रहने लगा। यह 1967 की बात है। उस समय एक हेंड-पंप लगाने के लगभग 40-45 रुपए मिल जाया करते थे। वह भी एक-दो दिन में। इसके साथ-साथ एक राज़ और खोलना जरूरी है कि मुझे देहाती गाने गाने का बड़ा ही शौक था। कोई ही ऐसा दिन जाता होगा, जब गाँव के लोग हमारी बैठक (दुकड़िया) पर गाना सुनने के लिए न आते हों। यहाँ यह पुन: उल्लेख करना जरूरी है कि यह संयोग ही था कि मैं रागनी गाने में रुचि रखता था। बस! इसी लगन ने मुझे रागनी लिखने की ओर भी खींच लिया।
गौरतलब है कि साठ-सत्तर के दशक में लिखी जाने वाली ज्यादातर रागनियाँ ऐतिहासिक किस्सों / कहानियों पर आधारित होती थीं, किंतु मैंने अपने एक साथी “संतराम प्रेमी” के साथ मिलकर रागनियों को आम –आदमी की समस्याओं से जोड़कर आगे का रास्ता तय करना मंजूर किया। वह ऐसा समय था कि जब मुझे “रचना धर्मिता” जैसे विषयों के बारे में सोचने का ज्ञान तक नहीं था। इस बीच मैंने और मेरे साथी संतराम प्रेमी ने आठ पेजी चार पुस्तिकाओं का प्रकाशन कर बुलन्दशहर के स्याना कस्बे में अवस्थित ‘ओम-शरण पुस्तक भंडार’ नामक पुस्तक विक्रेता को छपाई की लागत से करीब पाँच गुनी कीमत में बेच दी जाती थी। उस समय यह कार्य निसंदेह मेरी आजीवका का हिस्सा था। जब मैं 1969 में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करके दिल्ली आया तो दिल्ली में रुके रहने और नौकरी की तलाश में बने रहने के लिए मैने गोल मार्किट की बेयर्ड रोड पर स्थित “ओनिलको कैमिस्ट” नामक एक दुकान पर केवल दो रुपए रोज के वेतन पर कार्य किया। रविवार के पैसे कटते थे।
दिल्ली में आने के बाद सन 1971 में मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (डी.टी.यू.) में दैनिक दिहाड़ी पर संवाहक के पद पर नियुक्त हुआ। इस बीच मेरा लेखन कार्य अवरुद्ध ही रहा। कारण था, सुबह-शाम शिफ्ट में काम करना। वह भी केवल चार रुपए रोजाना। कभी काम मिला, कभी नहीं। इसी दौरान मुझे एक ऐसी ड्यूटी मिल गई जो सुबह के ही दस बजे समाप्त हो जाती थी। या फिर कभी दिन में नौकरी करता तो शाम खाली। रात को काम करता तो दिन खाली। इस खाली समय की भरपाई के लिए मैंने ईस्ट पटेल नगर स्थित “दिल्ली पब्लिक लायबरेरी की सदस्यता हासिल करली और लिखने-पढ़्ने की कुलबुलाहट के कारण अब मेरा खाली समय वहाँ गुजरने लगा। वहाँ अलग-अलग विधाओं की पुस्तकों का असीम भंडार था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक महसूस हो रहा है कि मैंने कालिज के समय में नाटक और उपन्यास खूब पढ़े थे। किंतु दिल्ली पब्लिक लायबरेरी की सदस्यता हासिल करने के बाद धीरे-धीरे मेरा ध्यान गद्य साहित्य से जैसे हटता चला गया। फलत: अब मैं नाटक और उपन्यास जैसी विधाओं की पुस्तकें पढ़ने से कटने लगा था। बदले में देवनागरी लिपी में छपी उर्दू और हिन्दी की ग़ज़लों/कविताओं की पुस्तकें पड़ने लगा था। मीर, गालिब और न जाने कितने ही शायरों की किताबें ज्यादा पढ़ने लगा। वह भी कई-कई बार। अब मैं उर्दूदां तो था नहीं, अत: शब्दार्थों के जरिए शायरी समझने का निरंतर प्रयास करता था। बस यहीं से मैं गद्य साहित्य व देहाती गानों/रागनियों से इतर शायरी ने जैसे मुझे ठग लिया। अब मैं ग़ज़ल और मुक्तक लिखने की ओर अग्रसर होने लगा था। और ग़ज़लों के अलावा अब मुझे केवल कविता ही लुभा पाती थी। गद्य से जैसे नाता लगभग टूट ही गया था। ग़ज़ल पढ़-पढ़कर मुझे लगा कि ‘ग़ज़ल’ ही एक मात्र ऐसी विधा है जिसकी दो पंक्तियों मात्र में बहुत सारा अर्थ भरा जा सकता है। इस काव्यात्मक विधा ने मुझसे मुझे छीन लिया और स्वयं मुझमें समा गई। निरंतर पठन-पाठन से मेरा रुझान गद्य से हटकर पद्य — वह भी शायरी की ओर चला गया। परंपरागत ग़ज़ल जहाँ सुरा और सुन्दरी के दामन से गुजरने के बाद हवा पा पाती थी, वहीं आज की हिन्दी ग़ज़ल आम आदमी के दुख दर्द की आवाज़ बन गई है, यह सब “दुश्यंत” के “साये में धूप के” पढ़ने के बाद ही जाना। और जब मेरी कलम आज की ग़ज़ल की ओर चली तो ठीक दुश्यंत की तरह ही मेरी कलम भी अक्सर कड़वा और सियासी जामा पहनकर संघर्षों के साथ निर्माण तलाशने लगी।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (डी.टी.यू.) में नौकरी करने के दौरान मेरा परिचय उस समय के जाने-माने ग़ज़लकार महेश चन्द ‘नक्ष’ से हुआ। गौरतलब है कि महेश चन्द ‘नक्ष’ भी डी.टी.यू. में ही सर्विस करते थे। मैंने उनकी ग़ज़लें बहुत बार आल इंडिया रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सुनी थीं। अब क्या था, मैं उनसे कुछ सीखने के आश्य से उनके बराबर संपर्क में रहने लगा। किंतु हाथ कुछ भी न लगा। वे चाय-पानी तो खूब और बड़े प्यार से पिलाते थे किंतु शायरी को नाकारा और आवारा लोगों का शौक बताकर मुझे पटरी से उतार देते थे। उनके ऐसे कहने पर मेरे मन में आता था कि मैं उनसे कभी पूछ कर देखूँ कि यदि शायरी नाकारा और आवारा लोगों का शौक है तो फिर आप क्यों शायरी से नाता क्यों जोड़े हुए हैं। किंतु उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं होता था। वैसे भी वो डी. टी. यू. में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और मैं एक अदना सा संवाहक, वह भी दैनिक दिहाड़ी वाला अस्थाई कर्मचारी। खैर! अंतत: उनसे मिलना-जुलना ही छोड़ दिया और जो भी जैसा भी मन में आया, लिखता रहा।
एक और कड़बा सच है कि दिल्ली आने के बाद, भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों/ विकृतियों/ सामाजिक भेदभाव/ राजनैतिक भ्रष्टाचार/ गरीब और निरीह तबके के प्रति राजनीतिक / प्रशासजिक उपेक्षा/ जाँति-पाँति और आर्थिक व श्रृमिक शोषण, धार्मिक पाखंडवाद जैसी जाने कितनी ही सामाजिक बुराईयों से साक्षात्कार हुआ। अब वक्त की आवाज़ से जैसे मेरा परिचय हो गया था। पद्य लिखने के मेरे शौक में आम आदमी दुख-दर्द पहले से ही शामिल था, सो आम आदमी का दुख-दर्द अब मेरी ग़ज़लों और कविताओं का खास विषय बनकर मुखर हो गया ।
यहाँ यह कहना ग़लत नहीं होगा कि प्रत्येक रचनाकार छपना तो चाहता ही है। मैं भी चाहता था किंतु अपनी शर्तों पर। जैसा मैंने लिखा है, वैसा छापना है तो छापो, अन्यथा कोई बात नहीं। तुम अपने घर, मैं अपने घर। हासिल ये हुआ कि किसी भी प्रकाशक ने मुझे छापने का जोखिम नहीं उठाया। दूसरे मैं अपने रचना के प्रकाशन के आश्य से किसी भी पत्र-पत्रिका के संपादक के पास चलकर नहीं कभी भी गया। अब इसे मेरी नादानी कहें अथवा अन्य कुछ और। इस तरह समय गुजरता गया और मैं साहित्यिक भँवर र्में हिचकौले खाता रहा।
सन 1972 के आसपास मैंने अपनी टूटी-फूटी ग़ज़लें इधर-उधर पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजनी शुरु कर दीं। इसी समय “गीतकार” नामक पत्रिका का प्रवेशांक पढ़ने को मिला। पद्मश्री गोपाल दास “नीरज” “गीतकार” के प्रधान संपादक थे। पत्रिका पढ़ी। अच्छी लगी। मैंने अपनी एक ग़ज़ल “गीतकार” में प्रकाशनार्थ भेज दी। किंतु मेरे द्वारा प्रेषित ग़ज़ल की केवल चार पंक्तियाँ ही प्रकाशित की गईं। वह भी संशोधन के बाद। प्रकाशित पंक्तियाँ ये हैं—
तुमने साँझ का वायदा किया तो मान लिया,
तुमने प्यार का वायदा किया तो मान लिया,
फिर मुहब्बते - तकरार का मतलब क्या है?
जब तुमने इंकार किया तो हमने मान लिया।
मुझे इन पंक्तियों के प्रकाशन पर खुशी कम, अवसाद ज्यादा हुआ क्योंकि वो मेरी विचारधारा के साथ एक छेड़छाड़ थी। शिल्पगत छेड़छाड़ तो मुझे कल भी स्वीकार थी और आज भी। किंतु इसे संयोग कहूँ या कुछ और, इसके बाद‘गीतकार” में मेरी रचनाओं को बिना किसी छेड़छाड़ के छापा और मुझे तेवरी भाषा का रचनाकार तक कहा जाने लगा जिससे मुझे अपनी बात को साफगोई के साथ रखने का बल व मेरे भीतर बैठे रचनाकार को नई दिशा मिली। मुझे लगा कि ग़ज़ल कहना आसान नहीं है। अभी और ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है। यद्यपि मेरा मानना है कि साहित्यिक सिद्धांत / व्याकरण का जानना आलोचकों और समालोचकों / विशेषज्ञों का काम है, रचनाकार का नहीं। फिर भी मैंने अपनी रचना में सुधार के लिए हल्के से ही सही, ग़ज़ल के व्याकरण को समझने का प्रयास किया।
यहाँ यह बताना जरूरी लग रहा है कि समय गुजरने के साथ-साथ मैंने भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करते हुए 1977 में स्नातक (बी.ए.) की परीक्षा भी उत्तीर्ण करली थी। अब साहित्यिक गोष्ठियों में आना-जाना मेरा शौक बन गया था।
1977 में आकाशवाणी, दिल्ली में कार्यरत माननीय श्याम दत्त पराग से अनायास रीगल सिनेमा के पास कनाट-प्लेस में स्थित काफ़ी हाउस (रीगल सिनेमा के सामने वाला) में मेरी मुलाकात हुई। मैं उस समय लगभग 28 वर्ष का था। पता नहीं, मेरे लम्बें बाल और दाढ़ी को देखकर उन्हें क्या आभास हुआ होगा? उन्होंने हाथ का इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, “लगता है तुम्हें कुछ लिखने-पढ़ने का शौक है ।” मैं कुछ देर सहमा सा चुप रहा। फिर सिर्फ इतना कहा कि शौक-भर है। उन्होंने शायद मेरा मन रखने के लिए कहा कि शौक होना ही तो भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। बोले, ’कुछ सुनाओ।”