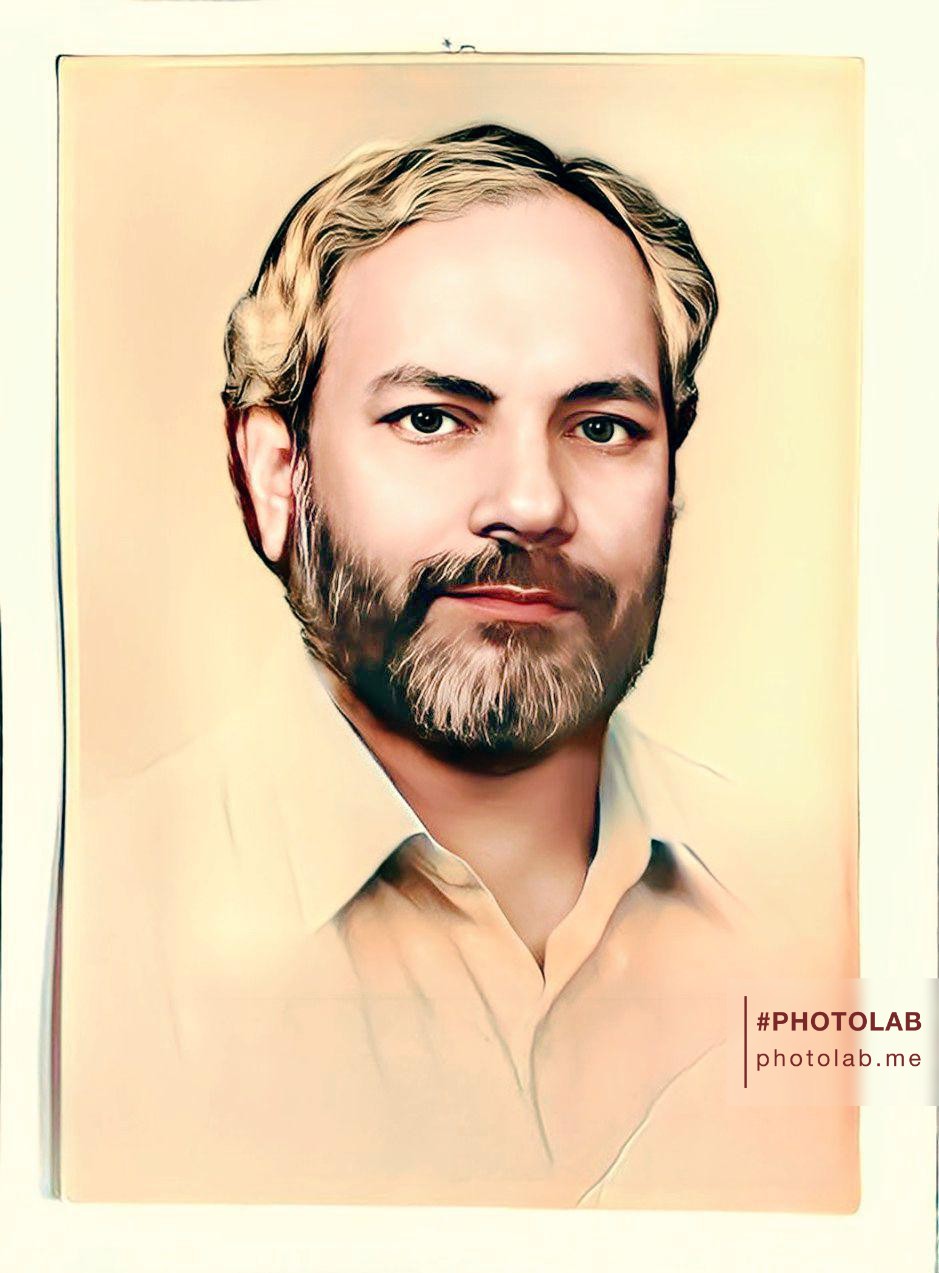मैं और मेरा गाँव
- तेजपाल सिंह 'तेज'
आज जब मैं (तेजपाल सिंह) जीवन की अस्सीवीं सीढ़ी पार करने को हूँ तो अपने गाँव की कहानी (अलाबास बातरी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश) लिखते समय कई प्रश्नों ने मुझे घेरा। सबसे बड़ प्रश्न तो यह था कि मैं अपने बचपन और शिक्षाकाल के गाँव के इतिहास वर्णन करूँ या फिर वर्तमान के विकसित गांव का। इस अवस्था में यही उचित होगा कि मैं अपने बचपन के गाँव के इतिहास और वर्तमान के गाँव को एक साथ लेकर चलूँ। किसी एक का वर्णन करके मैं शायद कहीं न कहीं अपनी मानसिक सिकुड़न का प्रमाण ही प्रस्तुत करूँगा। इसलिए मैं कल और आज के गाँव एक साथ लेकर चलूँगा। वैसे भी आज मैं बड़े ही असमंजस में हूँ, क्या याद करूँ क्या भूल जाऊँ? इसे पढ़ते हुए मेरी पीढ़ी के बहुत से लोग जो ग्रामीण पृष्ठ्भूमि से आते हैं, सभी मेरे जीवन के इस सच से कभी न कभी गुजरे होंगे।
विदित हो कि मेरा गांव मेरा कोई पुश्तैनी गाँव नहीं है। ‘कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा’ वाली तर्ज पर बसे इस गाँव में आजादी से लगभग 10-12 साल पूर्व, एक दूसरे के दूरदराज़ के रिश्तेदार आकर बसे थे। खानदानी कतई नहीं थे किंतु सगे से भी ज्यादा मिल-जुलकर रहते थे। एक दूसरे के दुख-दर्द में एक साथ खड़े होना उनकी प्रवृत्ति में शामिल था। गाँव के सब लोग अनपढ़ जरूर थे किंतु उनकी समझ का कोई तोड़ नहीं था। आपस में लाख लड़ाई-झगड़े हों किंतु मजाल कि कोई बाहर का आदमी गाँव में आकर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का साहस कर पाए।
जगराम, केसरी, महराज और प्रहलाद चार भाई थे जिनके बारे में सुना था कि उनके जन्म के अवसर पर खाने का इतना टोटा था कि उनकी माँ को उनके जन्म के अवसर पर जच्चा को मिलने वाला खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। केवल गाजर खा-खाकर अपने बच्चों को पाला-पोसा था। उनके बच्चे बड़े होकर इतने बलशाली बने कि वे जब एक साथ होते थे, तो उनके सामने किसी का इतना साहस नहीं होता था कि ऊँची आवाज में बोल सके। इनके बाद मेरे दूर के मामा के बेटे–चिरंजी और हरीसिंह और मेरे सगे भाए डालचन्द के नाम भी इस सूची में दर्ज थे, उनके हाथों में हमेशा तेल से तर लाठियाँ हुआ करती थीं। यही शारीरिक शक्ति उनकी असली ताकत हुआ करती थी। यहाँ दिवंगत काले तथा तोताराम का नाम लेना भी गैरवाजिब नहीं होगा। शरीर से बलिष्ठ लम्बा कद, स्याम रंग के मामा हारी राम (दिवंगत) बहुत ही मृदुभाषी थे। वे ज्यादातर किसी प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ते थे, बस अपने काम से काम रखते थे। सादगी और सज्जनता के नाम पर तो मोमराज और समेय सिंह का नाम लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे समय के सारे लोग अनपढ़ जरूर थे किंतु थे हरफनमौला।
मेरे गाँव में कुल 40-45 घर थे। जाटवों के घर अब कुछ ज्यादा हैं..परिवारों का निरंतर विकास जो हो रहा है। 1969 में जब मैंने गाँव छोड़ा था कुल चार-पाँच मकानों को छोड़कर बाकी सब मकान मिट्टी व छ्प्पर के बने थे, अब पक्के मकानों की संख्या कुछ ज्यादा है। मेरे समय में आँगन और मकान की दीवारों को गोबर में पीली मिट्टी मिलाकर लीपा-पोता जाता था। बारिश से पहले मकानों की कच्ची छतों को भुस की रैनी (भूसे का बारीक रेशा) और गोबर को चिकनी मिट्टी में मिलाकर वाटर-प्रूफ किया जाता था। आपको यह जानकर हैरत होगी कि मेरा पूरा का पूरा गाँव अनपढ़ों का था। केवल बादाम सिंह और टूकीराम नौवीं कक्षा तक पढ़े थे। उनको नौकरी मिली नहीं, या फिर उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, मुझे पता नहीं। लेकिन उनकी नाकामयाबी के चलते उनके घर वालों ने उनकी जल्दी ही शादी कर दी जिससे वो गाँव के ही हो कर रह गए। उनकी इस नाकामयाबी का गाँव के बाकी बच्चों पर ऐसा कुप्रभाव पड़ा, पढ़ने के प्रति सबका रुझान कम हो गया।
गाँव के पूरब में चित्सोना और दक्षिण में मंडोना जाट बाहुल्य गाँव हैं तथा उत्तर में केशोपुर सठला और पश्चिम में बी. बी. नगर अवस्थित हैं। ये दोनों ही कस्बे ब्राहम्ण व वैश्य बाहुल्य कस्बे हैं। आमतौर पर सभी जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे।कभी-कभार किसी अप्रिय घटना का होना अपवाद ही कहा जाएगा। मेरी याद में, जातीय दंगों के नाम पर कभी कोई तकरार नहीं हुई। एक दूसरे के यहाँ ब्याह-शादी में भी आना जाना भी होता था।
आज तेजपाल सिंह’तेज’ का गाँव अलाबास बातरी
विदित हो कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। बताया जाता था कि मेरे मां-बाप की चार औलादें थीं। सबसे बड़ा भाई, दो बहनें और मैं। तीनों मुझसे बड़े थे। पूरा परिवार शाकाहारी था। मेरे जन्म के समय मेरे माता-पिता की उम्र पक चुकी थी। यानी मैं बुढ़ापे की औलाद हूँ। शायद इसीलिए भाभी अक्सर मुझे ‘बुढ़ापे की औलाद’ कहकर चिढ़ाती थी। तब मैं इस बात का अर्थ नहीं जानता था। बड़ा हुआ तो जाना। भाभी ने बताया था कि मेरे जन्म के समय गाँव में हमारा अपना कोई घर नहीं था, मेरा जन्म मेरे दूर के मामा के बेटे– अमर सिंह के घर हुआ था। काफी अरसे उनके घर पर ही हमारा परिवार रहा। कब अपना घर बना, मालूम नहीं। जबकि मैं अपने बचपन को ढूँढने के प्रयास में हूँ, तो माँ और बाप के जाने के बाद मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी ने मेरे बचपन के पल जो समय ने मुझसे असमय ही छीन लिए थे। आज भी लगता है कि मेरे बचपन के पल सामने मुंह चिढ़ाए खड़े हैं।
स्कूली प्रमाण के आधार पर मेरा जन्म बुलन्दशहर (उ.प्र.) जिले के एक छोटे से गाँव ‘अला बास बातरी’ में सन 1949 के अगस्त माह में हुआ। भाभी ने बताया था कि जब मैं लगभग डेढ़ वर्ष का था, तब मेरे बाबा (पिता) हरिसिंह, जिन्हे गांव में ‘हरिया’ के नाम से पुकारता था, का देहांत हुआ था। उस धुंधली यादों में आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बाबा यानी मेरे पिता के देहांत के समय घर के आस पड़ोस के लोग-लुगाई हमारे घर आते, मेरी ओर भीगी आँखों से देखते, शायद मेरे बचपन में ही अनाथ होने की चिंता पर मन ही मन आहें भरते, आँसू गिराते होंगे। कई मेरे सिर पर हाथ रखकर दुख जताते और चले जाते। बचपन की सबसे बड़ी विरासत तो यही होती है की उन दिनों न किसी दुख का, न किसी सुख का अहसास होता। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, न कोई अपना, न कोई पराया। बच्चे का दुनिया से अनजानापन ही उसे दुनियावी होने से बचाता है। इसीलिए तो उसके चेहरे पर हमेशा हंसी तारी रहती है।
प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल की राह पर…
दीन-दुनिया से बेखबर, खेलते-कूदते न जाने कब मैं8-9 साल का हो गया। गाँव में बच्चों के साथ समय बिताने के लिए गिल्ली-डंडा खेलना, भैंस की कमर पर बैठकर गाँव से सटी पोखर में नहाना, कंचे खेलना और न जाने कितने ही ऊट-पटांग खेल ही हमारे मजोरंजन के साधन होते थे। घर वालों में से किसी को भी मेर्र पढ़ाई-लिखाई के बारे में कोई चिंता न थी। स्कूल में दाखिला तक नहीं हुआ था। माँ घर के काम-काज और डांगरों (पशुओं) की देख-रेख में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे कुछ और सोचने की फुरसत ही नहीं होती थी।
आखिर एक दिन भाभी ने उनसे मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ-खरी-खोटी बातें की तो भाई साहब अगले दिन ही मुझे गाँव के नजदीक वाले कस्बे ‘केशोपुर सठला’ के प्राथमिक स्कूल में ले गए और स्कूल में मेरे दाखिले की बात की। जन्म-प्रमाण तो उस समय हुआ ही नहीं करते थे सो मास्टर जी ने अपने हिसाब से मुझे पाँच वर्ष का बनाकर मेरी जन्म-तिथि 08.08.1949 लिखी और मेरा पहली कक्षा में दाखिला कर दिया। किंतु मुझे घर और स्कूल में कोई अंतर नहीं लग रहा था। मंद-बुद्धि जो था। किसी प्रकार की चंचलता मेरे आस-पास तक न थी। स्कूल में दो-चार दिन आने के बाद पता चला कि गाँव के और तीन-चार बच्चे पहली कक्षा में पढ़ते हैं और मुझे जोड़कर अब एक ही गांव के पाँच छात्र हो गए थे। स्कूल गांव से लगभग एक किलोमीटर ही होगा सो अब हम चारों का रोजाना साथ-साथ पैदल ही स्कूल आना-जाना हुआ करता था। किंतु पढ़ाई-लिखाई के प्रति मेरा कोई खास रुझान नहीं था। घर से किताब और तख्ती-किताबों का झोला (बस्ता) स्कूल ले जाना और वैसे ही स्कूल से घर आ जाता था। घर पर कोई कोई पूछताछ तो करता ही नहीं था। बाकी सब लड़के पढ़ने में मुझसे अच्छे थे।
जब स्कूल ही जाना बंद कर दिया….
स्कूल आते-जाते दो साल ही गुजरे होंगे। मुझसे बड़ी बहन अपनी बेटी की बीमारी का इलाज करवाने हमारे घर पर ही आई हुई थी। बच्ची साल-डेढ़ साल की होगी। एक दिन मैं और मेरे जीजाजी उसे डॉक्टर के पास, नजदीक के कस्बे भवन बहादुर नगर साइकिल पर लेकर जा रहे थे। मैं बच्ची को गोद में लेकर साइकिल की पिछली सीट पर बैठा था। गाँव से थोड़ी दूर जाने पर मैंने पाया कि बच्ची का हिलना-डुलना बन्द हो गया है। मैंने साइकिल रुकवाई और जीजा जी से बच्ची को देखने के लिए कहा। उन्होंने बच्ची को देखा और बिना कुछ कहे साइकिल गाँव की ओर मोड़ ली और भारी मन से बोले ‘गई’। मैं बच्ची को लेकर फिर साइकिल पर बैठ गया। घर पहुँचे तो रोआ-राट मच गया। यह जानते देर न लगी कि बच्ची मर गई है। मुझे वह बहुत प्यारी थी। मैं भी फफक कर रो पड़ा। मुझे उस दिन कुछ-कुछ यूँ लगा कि दुनिया के प्रति मेरी बचपन की बेहोशी जैसे छंटने लगी है और दुनियावी सोच के पंखों ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया हैं। खैर! हुआ यूँ कि मैंने बचपनी भावना में बहकर स्कूल जाना ही बंद कर दिया।
खेलकूद में लगभग एक सप्ताह गुजर गया, मैं स्कूल नहीं गया। इस पर एक दिन स्कूल में मुझे पढ़ाने वाले अध्यापकमा. हरपाल सिंह जी अचानक घर आ धमके। उस दिन संयोगवश मैं भी घर पर ही था। खेलने-कूदने कहीं नहीं गया था। घर वालों ने मास्टर जी को आदर सहित खाट पर बिठाया। मास्टर जी ने इधर-उधर देखा और मेरी ओर हाथ का इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। बोले – स्कूल क्यों नहीं आ रहा आजकल तू.? मैं जड़ बना सुनता रहा। उनके दोबारा पूछने पर मैंने सिर झुकाए हुए ही कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है। इतना सुनकर मास्टर जी का चेहरा-मोहरा बदल गया और उन्होंने घर वालों भाई व भाभी से सवाल कर डाला, सुना तुमने… ये क्या कह रहा है? क्या तुम भी नहीं चाहते कि ये पढ़े? भाई व भाभी ने मेरे स्कूल न जाने के प्रति अनभिज्ञता जताई और बड़े ही हल्के मन से कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये पढ़े। इसीलिए तो स्कूल में नाम लिखाया है.. इसका। इतना सुनकर मास्टर जी बोले – ठीक है तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, तुम जानो किंतु मैं इतना जानता हूँ कि इसे पढ़ना है। इसका झोला (बस्ता) लाओ। इसे आज से ही स्कूल जाना है। भाभी मेरा झोला ले आई। लाकर मेरे कंधे पर टांग दिया। मास्टर जी के हाथ में कमची लगी थी जिसे देखकर मेरी हवा खराब हो रही थी। मास्टर जी ने कमची हिलाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लेकर चल पड़े स्कूल की ओर। धीरे-धीरे मैं और मेरे अन्य साथी भी पाँचवी कक्षा में आ गए।
स्कूल में दो ही अध्यापक होते थे। एक हरपाल सिंह मास्टर और दूसरे – रघुनंदन शरण शर्मा मास्टर। रघुनंदन शरण जी बुजुर्ग और स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। चौथी व पांचवी कक्षाओं को पढ़ाया करते थे। वे पांचवी कक्षा के सभी बच्चों को बिना किसी जातिगत भेदभाव के सर्दी के मौसम में अपने घर पर रोजाना रात को बिना कोई पैसा लिए ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्होंने ट्यूशन पढ़ने के बाद बच्चों के सोने के लिए एक बड़े से कमरे में ईख की पताई (गन्ने के सुखे हुए पत्ते) डलवाकर उस पर जाजम बिछवा दी थी।
खटोले पर परीक्षा..
उस समय पांचवी की परीक्षा बोर्ड की होती थी। परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी हुआ करती थी। फरवरी-मार्च के महीने में सर्दियां कुछ कम हो ही जाती हैं। खेलकूद में छुट्टियां न जाने कब खत्म हो जाती थीं, कुछ पता ही नहीं पड़ता था। इस दौरान मेरे साथ एक दुखद घटना ये घटी कि खेलकूद में मेरे दाईं टांग के घुटने में गहरी चोट लग गई। उधर परीक्षा सिर पर आ गई। चोट पक गई और घुटने में मवाद पड़ गई थी। ऐसे में कैसी पढ़ाई, कैसी लिखाई। घुटने में दर्द के कारण वैसे ही पढ़ने में कौन सा मन था। परीक्षा नजदीक के दूसरे कस्बे भवन बहादुर नगर (बी.बी.नगर) में होनी थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि परीक्षा देने कैसे जाया जाएगा। घरवालों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं था। खैर! परीक्षा से पहले मेरी चोट के बारे में मा. हरपाल सिंह जी को पता लग गया था। वे परीक्षा से एक दिन पहले घर आ पहुंचे। मेरा हाल जाना और दुख जताते हुए मेरे भाई से मालूम किया कि घर पर कोई खटोला है कि नहीं। (छोटी खाट को गावों में आज भी खटोला ही कहते हैं। यदि नहीं तो आस-पडोस से मांगकर ले आवें। खटोले का इंतजाम तो कर दिया गया किंतु मास्टर जी को छोड़कर सबके दिमाग में एक ही प्रश्न था कि आखिर इस खटोले का होगा क्या। मास्टर जी से यह सब पूछने की हिम्मत भी किसी ने नहीं जुटाई। मास्टर जी ने मुझसे कहा कि कल परीक्षा देने चलना है – समझ गया कि नहीं। सुबह तैयार रहना। इतना कहकर मास्टर जी चले गए।
देहातों में कैसी तैयारी? दिन निकला, हाथ-मुंह धोए, कमीज पजामा पहना और हो गए तैयार। अगले दिन सूरज थोड़ा ही चढ़ा था कि मास्टर जी अपने साथ छ:-सात बच्चे लेकर घर आ गए। मुझे खटोले पर डाला, बच्चों ने खटोला उठाया और चल पड़े परीक्षा केन्द्र की ओर। परीक्षा समाप्त होने पर बच्चे ही मुझे खटोले पर डालकर घर पर छोड़ गए। परीक्षा के समाप्त होने तक यही सिलसिला चलता रहा। मैं भी पांचवी कक्षा में पास हो गया। यदि आज मैं ये कहूँ कि यदि मास्टर हरपाल सिंह जी न होते तो आज का तेजपाल सिंह ‘तेज’ देहात ही में ‘तेजू’ बनकर रह जाता। इधर-उधर चाकरी में लगा होता।
इस तरह मैं सातवीं कक्षा में आ गया। कालिज में सातवीं कक्षा के तीन सेक्शन होते थे। प्रत्येक सेक्शन में लगभग पैंतालीस-पैतालीस छात्र होते थे। स्कूल में साल में तीन परीक्षाएं हुआ करती थीं- तिमाही, छमाही और सालाना। तिमाही परीक्षा का परिणाम आया तो जाना कि मेरा एक साथी तीनों सेक्शनों में पांचवे नम्बर पर आया। मुझे इसकी खुशी तो थी किंतु पता नहीं क्यों, मुझे अचानक इस बात का दुख भी सताने लगा था कि मेरा कोई नम्बर क्यों नहीं। साथी छात्रों के संसर्ग में रहकर मेरी सोच का पंछी जैसे किसी खाई से निकलकर मैदान में आने को आतुर होने लगा था। अब सोते-जगते यही सवाल मेरे ज़हन में घूमता रहता। फलत: किताबों से कुश्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि इस कदर बढ़ी कि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ और भाता ही नहीं था।
मेरी इस हालत को देखकर, मेरी भाभी कभी-कभी सोचने लगती कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब न तो ये खेलने जाता है और घर पर भी चुप-चुप ही रहता है। भाभी ने ये बात माँ से भी शिकायती लहजे में कही होगी। माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं किंतु मुझ पर नज़र रखने लगी। दुकड़िया में मुझे देखने आती और मुझको पढ़ता हुआ देखकर वापिस हो जाती, फिर सारा किस्सा भाभी को सुनाती थी। जब कहीं मेरे ना खेलने और हमेशा चुप-चुप रहने का मामला उनके दिमाग से उठ गया था। पढ़ाई के प्रति बढ़ते रुझान के चलते, छमाही की परिक्षा में मुझे अप्रत्याशित सफलता मिली। इस बार मैं लगभग 135 बच्चों यानी पूरी कक्षा में दसवें-ग्यारहवें पायदान पर पहुँच गया। सीधे-सादे और सामान्य दर्जे के छात्र का अचानक छलांग लगाना, मेरे कुछ साथी छात्रों को खला भी, जो स्वाभाविक ही था। मेरे ही गाँव का साथी अमरनाथ तो मुझसे ऐसे ख़फा-ख़फा सा रहने लगा जैसे मैंने उसका नम्बर ही छीन लिया हो। अब सालाना परीक्षा की बारी थी। मैं और मन लगा कर पढ़ने लगा। सालाना परीक्षा सिर पर थी। कई बार तो सर्दियों के मौसम में रात को पढ़ते-पढ़ते मैं सो जाया करता था और मिट्टी के तेल का दीया (डिबिया) जलता ही रह जाता था। उसे माँ या भाभी में से कौन, कब बंद करता होगा, नहीं मालूम। पढ़ाई के लिए और तो कोई खास सुविधा थी नहीं, ना घड़ी, ना मेज। खैर! सातवीं की सालाना परीक्षा भी समाप्त हो गई। रिजल्ट आया तो जाना कि पूरी कक्षा में इस बार मेरी सातवीं पोजीशन थी। मैं बेहद खुश हुआ। टीचर्स भी मेरी निरंतर बढ़त को देखकर मुझे प्यार की नज़र से देखने लगे थे। अचानक इतना बड़ा परिवर्तन किसी और को तो क्या आज मुझे भी नहीं पच रहा है। ये सब कैसे हुआ? मैं खुद नहीं जानता कि आखिर मुझे हो क्या गया था कि पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं था। यदि मैं ये कहूँ कि सातवीं कक्षा का वह वर्ष ही पढ़ाई के मामले में मेरे लिए एक सकारात्मक ‘टर्निंग पाइंट’ था तो अनुचित न होगा।
अब मैं आठवीं कक्षा में था। पढ़ाई का सिलसिला पहले जैसा ही चलता रहा और मैं दिनोंदिन पढ़ाई से जुड़ता चला गया। अध्यापकों और तरक्की पसंद साथियों का भरपूर सहयोग मिल रहा था। जब भी चाहूँ कोई भी परामर्श लेने की छूट, मुझे सभी अध्यापकों से मिल गई थी। मेरे लिए अब वो समय था जब मैं अच्छे और बुरे की समझ से रुबरू हो रहा था। हकीकत ये है कि छोटेपन में मुझे छोटे-बड़े के सम्मान का कोई ख़याल नहीं था। सबको ‘तू’ कहकर ही संबोधित किया करता था किंतु अब सबके प्रति सम्मान का भाव स्वत: ही पनपने लगा था। मैं बचपन की भूल-भुलैया से जैसे बाहर आने लगा था। किंतु अचानक माँ का स्वास्थ्य गिरने लगा और वो इस कदर बीमार हो गई कि खाट पकड़कर रह गई। अब घर का सारा काम भाभी के कंधों पर आ गया था। माँ की सेहत निरंतर गिरती चली गई। एक दिन माँ ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मुझे सौ का एक नोट देकर सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोली – ले इसे अपने पास रख ले। मैंने नोट लिया और उसे पैसे रखने वाले मटके में ही रख आया। थोड़ी देर बाद पता चला कि माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी है।
अब मेरे बचपनी महल की बुनियादें जैसे बुरी तरह हिल गईं। अब केवल भाई और भाभी का ही आसरा शेष रह गया था। माँ के गुजरने के बाद बस्ती वालों से एक खिताब जो मुझे मिला, वह था ‘बेचारा अभागा’, शायद इसमें उनका मेरे प्रति प्यार और मेरे भविष्य के प्रति चिंता का भाव निहित था। किंतु माँ के गुजरने के बाद भी मेरे प्रति भाई-भाभी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था इसलिए कुछ ही दिनों में माँ-बाप की बिदाई जैसे मेरे दिमाग में भी धुंधली पड़ने लगी थी। और धीरे-धीरे एक समय ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फलत: पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान जस का तस बना रहा। आठवीं कक्षा में भी मैं अच्छे अंक लेकर पास हुआ। इस बार भी मेरी पांचवी-छटी पोजीशन ही रही। कहने की जरूरत नहीं कि मेरे बचपन का यही अंतिम पड़ाव भी था।
मेरी शिक्षा और मेरी कद-काठी की चौपाल पर चर्चा
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सातवीं कक्षा में आने से पूर्व मेरा पढ़ने-लिखने में कम ही मन लगता था। बस! खेलना-कूदना साथियों के साथ मार-पीट करना प्रत्येक शर्त पर अपनी बात को ही मनवाना, जाने क्या-क्या मेरी शरारतों में शामिल था। पूरा गाँव परेशान रहता था मेरी शरारतों से। सबकी नज़र रहती थी मुझ पर। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल रहता था, पता नहीं पढ़-लिखकर क्या करेगा ये छोरा। इसका कद भी तो इतना छोटा है कि ये पुलिस में भी तो भर्ती नहीं हो सकता अभी तक तो इस गाँव में कोई कुछ बनना तो क्या ठीक से पढ़ा-लिखा भी नहीं है। बादाम को देखो, टूक्की को देखो, दसवीं भी पास नहीं कर पाए। शादी करके गाँव के ही होकर रह गए। फिर ये ही क्या कर लेगा, पाँच फुटा तो वैसे ही है। डाकू-बदमाश भी तो नहीं बन सकता। कुछ कहते कि अरे! ये सब इसकी बचपनी शारारतें हैं, अभी नादान है, कुछ समझ नहीं है अभी इसे। समय शायद इसे ठीक रास्ते पर ले आए। इसने ये सब शरारतें छोड़ दीं तो कुछ आशा की जा सकती है पर ऐसा लगता तो है नहीं। ऊपर से न बाप है और न माँ, भाई है पता नहीं आगे पढ़ाए न पढ़ाए।
मेरे बारे में जाने क्या-क्या सोचते रहते थे मेरे गाँव वाले। एक बात साफ कर दूँ कि वे ये सब बातें मेरे पीछे नहीं, मेरे सामने ही किया करते थे। कुछ मुझे चिढ़ाने के भाव से तो कुछ मुझे समझाने के आशय से। जाहिर है कि इस प्रकार की बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगती थीं। तब मैं इतना समझदार भी कहाँ था, सब कुछ सुनता रहता औ बचपनी हंसी में उड़ा देता। उनकी बातें सुनकर कभी-कभी तो मुझे भी उनकी बातों में दम लगता था और मैं अन्दर ही अन्दर भविष्य के प्रति निराशा ओढ़कर मौन अवस्था में चला जाता था। आज जब मैं ये सत्य लिख रहा हूँ, मेरे वो अपने शेष नहीं रहे हैं किन्तु उन सबकी सूरतें आज भी रह रह कर आँखों से टकराती रहती हैं। सब के सब अंतर्यामी हो गए है अब जब मैं अस्सी साला होने वाला हूँ तो मुझे अपने उन बुजुर्गों की बातों का ख़याल आता है तो मुझे खुली आँखों सपने से दिखने लगते हैं। सपने भी कमाल होते हैं ना? खुली आँखों देखे जाते है और नींद में भी।
शिक्षा हेतु संघर्ष
यहाँ यह खुलासा कर दूँ कि मेरे बड़े भाई मां के देहांत से पहले जमीन से पानी निकालने वाले नल लगाया करते थे। लेकिन माँ के गुजरने के बाद मेरे बड़े भाई में जो बड़ा एक परिवर्तन आया, वह बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। अब भाई ने शारीरिक श्रम करना यानी नल लगाने का काम बंद कर दिया। माँ की भारी-भरकम जमा-पूंजी (जो बाद में लगभग पैंतालीस हजार रुपए बताई गई थी) जो मां ने किसी के जरिए डाकखाने में जमा कराई थी, ऐसा मैंने सुना भर था। और भैंसों को बेचने से अर्जित धन को एक के बाद दूसरा कारोबार करने में बरबाद कर दिया। इधर मैंने दसवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। किंतु दसवीं करने के बाद भाई ने मुझे आगे पढ़ाने से मना कर दिया। पर मैं पढ़ना चाहता था। भाभी के कहने का भी भाई पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर मैं निराश रहने लगा। कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि माँ के मरने पर बस्ती वालों द्वारा दिया गया खिताब ‘बेचारा अभागा’ जैसे अब साकार होने की दिशा में था। मुझे अपने चारों ओर खालीपन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अब माँ का अभाव सताने लगा था। कई बार अकेले में मेरी आँखे नम हो जाती थीं और मैं देर तक रोता रहता था। पढ़ाई के क्षेत्र में आए सकारात्मक ‘टर्निंग पाइंट’ के बाद माँ का देहांत, एक ऐसा नकारात्मक ‘टर्निंग पाइंट’ था जो शेष जीवन के लिए एक चुनौती बन गया था। अब जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह गया था। ऐसे में मैं कभी नौकरी तलाशने की बात सोचता तो कभी कुछ काम-धाम करके आगे पढ़ने की। मैं जैसे जीवन के प्रवेश द्वार ही पर ही उलझ गया था। सच तो ये है कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं सोच पा रहा था। मुझे लगा कि अब खुद को, जिन्दगी को और दुनिया की हकीकत से रूबरू होने का समय आ गया है। इसी सोच और फिक्र में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को आ गईं।
समय को पकड़ कर रख पाना किसी के हाथ में नहीं होता। अब क्या करूँ ये प्रश्न मुझे खाए जा रहा था। हारकर मैंने आगे पढ़ने का मन बना लिया और जैसे-तैसे स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज में ही कक्षा ग्यारहवीं (विज्ञान) में दाखिला ले लिया। नल लगाना तो मैं सीख ही गया था क्योंकि घरेलू काम था। कॉलेज की छुट्टी वाले दिनों में मैंने नल लगाने का काम शुरु कर दिया। कभी-कभार स्कूल से बंक मारके भी नल लगाने चला जाता था। महीने में कुछेक नल लगाकर किताबों और थोड़ा-बहुत फीस का काम चल जाया करता था। खाना और कपड़े तो घर से मिल ही जाते थे। उल्लेखनीय है कि कॉलेज में मुझे ही नहीं किसी को भी कभी कोई जातीय दुराव देखने को नहीं मिला जबकि मेरे कॉलेज में तीन-चार अध्यापकों को छोड़कर शेष सभी अध्यापक ब्राहम्ण थे लेकिन उनमें जातिभेद से इतर गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के प्रति एक अजीव सी सद्भावना थी कि वे उनकी हर संभव मदद किया करते थे। सभी छात्र भी जातिभेद की भावना से परे एक साथ मिलकर रहते थे। हाँ! केवल और केवल संस्कृत के अध्यापक जिन्हें सब गुरुजी कहकर पुकारा करते थे ऐड़ी तक का लम्बा धवल कुर्ता और धोती उनके पहनावे में शामिल थी पर थे बड़े ही खड़ूस माथे पर न जाने कितनी सिलवटें भौएं चढ़ी हुई, यह उनकी खास पहचान थी। किसी से भी सीधे मुँह बात नहीं करते थे वे।
वह स्कूल शिक्षा के बाद पढ़ाई की थी जहां, लेखक ने प्राथमिक
आपको यह जानकर हैरत होगी कि स्वतंत्र भारत इंटर कालेज, बी.बी. नगर (बुलंद्शहर) में समूचा स्टाफ ब्राहम्ण वर्ग से ही था केवल एक-दो अध्यापकों को छोड़कर याद पड़ रहा है कि एक थे एहसान अली सर और दूसरे थे सिरोही सर, ऐसे में सोचा जा सकता है कि गरीब तबके से आने वाले छात्रों की शिक्षा का क्या आलम होगा किंतु वैसा कतई नहीं था जैसा आप सोच रहे होंगे। गरीब तबकों से आने वाली छात्रों की शिक्षा का ही नहीं अपितु उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का भी सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से पूरा ध्यान रखा जाता था।
संदर्भ के चलते याद आया कि कालेज के प्रधानाचार्य माननीय रामाश्रय शर्मा प्रार्थना से पहले ही कालेज के मुख्य द्वार पर आ खड़े होते थे। हाथ में अंग्रेजों वाला छोटा सा रूल ऐसे झूलता था जैसे कितने क्रूर होंगे किंतु मैंने कभी अपने शिक्षाकाल में उस रूल का प्रयोग कभी-कभार ही करते देखा था। हाँ! तो होता यूँ था कि जो बच्चे प्रार्थना के बाद यानी कि कॉलेज देर से आते थे, उनमें से गरीब तबकों से आने वाले छात्रों को वो कॉलेज के मुख्य द्वार पर ही रोककर मुर्गा बनाकर खड़ा कर देते थे और उनके चूतड़ों पर कभी रूल तो कभी घूँसा मारकर उनकी खबर लिया करते थे।
एक बार मैं भी इस जाल में फंस गया, मुर्गा बनना पड़ा किंतु मुझे हैरत हुई कि वो हमें सजा देते थे या फिर सीख वो अक्सर कहा करते थे, ‘सोरे तुम्ह