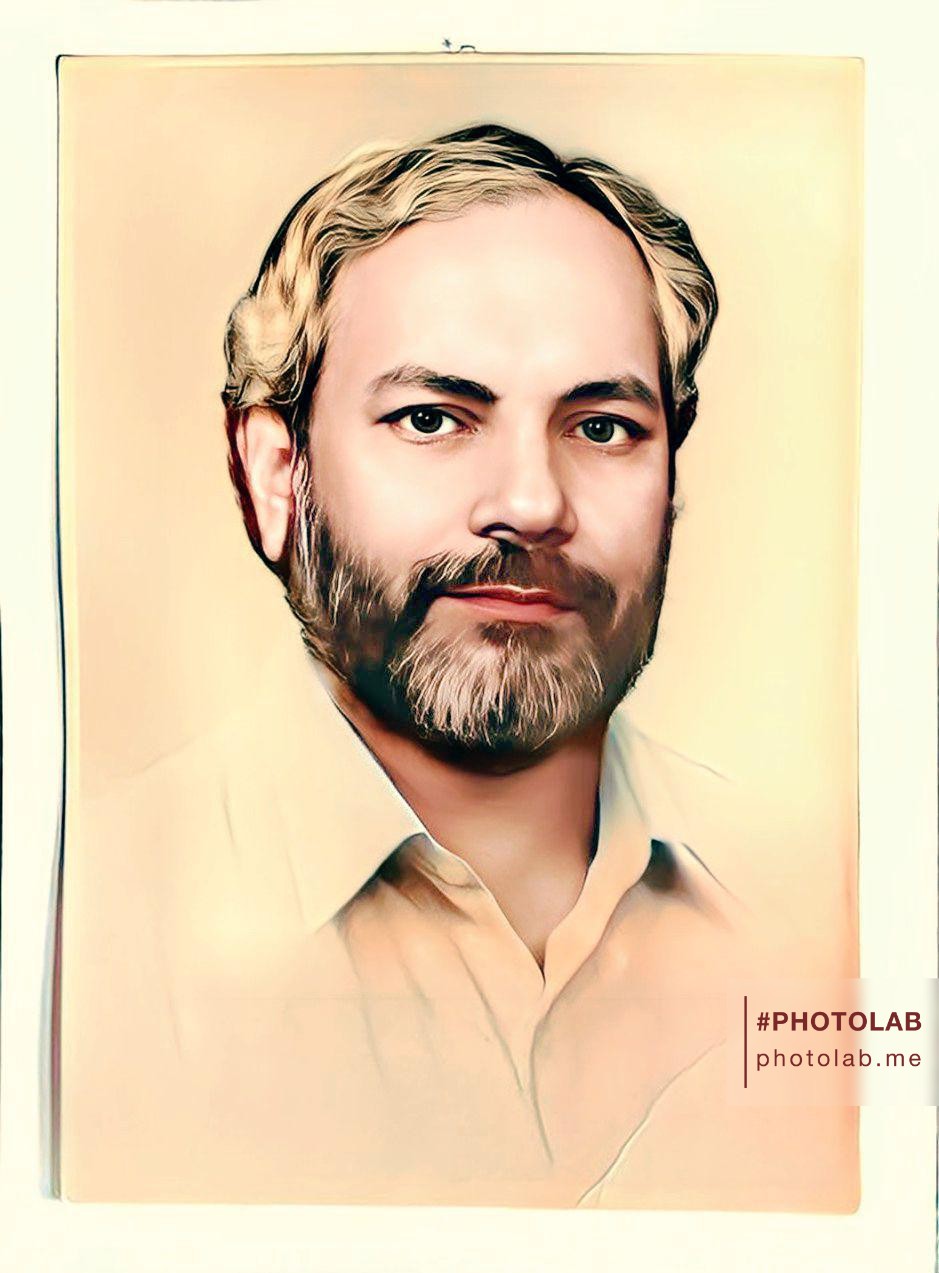पुस्तक समीक्षा : तेजपाल सिंह ‘तेज’ की आत्मकथा
फ्लैश बैक : बियोंड पैराडाइम (आत्म वृत्त)
प्रकाशन वर्ष : भाग–एक 2021 : भाग-दो 2022
प्रकाशक : बुक रिवर्सरिवर्स : मोबाइल – 9695375469
पृष्ठ संख्या : भाग –एक : 279 मूल्य : 150/-
भाग – दो : 213 मूल्य : 180/-
तेजपाल सिंह ‘तेज’ की आत्मकथा : संघर्ष और तजुर्बे का बयान
- मोहनदास नैमिशराय
नई शताब्दीके दो ढाई दशक बीतते-बीतते अच्छी खासी संख्या में दलित समाज के लेखकों/कवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। मेरे अपने अध्ययन और जानकारी के आधार पर पूरे देश से लगभग 160 आत्मकथा (मार्च 2023 तक) छप चुकी हैं। इनमें स्त्री/पुरुष दोनों की आप-बीती शामिल हैं।
वाणी प्रकाशन के लिए एक सौ दलित आत्मकथाएं इतिहास एवं विश्लेषण नाम से पांडुलिपि तैयार करने के दौरान मैंने लगभग 110 आत्मकथाएं पढ़ी थीं जिनमें से 90 किताबें मेरी अपनी लाइब्रेरी में थी। शेष का अन्य पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन किया। इसीलिए आत्मकथाओं का संदर्भ दिया। वाणी प्रकाशन से मेरी किताब 2021 में प्रकाशित हुई। उससे पूर्व 1-2 वर्ष मुझे शोध एवं संपादन करने में लगे।
जहां तक तेजपाल सिंह तेज की आत्मकथा फ्लैशबैक बियोंड पैराडाइम (जिसे उन्होंने आत्मवृत्त लिखा है) की बात है यह मुझे 2022 में मिली। देर से ही सही मिली तो सही इसीलिए अध्ययन भी कर सका और उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व के विभिन्न आयाम जान पाया। महसूस कर सका उनके सुख-दुख को। घर और घर के बाहर जो यातनाएं उन्होंने झेली उन्हें भी नजदीक से जान पाया। वैसे 80 के दशक से ही उनसे मुलाकात का सिलसिला चल निकला था।उन दिनों 80—90 के दशक में वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संसद मार्ग स्थित दिल्ली आँचलिक कार्यलय में कार्यरत थे और मैं उन दिनों नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान आदि के लिए लिखता था। इसी दौरान पहले बतौर संपादक डॉ अंबेडकर प्रतिष्ठान, अशोक रोड, नई दिल्ली में और बाद में इस ऑफिस में जो होटल मैरिडन के पास शिफ्ट गया था, मुख्य संपादक के रूप में लगभग साढे 6 वर्ष कार्य किया था। तेजपाल सिंह ‘तेज’ संसद मार्ग स्थित एसबीआई हेड ऑफिस में ही बैठेते थे। सामान्यत: लोग उन्हें ‘टी. पी. सिंह’ नाम से संबोधित करते हैं। उनके आत्मवृत्त भाग 2, 2022 में प्रकाशित हुआ था। स्वयं आत्मकथाकार लिखते हैं, मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी कहानी को परत दर परत खोलता हुआ अपने जीवन के हलके-फुल्के, ज्ञात- अज्ञात छुए-अनछुए पहलुओं को शब्दबद्ध करूं। जीवन की सच्चाई व यथार्थ स्थिति का बोध कराऊं।
जब नवंबर 2012 के प्रथम सप्ताह में भाई मुकेश मानस का फोन आया कि मैं अपने बचपन के विषय में कुछ लिखूँ। शायद उनको मेरी रुग्णावस्था के बारे में मालूम नहीं था। गौरतलब है कि अगस्त 2009 की उन्नतीसवीं तारीख को भारतीय स्टेट बैंक से उप-प्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हुआ था। मेरी सेवा-निवृत्ति के बाद मेरे दो-तीन वर्ष ठीक-ठाक गुजर गए किंतु वर्ष 2012 के जुलाई माह की सोलह तारीख को इस कदर बीमार हुआ कि दिल्ली के सर सर गंगाराम अस्पताल जा पहुँचा और फिर 2012 के अगस्त माह में घर वापसी हुई। बेशक मर्णासन्न अवस्था में.....घर आने पर सबको लग रहा था कि अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ तो मेरे छोटे बेटे ने पूछ ही लिया, पापा !... किसी का क्या देना है...क्या लेना है। अच्छी बात यह थी कि यदि मैं इस अवस्था में मर भी जाता तो मुझे न तो किसी का कुछ देना था और किसी से कुछ लेना था। दरअसर मैंने अपने जीवन की जरूरतों को हमेशा अपनी जेब की नाप के हिसाब से ही किया था। इस सबका लाभ ये हुआ कि मुझे घर वालों कोई भी हिसाब-किताब देने की कुछ नौबत न आई। हां! बस घर-मकानों के कागजात व बैंक खातों के विवरण मैंने उनको जरूर बता दिये थे। आत्मवृत्त के पहले भाग में उनके द्वारा बेबाक टिप्प्णी की यह शुरुआत थी।
स्वयं लेखक के अनुसार, मेरे जन्म के समय मेरे माता-पता की उम्र पक चुकी थी। शायद इसीलिए भाभी अक्सर मुझे बुढ़ापे की औलाद कहकर चिढ़ाती थी। स्कूली प्रमाण के आधार पर मेरा जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जिले के एक छोटे से गांव अलाबास बातरी में 1949 के अगस्त माह में हुआ था। मेरे माता-पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और आज जब मैं अपने बचपन की कहानी लिख रहा हूं मेरे भाई बहन की जीवित नहीं हैं। मेरे गांव में करीब 40-45 घर थे, सभी जाटवों के। अधिकांश मकान मिट्टी के बने थे। मेरे समय में आंगन और मकान की दीवारों को गोबर में पीली मिट्टी मिलाकर लीपा-पोता जाता था। बारिश से पहले मकानों की कच्ची दरारों को भूस की रैनी (भूस का बारीक रेशा) और गोबर को चिकनी मिट्टी में मिला कर वाटर प्रूफ किया जाता था।
स्कूल में प्रवेश
8—9 साल के करीब भाई साहब मुझे गांव के नजदीक वाले कस्बे केशोपुर सठला के प्राथमिक स्कूल में ले गए और पहली कक्षा में मेरा दाखिला करा दिया। बाद में पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से तीसरी और चौथी से पांचवी कक्षा में आ गया। मुझे याद है कि चौथी और पांचवी कक्षा के सभी बच्चों को बिना किसी जातिगत भेदभाव के रात में बिना पैसा लिए हैड मास्टर जी रात के समय अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाया करते थे। श्री हरपाल सिंह और दूसरे श्री रघुनंदन शरण शर्मा बस दो ही अध्यापक थे स्कूल में।
खटोले पर परीक्षा...
उल्लेखनीय है कि उस समय कक्षा पांच की परीक्षा बोर्ड की होती थी। परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी हुआ करती थी। फरवरी-मार्च के महीने में सर्दियां कुछ कम हो ही जाती हैं। खेलकूद में छुट्टियां न जाने कब खत्म हो जाती थीं, कुछ पता ही नहीं पड़ता था। इस दौरान मेरे साथ एक दुखद घटना ये घटी कि खेलकूद में मेरे दाईं टांग के घुटने में गहरी चोट लग गई। उधर परीक्षा सिर पर आ गईं। चोट पक गई थी और घुटने में मवाद पड़ गई थी। ऐसे में कैसी पढ़ाई, कैसी लिखाई। घुटने में दर्द के कारण वैसे ही पढ़ने में कौन सा मन था। परीक्षा नजदीक के दूसरे कस्बे भवन बहादुर नगर (बी.बी.नगर) में होनी थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि परीक्षा देने कैसे जाया जाएगा। चोट के कारण चल पाना तो दूर, मैं खड़ा हो पाने में भी अक्षम था। घरवालों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं था। खैर! परीक्षा से पहले मेरी चोट के बारे में मा. हरपाल सिंह जी को पता लग गया था।
वे परीक्षा से एक दिन पहले घर आ पहुंचे। मेरा हाल जाना और दुख जताते हुए मेरे भाई से मालूम किया कि घर पर कोई खटोलाहै कि नहीं। (छोटी खाट को गावों में आज भी खटोला ही कहते हैं) यदि नहीं तो आस-पडोस से मांगकर ले आवें। खटोले का इंतजाम तो कर दिया गया किंतु मास्टर जी को छोड़कर सबके दिमाग में एक ही प्रश्न था कि आखिर इस खटोले का होगा क्या। मास्टर जी से यह सब पूछने की हिम्मत भी किसी ने नहीं जुटाई। मास्टर जी ने मुझसे कहा कि कल परीक्षा देने चलना है, समझ गया कि नहीं! सुबह तैयार रहना है।
अगले दिन मास्टर जी अपने साथ ६—७ बच्चे लेकर घर पर आ गए। मुझे खटोले पर डाला, बच्चों ने खटोला उठाया और चल पड़े परीक्षा केंद्र की ओर। परीक्षा समाप्त होने पर बच्चे ही मुझे खटोले पर डालकर घर छोड़ गए।
पांचवी कक्षा में पास होने पर आगे की पढ़ाई के लिए स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज बी बी नगर में मेरा दाखिला करा दिया गया था। अब मेरा पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ता गया। सर्दियों के मौसम में रात को पढ़ते पढ़ते सो जाया करता था और मिट्टी के तेल का दिया जलता ही रह जाता था। पढ़ाई के लिए उन दिनों कोई खास सुविधा नहीं थी, ना कुर्सी, ना मेज। उन दिनों रोशनी के लिए बिजली का होना तो एक ख्वाब था।
इधर मैंने दसवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर थी। किंतु दसवीं के बाद भाई ने मुझे आगे पढ़ाने से मना कर दिया किंतु मैं पढ़ना चाहता था। आत्मकथाकार की अभी उम्र ही कितनी थी, पर वह भी क्या करता? नौकरी के लिए भागदौड़, वह भी नहीं मिली। आगे की पढ़ाई के लिए ग्यारहवीं (विज्ञान) में दाखिला ले लिया। नल लगाने का काम तो मुझे आता ही था.. कारण कि मेरे भाई भी नल लगाने का काम करते थे। सो कॉलेज की छुट्टी वाले दिनों में नल लगाने का काम शुरू कर दिया। इससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, जो फीस भरने के काम आता था।
तेजपाल सिंह लिखते हैं, कॉलेज में मुझे कभी भी कोई जातीय दुराव देखने को नहीं मिला, जबकि तीन चार अध्यापकों को छोड़ शेष अध्यापक ब्राह्मण थे। दलित आत्मकथाकारों के साथ ऐसा कम ही होता है, जब स्कूल मे उनके साथ जातीय भेदभाव न हो लेकिन यहाँ लेखक को अच्छे अध्यापक मिले। द्रोणाचार्यो से उनकी मुठभेड़ नहीं हुई।
1969 मैं मैंने 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। आर्थिक संकट तो सामने था ही। ऐसे में उनके जीजा जी – श्री श्रीराम ने अपने दोस्त रामभज के साथ मुझे दिल्ली भेज दिया। जो करोल बाग के टैंक रोड पर एक छोटे से मकान में रहा करते थे। मैंने भी उनके साथ रहना शुरू कर दिया।
दिल्ली तो आ गया, लेकिन स्कूल की यादें अभी भी आती थीं। कालेज के प्रधानाचार्य रामाश्रय शर्मा सुबह की प्रार्थना से पहले ही कालेज के मुख्य द्वार पर खड़े होते थे। हाथ में रूल लिए। हकीकत ये थी कि वो अक्सर देरी से आने वाले दलित वर्ग के छात्रों को ही मुख्य द्वार रोका करते थे। एक बार मैं भी फंस गया...मुर्गा बनना पड़ा......किंतु मुझे हैरत हुई कि वो हमें सजा कम सीख ज्यादा देते थी.... वो अक्सर कहा करते थे...., “ सोरे तुम्हारी माँ-बहनों के घास खोदते खोदते पेटीकोट फट जाते हैं... जब कहीं तुम्हे स्कूल भेज पाती हैं... और सोरे! तुम स्कूल भी समय से नहीं आ सकते..... पढ़ना तो दूर की बात... ये तो अमीर घरों के बालक हैं, ये पढ़ें... ना पढ़ें, इन पर कोई फरक नहीं पड़ने काये अमीर घरों के हैं... दुकान पर बैठके डंडी मारके भी कमा लेंगे...तुम क्या करोगे?... तुम्हारी तो मैं खाल छील दूंगा... देखता हूँ तुम कैसे नहीं पढ़ते हो...।" उनके इन उदगारों को रखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे कालिज के ब्राहमण अध्यापकों के बारे में कुछ और कहना शेष रह जाता है। ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा में मेरी तो फीस भी प्रधानाचार्य रामाश्रय शर्मा ही देते थे। जब कभी दलित-छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति मिलती थी तो कभी-कभी लौटा भी दी जाती थी... कभी नहीं...वो इस प्रकार के खर्चे अक्सर अपनी जेब से ही वहन किया करते थे।
छात्रवृत्ति की बात चली तो एक और वाकया याद आ गया कि छात्रवृत्ति की बात चली तो एक और वाकया याद आ गया कि वर्ष 1968 में प्रधानाचार्य महोदय ने सब बच्चों के वजीफे की लिए फार्म पूरे कराने की जिम्मेदारी मुझको सौंप दी थी.... जिस दायित्व को मैं बखूबी इसलिए निभा पाया क्योंकि उस समय 'बुलंदशहर जिला परिषद के सदस्य माननीय रामजीलाल जी (स्याने वाले) का हमारे घर भाई से मिलने आना-जाना अक्सर हुआ करता था। गौरतलब है कि उस समय मेरे भाई ग्राम प्रधान थे और रामजीलाल जी के दोस्त भी। इस कारण उनसे मेरी भी खासी जानकारी हो गई थी। इस वजह से कुछ छात्र-मित्र मुझे नेता की नजर से देखा करते थे और हाँ। उल्लेखनीय है कि 1968 में होने वाले इम्ताहन सिर पर थे किंतु मैं जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बुखार निमुनिया में बदल गया। और मैं शरीर से एक मानुसिक खाका बनकर रह गया था।
इस दौरान, बहुत से साथी मुझ बीमार से मिलने आया करते थे। लेकिन हर बार आने वाले छात्र-दोस्तों में से ज्यादातर को यह शिकायत रहती थी कि हमें मिलने वाले बजीफे में से कालेज दो रुपये महीने के हिसाब से कटौती कर लेता है....जो कटौती नाजायज थी। उनकी बात सुनकर मैं भी ये कह देता था कि भई! ये तो सबकी अपनी-अपनी मर्जी का मामला है.... जिसको कटवाना है कटवाओ...नहीं कटवाना तो मत कटवाओ ...जरूरी थोड़े ही है। पता चला कि उनमें से किसी ने भी उस वर्ष भवन निर्माण के नाम पर वसूला जाने वाला चन्दा, यह कहकर नहीं कटवाया कि तेजपाल ने मना कर दिया है। इस कारण बड़े बाबू ने मुझे भी बिना चंदा काटे ही छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया। मैंने चंदा के पैसे बड़े बाबू को दिए किंतु उन्होंने नहीं लिए और कहा कि जब तुमने सबको मना कर दिए तो तुम ही देकर क्या करोगे...तुम भी रहने दो।
स्वयं कथाकार लिखते है - बात बहुत पुरानी हैं। शायद 1962/63 की होगी। संभवतः मैं सातवीं या आठवीं का छात्र रहा हूंगा। मेरे भाई ग्राम प्रधान थे। गरीबों को रिहायशी भूखंड आवंटित किए जा रहे थे। पटवारी पट्टे लिखने के पैसे कुछ वसूलता था। हुआ यूं कि एक दिन अचानक मैंने मुफ्त में पट्टे लिखने शुरू कर दिए। करना क्या था, पुराने पट्टे की नकल ही तो करनी थी। बस! आवंटन के प्रार्थी का नाम व पता ही तो बदलना था। गांव वाले लोग बड़े खुश हुए। बस! यहीं से सेवा भाव का कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया। पहले बरात दो रात रुक्सआ करती थी। मैंने नवीं कक्षा में पढ़ते हुए अपने ही घर से अपनी भतीजी की शादी में दो रात बारात को रोकने की परंपरा को तोड़ दिया। भाई से इस काम के लिए पिटाई भी खाई। गांव वालों ने भी भांति-भांति से बुराई की किन्तु 2-3 वर्ष बाद ही मेरे इस काम की खूब प्रशंसा हुई। उस समय में बारहवीं पास करके नौकरी की तलाश में दिल्ली आ चुका था। इस खुशी का आभास तब हुआ जब मैं दिल्ली से गांव लौंट कर वापस गया था। अब परम्पराओं को तोड़ने की ओर मेरा साहस और बढ़ गया। अभी मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी।
खैर! मेरे दिल्ली में आने के बाद भी बड़े भाई ने मेरी शादी करने जिद नहीं छोड़ी और एक दिन वो शादी का प्रस्ताव लेकर दिल्ली आ गए। मेरे मना करने पर बाद में मेरे गांव के पड़ोसी सठला कस्बे के एक पंडित जी आ गए (जो भाई सहाब के मित्र थे।) और करने लगे शादी कराने की बात। पर मैं नहीं माना। किंतु बात खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि मेरे बड़े भाई ने मेरी सगाई का शगुन ले लिया है। लड़की वालों को भी न जाने क्या जल्दी थी कि बिना लड़के यानी मुझे देखे बिना ही मेरी गैरहाजरी में रिश्ता पक्का करके चले गए।
फलत: 13 मई 1973 को मेरी शादी कर दी गई।बाद में मैं पत्नी को दिल्ली ले आया। आत्मकथाकार दिल्ली तो आ गए लेकिन गांव और गांव वालों से अब भी रिश्ते बरकरार थे। रिश्तेदारों को वे 6-7 पृष्ठ के पत्र लिखा करते थे। पत्र लिखने का तेजपाल सिंह ने पुराना शौक बताया है। वे बताते हैं, जब मैं गांव में रहता था तब कभी-कभी गांव के लोग भी अपने ख़त लिखवाने आ जाया करते थे। इस प्रकार समाज की समस्याओं से मेरा नाता जुड़ता चला गया।
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कालेज में मुझे ही नहीं किसी को भी कोई जातीय दुराव देखने को नहीं मिला जबकि मेरे कालेज में तीन-चार अध्यापकों को छोड़कर शेष सभी अध्यापक ब्राह्मण थे। लेकिन उनमें जाति भेद से इतर गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के प्रति एक अजीव सी सद्भावना थी कि वे उनकी हर संभव मदद किया करते थे। छात्र भी जाति-भेद की भावना से परे एक साथ मिलकर रहते थे। महज संस्कृत के अध्यापक ही ऐसे थे जिनके दिमाग में जाति-भेद कूट-कूट भरा था।
किंतु दिल्ली आने के बाद मनुवादी दुराचरण गहरे से देखने को मिला। यह बात अलग है कि मैं यहां भी इसकी गिरफ्त से परे ही रहा। किंतु शासन-प्रशासन की घनी आबादी (अनाधिकृत) वाली बस्तियों के प्रति अनेक प्रकार की हो रही अनदेखी दिल को सालती रहती थी। सरकारी शिक्षा संस्थानों की दुर्दशा, बिजली की आँख-मिचौनी, बस्तियों की ऊबड़-खाबड़ गलियां होना जैसे आम बात थी और आज भी है। वैसे इस सब अव्यवस्था का कारण जनता का चुप रहकर मुश्किलों को झेलते रहना ही है ।
ऐसे में देश की न्यायपालिका और विधायिका जैसी संवैधानिक संस्थाएं आजकल जनता की अभिभावक होने की भूमिका का निर्वाह करने में कमजोर ही नहीं हो गई है बल्कि संज्ञा-शून्य हो गई हैं। गरीब और निरीह जनता के सामने दो ही विकल्प बचे थे। पहला विकल्प तो यही बनता है कि वे सरकारी/राजनीतिक झूठे और खोखले वायदों की बैसाखियां फेंक दें और मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए सामूहिक रूप से सड़कों पर निकल पड़े।
तेजपाल सिंह ‘तेज’ की आत्मकथा के दूसरे अध्याय में उनके साहित्यिक सफर का उल्लेखन है। इस अध्याय में वे अपनी रचना प्रक्रिया और रचना धर्मिता की भी चर्चा है जिसकी एक समग्र भावभूमि उनकी किताबों के शीषर्क भर महसूस होने लगेगी। अत: उनकी रचना प्रक्रिया और रचना धर्मिता की के इतर उनकी किताबों का ही उल्लेख किया जा रहा है। उनकी ग़ज़ल, कविता, और विचार-विमर्श की लगभग दो दर्जन से भी अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं – दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है,गुजरा हूँ जिधर से,ट्रैफिक जाम है , हादसों के शहर में, तूंफ़ाँ की ज़द में तथा चलते-चलते (6 ग़ज़ल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा(कविता संग्रह), रुन-झुन, खेल-खेल में, धमाचौकड़ी, खेल-खेल में अक्षर ज्ञान (बालगीत : दो खंड), कहाँ गई वो दिल्ली वाली (शब्द चित्र), सात निबन्ध संग्रह – शिक्षा मीडिया और राजनीति, दलित-साहित्य और राजनीति के सामाजिक सरोकार, राजनीति का समाज शास्त्र, लोक से विमुख होता तंत्र,मौजूदा राजनीति में लोकतंत्र, राजनीति और मानवाधिकार के प्रश्न और कानया की वापसी (लघु नाटिका) – (इसके पांच कड़ियो का टी वी सीरियल बन चुका है?)। अब ये पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है। तीन कविता संग्रहों और माननीय शिक्षाविद आर. सी. भारती जी की आत्मकथा का सम्पादन कार्य भी किया। तेजपाल सिंह ‘तेज’ साप्ताहिक पत्र ‘ग्रीन सत्ता’ के साहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका ‘अपेक्षा’ के उपसंपादक, ‘आजीवक विजन’ (पत्रिक) के प्रधान संपादक तथा ‘अधिकार दर्पण’ नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन के रत हैं। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार ( 1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। और भी अनेक नागरिक व सामाजिक सम्मान से सम्मानित। एस. एन. के. पी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सह आचार्य (हिंदी विभाग) में तैनात माननीय देवी प्रसाद जी द्वारा लिखित “ तेजपाल सिंह ‘तेज’ के काव्यमें जन सरोकार” शीर्षांकित पुस्तक का भी वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई। विदित हो कि तेजपाल सिंह ‘तेज’ की चार किताबें आडियो के रूप में कूकू एफ. एम. से भी प्रसारित हो चुकी हैं।
आत्मवृत्त भाग – 2 में वे लिखते हैं, कोई माने या न माने, जानते सब हैं कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसके बीच हमेशा जातिगत विद्वेष रहा है। सच तो ये है कि भारतीय जन-समूह में अलग-अलग प्रकार की अनेक जातियां है। वे दलित-दमित लोगों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते है। यही हिन्दू-धर्म में निरंतर विघटन का कारण रहा है और आज भी है। स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच की सामाजिक असमानता ने ही धर्म परिवर्तन में चार-चाँद लगाए हैं। किंतु हिन्दू कट्टरपंथी इस ओर से आंखें मूंदें हुए हैं।
कितना अफसोसनाक सत्य है कि एक हिन्दू, दूसरे हिन्दू के प्रति मुख्यतः हिन्दुत्व की भावना से व्यवहार करता है। किंतु अपने ही धर्म के अस्पृश्य हिन्दुओं के साथ जाति-भावना से व्यवहार करता है। फिर हिन्दू धर्म में कैसा भी विघटन क्यूं न होता रहे? खेद की बात तो ये है कि हिन्दूवादी संगठन तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए छोटे से छोटे सीरियल में हिन्दू-धर्म के तमाम देवी-देवताओं के करिश्मे दिखाकर समाज के गरीब और निरीह तबके के हृदयों में डर बिठाकर हिन्दू-धर्म में जारी विघटन की प्रक्रिया को रोकने का निरंतर और भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जो करना चाहिए उसकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है।
बकौल ईश कुमार गंगानिया आमतौर पर सरकारी कर्मचारी अपने आसपास हो रही अनियमितताओं या समस्याओं पर चुप्पी साधे रखता है। किसी प्रकार के पत्राचार से डरता है। लेकिन टी पी सिंह इस मामले में एक अपवाद हैं। उन्होंने सारे मिथकों को तोड़कर ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जिस पर दस्तक न दी हो। दरवाजे के पीछे भले ही कोई विधायक, सांसद, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष ही क्यूं न हो, टी पी सिंह ने अपनी बात डंके चोट पर रखी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर तक की शिकायत इलेक्शन कमीशनर टी एन शेषन को कर दी थी। उसमें बताया कि इस समय डा. अम्बेडकरका टिकट का जारी करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने इसे दलितों का शोषण करार दिया और इसे रोकने का आग्रह किया। वे अटल बिहारी वाजपेयी के बुद्धिस्टों को आरक्षण के विरोध पर भी चुप नहीं बैठे और अपनी कलम चला दी। इसके साथ वे एक अन्य पत्र में एतराज जाहिर करते हैं कि डा. बी. आर. अम्बेडकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था, लेकिन प्रचलन में क्यूं नहीं आया, इस पर सवाल उठाते हैं और वस्तुस्थिति की समीक्षा की आह्वान करते हैं।
आत्मवृत्त भाग 2 में लेखक ने कुछ सवाल किए हैं वे सवाल सरकार से भी है। और सरकार से भी हैं। कहना न होगा कि दोनों भाग में कुछ पत्र भी हैं। कहना न होगा कि दोनों भाग की आत्मकथा घटनाओं और दुर्घटनाओं से ओतप्रोत है। जैसा जीवन जिया वैसा लिखा। जीवन में जो भी रंग आए उनका चित्रण किया। यही उनकी खूबी रही। विचार प्रधान उनकी यह आत्मकथा बहुत कुछ कहती है।
आत्मकथा गद्य का वह रूप है जिसमें लेखक अपने जीवन-संघर्ष, उतार-चढ़ाव, गुणों-अवगुणों, सफलता-असफलताओं, पारिवारिक परिस्थितियों, परिवेश, योग्यता, कठिनाइयों, उपलब्धियों एवं अपने प्रेरणा स्रोतों आदि का स्वयं निःसंकोच भाव से यथार्थ रूप में कलात्मक लेखन करता है। तेजपाल सिंह ‘तेज’ की आत्मकथा इन माण्दण्डों पर खरी उतरती है, ऐसा मुझे लगता है।
- मोहनदास नैमिशराय
B. G. 5 A 30 - B, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110063 मोबाइल 88600 74922