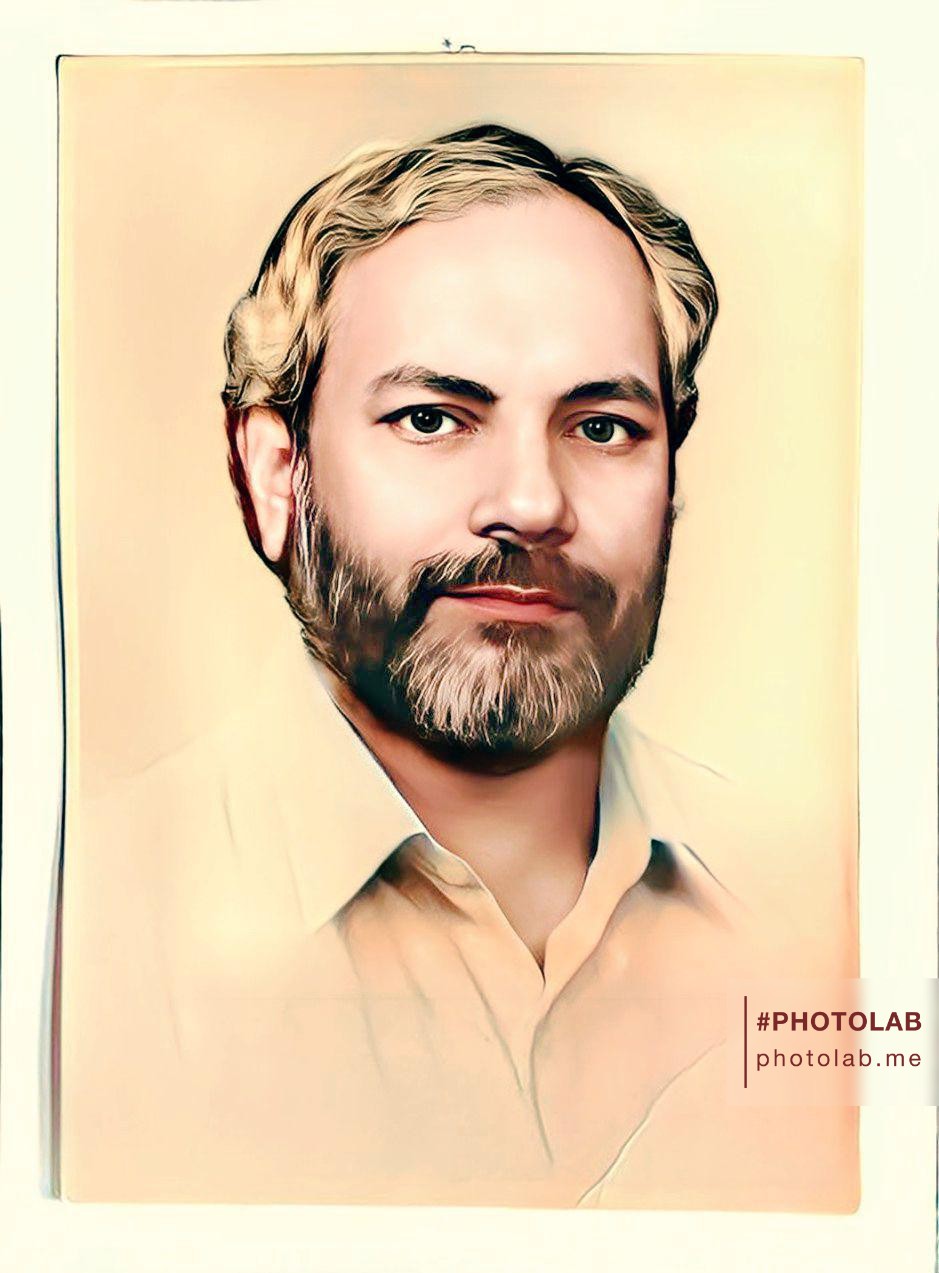तेजपाल सिंह 'तेज' : हिंदू राष्ट्रवाद का राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप
हिंदू राष्ट्रवाद का राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप
हिंदू राष्ट्रवाद — एक विमर्श का उदय
भारत, एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और विविधतापूर्ण राष्ट्र रहा है, जिसकी पहचान उसके लोकतांत्रिक ढांचे और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से बनी है। परंतु हाल के दशकों में एक वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जिसने न केवल भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, बल्कि समाज और संस्कृति की धारणाओं को भी पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की है। हिंदू राष्ट्रवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल की प्रतिक्रियाओं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण की बहसों में खोजी जा सकती हैं, परंतु उसका वर्तमान स्वरूप कहीं अधिक संगठित, मुखर और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो गया है। यह विचारधारा स्वयं को भारत की 'मूल सांस्कृतिक चेतना' के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है, किंतु आलोचकों का मानना है कि यह देश की बहुलतावादी आत्मा के विरुद्ध जाती है।
इस निबंध में हम हिंदू राष्ट्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैचारिक आधार, राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक प्रभाव और आलोचनात्मक दृष्टिकोणों की पड़ताल करेंगे। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यह विचारधारा भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं के साथ किस प्रकार संवाद या संघर्ष करती है। यदि आप चाहें, तो मैं इस प्रस्तावना को अधिक भावप्रवण, आलोचनात्मक या तटस्थ शैली में भी संशोधित कर सकता हूँ — यह आपकी निबंध की दिशा पर निर्भर करेगा।
हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन हैं?
हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं की सूची इतिहास और वर्तमान दोनों में फैली हुई है। इनमें से कुछ वैचारिक नेतृत्व प्रदान करते हैं, जबकि कुछ ने संगठनात्मक और राजनीतिक मोर्चे पर हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। इन्हें तीन broadly श्रेणियों में समझा जा सकता है: वैचारिक प्रवर्तक, संगठनात्मक नेता, और राजनीतिक नेता।
1. वैचारिक प्रवर्तक (Ideological Architects)
·वी. डी. सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) : हिंदू राष्ट्रवाद के सबसे प्रारंभिक और प्रभावशाली वैचारिक नेताओं में से एक। उन्होंने "हिंदुत्व" शब्द को परिभाषित किया और 1923 की पुस्तक "Hindutva: Who is a Hindu?" में भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में कल्पित किया। सावरकर का दृष्टिकोण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित था, जो मुस्लिम और ईसाई समुदायों को 'विदेशी' मानता था।
·एम. एस. गोलवलकर (M. S. Golwalkar, ‘Guruji’) : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दूसरे सरसंघचालक। उनकी पुस्तक "We or Our Nationhood Defined" (1939) हिंदू राष्ट्रवाद की कट्टर वैचारिकी का आधार बनी। उन्होंने भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया जिसमें अल्पसंख्यकों को "राष्ट्र के अधीन" रहना चाहिए।
2. संगठनात्मक नेता (Organizational Leaders)
·डॉ. के. बी. हेडगेवार RSS के संस्थापक (1925) : हिंदू समाज को संगठित कर एक अनुशासित 'राष्ट्र' बनाने का सपना। ब्रिटिश विरोधी थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा की रक्षा थी।
·बालासाहब देवरस गोलवलकर के बाद RSS प्रमुख बने। उनके कार्यकाल में RSS ने राजनीतिक गतिविधियों में परोक्ष भूमिका निभाना शुरू किया और जनता पार्टी में शामिल हुआ।
·मोहन भागवत (वर्तमान) वर्तमान RSS प्रमुख: हिंदू राष्ट्र को "भारतीय राष्ट्र" के समकक्ष बताते हैं, किंतु अपेक्षाकृत लचीली भाषा में। हाल के वर्षों में सामाजिक समरसता और दलितों के प्रति ‘सौम्य’ भाषा का प्रयोग करते रहे हैं।
3. राजनीतिक नेता (Political Leaders)
·अटल बिहारी वाजपेयी : भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संस्थापक नेताओं में से विशेष प्रतिनिधि रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुत्व को संयमित भाषा में प्रस्तुत किया।
·लालकृष्ण आडवाणी : 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन और रथ यात्रा के मुख्य रणनीतिकार। हिंदू राष्ट्रवाद को एक उग्र जन आंदोलन में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई।
·नरेंद्र मोदी : वर्तमान प्रधानमंत्री (2014–वर्तमान), जिन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को मुख्यधारा की राजनीति में पूरी तरह स्थापित किया। ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के साथ, वे हिंदुत्व की वैचारिकी को आधुनिक प्रशासन, सुरक्षा और विकास से जोड़ते हैं। उनके कार्यकाल में CAA, NRC, राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना जैसे निर्णय हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखे जाते हैं।
इन लोगों के अलावा अन्य उल्लेखनीय नाम ये भी हैं :
·योगी आदित्यनाथ – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिन्दू राष्ट्रवाद के कठोर स्वर के प्रवक्ता हैं।
·प्रवीण तोगड़िया – विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता, आक्रामक हिंदुत्व की शैली के लिए जाने जाते हैं।
·सुब्रमण्यम स्वामी – वैचारिक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद के पक्षधर, कानूनी और राजनीतिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं। राजनीति के मैंदान में वे अधिकतर मोदी जी की खिलाफ़त करते देखे जाते हैं।
हिंदू राष्ट्रवाद राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे प्रभावित करता है?
हिंदू राष्ट्रवाद ने भारत की राजनीति और संस्कृति दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। यह प्रभाव केवल किसी पार्टी की सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सोच, स्मृति और सामूहिक चेतना में धीरे-धीरे समाहित होता जा रहा है। नीचे इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के दो प्रमुख आयामों में समझा जा सकता है:
1. राजनीतिक प्रभाव
(क) राजनीतिक विमर्श का धार्मिककरण : हिंदू राष्ट्रवाद ने धर्म को राजनीतिक एजेंडे का केन्द्रीय बिंदु बना दिया है। चुनावों में मंदिर, गौ-रक्षा, लव जिहाद, घर वापसी जैसे मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं।
(ख) धर्मनिरपेक्षता की पुनर्परिभाषा : धर्मनिरपेक्षता को अब 'तुष्टिकरण' कह कर खारिज किया जाता है। इसके स्थान पर 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' को वैध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका असर यह हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष दल भी अब हिंदू प्रतीकों (जैसे मंदिर दर्शन, जनेऊ, गोत्र) का सहारा लेने लगे हैं।
(ग) राज्य की नीतियों में धार्मिक आग्रह : नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), तीन तलाक पर कानून, और राम मंदिर निर्माण जैसे निर्णय हिंदू राष्ट्रवाद की वैचारिक प्रेरणाओं से जुड़े हैं। सरकारी अनुदानों और पाठ्यक्रमों में भी धार्मिक दृष्टिकोण परोक्ष रूप से सम्मिलित होने लगे हैं।
(घ) अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हाशियाकरण: मुस्लिम और ईसाई समुदायों की राजनीतिक भागीदारी घट रही है।उनकी देशभक्ति को संदेह के दायरे में रखने का चलन बढ़ा है (जैसे 'भारत माता की जय' या 'वंदे मातरम्' जैसे नारों को अनिवार्य बनाना)।
2. सांस्कृतिक प्रभाव
(क) इतिहास का पुनर्लेखन : हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इतिहास को “गौरवशाली हिन्दू अतीत” के रूप में पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। मुगलों और ब्रिटिश शासन को 'विध्वंसक' के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि प्राचीन भारत को स्वर्ण युग के रूप में दिखाया जाता है।
(ख) त्योहारों और प्रतीकों का राजनीतिकरण: राम नवमी, हनुमान जयंती, और अन्य धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक शक्ति-प्रदर्शन का माध्यम बना दिया गया है। भगवा रंग, राम और शिव की छवियाँ अब केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी बन गई हैं।
(ग) संस्कृति में "अपनों" और "परायों" का निर्माण : खान-पान (बीफ पर बैन), पहनावा (हिजाब विवाद), और जीवनशैली (लव जिहाद का विमर्श) जैसे निजी मुद्दे अब सांस्कृतिक युद्ध का हिस्सा बन गए हैं। इससे बहुलतावादी संस्कृति संकुचित होती जा रही है।
(घ) मीडिया और सिनेमा में बदलाव : फिल्मों में 'राष्ट्रवादी' नायकों और 'आक्रामक राष्ट्रप्रेम' की लोकप्रियता बढ़ी है (उरी, द कश्मीर फाइल्स, The Kerala Story आदि)। समाचार चैनल भी सांप्रदायिक मुद्दों को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
हिंदू राष्ट्रवाद भारत की राजनीति को धर्म-आधारित पहचान की ओर, और संस्कृति को एकरूपता की ओर ढकेलता है। यह विचारधारा लोकतंत्र की बहुलतावादी प्रकृति के सामने एक वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करती है, जो बहुसंख्यकवाद पर आधारित है।
जहाँ एक पक्ष इसे "राष्ट्र की आत्मा की पुनर्रचना" मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे "लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती" के रूप में देखता है।
सांप्रदायिक तनाव में हिंदू राष्ट्रवाद की भूमिका क्या है?
सांप्रदायिक तनाव में हिंदू राष्ट्रवाद की भूमिका एक अत्यंत संवेदनशील, परंतु आवश्यक रूप से विश्लेषणीय विषय है। हिंदू राष्ट्रवाद, जब राजनीति और समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगता है, तो वह धर्म को केवल सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे राष्ट्र-निर्माण और पहचान की केंद्रीय कसौटी बना देता है। यही दृष्टिकोण सांप्रदायिक तनावों को जन्म देने या उन्हें भड़काने में भूमिका निभाता है। नीचे इसे विस्तार से समझा जा सकता है:
1. बहुसंख्यक पहचान को राष्ट्र की पहचान के रूप में प्रस्तुत करना: हिंदू राष्ट्रवाद का मूल तर्क यह है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और यह भूमि हिंदू धर्म की उत्पत्ति स्थली है। इस विचार में अल्पसंख्यक (विशेषकर मुस्लिम और ईसाई) समुदायों को "बाहरी", "विदेशी" या "कम विश्वसनीय" नागरिक के रूप में देखा जाता है। यह सोच सामाजिक असमानता और अविश्वास को जन्म देती है, जो सांप्रदायिक तनाव की आधारशिला बनती है।
2. सांप्रदायिक घटनाओं के राजनीतिक लाभ: राम जन्मभूमि आंदोलन (1990s), गोधरा कांड और गुजरात दंगे (2002), मुजफ्फरनगर दंगे (2013), और दिल्ली दंगे (2020) जैसी घटनाओं के पीछे धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति देखी गई है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक समुदाय विशेष को "सुरक्षा की आवश्यकता" का संदेश देकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। उदाहरणार्थ लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ सांप्रदायिक तनाव और चुनावी लाभ दोनों जुड़े थे।
3. प्रतीकों और भावनाओं का राजनीतिक दोहन : "जय श्री राम" जैसे नारों का इस्तेमाल अब केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांप्रदायिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में होता है। धार्मिक जुलूसों में तलवारें, भड़काऊ भाषण, और आक्रामक नारों का उपयोग सांप्रदायिक तनाव को तेज करता है। 2023–24 में देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी या हनुमान जयंती पर जुलूसों के दौरान दंगे इसी पृष्ठभूमि में हुए।
4. इतिहास और शिक्षा के माध्यम से वैमनस्य फैलाना : मुगलों और मुस्लिम शासकों को 'आक्रांता' या 'विधर्मी' के रूप में चित्रित कर इतिहास को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों और लोकप्रिय मीडिया में "हम बनाम वे" की मानसिकता पनपती है। इससे नई पीढ़ी में भी धार्मिक कटुता का निर्माण होता है।
5. ‘लव जिहाद’, ‘घर वापसी’, ‘लैंड जिहाद’ जैसे नैरेटिव्स: इन अभियानों का मकसद यह दिखाना होता है कि मुस्लिम समुदाय "षड्यंत्रपूर्वक" हिंदू धर्म या संस्कृति को कमजोर कर रहा है। ये कथाएं आम जनमानस में भय और घृणा की भावना उत्पन्न करती हैं और सामाजिक समरसता को तोड़ती हैं।
6. पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर असर : कई मामलों में आरोप लगाया गया है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस एकतरफा कार्रवाई करती है या मूकदर्शक बनी रहती है। यह असंतुलन हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों को सामाजिक नियंत्रण का अधिक अवसर देता है। उदाहरणार्थ 2020 दिल्ली दंगों में पुलिस की भूमिका पर कई मानवाधिकार संगठनों ने प्रश्न उठाए।
हिंदू राष्ट्रवाद, जब बहुसंख्यक वर्चस्व की विचारधारा बन जाता है, तो वह धार्मिक सह-अस्तित्व के स्थान पर प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और घृणा को बढ़ावा देता है।इससे सांप्रदायिक तनाव केवल अस्थायी टकराव नहीं रहते, बल्कि सामाजिक संरचना का स्थायी संकट बन जाते हैं।
भाजपा की हिंदू-मुस्लिम राजनीति और देश की वर्तमान स्थिति
आज का भारत एक विचित्र द्वंद्व से गुजर रहा है। एक ओर देश 'विकास', 'विज्ञान' और 'विश्वगुरु' बनने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर उसकी राजनीतिक धारा समाज को धार्मिक खांचों में बाँटने में व्यस्त है। इस धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का केंद्र भाजपा रही है, जिसने पिछले एक दशक में हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को जिस ढंग से उभारा है, उसने भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक समरसता को गहरे संकट में डाल दिया है।
1. धर्म की राजनीति: विकास से विमुखता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजनीति में हिंदू पहचान को केंद्र में रखकर जो रणनीति अपनाई है, उसने मुसलमानों को 'अन्य' और 'विरोधी' की तरह प्रस्तुत किया है। हर चुनाव के दौरान 'लव जिहाद', 'घर वापसी', 'गो-रक्षा', 'हज सब्सिडी', 'राम मंदिर' जैसे मुद्दे मुख्य बहस का हिस्सा बने हैं। यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया रही है जिसमें वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई को पीछे धकेल दिया गया है। जब राजनीति धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तब विकास एक नारे में सिमट कर रह जाता है। भारत की गिरती जीडीपी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की उपेक्षा, तथा बढ़ती बेरोजगारी इसका प्रमाण हैं। लेकिन इन समस्याओं की ओर ध्यान न जाकर बहस इस बात पर केंद्रित रहती है कि मुसलमान 'वंदे मातरम्' क्यों नहीं गाते या मस्जिद में लाउडस्पीकर क्यों बजता है।
2. सामाजिक सौहार्द्र पर हमला: भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति ने देश में आपसी विश्वास को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। देश के अनेक हिस्सों में दंगे, मॉब लिंचिंग, धार्मिक नफ़रत की घटनाएं बढ़ी हैं। मुसलमानों को संदेह की निगाह से देखा जाने लगा है — चाहे वह नागरिकता कानून (CAA/NRC) का मामला हो या धर्मांतरण कानूनों का। इस धार्मिक ध्रुवीकरण ने हिंदू समाज में भी एक तरह की कठोरता और असहिष्णुता को जन्म दिया है। आलोचना को 'देशद्रोह' और असहमति को 'गद्दारी' से जोड़ दिया गया है। यह लोकतंत्र नहीं, अधिनायकवाद की ओर बढ़ने का संकेत है।
3. लोकतंत्र की कमजोर होती नींव: भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की नींव पर खड़ा है, लेकिन भाजपा की राजनीति इस नींव को बार-बार चुनौती देती है। न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, लेकिन वे या तो मौन रहते हैं या सत्ताधारी पार्टी की लाइन पर चलते हैं। धर्म के नाम पर सत्ता प्राप्त करना लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि यह जनता को सोचने, सवाल पूछने और विकल्प चुनने के अधिकार से वंचित करता है। जब हिंदू-मुस्लिम विभाजन ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन जाए, तब लोकतांत्रिक मूल्य धीरे-धीरे दम तोड़ने लगते हैं।
4. भविष्य की दिशा: चेतना की आवश्यकता: भारत की आत्मा विविधता में एकता है। यदि हम इसे धर्म और जाति के नाम पर बाँटते रहेंगे, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जाएँगे। भाजपा की धार्मिक राजनीति ने हमें चेताया है कि जब नागरिकता से अधिक धर्म की पहचान महत्वपूर्ण हो जाए, तो देश गर्त की ओर ही बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि जनता धार्मिक भावनाओं में बहने की बजाय वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे — जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान और मजदूरों की हालत। एक सजग नागरिक ही इस धार्मिक विभाजनकारी राजनीति का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। भाजपा की हिंदू-मुस्लिम राजनीति ने न केवल सामाजिक ताने-बाने को क्षति पहुँचाई है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा को भी कमजोर किया है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यदि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक प्रगतिशील राष्ट्र के बजाय एक विभाजित समाज बनकर रह जाएँगे।
भाजपा की हिंदू-मुस्लिम राजनीति और भारतीय लोकतंत्र का पतन:
“यदि भारतीय राष्ट्र एक हिन्दू राष्ट्र बनता है, तो यह इस उपमहाद्वीप के लिए एक विनाशकारी आपदा होगी। यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं हिन्दुओं के लिए भी घातक सिद्ध होगा।” — डॉ. भीमराव आंबेडकर, “थॉट्स ऑन पाकिस्तान” (1940)
धर्म का राजनीतिकरण और लोकतंत्र की गिरती छाया:
आज का भारत न केवल आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है, बल्कि एक गहरे वैचारिक और नैतिक संकट में भी है। यह संकट धर्म और राजनीति के घातक संधि-बिंदु पर केंद्रित है — विशेषकर उस राजनीति पर, जो धार्मिक पहचान को वोट बैंक में बदल देती है। पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'हिंदू एकता' के नाम पर 'मुस्लिम विरोध' की राजनीति को जिस प्रकार संस्थागत स्वरूप दिया है, उसने भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को विकृत किया है। यह केवल एक दल की रणनीति नहीं, बल्कि एक पूरे लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा पर आघात है।
1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: धार्मिक राष्ट्रवाद की जड़ें: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल स्वभाव धर्मनिरपेक्ष था। गांधी, नेहरू, आंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने धार्मिक विभाजन के विरोध में आवाज़ उठाई थी। परंतु, स्वतंत्रता संग्राम के समानांतर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे संगठनों ने 'हिंदू राष्ट्र' की परिकल्पना को पोषित किया। 1947 के बाद संघ का विचार धीरे-धीरे राजनीति में पाँव जमाने लगा। भाजपा, जो 1980 में बनी, ने 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन के माध्यम से धार्मिक मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में ला खड़ा किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) कोई दुर्घटना नहीं थी — यह उस वैचारिक परियोजना का हिस्सा थी जिसमें अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश थी।
2. वर्तमान राजनीति: मुद्दों का धार्मिक ध्रुवीकरण: भाजपा की राजनीति अब एक “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” के नाम पर समाज को बांटने वाली राजनीति बन चुकी है। इसका सबसे प्रभावी हथियार है— हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण। प्रत्येक चुनाव में भाजपा द्वारा कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जो धार्मिक ध्रुवीकरण को तेज करे:
·2014 में “पिंक रेवोल्यूशन” (गोमांस निर्यात),
·2017 में “लव जिहाद” और “कब्रिस्तान-श्मशान”,
·2019 में बालाकोट स्ट्राइक और राष्ट्रीय सुरक्षा,
·2024 में राम मंदिर और मुस्लिम आरक्षण।
इन सभी मुद्दों का मूल उद्देश्य है— हिंदू बहुसंख्यक भावनाओं को भड़काना और मुसलमानों को शत्रु के रूप में प्रस्तुत करना। यदि इसे सांख्यिकीय दृष्टि से देखें तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं 2014 के बाद तीन गुना बढ़ीं (India Spend रिपोर्ट)। 90% पीड़ित मुसलमान हैं।
धार्मिक नफरत फैलाने के मामलों में 2014 से 2024 तक FIRs में 300% वृद्धि हुई (NCRB डेटा)।
3. डॉ. आंबेडकर का दृष्टिकोण: चेतावनी और समाधान: डॉ. आंबेडकर बार-बार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि लोकतंत्र केवल मतपत्र की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नैतिक अनुशासन है - जिसमें समानता, बंधुता और न्याय की भावना होनी चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि “धर्म का राज्य से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।” "राज्य को पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। किसी भी धर्म को न राज्य का संरक्षण मिले, न विरोध। यही धर्मनिरपेक्षता की आत्मा है।" — डॉ. आंबेडकर, संविधान सभा वाद-विवाद, 1949
परंतु आज भारत की राजनीतिक सत्ता (भाजपा) धर्म के नाम पर न केवल संरक्षण कर रही है, बल्कि एक विशिष्ट धर्म (हिंदू धर्म) की श्रेष्ठता स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इससे भारत न केवल 'संविधान-विरोधी' रास्ते पर बढ़ रहा है, बल्कि सामाजिक विद्वेष और द्वेष की आग में झुलसता जा रहा है।
4. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: जनता के मुद्दों से भटकाव: जब समाज धार्मिक आधार पर विभाजित हो जाता है, तब आर्थिक सवाल अप्रासंगिक हो जाते हैं। भाजपा की धार्मिक राजनीति ने आमजन के सामने “रोटी या राम” का सवाल रखा — और चतुराई से यह सुनिश्चित किया कि जनता बार-बार ‘राम’ को चुने। शिक्षा, गरीबी और स्वास्थ्य की दृष्टि दे देखें तो भारत की बेरोजगारी दर 8% के पार (CMIE, 2024), ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में 30% डॉक्टरों की कमी और शिक्षा बजट लगातार घट रहा है। जो देश के स्वास्थय में गिरावट के संकेत हैं। इन वास्तविक मुद्दों पर बहस गायब है। मीडिया भी भाजपा की “धर्म-नीति” का अनुचर बन गया है। सरकार के विरुद्ध बोलने वालों को 'देशद्रोही' और 'अर्बन नक्सल' कहा जाने लगा है।
5. धार्मिक राजनीति के विरुद्ध जनचेतना: भारत जैसे बहुलतावादी देश के लिए धर्म और राजनीति का गठजोड़ आत्मघाती है। भाजपा की हिंदू-मुस्लिम राजनीति ने लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक सौहार्द को गहरे संकट में डाल दिया है। इस संकट से निकलने का रास्ता केवल एक सजग, संवेदनशील और वैचारिक रूप से सजग नागरिक समाज ही दे सकता है। आंबेडकर की चेतावनी आज पहले से अधिक प्रासंगिक है — यदि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं करेंगे, तो न तो समाज बचेगा, न संविधान, और न ही लोकतंत्र। आवश्यकता तो इस बात की है कि धर्म नहीं, नीति ही राजनीति का आधार हो। भाजपा की राजनीति ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं जब वे सत्ता की भूख से जुड़ जाएं। अब यह जनता पर है कि वह “धार्मिक उन्माद” को त्यागकर “जननीति और जनहित” की ओर लौटे। भारत को अगर गर्त से निकलना है, तो उसे फिर से आंबेडकर, गांधी और नेहरू की धर्मनिरपेक्ष परंपरा की ओर लौटना होगा।
दलित-मुस्लिम की स्थिति: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाजपा की हिंदू-मुस्लिम राजनीति के संदर्भ में दलित और मुस्लिमों की साझा सामाजिक स्थिति पर विचार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि किस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण ने समाज के सबसे वंचित तबकों को और अधिक असुरक्षित तथा राजनीतिक रूप से हाशिये पर ढकेल दिया है। इसका विश्लेषण करने के भाव से हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं:
1. दलित और मुसलमान — समान सामाजिक पीड़ा: भारत के दो सबसे बड़े वंचित समुदाय — दलित (अनुसूचित जातियाँ) और मुसलमान — सामाजिक-आर्थिक रूप से लगभग समान पीड़ा के शिकार हैं। इन वर्गो सामाजिक अवस्था निम्न बिंदुओं से सहज ही आँकी जा सकती है।
·दलितों की साक्षरता दर केवल 66% और मुस्लिमों की 68% है। (स्रोत: NSSO और 2011 जनगणना)
·औसत मासिक घरेलू आय: दलित परिवारों की ₹7,000 - ₹8,000 तो मुस्लिमों की परिवारों की ₹6,000 - ₹7,000 है। (Azim Premji University की रिपोर्ट, 2022)
श्रमिक और असंगठित क्षेत्र:
दोनों समुदायों के 80% से अधिक लोग असंगठित मजदूरी में हैं — जैसे सफाई, निर्माण, घरेलू काम, दर्जी, रिक्शा चालक आदि। ये आँकड़े दिखाते हैं कि भले ही धार्मिक पहचान अलग हो, लेकिन दलित और मुस्लिम दोनों ही 'हाशिये' पर हैं — शिक्षा, आय,