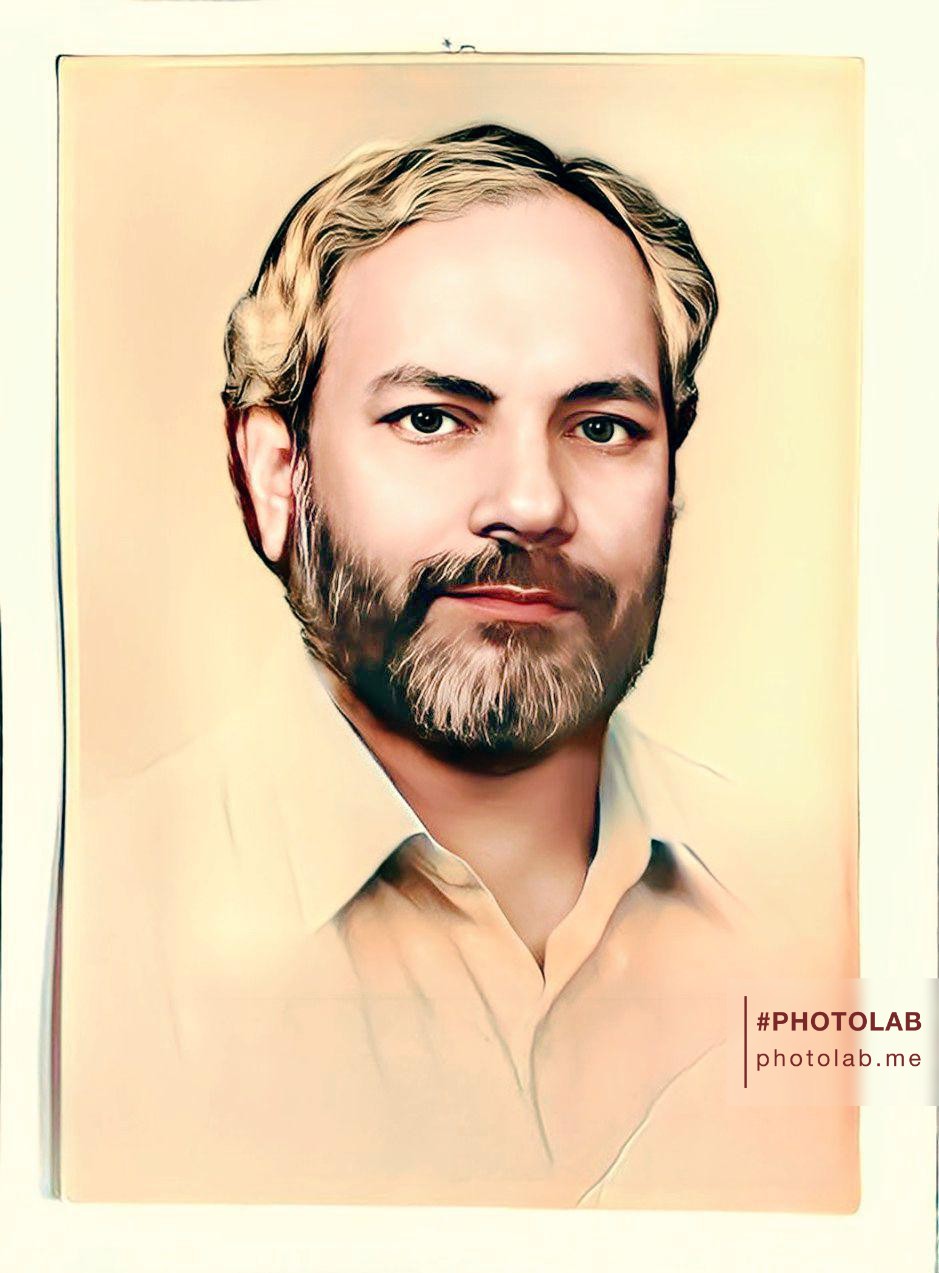प्रस्तुति : तेजपाल सिंह ‘तेज’
धृतराष्ट्रवाद का वर्तमान
-ईश कुमार गंगानिया
जब चारों ओर डिजिटल और गैर-डिजिटल पत्र-पत्रिकाओं की भरमार है। न्यूज़ चैनलों ने हमारे जीवन को अपनी कार्यशाला बना लिया है। सोशल मीडिया और यू-ट्यूब अपनी विविधता के साथ अपनी उपस्थिति से नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं। दलित जीवन व उनकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रिकाओं और पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में साहित्य आलोचना के संवाहक ‘अम्बेडकरवादी साहित्य के मुखपत्र’ यानी ‘अपेक्षा’ के पुनर्प्रकाशन को लेकर दिमाग में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। दीगर सवाल यह है कि वर्षों पहले बंद हो चुकी पत्रिका ‘अपेक्षा’ को फिर से शुरू करने की जरूरत क्या है? विशेष रूप से तब जब उस पत्रिका के संस्थापक व मार्गदर्शक डा. तेज सिंह हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। लेकिन उल्लेखनीय हकीकत यह भी है कि शेष टीम अपेक्षा आज इस मुहिम का हिस्सा है।
यकीनन यह वाजिब सवाल है। इसके बावजूद हमारा मानना हैं कि ‘अपेक्षा’ पत्रिका के पुनर्प्रकाशन की बेहद सख्त जरूरत है। दरअसल, अपेक्षा के बंद होने से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जैसे आलोचना के क्षेत्र में एक अजीब-सी रिक्तता ने घर कर लिया है। यह रिक्तता ‘अपेक्षा’ से जुड़े साहित्यकारों को ही नहीं अखरती है बल्कि इसके पाठकों को भी परेशान करती है। उनकी ओर से बराबर मांग उठती रहती है-‘अपेक्षा’ को फिर से शुरू क्यूं नहीं किया जा रहा?‘ पाठकों और साहित्यकारों की ओर से हर प्रकार के सहयोग की पेशकश की कमी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि इसको शुरू करने के लिए अब से पहले कोई प्रयास नहीं किए गए, यकीनन किए गए। लेकिन परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं बन सकी और लगभग सात साल बिना ‘अपेक्षा’ के गुजर गए। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
पहली मुश्किल ‘अपेक्षा’ के नाम से पत्रिका निकाले को लेकर ही शुरू हो गई। हमारा मानना है कि हमारे पाठकों को हकीकत से अवगत होना चाहिए। गौरतलब है कि पांच दिसम्बर 2021 को आलोचना की लोकप्रिय पत्रिका ‘अपेक्षा’ के पुनर्प्रकाशन के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसी दिन मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें यह भी घोषणा की गई थी कि ‘अगर जरूरत पड़ी तो नई पत्रिका के लिए जमीन तैयार होगी।’ इसके बाद से ‘अपेक्षा’ के पुनर्प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग तीन महीने चली। इस दौरान ‘अपेक्षा’ के नाम से ही संपादक मंडल व पत्रिका का मुकम्मल प्रारूप तैयार हुआ। पहले अंक के लिए प्रकाशन सामग्री भी ‘अपेक्षा’ नाम से इस उम्मीद से जुटाई गई कि इसके पुनर्प्रकाशन के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन हमें अफसोस है कि ‘अपेक्षा’ नाम से पत्रिका के पुनर्प्रकाशन के सारे प्रयास नाकामयाब होने की स्थिति में हमें ‘समय संज्ञान’ नाम से और एक प्रकार से नई पत्रिका निकालने का मार्ग अपनाना पड़ा, खैर...।
इस सबके बावजूद टीम ‘समय संज्ञान’ यह आश्वस्त करती है कि ‘अपेक्षा’ की अनुपस्थिति के कारण पैदा हुई शून्यता को भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसकी एक खास वजह यह भी है कि अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परेशानी पैदा करने वाला एक अजीब-सा उर्ध्वाधर बदलाव आ गया है। यह तय है कि ‘समय संज्ञान’ परिवार इस बदलाव के अनुरूप ही अपनी साहित्यिक भूमिका तय करेगा। वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियां इस ओर संकेत कर रही हैं कि जैसे हम ‘धृतराष्ट्रवाद’ का शिकार हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता कि धृतराष्ट्रवाद ने वर्तमान का अपहरण कर लिया है। यह मसला एक दिन का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दूर अतीत तक जाती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो धृतराष्ट्रवाद की गिरफ्त से बाहर हो। अब पाठक के दिमाग पर यह प्रश्न दस्तक दे सकता है कि आखिर ‘धृतराष्ट्रवाद’ है क्या? संभवत: यह पद किसी को भी अपरिचित लग सकता है। इसलिए ‘समय संज्ञान’ और ‘समय संज्ञान की भावी भूमिका’ पर विचार करने से पहले ‘धृतराष्ट्रवाद’ पद से परिचित हो जाना जरूरी हो जाता है।
यह पद ‘धृतराष्ट्रवाद’ अनायास ही अस्तित्व में नहीं आ गया है। इसका उदय वर्तमान के निरंतर अवलोकन, चिंतन-मनन और मूल्यांकन के कारण हुआ है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय हकीकत यह है कि ‘धृतराष्ट्रवाद’ जैसे पद तक पहुंचने में अम्बेडकरवाद हमारी मदद करता है। शायद अम्बेडकरवाद की मदद के बगैर ‘धृतराष्ट्रवाद’ तक नहीं पहुंचा जा सकता था। इसलिए ‘धृतराष्ट्रवाद’ को समझने के साथ-साथ हमें अम्बेडकरवाद को जानना जरूरी है। कहना जरूरी है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के रूप में धृतराष्ट्रवाद का महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र से सीधे-सीधे कोई लेना-देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार अम्बेडकरवाद का सीधे-सीधे डा. अम्बेडकर यानी एक व्यक्ति की निजता से कोई लेना-देना नहीं है। यहां सवाल एक सैद्धांतिकी का है, एक विचारधारा का है और एकवैचारिक प्रतिबद्धता का है।
स्पष्ट करना जरूरी हैं कि अम्बेडकरवाद वह बैनर है जिसमें चार्वाक, लोकायतव तथागत बुद्ध का चिंतन-दर्शन समाहित है। डा.अम्बेडकर, फुले दंपति, पेरियार, सिद्ध, संतआदि अम्बेडकरवाद के ऊर्जा स्त्रोत हैं। विचारधारा के स्तर पर इसमें भगत सिंह, ओशो, एपीजे अब्दुल कलाम, सुकरात, मार्टिन लूथर किंग यानी कोई भी अम्बेडकरवाद का सहमार्गी हो सकता है। गौरतलब है कि इसका आधार मूलतः विचारधारा है, जाति या जातिवाद नहीं। कहना जरूरी है कि अम्बेडकरवाद के बैनर तले लड़ी लाने वाली साहित्यिक जंग सिर्फ और सिर्फ जाति के चश्में से नहीं लड़ी जाने वाली है।
इसका कैनवास बहुत व्यापक है। इसके साथ-साथ यह भी रेखांकित करने वाली हकीकत है कि जाति का प्रश्न इसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। इसकी साफ वजह है कि जाति भारतीय समाज और देश के माथे पर एक बदनुमा दाग है। कई मायने में यह नस्ल भेद व दास प्रथा से ज्यादा घातक है। यह देश और समाज की प्रगतिशीलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां जाति विलेन न बनी हो। इसलिए इस विलेन का खात्मा हमारी पहली चुनौती होगी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अन्य किसी भी विचार को अम्बेडकरवाद का हिस्सा बनने के लिए इसे वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक व मानवीय मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
पुन: मुख्य बिंदु यानी ‘धृतराष्ट्रवाद’ पर आते हैं। दरअसल, धृतराष्ट्रवाद का किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट, बाहरी आवरण व किसी सीमित परिवेश से कोई लेना-देना नहीं होता है। इस प्रवृत्ति के मूल में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इन महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। ये महत्वाकांक्षाएं एक व्यक्ति की हो सकती हैं। ये महत्वाकांक्षाएं किसी वर्ग व समुदाय विशेष की सामूहिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय हकीकत यह भी है कि धृतराष्ट्रवाद कभी अकेला व निहत्था नहीं रहता। यह सदैव धर्म, धृष्टता, सत्ता, साजिश, पूंजी, पूर्वाग्रह आदि जैसे हथियारों से लैस रहता है। इन हथियारों के प्रयोग के लिए उसे किसी कायदे-कानून व बंदिश का डर नहीं रहता। यह कहना गलत नहीं होगा कि नैतिकता और कायदे-कानून को रौंदना इसकी मूल प्रवृत्ति होती है।
इसका मात्र एक ही लक्ष्य रहता है, वह है-अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। इसके पोषक तत्व कोई वाद, धर्म, सत्ता, परंपराएं, पूंजी यानी कुछ भी हो सकता है। मगर ये महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल होती हैं कि इनके चलते किसी व्यक्ति, समाज, देश-दुनिया और मानवता के वजूद तक को चुनौती दी जा सकती है। देश-विदेश का इतिहास ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी खूनी इबारतों से भरा पड़ा है। अपने देश में होने वाले नरसंहारों के पीछे भी यही धृतराष्ट्रवादी मानसिकता काम करती रही है और कमोबेश आज भी कर रही है। मौजूदा संदर्भ में भारत में घुसपैठ कर शासन करने वाले विदेशियों की क्रूरता को भूल जाना अपने आप में बड़ी भूल होगी।
‘धृतराष्ट्रवाद’ को समझने के लिए, न चाहते हुए भी मैं जानबूझकर रामायण व महाभारत को बीच में लाना जरूरी समझ रहा हूं। वजह साफ है कि इनके अनेक किस्से-कहानियां ‘धृतराष्ट्रवाद’ के पोषक हैं और भयंकर विनाश द्योतक भी हैं। यहां मसला कौन ठीक या कौन गलत का कारण तलाशने का नहीं है। मसला एक ‘वाद’ का है जो विनाश करता है। लगता है कि हमारा वर्तमान भी इतिहास जैसे किसी बड़े विनाश के भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इसलिए इस ‘वाद’ की यहां चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि मौजूदा संदर्भ में हमारा आशय रामायण व महाभारत के वजूद या इसके खंडन-मंडन की मुहिम से कोई लेना-देना नहीं है। यहां रामायण व महाभारत के पद का प्रयोग मात्र इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ‘धृतराष्ट्रवाद’ को समझने में सुविधा हो। वरना इसके बगैर भी आसानी से बात की जा सकती थी।
इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हर कोई किसी न किसी रूप में इस ‘धृतराष्ट्रवाद’ का शिकार हैं। कोई इसका राजनीतिक रूप से शिकार है तो कोई आर्थिक रूप से। मगर समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो इनके अतिरिक्त सामाजिक रूप से भी इस धृतराष्ट्रवाद का शिकार है। इस ‘वाद’ के चलते एक बड़े वर्ग को विभिन्न जातियों के घिनौने खांचे में फिट कर दिया गया है। यह वर्ग सदियों से शोषण-उत्पीड़न झेलने को विवश रहा है। इस विवशता से राहत के लिए इस वर्ग की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बेवजह जाति के दैत्य से (खुद के अंदर और बाहर) लड़ने में जाया हो जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति व समाज के उत्थान में किया जा सकता है जो देश की प्रगति व खुशहाली के लिए बेहद कारगर कदम हो सकता है।
जब हम जाति के प्रश्न पर जरा ठहर कर विचार करते हैं तो पाते हैं कि ‘जाति’ एक प्रकार से भारतवासियों के खून का नया हीमोग्लोबिन जैसा अव्यव हो गया है। यह हीमोग्लोबिन गर्भ से सीधे शिशु के शरीर में संचार पाता है। जब यह शिशु परिवार में अपनी आंखें खोलता है तभी से परिवार द्वारा इसका भरण-पोषण इस नवजात शिशु में कोलोस्ट्रम का काम करता है। कोलोस्ट्रम यानी मां का पहला दूध जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह एंटीबॉडी भी खूब बनाता है। इन एंटीबॉडीज का काम शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाना होता है। शारीरिक बीमारियों से बचाव के लिए एंटीबॉडीज की भूमिका काबिल-ए-तारीफ है।
लेकिन जब ये एंटीबॉडीज ‘जाति’ का आवरण ओढ़ लेती हैं तो ये इंसान से इंसान के मिलने को संक्रमण की श्रेणी में रखने का काम करती हैं। आपसी अलगाव व ऊंच-नीच को जन्म देती हैं। शोषण-उत्पीड़न का बाजार गर्म करती हैं। इस प्रकार निर्मित जातिवादी साम्राज्य धृतराष्ट्रवाद का पोषण करता नजर आता है। इस ‘वाद’ के अंतर्गत विवेक और नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। निजी स्वार्थ की पूर्ति के चलते संवेदना जैसी मानवीय अनुभूति का क्षय होता रहता है। अंतत: यह संवेदनहीनता में तब्दील हो जाती है। समता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। न्याय व आपसी भाईचारे से परे समाज एक अराजक अवस्था को प्राप्त होता है। आज का दलित व बहुजन समाज सदियों से इस अराजकता के नए-नए हथकंडे झेलने को बाध्य है।
कुछ समय पहले इस अराजकता से निपटने के लिए एक ठोस विकल्प के रूप में जातीय चेतना की एक अनोखी मुहिम सामने आई। इसके चलते जातीय पहचान को प्राथमिकता दी जाने लगी। जातियों पर गर्व करने और इनके महिमामंडन के नए-नए इतिहास गढ़ने की एक अजीब-सी होड़ आज भी मौजूद है। ‘समय संज्ञान’ परिवार का मानना है कि अम्बेडकरवाद ऐसी किसी भी होड़ की अनुमति नहीं देता है। अम्बेडकरवाद का एक अनिवार्य चिंतन-दर्शन यानी बुद्धिज्म भी इस ‘आग को आग से बुझाने’ को प्रोत्साहित नहीं करता है। यह आग को पानी से बुझाने की बात करता है।
जातीय चेतना की बजाय ‘दलित चेतना’ को प्राथमिकता देना अलग से सवाल खड़ा करता है। अम्बेडकरवादी साहित्य अकेले दलित समाज से जुड़े व्यक्तियों का साहित्य नहीं है; इसमें बहुजन समाज पहले से मौजूद हैं। समाज के किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए भी इसके दरवाजे बंद नहीं हैं। मगर इस मसले में कुछ दिमागी खुलेपन की जरूरत है। इस खुलेपन के मसले को कुछ शब्दों में बांध देना शायद ठीक नहीं है। यकीनन इस पर समय-समय पर विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में संवाद बना रहेगा। जाहिर है, नीयत साफ होगी तो परिणाम सकारात्मक ही होंगे।
‘वर्ग चेतना’ का सवाल भी बहुधा चर्चा के केन्द्र में आता-जाता रहता है। अन्य क्षेत्रों से भी प्रायः इस बात पर बल दिया जाता है कि जातीय आधार पर वर्ग का निर्माण होना चाहिए। यह जातीय उत्पीड़न की जंग लड़ने का एक माध्यम हो सकता है। बहुत संभव है कि ‘वर्ग’ की मुहिम के चलते कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम उत्साहवर्धक होंगे, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता। यदि इसे दीर्घ-कालीन रणनीति का हिस्सा बनाया जाता है तो यह अम्बेडकरवाद की मूल भावना यानी जातिविहीन व वर्गविहीन समाज की अवधारणा के खिलाफ होगा। यह राजकीय समाजवाद के भी खिलाफ होगा, जिसके पक्षधर बाबा साहब हमेशा बने रहे हैं।
डा. तेज सिंह भी ‘वर्ग’ की अवधारणा के पक्षधर रहे हैं और अपने संपादकीय में इसकी चर्चा करते रहे हैं। बहुत संभव है कि डा. तेजसिंह वर्ग चेतना को मार्क्सवाद की तर्ज पर अम्बेडकरवाद का हिस्सा बनाने के पक्षधर हों। ऐसा भी नहीं है कि हमें मार्क्सवाद से कोई परहेज है। किसी भी स्तर पर भारतीय मार्क्सवादियों के ब्राह्मणवाद से परहेज हो सकता है। उनके जाति के सवाल को लेकर उपेक्षा या घालमेल को लेकर परहेज हो सकता है। हमारा मानना है कि मार्क्सवाद की मूल वैचारिकी अम्बेडकरवाद की सहयोगी हो सकती है, सह-यात्री हो सकती है, मगर शत्रु नहीं। मौजूदा संदर्भ में मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के आपसी संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। ‘समय संज्ञान’ इन दो अलग-अलग वैचारिक