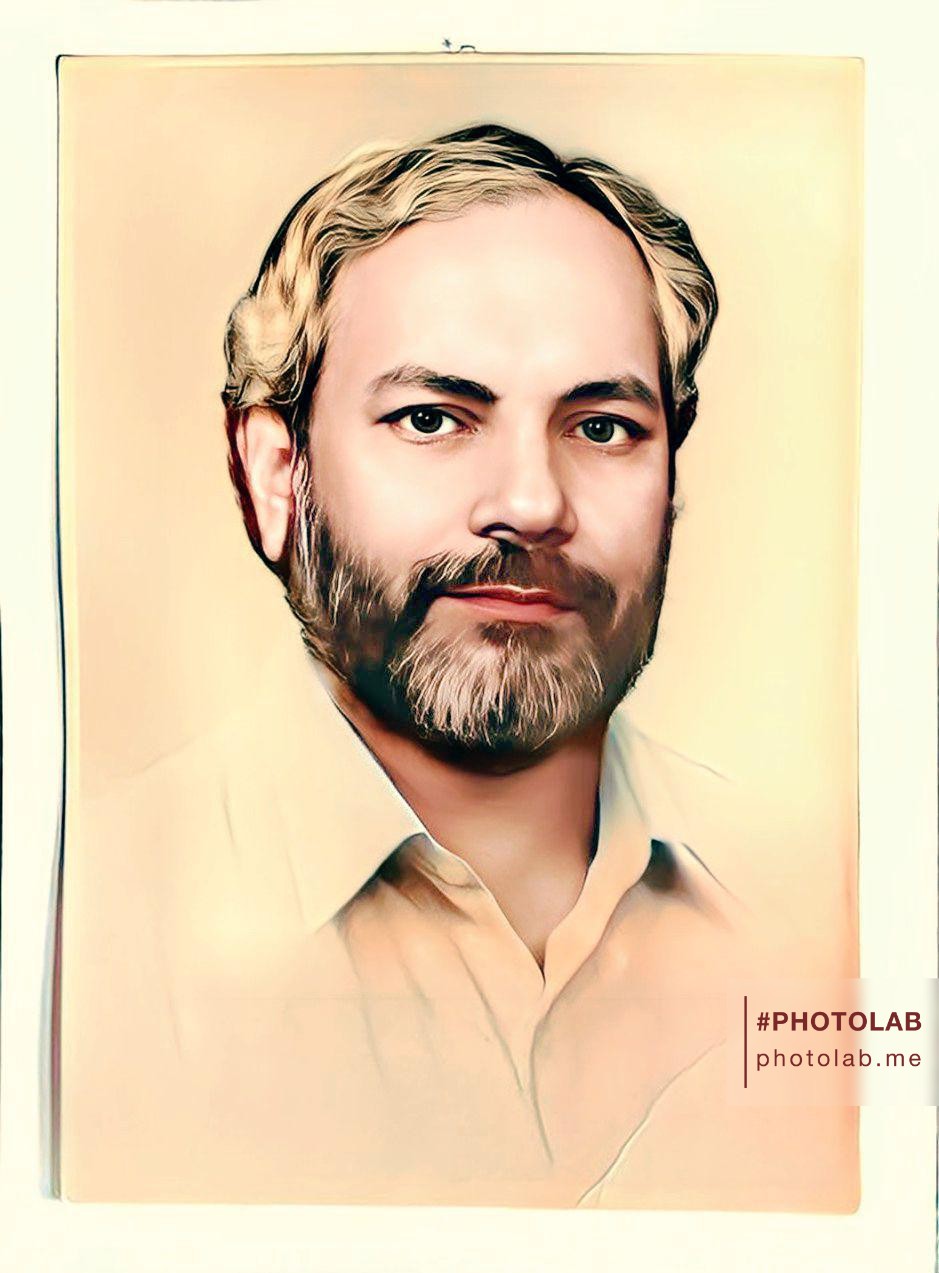"दलित राजनीति का उद्भव और पतन"
स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में दलित राजनीति का उद्भव एक क्रांतिकारी मोड़ था, जिसने सदियों से हाशिए पर ढकेल दिए गए समुदायों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मंच पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का अवसर दिया। यह राजनीति न केवल प्रतिनिधित्व की मांग थी, बल्कि आत्मसम्मान, अधिकार और समानता की लड़ाई भी थी। डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित होकर दलित राजनीति ने एक समय बहुजन चेतना का शंखनाद किया, जो भारतीय राजनीति के चरित्र को चुनौती देता दिखाई पड़ा।किन्तु विडंबना यह रही कि जिस राजनीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय था, वह समय के साथ व्यक्तिगत स्वार्थों, जातीय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धाओं और अवसरवादी गठबंधनों में उलझती चली गई। सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने की होड़ में नीतियों की जगह चालाकियाँ, और जनहित की जगह निजी लाभ ने ले ली। दलित नेतृत्व का वह तेजस्वी स्वप्न, जो बहुजन मुक्ति का प्रतीक था, धीरे-धीरे एक सीमित जातिगत रणनीति में बदल गया, और इस प्रकार उसका नैतिक व वैचारिक पतन आरंभ हो गया।
यह आलेख दलित राजनीति के उस पूरे यात्रा-वृत्त को समझने का प्रयास है—जहाँ उसका जन्म हुआ, वह कैसे फला-फूला, किन परिस्थितियों में वह सशक्त हुआ, और फिर किन कारणों से उसका विघटन और पतन आरंभ हुआ। यह विश्लेषण केवल अतीत को समझने का नहीं, बल्कि वर्तमान दलित नेतृत्व और राजनीति की दिशा पर पुनर्विचार का आमंत्रण भी है।
दलित राजनीति का इतिहास – संघर्ष से सशक्तिकरण तक की यात्रा
भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह रही है कि जिस देश ने "वसुधैव कुटुम्बकम्" का संदेश दिया, उसी भूमि पर दलितों को सदियों तक अस्पृश्यता, बहिष्कार और सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लेकिन इस अंधकारपूर्ण इतिहास में एक तेजस्वी राजनीतिक जागरण भी विकसित हुआ — जिसे हम दलित राजनीति के नाम से जानते हैं। यह राजनीति कोई साधारण सत्ता-संघर्ष नहीं, बल्कि सदियों के सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ एक ऐतिहासिक प्रतिरोध है।
1. प्रारंभिक चेतना और सामाजिक सुधार आंदोलन (19वीं सदी) की बात करें तो दलित राजनीति का इतिहास केवल चुनावों या पार्टियों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के प्रस्फुटन से शुरू होता है। ज्योतिराव फुले ने अपने सत्यशोधक समाज (1873) के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की और शूद्र-अतिशूद्रों को शिक्षा, आत्मसम्मान और संगठित प्रतिरोध का संदेश दिया। दक्षिण भारत में पेरियार (ई. वी. रामास्वामी) का आत्मसम्मान आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बना, जिसने जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती दी। इन आंदोलनों ने राजनीति को सामाजिक क्रांति से जोड़ा, जो आगे चलकर दलित राजनीति की बुनियाद बनी।
2. डॉ. भीमराव आंबेडकर और वैचारिक आधार (20वीं सदी का पूर्वार्द्ध) पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि डॉ. आंबेडकर दलित राजनीति के निर्विवाद शिल्पी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दलित मुक्ति केवल धार्मिक सुधार या सहानुभूति से नहीं, बल्कि राजनीतिक अधिकारों से ही संभव है। उन्होंने 1930 में 'पूना समझौता' के माध्यम से दलितों को आरक्षण का अधिकार दिलाया। 1936 में "इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी" की स्थापना करके उन्होंने पहली बार दलितों को संगठित राजनीतिक विकल्प दिया। 1947 के बाद संविधान सभा में उनका नेतृत्व, विशेष रूप से अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), दलित इतिहास की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धि बना। "हम केवल सामाजिक समानता की नहीं, राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी की भी मांग करते हैं।" — डॉ. आंबेडकर
3. कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों में दलितों की भूमिका (1950-70) के आधार पर, स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में दलित नेतृत्व मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के भीतर सीमित रहा। दलित नेताओं को सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन उनके विचारों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं मिली। कम्युनिस्ट पार्टियों में भी जातिवादी मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई। इस दौर में दलित राजनीति ने संगठनात्मक स्वतंत्रता के लिए आधार बनाना शुरू किया, जो आगे चलकर एक शक्तिशाली आंदोलन में बदला।
4. कांशीराम और बहुजन आंदोलन (1970-1990) बेशक उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में दलित राजनीति ने एक नया मोड़ लिया जब कांशीराम ने एक गैर-कांग्रेसी, गैर-पूंजीवादी दलित आंदोलन का आह्वान किया। कांशीराम जी ने 1978 में BAMCEF (Backward and Minority Communities Employees Federation) और 1981 में DS4 (Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti)का गठन किया और अंततः 1984 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की स्थापना हुई। कांशीराम ने "बहुजन" शब्द को नया राजनीतिक अर्थ दिया — “हम जो 85% हैं, सत्ता उन्हीं की होनी चाहिए।” उन्होंने दलित राजनीति को केवल विरोध से निकालकर सत्ता के केंद्र तक पहुँचाया। मायावती का उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना उसी यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव था।
5. 21वीं सदी में दलित राजनीति – अवसर, विघटन और चुनौतियों के दृष्टिगत 21वीं सदी में दलित राजनीति ने सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन इसके साथ विचारधारा की शिथिलता, गठबंधन की अवसरवादिता और नेतृत्व का केंद्रीकरण भी सामने आया। बिहार में रामविलास पासवान की राजनीति ने एक समय प्रभाव छोड़ा, पर बाद में वह सत्ता से समीकरण बनाने में उलझ गई। दलित राजनीति अब केवल 'दलितों की' नहीं रही, बल्कि उसने ओबीसी, मुस्लिम और वंचित वर्गों से गठबंधन के नए प्रयोग किए। लेकिन विचारधारात्मक दिशा और वैचारिक प्रतिबद्धता का अभाव आज दलित राजनीति को संकट में डाल रहा है।
दलित राजनीति का इतिहास एक अद्वितीय सामाजिक क्रांति का इतिहास है। यह इतिहास हमें बताता है कि जिन वर्गों को सदियों तक मानव नहीं समझा गया, उन्होंने लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता, सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी और कई बार जीत भी हासिल की। आज यह ज़रूरी है कि दलित राजनीति अपने अतीत से सबक ले, अपने वैचारिक आधार को पुनःस्थापित करे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल चुनावी आंकड़ों की नहीं, बल्कि समानता और न्याय की राजनीति का मार्ग प्रशस्त करे। क्योंकि दलित राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि संविधान के मूल विचार — "न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व" — को धरातल पर लाना है।
दलित राजनीतिक उद्भव – एक सामाजिक न्याय की पुकार
भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक इतिहास अत्यंत जटिल, विषम और विडंबनाओं से भरा रहा है। हज़ारों वर्षों तक जाति-व्यवस्था ने जिस तरह से समाज को ऊँच-नीच के कठोर खांचों में बाँटा, उसने एक बड़े वर्ग—दलितों—को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से हाशिये पर डाल दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद, भारत में दलितों की राजनैतिक चेतना का जो प्रस्फुटन हुआ, वही दलित राजनीतिक उद्भव का आधार बना।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: दलित राजनीतिक चेतना का बीज कहीं न कहीं 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में पड़ चुका था—ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज, रामस्वामी पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन, और दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलनों ने दलित वर्ग को पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि सामाजिक अपमान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक असमानता की उपज भी है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर का नेतृत्व: दलित राजनीति के वास्तविक और ठोस स्वरूप की नींव डॉ. भीमराव आंबेडकर ने रखी। वे न केवल एक संविधान-निर्माता थे, बल्कि दलित आत्मसम्मान के पहले वैचारिक और संगठित प्रवक्ता भी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक समानता का मार्ग राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति से होकर जाता है। उनका यह कथन – “राजनीति हमें उस स्वतंत्रता की कुंजी देती है, जिससे हम अपने सामाजिक और आर्थिक बंधनों को तोड़ सकते हैं” दलित राजनीति के मूल तत्त्व को दर्शाता है।
डॉ. आंबेडकर ने न केवल दलितों के लिए आरक्षण की माँग की, बल्कि उन्होंने "इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी" (1936) और बाद में "शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन" (1942) जैसी राजनीतिक पार्टियाँ बनाकर दलितों को संगठित राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश की। उनकी राजनीति केवल 'सहभागिता' नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और नेतृत्व में हिस्सेदारी की मांग थी। उन्होंने राष्ट्र निमार्ण के भाव से महिलाओं के उत्थान, मजदूरों के लिए नियत काम के धंटे, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना आदि अनेक काम किये। माननीय के.वी. राव ने उन्हें “ Father of Constitution” ही नहीं अपितु“ Mother of Constitution” भी कहा था।
स्वतंत्रता के बाद के दौर में दलित राजनीति के दृष्टिगत स्वतंत्रता के बाद आरंभिक वर्षों में दलित राजनीति अपेक्षाकृत शांत रही। यह कांग्रेस के भीतर सीमित प्रतिनिधित्व तक सिमटी रही। लेकिन 1970 और 80 के दशक में, जब सामाजिक न्याय की राजनीति ने उभार लिया, तब दलित राजनीति को नया आयाम मिला।
कांशीराम ने ‘बामसेफ’ (BAMCEF), ‘दलित शोषित समाज संघर्ष समिति’ (DS4), और अंततः बहुजन समाज पार्टी (BSP) की स्थापना करके दलित राजनीतिक चेतना को एक स्वतंत्र सामाजिक आधार और संगठनात्मक ढांचा दिया। उन्होंने “बहुजन” शब्द को दलित राजनीति का नया ध्वज बना दिया और नारा दिया: "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी!"
दलित राजनीति की विशेषताएँ के रूप में दलित राजनीति का ‘सामाजिक न्याय पर आधारित वैचारिक आग्रह’, ‘ब्राह्मणवाद और जातिगत वर्चस्व का प्रतिरोध’, ‘संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास’, ‘राजनीतिक सत्ता को सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाना’ और ‘दलित-बाहुल्य क्षेत्रों में संगठित राजनीतिक ध्रुवीकरण’ का आग्रह प्रमुख रहा है
दलित राजनीतिक उद्भव के महत्त्व को देखें तो दलित राजनीति ने भारत के लोकतंत्र को वास्तव में सहभागी और चुनौतीपूर्ण बनाया। इसने न केवल दलितों को सत्ता में भागीदारी दी, बल्कि सामाजिक बहसों को भी नया आयाम दिया। भारतीय राजनीति, जो पहले उच्च जातीय वर्चस्व का मैदान थी, अब नए चेहरे, नए नारे और नई माँगों से बदलने लगी।
दलित राजनीतिक उद्भव केवल सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान, सामाजिक बराबरी और ऐतिहासिक पीड़ा के खिलाफ़ संगठित संघर्ष की परिणति थी। यह राजनीति किसी एक व्यक्ति या चुनावी पार्टी का नाम नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी चेतना का विस्तार है। आज जब हम दलित राजनीति के पतन की बात करते हैं, तो उसके उद्भव के इस गौरवपूर्ण और विचारशील पक्ष को समझना और उससे प्रेरणा लेना और भी ज़रूरी हो जाता है।
दलित राजनीति की भूमिका — सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला
भारत जैसे बहुजातीय और बहुस्तरीय समाज में लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन और न्याय का साधन भी है। इस परिप्रेक्ष्य में दलित राजनीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रही है। यह केवल राजनीतिक सत्ता की भागीदारी का प्रश्न नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बहिष्करण से मुक्ति का आंदोलन है, जिसने दलित समुदाय को अस्मिता, अधिकार और आत्मसम्मान की नई चेतना प्रदान की।
1. सामाजिक न्याय की आवाज़ : दलित राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक न्याय का वास्तविक आयाम दिया। यह राजनीति उस व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी हुई, जिसमें दलितों को हजारों वर्षों तक धार्मिक और सामाजिक आधार पर अछूत, अस्पृश्य और अस्वीकार्य माना गया। दलित राजनीति ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय केवल नीति-निर्माण का विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धता है।
डॉ. आंबेडकर ने कहा था: "हमारे लिए राजनीति केवल अधिकारों की बात नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का माध्यम है।"
2. राजनीतिक भागीदारी का विस्तार : भारत में राजनीतिक सत्ता लंबे समय तक ऊँची जातियों के नियंत्रण में रही। दलित राजनीति ने इस असंतुलन को तोड़ते हुए दलित समुदाय को सत्ता में भागीदारी दिलाई। कांशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने इसे संगठित राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप दिया और 'बहुजन' शब्द को शक्ति का प्रतीक बनाया। BSP की स्थापना के साथ दलित राजनीति ने यह दिखाया कि अगर संगठित प्रयास किया जाए, तो सत्ता केवल सुविधाभोगियों की जागीर नहीं रह सकती। इसने दलितों को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में भागीदार बनने का हक़ दिलाया।
3. दलित अस्मिता और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना : दलित राजनीति ने दलित समाज को अपने इतिहास, संस्कृति और अस्तित्व पर गर्व करना सिखाया। 'जय भीम', 'बहुजन हिताय', 'हम होंगे कामयाब' जैसे नारे केवल नारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दलित चेतना को जनचेतना में बदल दिया। इस राजनीति ने अस्पृश्यता को चुनौती दी, मंदिर प्रवेश आंदोलन, अधिकार यात्रा, शिक्षा अधिकार, भूमि अधिकार जैसे आंदोलनों को जन्म दिया, और दलितों को एक नव-मूल्यबोध के साथ खड़ा किया।
4. संविधान के मूल्यों की रक्षा : जब भी भारत में लोकतंत्र पर खतरे के बादल छाए, दलित राजनीति ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज़ बुलंद की। डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान दलित राजनीति के लिए एक धार्मिक ग्रंथ के समान रहा, और इस राजनीति ने हर स्तर पर संवैधानिक नैतिकता की रक्षा का बीड़ा उठाया।
5. सामाजिक बहसों में भागीदारी : दलित राजनीति ने भारतीय समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि जाति केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संरचना है। इसने साहित्य, कला, मीडिया और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दलित उपस्थिति को मज़बूत किया। आज जब हम 'दलित साहित्य', 'दलित नारीवाद', 'दलित इतिहास' जैसी अवधारणाओं की चर्चा करते हैं, तो यह इसी राजनीति की वैचारिक देन है।
6. नवयुवाओं और महिलाओं को नेतृत्व देना : दलित राजनीति ने युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिए, जो पारंपरिक राजनीति में अक्सर हाशिये पर थे। चाहे छात्र संगठनों के रूप में हो, या पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण के माध्यम से—दलित राजनीति ने प्रातिनिधिक लोकतंत्र को जमीनी सच्चाई से जोड़ने का काम किया।
दलित राजनीति की भूमिका केवल एक वर्ग की मांगों तक सीमित नहीं रही है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, अधिक संवेदनशील और अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि आज इसकी दिशा और स्वरूप को लेकर आलोचना भी होती है, लेकिन इसके ऐतिहासिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अब आवश्यकता इस बात की है कि दलित राजनीति अपने वैचारिक मूल्यों की पुनः स्थापना करे, नए सामाजिक गठबंधनों का निर्माण करे और आगामी पीढ़ियों को न केवल राजनीतिक, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक नेतृत्व के लिए भी तैयार करे। केवल तभी यह राजनीति अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से साध पाएगी और एक समानता आधारित भारत की कल्पना को साकार कर सकेगी।
आज दलित नेतृत्व कैसे बदल रहा है?
यह प्रश्न — "आज दलित नेतृत्व कैसे बदल रहा है?" — बेहद महत्वपूर्ण और समयानुकूल है।दलित राजनीति के इतिहास में नेतृत्व हमेशा एक केंद्रीय भूमिका में रहा है। बाबासाहेब आंबेडकर जैसे विचारशील, साहसी और दूरदर्शी नेता से लेकर कांशीराम जैसे संगठक तक — दलित नेतृत्व ने सामाजिक न्याय की दिशा तय की। किंतु आज जब हम वर्तमान संदर्भ में दलित नेतृत्व की प्रकृति को देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वह बदल रहा है — अपनी संरचना, भाषा, उद्देश्य और रणनीति में। दलित राजनीति आज संक्रमण के दौर में है, जहाँ एक ओर पुरानी वैचारिक स्पष्टता और सांगठनिक मज़बूती कमजोर हुई है, वहीं दूसरी ओर नई तरह का नेतृत्व उभर रहा है — जिसमें मिश्रित प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ इस बदलाव को विभिन्न स्तरों पर समझाया गया है:
1. विचारधारा से अधिक अवसरवाद: आज का दलित नेतृत्व पहले की तरह विचारधारा-आधारित नहीं रहा। जहाँ अतीत में नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति-व्यवस्था को चुनौती देना था, वहीं आज कई नेता सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन राजनीति में लीन हैं, चाहे वह विचारधारात्मक रूप से विपरीत क्यों न हो।
2. व्यक्ति की जगह चेहरे की राजनीति: नई राजनीति में नेतृत्व का चेहरा बदला है — अब विचारशील नेता कम, और लोकप्रिय, मीडिया-प्रसिद्ध चेहरे अधिक उभर रहे हैं। नेता अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिजिटल अभियानों से जुड़ रहे हैं, परंतु जमीनी संगठन निर्माण की प्रक्रिया अक्सर कमजोर है।
3. छात्र और युवा आंदोलनों से उभार: हाल के वर्षों में रोहित वेमुला आंदोलन, भीम आर्मी, JNU-HCU जैसे विश्वविद्यालयों से निकले छात्र नेता, जैसे कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद —इसने एक नई चेतनशील पीढ़ी को सामने लाया है, जो सवाल पूछती है, बहस करती है, और सड़कों पर उतरती है। यह नेतृत्व पहले की तरह पार्टी-केन्द्रित नहीं, बल्कि आंदोलन-केन्द्रित होता जा रहा है।
4. अंतरजातीय समन्वय की बढ़ती समझ: नया नेतृत्व केवल चमार समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह अन्य दलित जातियों (जैसे पासी, बाल्मीकि, कोरी) और पिछड़े वर्गों के साथ मिलकर एक व्यापक बहुजन एकता की खोज में है। यह दृष्टिकोण समावेशी है, भले ही व्यावहारिक सफलता अभी सीमित हो।
5. प्रतीकवाद बनाम वास्तविक हस्तक्षेप: यद्यपि नया नेतृत्व शिक्षा, आरक्षण, उत्पीड़न, नौकरियों में भेदभाव जैसे ज़मीनी मुद्दों को उठाता है, तथापि एक बड़ा वर्ग प्रतीकात्मक राजनीति में उलझा है, जैसे — मूर्ति स्थापना, जन्मदिवस रैलियाँ, भावनात्मक भाषण आदि। ऐसे लोगों की वास्तविक नीति-निर्माण में उनकी भूमिका अब भी सीमित है।
6. गठबंधन की राजनीति और पहचान संकट: कुछ दलित नेता सत्ता में भागीदारी के लिए हिंदुत्ववादी दलों से समझौता कर लेते हैं, जिससे दलित राजनीति का स्वरूप और संघर्षशीलता कमजोर होती है। दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक एकता का स्वप्न कहीं गुम-सा हो गया है। यदि आज की ही बात करें तो लोकसफा में दलित सांसदों की संख्या लगभग 131 है किंतु दलित समस्या से जुड़े किसी भी मुद्दे पर मुंह खोलने का साहस नहीं करता। अपने पैत्रिक दल की सेवा में रहते हैं।
7. दलित महिलाओं का नेतृत्व: दलित नारीवाद के तहत आज दलित महिलाएँ अपनी दोहरे शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेखिका सावित्रीबाई फुले, सिंधुताई जैसी अन्य प्रतिभाओं की प्रेरणा से आज कई दलित महिलाएं लेखन, सामाजिक कार्य और राजनीति में सक्रिय हैं।
8. नए मंच और संचार माध्यमों का उपयोग: आज का दलित नेतृत्व सोशल मीडिया, यूट्यूब, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिये युवाओं से संवाद कर रहा है। यह परिवर्तन जनजागरण के नए साधन तो लेकर आया है, लेकिन इसके साथ सतही और मनोरंजन तक ही सीमित रह जाता है। हाँ! कुछ दलितों ने भी यूट्यूब चैनल बना लिए है और समाज के हक में अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। इससे उन्हें यूट्यूब से कुछ आर्थिक लाभ भी मिल जाता है, इसलिए उनकी सक्रीयता बनी रहती है।
आज का दलित नेतृत्व एक संक्रमण काल से गुज़र रहा है — जहाँ वह एक ओर नई तकनीक, शिक्षा और मंचों के सहारे नई भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह वैचारिक गहराई और संगठनात्मक प्रतिबद्धता के संकट से जूझ रहा है। एक ओर विचारधारा से जुड़ा, संघर्षशील युवा नेतृत्व उभर रहा है; दूसरी ओर सत्ता के समीकरणों में समाहित, व्यक्तिवादी नेता भी हावी हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह नया नेतृत्व कितनी दूरदर्शिता, संगठन क्षमता और वैचारिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। "अगर नेतृत्व केवल चुनाव जितना सिखाए, तो समाज हारता है; अगर नेतृत्व चेतना और संघर्ष सिखाए, तो परिवर्तन अवश्य होता है।"
दलित राजनीति के उतार-चढ़ाव और कारण :
दलित राजनीति के उतार-चढ़ाव और कारण जटिल हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के साथ-साथ दलित समुदायों की अपनी सक्रियता और संघर्ष शामिल हैं। दलित राजनीति के इतिहास में दो महत्वपूर्ण चरण हैं: पहला, दलित समुदाय का अस्तित्व में आना और राजनीतिक चेतना का विकास, और दूसरा, दलितों की राजनीतिक भागीदारी का बढ़ना और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन की मांग।
दलित राजनीति का उदय और विकास :
दलित समुदाय का उत्कर्ष : भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
दलितों की राजनीतिक चेतना: अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने अपनी राजनीतिक चेतना विकसित की और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे।
दलित आंदोलन: दलितों ने समानता की मांग के साथ अपना आंदोलन शुरू किया और समाज में असमानता से लड़ने के लिए संघर्ष किया।
राजनीतिक दलों में दलितों की भूमिका: कुछ राजनीतिक दलों ने दलितों को अपने साथ जोड़ा और दलितों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया।
दलित राजनीति में उतार-चढ़ाव:
मंडल आयोग की सिफारिशें: 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत होने में मदद मिली।
सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन: दलितों ने सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन के लिए आवाज उठाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। दलितों ने राजनीतिक दलों में सक्रिय भूमिका निभाई और चुनाव जीते। दलितों की राजनीतिक शक्ति बढ़ने से उन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतियों में बदलाव करने में मदद मिली। दलितों को अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्याय का सामना करना पड़ता है।
दलित राजनीति के उतार-चढ़ाव के कारण:
- को सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है, जो उनके राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है।
- राजनीतिक दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में देखा और उनके अधिकारों की रक्षा में रुचि नहीं दिखाई।
- को अभी भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है।
- को आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है।
राजनीतिक दल-बदल: कुछ राजनीतिक दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में देखा और उनके अधिकारों की रक्षा में रुचि नहीं दिखाई। दलित राजनीति के उतार-चढ़ाव के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के जटिल मिश्रण के कारण हैं। दलितों को सामाजिक और आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है। कुछ राजनीतिक दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में देखा और उनके अधिकारों की रक्षा में रुचि नहीं दिखाई। जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता भी दलितों की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। यहां तक की महात्मा गांधी भी इन मांगों के विरोध में कूद पड़े। बाबा साहब ने मांग की कि दलितों को अलग प्रतिनिधित्व (पृथक निर्वाचिका) मिलना चाहिए यह दलित राजनीति में आज तक की सबसे सशक्त और प्रबल मांग थी...
दोराहे पर दलित राजनीति: भारतीय लोकतंत्र में दलित राजनीति एक अहम लेकिन जटिल परिघटना रही है। यह राजनीति सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान की भावना से जन्मी, लेकिन आज यह एक ऐसे दोराहे पर खड़ी दिखाई देती है जहाँ उसे अपने अतीत की विरासत और वर्तमान की चुनौतियों के बीच संतुलन साधना कठिन हो रहा है। यह दोराहा केवल वैचारिक नहीं, रणनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है।
इतिहासिक पृष्ठभूमि: दलित राजनीति का उद्भव डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व से जुड़ा है, जिन्होंने दलितों को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक गरिमा, शिक्षा और आर्थिक स्वायत्तता की ओर प्रेरित किया। ‘जय भीम’ का नारा केवल एक सामाजिक उद्घोष नहीं, एक वैचारिक आंदोलन की नींव थी। दलित राजनीति का मूल उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना और समतावादी समाज की स्थापना करना था।
दोराहे की पहचान: विचार बनाम सत्ता
- की दलित राजनीति विचारधारा और सत्ता की राजनीति के बीच झूलती दिख रही है। एक ओर आंबेडकरी विचारधारा है – जो बुद्ध, फुले और पेरियार की आलोचनात्मक परंपरा से जुड़ी है; दूसरी ओर सत्ता की भूख है – जो गठबंधन, अवसरवाद और पहचान की राजनीति के जाल में उलझती जा रही है।
- नेतृत्व सत्ता के साझेदार बनने में आत्मसंतोष पा रहा है।ऐसा भी लगता है कि दलित नेतृत्व विचारधारात्मक संघर्ष को त्याग कर केवल प्रतीकों और पहचान तक सीमित हो रहा है।
- दलित नेता सवर्ण-प्रधान पार्टियों में शामिल होकर व्यक्तिगत लाभ तो पा रहे हैं, लेकिन व्यापक दलित समाज की स्थितियाँ नहीं बदल रहीं।
दलित नेतृत्व की नई प्रकृति और बिखराव :
यह सच है कि आज का दलित नेतृत्व अनेक भागों में बँटा हुआ है
- के साथ समायोजन करने वाले वे नेता हैं जो भाजपा, कांग्रेस या अन्य दलों में जाकर दलित प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा अक्सर दलित समाज की मूल समस्याओं से हट जाता है।
- से जुड़ी राजनीतिक नेतृत्व अपेक्षाकृत कमज़ोर है, लेकिन विचार और संघर्ष के स्तर पर सक्रिय है। यह नेतृत्व बहुजन चेतना, जातिविरोधी विमर्श और वैकल्पिक सामाजिक सोच को ज़िंदा रखे हुए है।
- की बदलती चेतना और मीडिया का असर के चलते दलित समाज की चेतना अब पहले जैसी समरूप नहीं रही। शिक्षा, इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया ने एक नए प्रकार की राजनीतिक समझ को जन्म दिया है, जहाँ दलित युवा अब केवल वोट बैंक नहीं रहना चाहता, वह सवाल पूछना चाहता है, संवाद करना चाहता है।
- मुख्यधारा मीडिया और राजनीति ने दलित मुद्दों को या तो हाशिये पर डाल दिया है या उन्हें केवल भावनात्मक प्रतीकों तक सीमित कर दिया है (जैसे: आंबेडकर की मूर्तियाँ, ‘जय भीम’ का नारा, इत्यादि)। जबकि जमीनी सवाल – शिक्षा, बेरोजगारी, अत्याचार, आरक्षण, भूमि – अभी भी अधूरे हैं।
भविष्य की दिशा: रास्ता क्या हो सकता है?
दलित राजनीति को दोराहे से आगे निकलने के लिए आत्मचिंतन और नवचिंतन दोनों की ज़रूरत है। दलित राजनीति को आंबेडकर, फुले, बुद्ध की आलोचनात्मक परंपरा में लौटना होगा।
सामूहिक नेतृत्व का निर्माण हेतु वैचारिक और जमीनी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व उभारना होगा। सत्ता केंद्रित राजनीति से अलग वैकल्पिक सामाजिक आंदोलनों की ज़रूरत है। दलित युवाओं को डिजिटल माध्यमों में वैचारिक विमर्श और जागरूकता के लिए प्रशिक्षित करना होगा।
दलित राजनीति का दोराहा केवल भ्रम की स्थिति नहीं है, यह एक संभावना का बिंदु भी है। यह तय करना दलित समाज और नेतृत्व के हाथ में है कि वे कौन सा रास्ता चुनते हैं – सत्ता में हिस्सेदारी की राजनीति जो विचारधारा से समझौता करती है, या वैकल्पिक सामाजिक परिवर्तन का मार्ग जो संघर्षशील, नैतिक और समावेशी है। आंबेडकर ने कहा था: “मैं किसी भी राजनीतिक जीत को तब तक सार्थक नहीं मानता जब तक वह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रयोग न की जाए।” यह कथन आज भी दलित राजनीति के लिए दिशासूचक बन सकता है — बशर्ते हम इसे गंभीरता से लें।
राजनीतिक ब्राह्मणवाद में दबकर रह गई दलित राजनीति
भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और समता की पुकार कई बार सुनाई दी, परंतु वास्तविकता यह रही कि राजनीतिक सत्ता का ढांचा आज भी ब्राह्मणवादी सोच और संरचना से नियंत्रित है। दलित राजनीति, जो कभी सामाजिक बदलाव की सबसे तेज़ आवाज हुआ करती थी, आज उस राजनीतिक ब्राह्मणवाद के नीचे दबकर अपनी दिशा, दृष्टि और धार खो बैठी है। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की विफलता है, बल्कि सामाजिक न्याय की पराजय भी है।
1. ब्राह्मणवाद क्या है और राजनीति में इसका स्वरूप: ब्राह्मणवाद केवल जाति नहीं, एक मानसिकता है — वर्चस्व की मानसिकता। जहाँ एक वर्ग विशेष को शेष समाज से ऊपर मानने की सोच हो, वहीं ब्राह्मणवाद जीवित रहता है। राजनीतिक ब्राह्मणवाद उसी सोच का आधुनिक रूप है, जिसमें सत्ता का नियंत्रण सामाजिक दृष्टि से ऊंची जातियों और विचारधाराओं के हाथों में रहता है, और वंचित वर्गों को केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देकर शांत रखा जाता है।
2. दलित राजनीति का प्रारंभ — चेतना से संघर्ष तक: बाबासाह