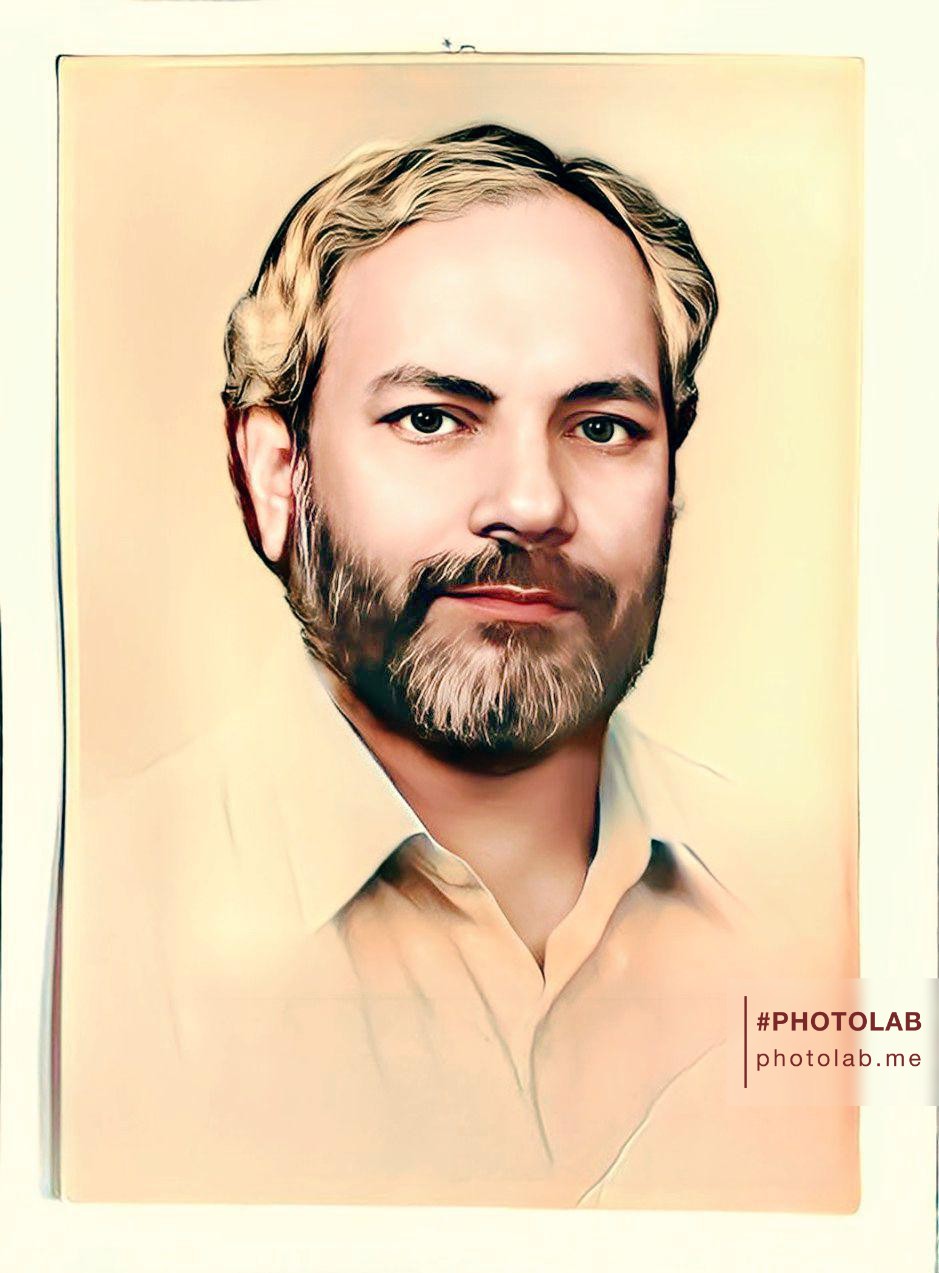E- BOOK
अपाहिज लोकतंत्र
तेजपाल सिंह ‘तेज’
अपाहिज लोकतंत्र
तेजपाल सिंह ‘तेज’
कॉपीराइट :- तेजपाल सिंह ‘तेज’
मुख पृष्ठ:- शीलबोधी
वेबसाइट :-www.bookrivers.com
प्रकाशकईमेल :-publish@bookrivers.com
प्रकाशनवर्ष :-2024
मूल्य:- 325/-रूपये
ISBN:-978-93-5842-979-4
यह पुस्तक इस शर्त पर विक्रय की जा रही है कि लेखक की पूर्वानुमति के बिना इसे व्यावसायिक अथवा अन्य किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे पुनः प्रकाशित कर बेचा या किराए पर नहीं दिया जा सकता तथा जिल्दबंद या खुले किसी अन्य रूप में पाठकों के मध्य इसका वितरण नहीं किया जा सकता। ये सभी शर्तें पुस्तक के खरीदार पर भी लागू होती हैं। इस सम्बन्ध में सभी प्रकाशनाधिकार सुरक्षित हैं। इस पुस्तक का आंशिक रूप से पुनः प्रकाशन या पुनः प्रकाशनार्थ अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने, इसे पुनः प्रस्तुत करने के लिए अपनाने, अनूदित रूप तैयार करने अथवा इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी तथा रिकॉर्डिंग आदि किसी भी पद्धति से इसका उपयोग करने हेतु पुस्तक के लेखक की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है।
भूमिका...
वर्तमान लोकतंत्र का सटीक स्केच
मैं अच्छे से जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में ‘तेज’ साहब के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। उनका घर से बाहर आना-जाना लगभग बंद ही हो गया है। यदि यह कहा जाए कि उनकी दुनिया उनके कमरे तक सीमित होकर रह गई है, तो गलत नहीं होगा। मोबाइल द्वारा भी उनका बाहरी दुनिया से संपर्क कुछ खास नहीं रह गया है। लेकिन दीगर हकीकत यह भी है कि उन्होंने इस एकांकी जीवन में समाचार पत्र, सोशल मीडिया व इंटरनेट को अपना हमसफर बना छोड़ा है। वर्तमान पुस्तक भी इन्हीं का बाई-प्रोडक्ट है। भूमिका लिखने के लिए तेजपाल सिंह ‘तेज’ की मौजूदा पुस्तक की सॉफ्ट कापी जब मेरे पास आई तो इसके शीर्षक ने मेरे अंदर एक अजीब-सी टीस पैदा की। इसके शीर्षक को देखकर पहला ख्याल आया-‘अपाहिज लोकतंत्र’ जैसा शीर्षक देने के पीछे कहींतेज’साहब का निरंतर गिरता स्वास्थ्य तो नहीं? मुझे लगा- कहीं उन्होंने लोकतंत्र को अपने स्वास्थ्य से जोड़कर इसे अपाहिज तो नहीं कह डाला? मैं जानता हूं-अक्सर ऐसे हालात में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तेज साहब धारा के विपरीत तैरने वालों में से हैं,एक अपवाद हैं। अपवाद के नाते ही वे सारी नकारात्मकता को धता बताते हुए वर्षों से निरंतर अपनी सकारात्मकता का परिचय देते चले आ रहे हैं। मैं उनकी सकारात्मकता और जिजीविषा का कायल हूं और यही हमारे आपसी संबंधों का मूलाधार भी है।
लेकिन जब मैं उनकी पुस्तक के शीर्षक ‘अपाहिज लोकतंत्र’ की विषय सूची से रूबरू हुआ तो लगा- तेज साहब का लोकतंत्र को अपाहिज कहना काफी हद तक जायज है। यद्यपि मैंने इस नजरिए से पहले सोचा नहीं था, लेकिन जिस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की बानगी तेज साहब के शीर्षक प्रस्तुत कर रहे थे, उसके हिसाब से लगा जैसे हम सभी एक अनूठे अपाहिजपन का शिकार होकर रह गए हैं; क्योंकि जिस शिद्दत के साथ हमें करप्ट सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए थी, हम उठा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान निजाम की छत्रछाया में देश में जो कुछ हो रहा है, हम उससे अनजान हैं। लेकिन जिस संजीदगी से तेज साहब लोकतंत्र के अपाहिज होने के मसले को डील कर रहे है, वह साहस से कहीं ज्यादा जोखिम का काम है। जब मैं तेज साहब के चश्में से लोकतंत्र के खिलवाड़ को देख रहा था तो मेरे ख्यालों और स्वानुभूति का काफिला मुझे फिल्मों में दिखाए जाने वाले डॉन की उस अंधेरी दुनिया में ले गया जहां एक डॉन बच्चों के हाथ-पांव तोड़कर सड़क पर भीख मांगने के लिए अलग-अलग ट्रैफिक सिगनल पर बैठा छोड़ता है। यह वह दुनिया होती है जहां सिर्फ डॉन का ही जलवा रहता है। पीडि़त पक्ष के पास डॉन के रहमोकरम के अलावा जिंदा रहने के दूसरे विकल्प कम ही नजर आते हैं। यह अलग बात है कि फिल्म के अंत में डॉन का निरंकुश साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। खैर यह जो कुछ भी है-तेज साहब का साहस और जोखिम उठाने का जज्बा दोनों काबिल-ए-तारीफ हैं।
इसमें दो राय नहीं हो सकती कि तेज साहब की पुस्तक वर्तमान भारत की जो तस्वीर पेश करती है, वह किसी डॉन की अंधेरी दुनिया से कम डरावनी नहीं है। अगर सिलसिलेवार देखा जाए तो जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर तेज साहब ने कलम न चलाई हो। मुझे लगता है कि लेखक के दायरे की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से करना श्रेयकर रहेगा। लेखक हमेशा से शिक्षा के प्रति बेहद संजीदा रहे हैं। इसी संजीदगी के चलते वे एक साथ दर्जनों स्कूलों की समस्याओं के लेकर विभिन्न विभागों व समाचार पत्रों में अपनी आवाज ऐसे उठाते रहे हैं, मानो कि उन्होंने इन स्कूलों को गोद ले रखा हो।लेकिन वर्तमान पुस्तक में उनकी चिंता के केन्द्र में नई शिक्षा नीति है। इसको लेकर वे असंतुष्ट हैं। उन्हें लगताहै कि वर्तमान शिक्षा नीति समाज के कमजोर तबके को पीछे धकेलने की साजिश है। उनका मानना है कि वर्तमान शैक्षिक ढांचा सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए वे नई शिक्षा नीति के विरुद्ध जंग छेड़े हैं।
देश में बढ़ती बेरोजगारी उनकी आंखों की किरकिरी बनी है; यह उन्हें बेचैन किए है। वे इस हकीकत से अनजान नहीं है कि जब चतुर्थ श्रेणी के दो-चार सौ पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, बेरोजगार आवेदकों की संख्या एक डरानी तस्वीर पेश करती है। इन पदों के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों की बाड़-सी नजर आती है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इन पदों के लिए जब विभिन्न व्यवसायिक स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों के साथ-साथ पीएचडी के डिग्रीधारियों तक के आवेदन बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। ऐसी दुर्दशा पर समाज का कोई भी संवेदनशील नागरिक कैसे चैन से बैठ सकता है। तेज साहब की विशेषता है कि वे अपनी बेचैनी को कलमबद्ध कर जनमानस को जाग्रत करने को उठ खड़े होते हैं। अग्निवीर योजना ने उनके सब्र का पैमाना ही तोड़ डाला। वह अग्निवीर योजना को अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित युवाओं के खिलाफ बड़ी साजिश के रूप में दखते हैं। वे युवाओं के साथ इसे एक घिनौनी साजिश के रूप में देखते हैं। इसके लिए वे वर्तमान भारतीय राजनीति और उसकी संवेदनहीनता पर उंगली उठाते हैं। इसकी तसदीक समूचा संगठित विपक्ष भी करता नजर आता है। वह कितना संजीदा है, यह तय होना अभी बाकी है।
लोकतंत्र को अपाहिज बनाने की इस कड़ी में लेखक का मानना है कि वर्तमान सत्ता जनता को धर्म की अफीम चटाकर आपस में लड़ाती है और अपनी राजनीति की रोटियां सेंकती है। वे वर्तमान निजाम के अहंकार पर सवाल उठाते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं कि यह दावा-सत्ताधीश भगवानों को जमीन व घर देने जैसे काम कर रहा है, एकदम खोखला है। वह राजशाही थी, जब राज दरबारों में चारण व भाट राजा की शान में कशीदे काढ़ा करते थे। लेकिन आज हम लोकतंत्र के ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां चाटुकार लोग जनता के रहमोकरम पर सत्ता पाने वालों को भगवान का अवतार घोषित करने में पीछे नहीं हैं। हद तो तब हो जाती है जब जनता से भीख की तर्ज पर वोट मांगने वाला व्यक्ति खुद को भगवान का अवतार घोषित करने का दुस्साहस करता है और जनता बेबस देखती रहती है। अगर लेखक ऐसे लोकतंत्र को अपाहिज न कहे तो और क्या कहे, यह तेज साहब जैसे लोगों के लिए ही नहीं, देश के हर जिम्मेदार नागरिक के लिए विचारणीय बिंदु होना चाहिए।
इसे मानसिक गुलामी कहें या अवसरवाद, लोगों की अपनी कोई स्वतंत्र आवाज ही नहीं रह गई है। हिन्दू राष्ट्र के बड़े-बड़े दावे देश कई कोने-कोने से बराबर किए जा रहे हैं। इन दावों की निरंकुशता के चलते जो अल्पसंख्यक हैं, धर्मांतरित हैं, दलित हैं या जो हिंदुत्व (इसे हिंदुओं की एक अलग प्रकार की नस्ल के रूप में देखा जा सकता है) के समर्थक नहीं हैं, उनके मानवाधिकार के लिए जगह ही कहां बचती है। यद्यपि भारत का संविधान व्यक्ति की निजता से जुडे़ मसलों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है लेकिन फिर भी वर्चस्ववाद और तानाशाही अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे कारनामे लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति किसी भी प्रगतिशील, सभ्यऔर लोकतांत्रिक समाज के हित में नहीं हो सकती। लेखक की चिंता दलित व पिछड़े वर्ग को लेकर अधिक है क्योंकि इसका खामियाजा हाशियाकृत समाज को अधिक भुगतना पड़ता है। इसके लिए लेखक सीधे-सीधे बीजेपी व आरएसएस की नीतियों को कठघरे में खड़ा करते हुए अपनी बेबाकी, ईमानदारी और साहस का परिचय देता है।
‘तेज’साहब अपने आलेखों में राजनीति के बदलते चरित्र और राजनेताओं द्वारा जनभावना के साथ खिलवाड़ पर गंभीर व तर्कयुक्त सवाल उठाते हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविद और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के निर्वाचन से संतुष्ट नहीं है।वे इसे एक राजनीतिक चाल के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान सत्ता दलित और आदिवासियों को राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन करके कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। वे इस जन्नत की हकीकत जानते हैं कि इसकी आड़ में वर्तमान निजाम खुद को दलित व आदिवासियों के हितैषी होने का भ्रम पैदा करता है। यह दलित व आदिवासी समाज के वोट हड़पने के षडयंत्र के अलावा कुछ और नहीं है।वे राजनीति के दोगलेपन पर सवाल उठाते हैं-दलित नेताओं को राष्ट्रपति तो बनाया गया, प्रधानमंत्री नहीं...क्यों?वे अनुभव से यह जानते हैं कि यह सारी कवायद राजनीतिक पैतरेबाजी और जन-साधारण को मूर्ख बनाने के अतिरिक्त कुछ और नहीं है।लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता को छलने का कृत्य किस श्रेणी में आता है, लेखक अपने आलेख में पाठक को यही बताने का प्रयास करता है। लेखक अपने मकसद में कितना सफल हुआ, कितना नहीं यह तय करना पाठक का विशेषाधिकार है।
तेजपाल सिंह ‘तेज’ के आलेखों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वे एक स्थाई विपक्ष की भूमिका में हैं और सरकार पर पैनी दृष्टि बनाए हुए हैं। यह वह दौर है जब प्रतिरोध की अनेक आवाजें मूक हो गई हैं या मूक कर दी गई हैं, लेकिन लेखक है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो अपनी आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं है। वहआज के लोकतंत्र की नई हकीकत और राजशाही के शिकंजे में कसमसाती लोकशाही जैसे लेख लिखकर लोकतंत्र पर मंडराते खतरे की परत दर परत खोलता नजर आता है। उनकी चिंता के केंद्र में संवैधानिक संस्थाएं हैं। उन्हें लगता है कि लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं वर्तमान निजाम के दबाव में हैं या वे अन्य किन्हीं निजी कारणों की वजह से सरकार के शरणागत हो गई हैं। उन्हें लगता है जैसे लोकतंत्र मात्र कहने में या कागजों तक में सिमट कर रह गया है, व्यवहार में इसकी झलक कम ही देखने को मिलती है। संभवत: लेखक इसी अवस्था को अपाहिज कहने का साहस कर रहा है।
गौरतलब है, सिस्टम की नैया स्वत: ही एक दिशा में नहीं चलने लगती। इसे दिशा विशेष में ले जाने के लिए पतवार की जरूरत होती है। लेखक का मानना है कि मुख्यधारा की मीडिया रूपी नैया यूं ही दिशा विशेष में नहीं बह रही है, जाहिर है, इस नैया के खिवैया की पतवार में बड़ी ताकत है। इसी के चलते लेखक मुख्यधारा के मीडिया की ईमानदारी पर सवाल उठाता है और आरोप लगाता है कि यह सरकार की एक एजेंसी की तरह काम करता है। संभवत: रवीश कुमार भी इसी मत के हैं और वे मुख्यधारा के मीडिया से दूर रहने, इसे न देखने की सलाह देते हैं। एक आम धारणा है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा कोई दरवाजा खुल जाता है। लेखक यू-ट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स को दूसरे दरवाजे के रूप में देखता है। लेकिन उसका मानना है कि सरकार इस दूसरे दरवाजे पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। लेखक सवाल उठाता है कि सरकार यू-ट्यूब चैनल्स/सोशल मीडिया से इतना क्यों घबराती है। लेखक सरकार के चरित्र को राजशाही की संज्ञा देता है और मीडिया को सरकार की कठपुतली रूप में देखता है, आज जिसका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। लेखक इसे अमर्यादित पत्रकारिता की संज्ञा देता है और लोकतंत्र पर हमले के रूप में देखता है। लेखक इसे वर्तमान लोकतंत्र के अपाहिजपन की एक अन्य कड़ी के रूप में देखता है।
वर्तमान निजाम के सहयोगी, तथाकथित सामाजिक संगठनों और वर्तमान निजाम के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेखक को इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर बाध्य करता है- हिंदू कुछ भी कहें “हिंदुत्व” स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा तो है ही”। वर्तमान चुनाव के दौर में सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चार सौ पार के आंकड़े की मांग और इसके कारण के रूप में संविधान बदलने की घोषणा लेखक को इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर बाध्य करती है कि भाजपा संविधान को बदलकर मनु-स्मृति से देश को चलाने की साजिश कर रही है। मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी साधारण से व्यक्ति के मन में ऐसी शंका का घर कर जाना स्वाभाविक है। वह भी तब जब वर्तमान निजाम के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा इसका मुखर रूप से खंडन नहीं किया गया है।
गौरतलब है- हाशियाकृत समाज के जीवन में जैसी भी, जो भी उजाले की किरण आई है, वह संविधान की ही बदौलत है। संविधान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगना इस हाशियाकृत समाज की आशा की किरण पर प्रश्न चिन्ह लगने जैसा है। इस मसले पर लेखक का आंदोलित होना किसी भी सूरत में नाजायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर यह कहा जाए कि समाज के हर जिम्मेदार नागरिक का आंदोलित होना समय की मांग है और इसकी पूर्ति होना, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। गलत तो क्या, यह समाज व राष्ट्र के हित में है। लेखक संविधान पर हमले को लेकर इतना आशंकित है कि वह तथाकथित दलित समाज की हितैषी मायावती को संदेह की नजर से देखते हैं। यह धारणा आम होती जा रही है- कारण कोई भी हो, लेकिन मायावती भी मीडिया व संवैधानिक संस्थाओं की तरह भाजपा के प्रभाव में लगती है। लेखक मायावती की मौजूदा संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाता है- मायावती कब क्या किस आधार पर निर्णय लेती हैं कुछ पता नहीं। मैं इसे लेखक की ईमानदारी और देश के व्यापक हित में देखता हूं। पाठक इसे किसी भी रूप में देखने के लिए स्वतंत्र हैं।
यह चुनाव का दौर है, बेशक हर तरफ अफवाहों का जोर है। ऐसे में लेखक का चुनाव की आंधी की चपेट में आने से बच पाना मुश्किल था।जाहिर है, लेखक ने भी चुनाव की बहती गंगा में डुबकी लगा ही डाली। इसे लेखक की जागरूकता कहें या कुछ और, लेखक सवाल उठाता है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं हिन्दू-मुसलमान का जिक्र नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव में जमकर हिंदू-मुसलमान को आमने-सामने खड़ा कर ध्रुवीकरण की मुहिम जारी है। राजनीति का इतना पतन किसी ने नहीं देखा होगा जितना इस बार हर नागरिक देखने को विवश है। स्पष्ट है, लेखक की दृष्टि में इस पतन के लिए भाजपा जिम्मेदार है। इसी के चलते वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है- दिखने लगी बीजेपी में चुनाव जीतने की बौखलाहट। लेखक इतने पर ही नहीं रुकता और एक कदम आगे बढ़कर भाजपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहता है - जीतने के लिए भाजपा सरकार देश में सब कुछ बदल देना चाहती है। लेखक का वर्तमान सरकार को तानाशाही व संविधान विरोधी सरकार कहने का अलग अंदाज है।
वर्तमान पुस्तक में लेखक द्वारा शामिल सभी आलेख व्यवस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ का पोस्टमार्टम करते नजर आते हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे यहां चर्चा का विषय नहीं बनाया गया है। दीगर हकीकत यह भी है कि प्रत्येक आलेख में लेखक बराबर सवाल उठाता है। ये वे सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि लोकतंत्र के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। लेखक इस खिलवाड़ के लिए वर्तमान सत्ता को जिम्मेदार मानता है और इसे तानाशाही व निरंकुशता की संज्ञा देता है। इस तानाशाही से निपटने के लिए लेखक भारत को मिलीजुली व समावेशी सरकार की आवश्यकता महसूस करता है। मिलीजुली इसलिए कि लेखक भली भांति जानता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में नहीं है। समावेशी सरकारका आग्रह दर्शाता है कि लेखक की मान्यता है कि लोकतंत्र के अपाहिजपन के लिए वर्तमान निजाम जिम्मेदार है और लोकतंत्र की इससे मुक्ति लोकतंत्र के पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह लेखक की स्थापना है, पाठक इसके अन्य विकल्पों पर भी विचार करने के लिए स्वतंत्र है।
लेखक के सभी आलेख पूर्व प्रकाशित हैं। इन आलेखों को किसी भी मुद्दे पर लेखक की त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। इतना तय है कि लेखक बेहद संवेदनशील है और उसे सिस्टम में जो कुछ भी संदिग्ध लगता है, लेखक उस बिंदु पर अपनी कलम बेबाकी से चला देता है।कुछ आलेखों के विषयों की साम्यता के चलते ये पुनरावृत्ति से अछूते नहीं रह पाए हैं। मौजूदा आलेखों का संग्रह पूर्वाग्रह की परिधि से बाहर नजर आता हैऔर लेखक की ईमानदारी का समर्थन करता है। यह कतई जरूरी नहीं कि पाठक का मत मेरे मत से मेल खाए। अंत में इतना दावे से कहा जा सकता है कि असहमति के अनेक बिंदुओं के बावजूद, इन आलेखों को पढ़ते वक्त पाठक को ऐसा कुछ अवश्य मिलेगा जो पाठक को परिस्थितियों के मूल्यांकन और उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा। इस मदद से मेरा तात्पर्य पाठक का अपनी स्वतंत्र राय बनाने से है, जो लेखक के मत से भिन्न भी हो सकती है। उम्र के अस्सीवें पड़ाव पर लेखक का समाज व देश के प्रति जागरूकता लेखक को साधुवाद का पात्र बनाती है। लेखक की लेखनी की निरंतरता की कामना के साथ...
- ईश कुमार गंगानिया
आमुख...
लोकतंत्र का अलोकतांत्रिक स्वरूप
लोकतंत्र को अब तक की सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना गया है। ज्यादातर देश इसे पाने या बनाये रखने की रात-दिन कोशिशें करते रहे हैं।लेकिन भारतीय लोकतंत्र की कुछ समस्याएं और लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी है। चार प्रमुख समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं- देश की एकता और पूर्णता बनाए रखना, उच्च एवं न्यायिक स्थिति पर व्यापक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, आंतरिक सुरक्षा जैसी समस्याएं,सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी, अशिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च आदि राजनीतिक समस्याएं। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए लोकतंत्रके समक्ष जो चुनौतियां हैं वो हैं - भारत का लोकतंत्र निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण और हिंसा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की मुख्य दो शर्ते हैं - लोकतन्त्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतन्त्र एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, जिसमे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता हैं। एक अच्छा लोकतन्त्र वह है जिसमे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। लोकतांत्रिक भारत से पता चलता है कि चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी पंथ के बावजूद, बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। भारत की लोकतांत्रिक सरकार जिन सिद्धांतों पर आधारित है-वे हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय।
लेकिन जिन लोगों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, उन्हें ईमानदारी और समर्पण भाव से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की आवश्यकता है-फिर वे चाहें सरकारें हों, संवैधानिक संस्थाएं हों, विपक्षी दल अथवा नागरिक हों। लोकतंत्र अगर लोगों की पहली वरीयता नहीं रह जाता तो नि:संकोच यह माना जा सकता है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर जा खड़ी हुई है। किंतु आज के राजनीतिक परिवेश में यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज लोकतंत्र के हालात चिंताजनक हैं।खेद की बात है कि आज राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। आज के अधिकतर युवा वर्तमान राजनीति की अराजकता/भ्रष्टाचार के चलते राजनीति से जुड़ऩा चाहते हैं, यह एक अच्छा संकेत नहीं हैं, होना तो ये चाहिए कि युवाओं को लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि किसी की अंध-भक्ति करना चाहिए। इन युवाओं को सोचना चाहिए कि किसी भी राजनेता की व्यक्तिगत पूजा करने में उनका ही शोषण होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि देश में सत्तासीन राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक शक्तियां देश के संविधान में अपने दिमागी दिवालियापन के चलते हुए कुछ न कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं और संविधान की समीक्षा के नाम पर संविधान को बदलना चाहते हैं। ये कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखा तो ये भी गया हैं कि चाहे तो सामाजिक/धार्मिक संगठन हों अथवा राजनीतिक दल सबके अपने-अपने संघर्ष और उद्देश्य होते है और जब उनके संघर्ष आपस में टकराते हैं तो सबकुछ घालमेल हो जाता है। यह एक चिन्ता का विषय है।
सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा। देश में हर महीने 70 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं।दूसरी तरफ “कॉर्पोरेट” देश को लूट रहे हैं और उनके लाखों-करोड़ों रुपये के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। साथ ही अनेक कर्जदार पूंजीपति विदेश भाग जाते हैं। भारत के 25 सबसे बड़े विलफुलडिफॉल्टरों (Willful Defaulters) पर देश की विभिन्न बैंकों के जरिए आम जनता की कमाई को लूट रहे हैं। और सरकार की इनके कर्जों को वसूलने की मंशा सामने नहीं आ रही है। लोकतांत्रिक देशों की सरकारें जो भी काम करती हैं, वो केवल और केवल चुनाव जीतकर हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए करती हैं...राजनेताओं का यही एक भाव है कि सत्ता में बने रहने के लिए वो जो भी अच्छे-बुरे कार्य करते है,वो ऐसे होते हैं कि उनसे भूल से ही जनता का कुछ भला हो जाए तो ठीक...अन्यथा अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए सभी लोकतांत्रिक देशों के सभी सत्ता प्रमुख जनहित में दिखने वाले एक के बाद एक अनेक योजनाओं की घोषणाएं करते रहतें हैं।...उनके क्रियान्वयन का होना न होना, प्रशासन के सिर मढ़ दिया जाता है। इस प्रकार आज के दौर में हर क्षेत्र में पराभव ही हुआ है...चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर कोई और। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस प्रकार की समस्याओं के केंद्र में ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ ही होता है... सरकार और पूंजीपतियों के बीच एक साठगांठ वाला पूंजीवाद, जो कुटिल राजनेता और व्यवसायी को धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के अनुरूप होता है जिससे वह चुनाव लड़ सके। भ्रष्ट व्यवसायी को सार्वजनिक संसाधन और ठेके सस्ते में पाने के लिए कुटिल राजनेता की आवश्यकता होती है। और राजनेता को गरीबों और वंचितों के वोट चाहिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र निर्भरता के चक्र में दूसरे से बंधा हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यथास्थिति बनी रहे। आर्थिक व्यवस्था का ऐसा गठबंधन देश के लिए सर्वथा विनाशकारी है जिसमें आम आदमी की उपेक्षा होना लाजिम है। एक सौ चालीस करोड़ के देश में 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर जिंदा रहना इसका जिंदा प्रमाण है। जाहिर है कि पिछले दशक में गरीबी के रेखा नीचे जीने वालों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इस दृष्टि से आज के भारतीय लोकतंत्र को अपाहिज लोकतंत्र न कहा जाए तो और क्या कहा जाए?
शरीर के किसी हिस्से या भाग के ठीक काम न करने अथवा उससे वंचित रहने वाले व्यक्ति को विकलांग, अपंग या अपाहिज कहा जाता है। ये बड़े आम शब्द हैं और हिन्दी में खूब इस्तेमाल होते है और इनके विकल्प के तौर पर अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा का दूसरा कोई शब्द इनसे ज्यादा प्रचलन में नहीं है। बतौर मुहावरा अपाहिज या विकलांग जैसे शब्दों का प्रयोग परिस्थिति पर व्यंग्य करने में भी किया जाता है जैसे अपाहिज व्यवस्था, अपाहिज कुर्सी वगैरह। आशय किसी प्रणाली के समुचित रूप से कार्य न करने से ही होता है।
यहाँ यह भी उल्लेख करता चलूं कि प्रस्तुत पुस्तक में संकलित सभी लेख वर्ष 2024 के फरवरी से मई तक की समयावधि में स्वरूप ले पाए हैं। विदित हो कि ये समयावधि चुनावी शोरशराबे का रहा है।और यह भी कि सभी के सभी के लेख सम्मानित ‘गाँव के लोग’ व ‘न्याय तक’ जैसे प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टलस में प्रकाशित हो चुके हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत लेखों में आपको एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा के समरूप अपाहिज लोकतंत्र का चित्रण देखने को मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ।
अपाहिज लोकतंत्र की पीड़ा ठीक एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा के समकक्ष है। फर्क है तो बस इतना कि एक अपाहित व्यक्ति अपने अपाहिज होने की पीड़ा को स्वयं सहता है लेकिन अपाहिज लोकतंत्र की पीड़ा समूचे देश और उस देश के तमाम वंचित समाज को झेलना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि इस विषय को अनेक अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर एक अनापेक्षित तमाशा खड़ा किया सकता है किंतु हमें पुस्तक के शीर्षक की भावना और सच्चे लोकतंत्र की भावना को समझना जरूरी है। यह भी कि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा की भाँति ही अपाहिज लोकतंत्र की पीड़ा का सार्वजनिक प्रदर्शन अत्यंत अपमानजनक है किंतु इस प्रकार की पीड़ा का उल्लेख करना पीड़ा को गहरे से अनुभव करनाएक मानवीय अवस्था होने के साथ-साथ राजनीति में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना भी एक मुख्य उद्देश्य है।
ज्ञात हो कि राजनीतिक दल भी एक प्रकार का संगठित पंथ अथवा समूह है जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक हेरफेर और दबाव रणनीतियों के माध्यम से पंथ/दल के सदस्यों व आम जनता पर हावी होना होता है। सरकार का नेतृत्व आमतौर पर एक शक्तिशाली नेता द्वारा किया जाता है जो सदस्यों को शेष समाज से अलग करता है। और आम जनता पर शासन करता है। दरअसल आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई सरकार नहीं होती। सरकार सदैव जनता के हित में वो कदम उठाती है जिससे उसकी सत्ता बनी रहे। न्याय व्यवस्था भी अक्सर ऊँची पहुँच वाले लोगों के हक में काम करती है। यथा – यदि कोईं पहुंच वाला व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे केवल एक महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि कोई वंचित/गरीब व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का चिकन भी चुरा लेता है तो उसे असीमित समय के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इसलिएसरकार को देश में सामाजिक न्याय प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए लेकिन कागजों में ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है किंतु जमीन पर काम करती नजर नहीं आती।
वी-डेम की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से भारत एक ‘चुनावी तानाशाह’ राष्ट्र बना हुआ है: 'डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूज़िंग एट द बैलट (चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार)' शीर्षक वाली रिपोर्ट वी-डेम इंस्टिट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2024 में कहा गया है कि भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है. वी-डेम (वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी) इंस्टिट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2024 के अनुसार, विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही (Electoral Autocracy) वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा, जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। यह एक अपाहिज लोकतंत्र की ही मिसाल है। अपाहिज लोकतंत्र के और भी अनेक कारण हैं जिनसे जनता भली-भाँति परिचित तो होती है किंतु रोजमर्रा की गतिविधियों के चलते कभी उनपर ध्यान नहीं देती है।......
04.06.2024 : अब जबकि 2024 के आम चुनाव का परिणाम जनता के सामने आ गए हैं तो एक सवाल जोरों से उठ रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ़ 100 सीटें मिली हैं। फिर कांग्रेस कोइसमें इतना उत्साहित और खुश होने की क्या जरूरत है? एनडीए को बहुमत मिला है। सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। तमाम गोदी मीडिया इसी सवाल को बार-बार ही दोहरा रहे है। इस सवाल में समझ का कितना बड़ा स्तर दिखाई देता है? गोदी मीडिया नहीं जानता कि जो भी नतीजे आए हैं, इन नतीजों का मतलब क्या है? इन नतीजों से इस देश में क्या बदलने वाला है? सरकार किसी की भी बने, इस देश में क्या बदलाव होने वाला है? इस देश में क्या शुरू होने वाला है? वो कौन सी चीजें होने वाली हैं, जिनकी वजह से हम फिर से एक बेहतर स्वर्णिम युग में आ गए हैं? क्या अब लोकतंत्र बच गया है? इस पर अभी हमें सरकार बनने का इंतजार और आने वाले दिनों में सरकार की कार्यप्रणाली को देखना बाकी है। हाँ! इतना अवश्य है कि अब महज गठबंधन की सरकार बनना नितांत तय है जिसमें शामिल अब कोई भी राजनेता अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, जैसा कि पिछ्ले दस वर्षों की सरकार के कार्यकाल में देखन को मिला है। खैर.....अब देखना यह है कि लोकतंत्र के बंद होते दरवाजे कितने खुलते नजर आते हैं।
एक बात और स्पष्ट करदूँ कि मेरे ये आलेख किसी प्रकार के व्याकरण और पांडित्य से अभिभूत नहीं हैं, केवल समाज को उद्वेलित करने वाली घटनाओं को केवल शब्द रूप-भर दिया है।पाठकों से मेरी अपेक्षा है कि वे शब्दों और उनके प्रस्तुतिकरण के उलट-फेर में न पड़कर मेरे लेखों की जीवंतता की गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे ताकि वो मेरे करीब, और करीब आ पाएं। उनकी सार्थक प्रतिक्रियाएं निःसंदेह मेरा उत्साहवर्धन करेंगी।
मेरी इस यात्रा में आलोचक/समीक्षक/उपन्यासकार ईश कुमार गंगानिया और सामाजिक एक्टिविस्ट व विचारकशीलबोधि सदैव मेरे भागीदार बने रहे, इस हेतु मैं उनका आभार-भर व्यक्त करके मुक्त नहीं होना चाहताबल्कि मैं उनकी इस उदारता की निरंतरता का अभिलाषी बना रहना चाहता हूं। हां! अपने सभी सहयोगियों का सहृदय आभार जरूर प्रकट करता हूं। मेरी इस पुस्तक के उत्कृष्ट और त्वरित प्रकाशन के लिए प्रकाशक श्री वरुण मिश्रा जी, BOOK RIVERS Publish@bookrivers.comsलखनऊ को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।
- तेजपाल सिंह ‘तेज’
अनुक्रमिका
क्र.सं. | अध्याय | पृष्ठ सं. |
1 | सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रही है शैक्षिक ढांचे की विषमता | 1 |
2 | नई शिक्षा नीति में समाज के कमजोर तबके को पीछे धकेलने का खतरा है | 10 |
3 | ....तो यह है हमारे आज के लोकतंत्र की नई हकीकत | 20 |
4 | भला! घुट-घुटकर जीवन यापन करने की बाध्यता शादी ही क्यों हो? | 29 |
5 | राजनीति रोजगार/व्यवसाय का हिस्सा बनती जा रही है | 37 |
6 | सरकार सोशल मीडिया से इतना क्यों घबराती है | 44 |
7 | अपने ही जाल में फंसताजा रहा है बहुजन समाज | 53 |
8 | राजशाही के शिकंजेमें कसमसाती लोकशाही | 57 |
9 | संविधान को बदलकर भाजपा कर रही है मनुवाद से राष्ट्र को चलाने की साजिश | 65 |
10 | भारतीय राजनीति अब भगवानों को भी जमीन पर उतार लाने में सक्षम | 74 |
11 | आमचुनाव 2024जीतने के लिए भाजपा सरकार देश में सब कुछ बदल देना चाहती है | 82 |
12 | सत्ता और राजनीति के दबाव में गायब हो रहे हैं मानवाधिकार के प्रश्न | 89 |
13 | मोदी जीपद की गरिमा के प्रतिकूल बातें क्यों करते हैं | 94 |
14 | बीजेपी/ आरएसएस को भीतरखाने दलितों व पिछड़ों से घिन आती है | 104 |
15 | मनुवाद से राष्ट्र चलाने की नियत से संविधान बदलने की साजिश की जा रही है | 110 |
16 | आम चुनाव 2024 : दिखने लगी बीजेपी में चुनाव जीतने की बौखलाहट | 119 |
17 | अग्निवीर योजना : दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक युवाओं के खिलाफ भाजपा-आरएसएस की बड़ी साजिश | 127 |
18 | मायावती अब नहीं रहींबाबा साहब के आदर्शों का मार्ग प्रशस्त करने वाली बहुजन नेता | 136 |
19 | तानाशाही के खात्मे के लिए देश को चाहिए एक मिली-जुली समावेशी सरकार | 146 |
20 | भाजपा और आरएसएस की हिंदुत्ववादी मानसिकता स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए सबसे बड़ा खतरा है | 156 |
21 | राजशाही के दबाव मेंमीडिया : अमर्यादित पत्रकारिता लोकतंत्र पर हमला | 166 |
22 | दलित नेताओं को राष्ट्रपति तो बनाया किंतु प्रधान मंत्री नहीं..क्यो | 173 |
23 | बेरोजगारी खत्म करने के बजाय क्यों दिया जा रहा है मुफ्त राशन के वितरण पर जोर | 181 |
24 | फाइबर की थाली में पनीर का जायक | 188 |
25 | 2024 आम चुनाव : भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तोहफा | 194 |
26 | कवि अपनी निजता को लोक-सत्ता में लीन किए रहता है | 201 |
27 | प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण में हुई भारी चूक : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू विवादों के घेरे में' | 209 |
सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रही है शैक्षिक ढांचे की विषमता
अशिक्षा किसी भी देश के ग़रीब और पिछड़ों को निरंतर दास बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। सरकार का सबको नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है किन्तु व्यावहारिकता इसके क़तई प्रतिकूल है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को नि:शुल्क शिक्षा, पुस्कालय की व्यवस्था, वैज्ञानिक शिक्षा जैसी अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की राष्ट्रीय व्यवस्था तो है किन्तु इसका क्रियात्मक स्वरूप एकदम उलट है। तब यह सोचना ही होगा कि क्या देहाती बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के उतने ही अवसर प्राप्त हैं जितने शहरी क्षेत्र के धनी परिवारों के बालक-बालिकाओं को हैं। क्या देहाती क्षेत्रों के स्कूलों में शहरी क्षेत्र के स्कूलों के समान शिक्षा-साधन उपलब्ध हैं? आमतौर पर देहात के सभी स्कूलों की स्थिति कमोवेश एक सी है। कहीं पर्याप्त अध्यापक है तो कमरे नहीं और कहीं पर्याप्त कमरे हैं तो अध्यापक नहीं। सामान्यतः सभी देहाती स्कूलों में अध्यापकों और कमरों, दोनों का ही अभाव है। इस प्रकार ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है।
कुछ वर्षों पूर्व की बात है कि जब कांग्रेस नए भारत की जनता से अनुरोध किया था, “भारत के दलित वर्गों पर जो रूढ़िगत अयोग्यताएँ लगाई हुई हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता न्यायसंगत है क्योंकि ये अयोग्यताएँ अत्यंत अमानुषिक और दमनकारी हैं जिस कारण इन्हें बहुत अधिक कठिनाइयाँ एवं असुविधाएँ सहनी पड़ती हैं।” लेकिन हुआ क्या? यह सबके सामने है। दलितों का न तो आर्धिक स्तर ही सुधरा है और न ही सामाजिक। दलितों की स्थिति जस की तस है। कारण है कि नेता लोग केवल व्यक्तव्यों और भाषणबाज़ी की आधार पर ही दलितों की स्थिति में सुधार का सपना देखते हैं, रचनात्मक कुछ भी नहीं करते। हाँ, दलितों के हक़ में घोषणा-दर-घोषणा ज़रूर करते रहते हैं किन्तु उनका कार्यांवयन क़तई नहीं होता। इस प्रकार राजनेताओं द्वारा दलितों के सुधार के तमाम वादे केवल वादे ही बनकर रह जाते हैं। यहाँ यह जानना भी ज़रूरी है कि दलितों की आर्थिक/शैक्षिक स्थिति में यदि कोई सुधार नज़र आता है तो वह सरकार की नीतियों के कारण नहीं अपितु विश्व स्तर पर आए परिवर्तनों के एक हिस्से के रूप में आया है।आज के संकुचित राजनीति और सामाजिक संस्कृति के चलते सरकार के ‘शिक्षा सबके लिए’ नारे का महत्त्व प्रशासनिक उपेक्षा का पूरी तरह शिकार है। सत्ता पर क़ाबिज़ मुट्ठी-भर लोग नहीं चाहते कि भारतीय समाज सक्षम बनें। शिक्षा-साधनों का अभाव और शिक्षा विभाग द्वारा देहाती बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। ख़ासतौर पर देखा जाए तो भारत में उपेक्षित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक कमज़ोरी कारण मूलतः अशिक्षा ही है।
और तो और आज भी आज़ादी प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी स्कूली बच्चों की शिक्षा का स्तर एक प्रश्नचिन्ह ही बना हुआ है। बच्चों को फटी-पुरानी टाट-पट्टियों पर बिठाने की व्यवस्था क्या आश्चर्यजनक नहीं? अधिकांश देहाती स्कूलों में शौचालय और पेशाब-घर नहीं हैं। नि:शुल्क पुस्तकों और वर्दियों का असमय वितरण तो आम बात है। नन्हें-मुन्हों को सरकारी स्तर से अल्पाहार की वैधानिक व्यवस्था तो है किन्तु इसका वितरण न तो नियमित है और न ही आवश्यक। आया तो आया, नहीं तो नहीं। यह सब स्कूली प्रशासन और ठेकेदारों की मिली-भगत के चलते ही होता है। कई बार तो ऐसी ख़बर सुनने-पढ़ने को मिलती है कि वर्ष-भर का कोटा एक ही महीने में समाप्त कर दिया जाता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में, न केवल समुचित शिक्षा-व्यवस्था है, बल्कि भाषाई अंतर भी विद्यमान है। वहीं देहाती स्कूलों में शिक्षारत देहाती बच्चों को केवल हिन्दी भाषा पढ़ाने के भी पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस प्रकार की दोहरी शिक्षा-प्रणाली ग़रीब और वंचित देहातियों के बच्चों के साथ एक साज़िश नहीं तो और क्या है? प्रतिक्रायात्मक दृष्टिकोण से भारत में विद्यमान दोहरी शिक्षा-प्रणाली, भारतीय समाज के लगभग 80/85 प्रतिशत ग़रीब और वंचित देहातियों के बच्चों के साथ एक अप्रत्यक्ष साज़िश ही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता।
ग़ौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में नियुक्त अध्यापक जितने सुशिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं, अध्यापन-कार्य उतना घटिया स्तर का होता है। क्यों? इसका मुख्य कारण उनकी किसी प्रकार की जवाबदेही न होना ही है। यहाँ तक देखा गया है कि सरकारी स्कूलों के अधिकांश अध्यापकों के अपने बच्चे अक़्सर निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह भी पाया गया है कि अधिकांश अध्यापकों के अपने बच्चों का दसवीं और बारहवीं का परीक्षा परिणाम औसत से नीचे ही रहता है। कारण है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक ज़्यादातर ट्यूशन पढ़ाने में ही व्यस्त रहते हैं। अपने बच्चों के प्रति नकारात्मक रवैया रखने वाले अध्यापक अन्य बच्चों के पठन-पाठन का ध्यान रख पाएँगे, यह एक प्रश्न-चिन्ह ही है। इस स्थिति में सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर सहज ही आँका जा सकता है। सरकारी स्कूलों के ढुलमुल रवैये और निम्नस्तरीय शिक्षा-प्रबन्धों के चलते निजी स्कूलों को अप्रत्याशित बढ़ावा मिला है जो अच्छी शिक्षा के नाम पर मनमाने ढंग से अनाप-शनाप पैसा वसूलते हैं। खेद की बात तो ये है कि सरकारी तंत्र पूर्णरूपेण: निजी स्कूलों साथ खड़ा दिखता है। सरकार सामाजिक हितों को अत्यधिक सस्ती दरों पर ज़मीन का आवंटन करती है और ये स्कूल सरकार और समाज की आँख में धूल झोंक कर पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देते हैं।
यथोक्त के आलोक में यह ज़रूरी है कि अध्यापकों और अभिवावकों को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि शिक्षा, मीडिया और राजनीति तीनों विषय बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हमें दुनिया के बारे में जानकारी देता है। राजनीति एक ऐसा विषय है जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। किन्तु शिक्षा और मीडिया का आचरण राजनीति के आचरण पर निर्भर करता है। बिना हम अपने देश को सफल नहीं बना सकते अथवा असफल। शिक्षा एक व्यापक माध्यम है, जो छात्रों में कुछ सीख सकने के सभी अनुभवों का विकास करता है। शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रकार यह कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं तंत्रिका विकास, मानसिक, नैतिक विकास और सौन्दर्यविषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा, समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्त्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। किन्तु यह तब ही सम्भव है जब देश की शहरी और ग्रामीण शिक्षा का स्तर न केवल समान हो अपितु आवश्यक प्रबंध व्यवस्था के तहत उत्तम शिक्षा के सबकों बराबर अवसर प्रदान हों। ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है।
आज भी ग्रामीण अंचल के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ कमरों व डेस्क-बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते नज़र आते हैं। अधिकतर स्कूल तो कक्षा एक से कक्षा पाँच तक के बच्चे लगभग एक ही कमरे में केवाल एक ही अध्यापक द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं। कहना अनुचित न होगा कि आजकल केवल ग़रीब परिवारों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने को बाध्य हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को पीने के पानी के लिये भी भटकना पड़ता है। शौचालय स्कूलों में बनाए अवश्य गए हैं, लेकिन पानी के अभाव में उनमें साफ़-सफ़ाई रख पाना मुश्किल हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, लेकिन इस दिशा में कोई बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती। शिक्षा सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद तक भी पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पातीं। देश के बहुत से ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से एडूसेट के उपकरण लगाए गए हैं। लेकिन भारी-भरकम ख़र्च से लगाए गए ये उपकरण अधिकांश स्कूलों में मात्र शो-पीस बनकर रह गए हैं। ग्रामीण सरकारी स्कूलों की छवि ग़रीबों और अशिक्षितों के बच्चों के स्कूल वाली बन गई है, जो पूरी तरह शिक्षकों की दया पर निर्भर हैं।
आज भी शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही ख़र्च होता है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। ग्रामीण स्कूलों में अक़्सर यह देखने में आता है कि अध्यापक आते ही नहीं हैं और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज़ कोई-न-कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है।
संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है और इसका प्रमुख ज़िम्मा राज्यों पर है। ऐसे में ज़रूरत है कि सभी राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसकी चुनौतियों को अपने ढंग से हल करें। ऐसा हुआ भी है और इसके अलग-अलग परिणाम सामने आए। जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का विकास बेहतर तरीक़े से हुआ, वहाँ ग़रीब बच्चों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अंग्रेज़ी शिक्षा दिलाने के लिये निजी स्कूलों में भेजता है।
द हिंदू के अनुसार ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को वर्णित करते हुए कहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति-2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छात्रों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। यह रिपोर्ट NGO ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (NGO Transform Rural India) और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस (Sambodhi Research and Communications) के सहयोग से डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (Development Intelligence Unit-DIU) द्वारा किये गए सर्वेक्षण पर आधारित थी। इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के 6,229 माता-पिता से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं।
सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसारहैं:
49.3% छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच है। 76.7% माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लिये करते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त 56.6% छात्र फ़िल्में डाउनलोड करने और देखने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 47.3% छात्र गाने डाउनलोड करने और सुनने हेतु स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत केवल 34% छात्र अध्ययन-संबंधी सामग्री डाउनलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और केवल 18% छात्र ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिये इसका उपयोग करते हैं।
कक्षा के आधार पर विभेदक सूचना निम्नानुसार है:
कक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच अलग-अलग होती है। उच्च कक्षाओं (आठवीं और उससे ऊपर) के छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुँच (58.32%) है, जबकि 42.1% छोटे छात्रों (कक्षा I-III) तक पहुँच है। यह इंगित करता है कि मनोरंजन के लिये स्मार्टफोन का उपयोग सभी आयु समूहों में प्रचलित है, जो संभावित रूप से उनकी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है।
इस रिपोर्ट में माता-पिता की आकांक्षाएँ और व्यस्तता का भी ज़िक्र करते हुए कहा गया है:78% माता-पिता अपने बच्चों को स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, किन्तु इस संदर्भ में अभिभावकों की अपने बच्चों के साथ सहभागिता काफ़ी कम है। केवल 40% माता-पिता अपने बच्चों के साथ उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में दैनिक बातचीत करते हैं, जबकि 32% सप्ताह में कुछ दिन ऐसी बातचीत में संलग्न रहते हैं।
स्कूल से ड्रॉपआउट करने वाले बच्चों के बारे में जो कारण बताए गए हैं- वो है कि लड़कियों के मामले में 36.8% माता-पिता ने उल्लेख किया कि पारिवारिक कार्यों में योगदान देने के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इस बीच 31.6% ने अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचि की कमी को स्कूल छोड़ने के लिये ज़िम्मेदार ठहराया और 21.1% का मानना था कि इसमें घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी अहम भूमिका निभाती हैं। 71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार, पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण विषय-वस्तु में रुचि की कमी थी। इसके बाद 48.7% उत्तरदाताओं को परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिये लड़कों की आवश्यकता महसूस हुई। 84% अभिभावकों ने नियमित उपस्थिति दर्ज की। गैर-उपस्थिति के दो मुख्य कारण हैं-अल्प सूचना और इच्छा की कमी। इसके अतिरिक्त 40% अभिभावकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य आयु-उपयुक्त पठन सामग्री की उपलब्धता की सूचना दी गई, जो घर पर बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिये अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
यथोक्त के आलोक में कहा गया है कि घर पर शैक्षिक माहौल बनाने तथा मनोरंजन और सीखने दोनों उद्देश्यों के लिये स्मार्टफोन के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा संविधान में किया गया है। इसे दस साल में पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया था, जो पूरा नहीं हो सका। सभी बच्चे स्कूल जाएँ और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले . . . ये दो धाराएँ न होकर एक-दूसरे से परस्पर संबंधित और अपरिहार्य शर्तें हैं। इनमें से किसी एक को पूरा करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। बच्चों की असफलता का दोष केवल स्कूल के संस्थागत कारणों को नहीं दिया जा सकता। दोष प्रायः संसाधनों के अभाव और शिक्षकों के अकुशल रवैये को दिया जाता है। लेकिन यह भी तय है कि केवल इन्हें ही दोषी मानकर इस समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता। इस समस्या का समाधान यही है कि अध्यापकों पर संदेह करने और उनके कार्यों की निगरानी के बजाय उन पर भरोसा किया जाए और उन्हें समर्थ और कुशल बनाने की दिशा में क़दम बढ़ाए जाएँ। इसके अलावा पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, पास-फेल की नीति में बदलाव या बाल केंद्रित शिक्षा के बहाने संसाधनों की भरमार के बावजूद यह विचार करना होगा कि कैसे शिक्षा की प्रक्रिया में गाँव और शहर का अंतर कम हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाने के लिये हर हाल में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। लेकिन इस दिशा में न तो जनप्रतिनिधि पर्याप्त रुचि दिखाते हैं और न ही शिक्षा विभाग के अधिकारी। सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएँ देने के बावजूद धरातल पर स्थिति में बहुत बदलाव नज़र नहीं आता।
बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों से बेहतर हैं। 2018 के आँकड़े बताते हैं कि पाँचवीं कक्षा के ऐसे बच्चे जो कक्षा 2 की पठन दक्षता रखते हैं, का प्रतिशत सरकारी स्कूलों में 44 और निजी स्कूलों में 66 है। इसके पक्ष में निजी स्कूलों की आधार-संरचना, अध्यापकों की निगरानी और समर्पित प्रबंधन का तर्क पर्याप्त नहीं है। यह ज़रूर है कि निजी स्कूलों के बच्चों के अभिभावक पढ़ाई का ख़र्च उठा सकते हैं। यानी कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश घर पर पढ़ने-पढ़ाने में सहयोग देने वाला होता है। घर और स्कूल दोनों जगहों पर सीखने के कारण बच्चे कुशलता को अर्जित कर रहे हैं। दूसरी ओर, गाँवों के निजी स्कूल शहरी निजी स्कूलों की तरह सुविधायुक्त नहीं हैं। वे कम फ़ीस लेते हैं और साधारण संसाधनों से युक्त हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों के संदर्भ में इसका अभाव है। गाँवों और शहरों में सांस्कृतिक अंतर भी है एक बड़ा कारण है। असर की इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के लिये स्कूल ऐसी जगह बनता जा रहा है जहाँ बच्चे अपने दिन का बड़ा हिस्सा तो बिताते हैं लेकिन स्कूल जाने का जो प्रयोजन या उद्देश्य है, उसे वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं। आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं जहाँ कमरों व डेस्क-बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते नज़र आते है। गर्मी के मौसम में बच्चों को पीने के पानी के लिये भी भटकना पड़ता है। शौचालय स्कूलों में बनाए अवश्य गए हैं, लेकिन पानी के अभाव में उनमें साफ-सफाई रख पाना मुश्किल हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, लेकिन इस दिशा में कोई बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती। शिक्षा सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद तक भी पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पातीं।
एक समय था कि जब निजी स्कूल गिने-चुने ही हुआ करते थे, वह भी शहरी क्षेत्रों में। किन्तु आज यह स्थिति हो गई है कि गाँवों, नगरों व शहरों में या यूँ कहें कि सर्वत्र निजी स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। अंग्रेज़ी भाषा को जानना कोई बुरा काम नहीं है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना दूसरे देशों से सम्पर्क बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम है, इसे मानने से इंकार नहीं किया जा सकता किन्तु यह सुविधा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि निजी स्कूलों के बच्चे बेहतर है।बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों से बेहतर हैं। आँकड़े बताते हैं कि पाँचवीं कक्षा के ऐसे बच्चे जो कक्षा 2 की पठन दक्षता रखते हैं, का प्रतिशत सरकारी स्कूलों में 44 और निजी स्कूलों में 66 है। इसके पक्ष में निजी स्कूलों की आधार-संरचना, अध्यापकों की निगरानी और समर्पित प्रबंधन का तर्क पर्याप्त नहीं है। यह ज़रूर है कि निजी स्कूलों के बच्चों के अभिभावक पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। यानी कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश घर पर पढ़ने-पढ़ाने में सहयोग देने वाला होता है। घर और स्कूल दोनों जगहों पर सीखने के कारण बच्चे कुशलता को अर्जित कर रहे हैं। दूसरी ओर, गाँवों के निजी स्कूल शहरी निजी स्कूलों की तरह सुविधायुक्त नहीं हैं। वे कम फीस लेते हैं और साधारण संसाधनों से युक्त हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों के संदर्भ में इसका अभाव है। इसके अलावा, बच्चों की उपलब्धि और सीखने में एक सांस्कृतिक अंतर भी है जो स्कूल में प्रवेश के पहले से सक्रिय हो जाता है। शिक्षा का अधिकार भी इस सांस्कृतिक अंतर को पाटने में असमर्थ है। यहाँ इस तथ्य को मद्देनज़र रखना होगा कि जैसे ही गाँव के निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को मौका मिलता है, वे अपने बच्चे को शहर के स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। अत: शैक्षिक अवसरों की समानता व गुणवत्ता की दृष्टि से गाँवों में बसने वाला भारत ऐसी भौगोलिक इकाई बनता जा रहा है जहाँ शिक्षा के मूलाधिकार की प्रक्रिया और परिणाम में गहरी खाई है। अमीरी और गरीबी ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। लिंग, जाति, क्षेत्र, भाषा और धर्म भी इनसे जुड़कर एक जटिल संरचना बना रहे हैं जो इसे बढ़ावा दे रहा है।
निजी स्कूलों के चलते, छोटे-छोटे बच्चों पर अधिक से अधिक कॉपी-किताबों का बोझ ही जैसे अच्छी पढ़ाई का पर्याय बन गया है। कहना अतिश्योक्ति नहीं कि आधुनिक भारत में शिक्षा के नाम पर दुकानदारी ही पनपी है। सच्चाई तो है कि आजकल बच्चों को जो कुछ भी प्रारंभिक शिक्षा के नाम पर पढ़ाया जा रहा है, उससे न केवल उनका बचपन छीना जा रहा है, अपितु बच्चों को सुसंस्कार भी नहीं मिल पा रहे हैं। किताबों के साथ-साथ बस्ते में उनका बचपन भी समा गया है। आर्थिक संकट में फँसे ग्रामिणों के बच्चों की शिक्षा केवल सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर रहती है क्योंकि वे आर्थिक संकट के चलते निजी स्कूलों का ख़र्चा उठाने में पूरी तरह से अक्षम होते हैं। एक दृष्टिकोण से निजी स्कूलों के प्रचलन से निम्न और उच्च वर्गों के बीच का अंतर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आधार पर वर्तमान ढाँचे से सामाजिक विषमताएँ और भी बढ़ी हैं। सामाजिक असमानता की जड़ें और भी गहरी हुई हैं किन्तु अफ़सोस कि किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता।
0000
नई शिक्षा नीति में समाज के कमजोर तबके को पीछे धकेलने का खतरा है
किसी भी तानाशाह की पहली सोच होती है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल को अपने दो तोन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दे। मीडिया और अन्य जाँच एजेंसियों को अपने काबू में ले ले। इतना ही नहीं न्याय प्रणाली को अपने आधीन करले और 95% जनता को भिखारी बना दे। उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। इस संदर्भ में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रधान मंत्री की कार्यप्रणाली भारतीय लोकतंत्र को तानाशाही का जामा पहनाने की ओर अग्रसर है? इस लेख में केवल नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही बात की जा रही है।
नागरिकों के बुनियादी अधिकारों में शिक्षा भी शामिल है और बेहतर नागरिक बनाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र औजार है, लेकिन अफसोस ये है कि चुनावी विमर्श और वोट की राजनीति में शिक्षा कभी प्रमुख मुद्दा नहीं बनती है। विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक सिर्फ वोट बैंक की तरह ट्रीट किए जाते हैं और चुनावी राजनीति में बस उनका इस्तेमाल किया जाता है।
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा संविधान में किया गया है। इसे दस साल में पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया था, जो पूरा नहीं हो सका। सभी बच्चे स्कूल जाएँ और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये दो धाराएँ न होकर एक-दूसरे से परस्पर संबंधित और अपरिहार्य शर्तें हैं। इनमें से किसी एक को पूरा करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। बच्चों की असफलता का दोष केवल स्कूल के संस्थागत कारणों को नहीं दिया जा सकता। दोष प्रायः संसाधनों के अभाव और शिक्षकों के अकुशल रवैये को दिया जाता है। लेकिन यह भी तय है कि केवल इन्हें ही दोषी मानकर इस समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता। इस समस्या का समाधान यही है कि अध्यापकों पर संदेह करने और उनके कार्यों की निगरानी के बजाय उन पर भरोसा किया जाए और उन्हें समर्थ और कुशल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएँ। सिद्धांतत: यह एक आदर्श विचार हो सकता है किंतु अध्यापकों में जो समाज के गैरदलित वर्ग से आते हैं, उनका गरीब बच्चों के प्रति सामाजिक प्रतिकार का स्वभाव हमेशा बना रहता है।
अक्सर देखने को मिलता है कि आधिकारिक स्तर पर मिड-डे मील स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर ठोस योजना का अभाव एक बड़ा गतिरोध है।ग्रामीण स्कूलों में मिड-डे मील संचालन के तौर-तरीके भी हमेशा सवालों के घेरे रहते हैं। कहना न होगा कि स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने में ही शिक्षकों का काफी समय व्यर्थ हो जाता है। और बच्चों का ध्यान भी मिड-डे मिल की ओर लगा रहता है। होता क्या है कि ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे समाज के गरीब और निरीह वर्गों के परिवारों से आते हैं। मुझे तो कभी-कभी आशंका होती है कि ग्रामीण स्कूलों में मिड-डे मील संचालन की व्यवस्था बच्चों में शिक्षा के प्रति मोह भंग करने की एक साजिश है।
इसके अलावा पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, पास-फेल की नीति में बदलाव या बाल केंद्रित शिक्षा के बहाने संसाधनों की भरमार के बावजूद यह विचार करना होगा कि कैसे शिक्षा की प्रक्रिया में गाँव और शहर का अंतर कम किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये हर हाल में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। लेकिन इस दिशा में न तो जनप्रतिनिधि पर्याप्त रुचि दिखाते हैं और न ही शिक्षा विभाग के अधिकारी। सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएँ देने के प्रावधानों के बावजूद धरातल पर स्थिति में बहुत सुधार नज़र नहीं आते।
नई एकीकृत शिक्षा योजना : केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2018 में नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाई गई थी। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित हैं। इस योजना के लिये 75 हज़ार करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं। इस योजना का लक्ष्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना तथा पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिये राज्यों की मदद करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास ज़ोर दिया गया है।
गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता के अंतर को कम करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता औरसमग्रता सुनिश्चित करना, स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिये राज्यों की मदद करना, राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं तथा ज़िला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना नई एकीकृत शिक्षा योजना के योजना के प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं।
योजना के प्रमुख लाभ : शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण : पहली बार स्कूली शिक्षा के लिये उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश संपूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं को सशक्त बनाना, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम के ज़रिये शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, विद्यालयों को स्वच्छ बनाए रखने के लिये स्वच्छता गतिविधियों की विशेष व्यवस्था करना इस नई एकीकृत शिक्षा योजना के मुख्य के लाभ बताए जाते हैं।
सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारने के चलते ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिये कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन और स्कूलों में कौशल विकास पर ज़ोर देना और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉकों, चरमपंथ प्रभावित राज्यों, विशेष ध्यान देने वाले राज्यों/ज़िलों और सीमावर्ती इलाकों तथा विकास की आकांक्षा वाले 115 ज़िलों को प्राथमिकता देना इस योजना का प्रमुख उद्देशय बताया गया है। ( स्रोत: ASER रिपोर्ट 2018 तथा PIB से मिली जानकारी पर आधारित)
बजट 2024: पिछले 10 साल में मोदी सरकार के एजुकेशन बजट में क्या-क्या बदला? यह भी जानना बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है 2024 के अंतरिम बजट में लोगों को ज्यादा बड़े ऐलानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, पिछले दो वित्त वर्ष में शिक्षा, कौशल विकास आदि के आवंटन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगले साल का अंतरिम बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 10वां बजट होगा। हम आपको यहां पिछले दशक के दौरान बजट में शिक्षा से जुड़े किए गए अहम प्रावधानों के बारे में जानकारी पेश कर रहे हैं।2023 के बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपये का आवंटन मिला और इसमें 13 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई।
साल 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के केन्द्र में दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इसमें 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए थे। यह आवंटन सालाना आधार पर 5% ज्यादा था। इसके अलावा, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश लाने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) को लागू करने पर फोकस किया गया था। मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया गया था, जिसमें शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके विपरीत Union Budget 2021-22: 2021 का बजट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो एजुकेशन सेक्टर में पिछले साल के वास्तविक खर्च से 2।1% ज्यादा था। 2021 के बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए स्कूलों और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना के जरिए स्कूली और उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने का ऐलान किया गया था। इस बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 54,874 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह आवंटन वित्त वर्ष 2021 के वास्तविक खर्च से 2।2% ज्यादा था। उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्त वर्ष के वास्तविक खर्च से 1।9% ज्यादा (38,351 करोड़) का आवंटन किया गया। जो 2024 के बजट से ज्यादा है।
2022 के बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1।04 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जोकि 2021-22 के संशोधित खर्च के मुकाबले 18।5% अधिक था। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए 63,449।37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमानों से 22।1% ज्यादा था। उच्च शिक्षा का बजट 40,828 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमानों से 13।3% ज्यादा था। बजट में मॉडल स्कूलों, शिक्षकों की ट्रेनिंग और कुछ खास संस्थानों को स्कॉलरशिप के आवंटन पर जोर दिया गया था। वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को 13% की बढ़ोत्तरी के साथ 1,12,899 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। यह वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार के कुल अनुमानित खर्च का 2।9% था। इस बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए बड़ी रकम (37,453 करोड़ रुपये) आवंटित की गई। बजट में एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान भी किया गया था। इस साल स्कूली शिक्षा के लिए 68,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित अनुमानों से 16।5% ज्यादा है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के लिए 44,095 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 8% ज्यादा है।
पिछले सालों में देशभर में बंद हो गए 20 हजार से अधिक स्कूल, शिक्षकों की संख्या में भी आई गिरावट भारत में स्कूली शिक्षा के लिये एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई-प्लस) की 2021-22 की बृहस्पतिवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2021-22 में स्कूलों की कुल संख्या 14।89 लाख है जबकि 2020-21 में इनकी संख्या 15।09 लाख थी। शिक्षा मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि देशभर में 2020-21 के दौरान 20,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए, जबकि शिक्षकों की संख्या में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1।95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिये एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई-प्लस) की 2021-22 की बृहस्पतिवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2021-22 में स्कूलों की कुल संख्या 14।89 लाख है जबकि 2020-21 में इनकी संख्या 15।09 लाख थी। स्कूलों की संख्या में गिरावट मुख्य रूप से निजी और अन्य प्रबंधन के तहत आने वाले विद्यालयों के बंद होने के कोरोना जैसी घटनाओं के साथ-साथ और कई कारण बताए गए किंतु देखने की बात है कि स्कूलों की यह दुर्दशा केवल ग्रामीण इलाकों में क्यूँ देखी गई है। इतना ही नहीं शासकीय उदासीनता के कारण अनेक स्थानों पर बंद होते सरकारी स्कूल चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में स्कूल शिक्षा के संदर्भ में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है या फिर उन्हें दूसरे स्कूलों में समायोजित किया गया है जो वाकई चिंताजनक है। लेकिन बीते कुछ वर्षो में सरकारी स्कूलों की संख्या में हो रही कमी चिंता का विषय है। और 2020-21 में बंद किए जाने के कारण लगभग सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी हुई है, जबकि इसके विपरीत निजी स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह बात स्कूल शिक्षा विभाग की इकाई यूनाइटेड डिस्टिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस (यूडीआइएसई प्लस) 2020-21 की रिपोर्ट में सामने आई है। हालांकि यह यूडीआइएसई के प्राथमिक गणना के आंकड़े हैं, लेकिन अंतिम आंकड़ों में भी कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। लिहाजा इस रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में 10,83,678 थी, जो साल 2019-20 में घटकर 10,32,570 रह गई है। यानी इस सत्र के दौरान देशभर में 51,108 सरकारी स्कूल बंद या फिर उनका किसी अन्य स्कूल में समायोजन कर दिया गया। वहीं यह संख्या 2020-21 में घटकर 10,32,049 रह गई है।
वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देशभर में प्राइवेट स्कूलों की संख्या सत्र 2018-19 में 3,25,760 हुआ करती थी, जो 2019-20 में बढ़कर 3,37,499 हो गई है। इस तरह केवल इन दो सत्रों में प्राइवेट स्कूल की संख्या में खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, वहीं सत्र 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 3,40,753 तक पहुंच गई। हालांकि इसके विपरीत चंद राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या में वृद्धि भी देखी गई। इस दौरान बंगाल में सरकारी स्कूलों की संख्या 82,876 से बढ़कर 83,379 हो गई, जबकि बिहार में 72,590 से बढ़कर 75,555 हो गई। निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस के कारण गरीब और पिछड़ा तबका हमेशा से शिक्षा से वंचित रहा है। ऐसे में उनके लिए सरकारी स्कूल की नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था ही शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र सहारा रहा है।
दरअसल, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था के प्रति शासकीय उदासीनता के चलते अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वहीं नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में सरकारों की विफलता और गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की नियुक्ति ने शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित किया, जिससे माता-पिता निजी स्कूलों की ओर देखने के लिए मजबूर हो गए। फिर सरकारी स्कूलों में कम एनरोलमेंट होने के कारण इन स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों के साथ विलय करके बंद करने का बहाना ढूंढ लिया गया है।
वर्ष 2016 में सरकारी सचिवों के एक समूह ने कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करके पास के स्कूलों में विलय की सिफारिश की थी। नीति आयोग ने अगले वर्ष 2017 में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि यूडीआईएसइ प्लस की इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट के कारणों की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन तर्क यह दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर कक्षा में एक शिक्षक होना जरूरी है। लेकिन यदि प्राथमिक विद्यालय में सभी पांच कक्षाओं में 50 से कम बच्चे हैं, और वहां पांच टीचर कार्यरत हैं, तो सरकार के लिए ऐसे स्कूल का समर्थन करना बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए इन्हें बंद करके पास के स्कूल में समायोजित कर दिया जाना चाहिए। परंतु यहां बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए गए हैं और अगर वहां स्कूल बंद करके अन्यत्र समायोजित किया गया है, तो यदि वह स्कूल अधिक दूर है, लिहाजा अधिकांश बच्चे समायोजित हुए विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी शिक्षा वहीं पर आकर थम जाती है।
समग्रता में देखा जाए तो बात यह भी है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब व पिछड़े तबके के विद्यार्थी निशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल के बाद कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के नामांकन में रिकार्ड वृद्धि हुई है। वहीं एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक अब भी देशभर में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 60 लाख से अधिकहै। ऐसे में सरकारी स्कूल बंद करने का निर्णय एक बड़े वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा की पहुंच से दूर करने वाला कदम है। ऐसे स्कूलों को बंद करने के बजाय वहां बजट बढ़ाकर सरकारी स्तर पर सारी सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस स्कूल की तरफ आकर्षित हो सकें। कई दफा यह देखने में आया है कि स्कूल में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने पर वहां नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। शिक्षा का अधिकार कानून प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, अब अगर इस तरह सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे तो एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इस पर विचार करना होगा।
इस नई शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में नए-नए चीजों को सीखने के प्रति रुचि जगाना है। ताकि बच्चे जीवन में अपनी योग्यताओं के बलबूते एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके अतिरिक्त अपने मातृभाषा को बढ़ावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य हैं। जैसे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना और इन कक्षाओं के बच्चों को गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं इन पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बच्चो को टेक्निकल ज्ञान भी दिए जाएंगे। बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जिससे वे भी चाइना के बच्चों की तरह ही छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और ऐप बनाना सीख पाएंगे। आगे के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को अंतिम स्तर में रखा जाएगा, जिसके दौरान बच्चे अपने मनपसंद विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। इस तरीके से नई शिक्षा नीति के माध्यम से न केवल बालकों के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा बल्कि बच्चों के शिक्षण के तरीके में भी सुधार होगा। यहाँ सोचने बात यह भी है कि अपने घर के बजाए दूसरे के घरों में झाँककर सीमित संसाधनों के चलते नीतियाँ बनना कितना सार्थक और व्यावहारिक होगा।
2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में एक ‘नवीन शिक्षा नीति’ बनाने का विषय था। अत: सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार (मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार) द्वारा ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून, 2017 में इसर (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 2019 में ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ के लिये जनता से सलाह माँगना प्रारम्भ किया और मई, 2019 में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ का मसौदा आया। 29,जुलाई-2020 को केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ (National Education Policy- 2020) को मंज़ूरी दी। ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ पुरानी ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, वर्ष 1968 और 1986 [National Policy of Education (NPE), 2020] के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति बनी। जिसमे ‘मानव संसाधन विभाग’ अब ‘शिक्षा विभाग’ में बदल गया।
हर शिक्षा नीति अपने विजन और आकांक्षाओं में अच्छी ही थी, लेकिन उसके धरातल पर उतरने में जमीन आसमान का फर्क रहा है। क्या यह शिक्षानीति भी समूचे समाज की आकांक्षाओं, आग्रहों और सोच को संतुष्ट कर पाएगी, क्योंकि व्यावहारिक जरूरतें कुछ और हैं और शिक्षा नीति अपने ढंग से चीजों को देखती है। तो क्या स्वतंत्र भारत की यह तीसरी ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ नई सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी? शिक्षा नीति का महत्त्वपूर्ण बिन्दु प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना है। किन्तु बीते दशक में जिस तरह से शिक्षा में निजीकरण और अर्थ व्यवस्था के कारपोरेटीकरण ने भारतीय भाषाओं की शिक्षा के आग्रह को अंगरेजी शिक्षा की जरूरत और जुनून ने लगभग दफन किया है, वह इसमें सबसे बड़ी बाधा है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में मदरसों को छोड़कर क्या अन्य अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में बहुसंख्यक विधार्थियों के प्रवेश पर कोई रोक या नियम बनेगें इसमें कोई चर्चा नहीं है। फिर मातृभाषा का क्या होगा?
त्रिभाषा फार्मूले का क्या होगा? तामिलनाडु इसके लिये तैयार नहीं। वह दो ही भाषा अंग्रेजी और तमिल पढ़ाना चाहता है। ऐसे ही कुछ और राज्यों की ओर से विषय आयेंगे। छठी के पूर्व बच्चे को क्रियेटिव बनाया जायेगा तथा कक्षा छह के बाद वोकेशनल। क्या यह सम्भव है और छठी कक्षा के विद्यार्थी को क्या यह बौद्धिक सामर्थ्य रहेगा? क्या ग्रामीण विद्यालयों के कक्षा छह के विद्यार्थियों को अपरेंटिस अवसर देने के लिए संस्थान और उद्योगिक संस्थाएं हैं?क्या प्रत्येक विद्यालय में सभी मनचाहे विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे? क्या प्राइवेट और शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की अमीर- गरीब की खाई खत्म हो पाएगी? क्या निजीकरण के इस दौर में माता-पिता बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाने को तैयार होंगे? ऐसे प्रश्नों के समाधान तथा अपेक्षित परिणामों हेतु कुछ और नीतियाँ बनानी होंगी।ऐसा लगता है। इसके लिए यह जरूरी है कि ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ में शिक्षा अंतिम छात्र तक पहुँचे, यह समानता और गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो और उत्तरदायित्व का विकास करे। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा को अलग-अलग करके देखना होगा।
नई शिक्षा नीति में समाज के कमजोर तबके को पीछे धकेलने का खतरा साफ झलकता है। शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली कस्तूरी रंगन समिति ने 2019 में नई शिक्षा नीति के चौथे ड्राफ्ट में नई शिक्षा नीति में समाज को पीछे धकेलने का खतरा है। इसका एक पहलू यह भी है कि जिन बच्चों के परिजन शिक्षित नहीं रहे हैं, उनके ही बच्चे ऐसे केंद्रों में जाकर कम आय वर्ग और जातिगत पेशों में ही फंसे रह जाएंगे।
1990 के दशक में आर्थिक और राजनीतिक नीतियां समाज के संकटों का सामना करने में असफल रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि जटिल और अप्रत्याशित समस्याओं के इस दौर में नई पीढ़ी को एक वैश्विक समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जीवन-यापन करने के लिए सक्षम बनाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि कब लाइब्रेरी में गांधी, टैगोर और विवेकानंद को पढ़ने की जगह कुंजियों ने ले ली है। छात्र क्लास से गायब हो गए हैं और कोचिंग संस्थानों में सिर धुन रहे हैं। उस पर भी कोटा जैसा शहर कोचिंग का नहीं सुसाइड का सेंटर बनने लगा है तो इस पर सोचना चाहिए। क्या ऐसी शिक्षा की कल्पना की जा सकी है जिसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना न हो। युवाओं के लिए ‘नाकामी’ को जज्ब कर पाना आज मुश्किल हो गया है।
0000
....तो यह है हमारे आज के लोकतंत्र की नई हकीकत
जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि कुछ ऐसा भी समय होता है, जब लोग वास्तविक सोच से कहीं अधिक दूर अथवा वर्तमान से अनजान होने का दावा करने लगते हैं। 13 दिसंबर 2023 कोकुछ प्रदर्शनकारी गैस-केन (कनस्तर) लेकर संसद में घुस गए। वे सदन के पटल पर कूद पड़े और उन्होंने अपने कनस्तरों से रंगीन गैस बाहर निकाल दी। संयोंग की बात है कि उनमें जहरीली गैस या आंसू गैस जैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि कुछ सांसदों को डर था। गैस भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी। प्रदर्शनकारी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे न कि सदन के सदस्यों की हत्या करने की। यह तथ्य है कि प्रदर्शनकारी 2001 में संसद पर हुए घातक हमले की बरसी पर इतनी आसानी से संसदीय सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल रहे। 2001 के हमले में नौ लोग मारे गए (पांच आतंकवादियों को छोड़कर) थे। यह चौंकाने वाली और भयावह घटना थी। लेकिन इस बार रहस्य तब और गहरा गया जब यह पता चला कि मैसूर से भारतोय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद प्रताप सिम्हा ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने की इजाजत देने वाले पास दिलवाए थे।
आपको क्या लगता है कि सरकार और संसद चलाने वाले संवैधानिक अधिकारियों (राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष) ने सुरक्षा के इस गंभीर उल्लंघन पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या हमलावरों को पास (PASS) देने वाले सांसद को निलंबित किया गया? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देकर यह बताने को कहा गया कि ऐसा हमला कैसे हो सकता है।किंतु इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला , उलटे इस वाकये का ठीकड़ा भी विपक्ष के सिर मथ दिया गया।
उपरोक्त मसले में किसी पर भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई यानी कि यह मसला एक साधारण घटना के जैसे धीरे-धीरे शांत होता चला गया। किसी का कुछ भी नहीं हुआ। अबतक बीजेपी सांसद को भी निलंबित नहीं किया गया है। शाह ने दोनों सदनों में कोई बयान नहीं दिया। इसके बजाय, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दियागया। सांसदों ने गुस्से में प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री से हमले पर बयान देने की मांग की तो कोई जवाब न देकरउन्हें ही सदन से बाहर कर दिया गया। और लोकसभा में विपक्ष की ताकत दो-तिहाई कम करने के साथ, सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक पास कर लिए और कहा गया कि ये विधेयक देश में आपराधिक कानून में सुधार लाएंगे।
इस तरह के अवास्तविक कथानक पर कौन विश्वास करेगा? पीठासीन अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए, कई निलंबित सांसद सदन के वेल में पहुंच गए और संसद के कामकाज में बाधा डाली। यह संसद की गरिमा का अपमान हो सकता है। लेकिन यह भी, चाहे अच्छा हो या बुरा, भारत में असामान्य नहीं है। सांसद अक्सर सदन के वेल में आ जाते हैं। सामान्य प्रतिक्रिया यह है कि कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और उम्मीद की जाए कि जब सदन की बैठक दोबारा होगी तो व्यवस्था बहाल हो जाएगी। विदित हो केवल बेहद खराब व्यवहार के मामलों में विपक्षा के सांसदों को ही निलंबित किया जाता है। भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी दो-तिहाई विपक्ष को निलंबित नहीं किया गया था। तो यह है हमारे आज के लोकतंत्र की नई हकीकत।
इसके अलावा, संसद को बाधित करने के बारे में आत्मतुष्ट होने के लिए बीजेपी आवश्यक रूप से सर्वोत्तम स्थिति में नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के दौरान, यह बीजेपी ही थी जो नियमित रूप से संसद को बाधित करतो थी। और यह कोई अजीब दुष्ट तत्वों का काम नहीं था। लोकसभा में बीजेपी की तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से कम कोई व्यक्ति नहीं, जिन्होंने 2012 में घोषणा की थी कि “संसद को चलने न देना भी किसी अन्य रूप की तरह लोकतंत्र का एक रूप है।” और राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता अरुण जेटली के इस बयान के बारे में क्या ख़याल है: “कई बार, संसद का उपयोग मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने के लिए किया जाता है और ऐसी स्थितियों में संसद में बाधा डालना लोकतंत्र के पक्ष में है। इसलिए, संसदीय कार्य में बाधा डालना अलोकतांत्रिक नहीं है।”
जेटली ने संसद में बाधा डालने और बाधित करने का अधिकार कभी नहीं छोड़ा। एक साल बाद जब उन्होंने देश को बताया था कि संसदीय बाधा लोकतंत्र के पक्ष में है, वह फिर से उसी स्थिति में थे। उन्होंने कहा, “ऐसे मौके आते हैं जब संसद में रुकावट से देश को अधिक लाभ होता है।” किंतु वर्तमान स्थिति के चलते तो यह लगता है कि सुषमा स्वराज और जेटली गलत थे। हालांकि, बीजेपी उनके बार-बार दिए गए बयानों से इनकार नहीं कर सकते, जो पार्टी की नीति बन गई है। अब वह जो चाहते हैं - वह यह है कि बीजेपी के लिए एक नियम हो और बाकी सभी के लिए दूसरा। दो प्रश्न बाकी हैं।
पहला - सरकार विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित कर रही है? लगता तो ये है कि दोनों पीठासीन अधिकारी औपचारिक रूप से सरकार का हिस्सा नहीं हैं। क्या इसे एक साधारण धटना जानकर भुला दिया जा सकता है। यह प्रश्न भी उठता कि ऐसी घटनाओं सरकार के अलावा कौन रोक सकता है?गए दिनों कुछ राज्यों में हुएविधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का मानना है कि उसे केंद्र की सत्ता में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। उसका मानना है कि विपक्ष कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर अप्रासंगिक है। इसलिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या मानता है या क्या चाहता है। न ही पार्टी खुद को संसद में विपक्ष के प्रति जवाबदेह मानती है। हां, सुरक्षा उल्लंघन हुआ था, ऐसा उसके रवैये से प्रतोत होता है, लेकिन हम इसे स्वयं संभाल लेंगे। स्पष्टीकरण मांगने वाले आप कौन होते हैं? और जब विपक्ष प्रतिक्रिया से परेशान है और इसके बारे में हंगामा कर रहा है, तो बीजेपी ने अपने सांसदों को सदन से बाहर निकालकर उसे चुप करा दिया।
और दूसरा प्रश्न है - क्या कोई सार्वजनिक आक्रोश होगा जो देश के भीतर सरकार की स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा? क्या इस व्यवहार की स्पष्ट मनमानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के आसपास की छवि को कम कर देगी? क्या इससे बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? संसद में सोमवार को 78 विपक्षी सांसदों को आसन की अवमानना तथा अशोभनीय आचरण करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 34 सांसदों को संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। वहीं 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया। यह समिति तोन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। इन सांसदों को नियम 256 के तहत सस्पेंड किया गया है। नियम 256 के तहत सभापति आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य को निलंबित कर सकता है, जो सभापीठ के अधिकार की अपेक्षा करे या जो बार-बार और जानबूझकर राज्य सभा के कार्य में बाधा डालकर राज्य सभा के नियमों का दुरूपयोग करे।संसदीय इतिहास में लोकसभा में सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। जिसके बाद अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था।
हालिया हालात में मोदी के सबसे चतुर राजनेता होने का एक कारण यह है कि उन्होंने इस बात पर काम किया है कि यदि आप अपनी पार्टी को स्थायी चुनाव मोड में रखते हैं, तो आप उन घनी आबादी वाले राज्यों में जनता का समर्थन बनाए रख सकते हैं जो आपका आधार हैं।और फिर, आप लोकतंत्र की संस्थाओं के साथ जो चाहें वह कर सकते हैं। आख़िरकार, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है, है ना? वीर सांघवी (प्रिंट और टेलीविजन) पत्रकार ने इस प्रकार के विचार स्पष्ट किए हैं।
2024 : सर्व विदित है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। अचानक चुनाव रद्द कर दिया गया। जो शायद एक-दो दिन बाद कराया गया। पूरा मामला क्या है? आखिर कैसे? क्यों क्या कारण था भाजपा के पासनगर निगम पर काबिज भाजपा का इस चुनाव से भागने का? आखिरकार चंढीगढ़ में चुनाव हुए और भाजपा को अल्पमत होते हुए भी चुनाव अधिकारी ने मनमाने ढंग से आप के 8 वोट रद्द करके भाजपा का मेयर बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट मामला पलट दिया और इस तरह ‘आप’ मेयर बन गया। 8 साल में बहुत ऐसे मौके आए जब कई राज्यों मैं भाजपा का बहुमत नहीं था। लेकिन बहुमत न रखते हुए भी जोड़तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में कामयाव रहे।
आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के 75 वर्ष होने पर रजत जयंती अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारां प्रजातंत्र और फल फूलना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि 2014 के बाद जो लोग सत्ता में आए, उनको चुनाव जीतने का और सत्ता में रहने का एक नशा हासिल हुआ। यह चुनाव हारते हैं तो फिर वो सत्ता किसी को मिलने नहीं देते। खुद ही सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते रहे हैं । चाहे कोई गठबंधन हो, विपरीत गठबंधन हो, कोई विचारधारा नहीं, कोई लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई वगैरह। भारतोय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद हैं। किंतु वर्तमान में बीजेपी की अपनी ताकत कुछ गिरती जा रही है। तो बीजेपी का पूरा लक्ष्य रहेगा कि विपक्ष किसी भी तरह से एकजुट न हो पाए अन्यथा बीजेपी के लिए 2024 भारी पड़ेगी। इसका रास्ता क्या है? ये अलोकतांत्रिक तरीका है। अगर ये मान लिया जाए कि यदि 2024 में लोकसभा चुनाव भाजपा बहुमत नहीं आता है तो क्या भाजपा सरकार बनाने के लिए चंडीगढ़ जैसा खेल कर सकती है? उल्लेखनीय है कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जब राष्ट्रपति बीमार पड़ते हैं या राष्ट्रपति कहीं बाहर चले जाते है तो उपराष्ट्रपति उनके अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति किसी न किसी तरह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? लेकिन मोदी जी के नए भारत में कुछ भी हो सकता है।महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बनी जब तक बीजेपी जुगाड़ नहीं कर पायी। क्या जो महाराष्ट्र में हुआ लोकतंत्र का मजाक नहीं है? ऐसे में जो लोग संविधान की लड़ाई लड़्ने का उपक्रम कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से तैयार रहना होगा। सवाल चंडीगढ़ नगर निगम छोटा नहीं? सवाल है सोच का? सवाल है संविधान की धज्जियां उड़ाने का? सवाल है लोकतांत्रिक प्रणाली को रौंदने का? गए डिनो मैं उन परम्पराओं को व लोकतांत्रिक मान्यताओं को बनाए रखने का हर ध्यान रखा जाता था, जो आज नहीं हैं। अटल जी क़े समय मैं अटल जी का सरकार बनाने में केवल एक सांसद की कमी थीं तो प्रमोद महाजन ने अटल जी से कहा कि हम सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अटल जी ने एकदम से मना कर दिया। और कहा कि जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। जनता केआदेश का अपमान नहीं करना है।
जब आपातकाल घोषित हुआ तो प्रेस घर में सब पत्रकारों ने मीटिंग लेकर रोष व्यक्त किया। और निर्णय लिया कि सब अखबार संपादकीय पेज खाली छोड़ेंगे। आपातकाल में तो अधिकार ही नहीं थे। किसी को पता नहीं था कि कितने दिन रहेगा, ये संविधान रहेगा या नहीं? पुलिस का दमन था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? नागैरत लोगो की फौज आ गई। मीडिया घुंघरू बाँध सरकार के दरबार में नाच करने लगी, आज भी वोही काम कर रही है। दुर्भाग्य है कि जो पत्रकारिता सोशल मीडिया के जरिए बच पा रही है।यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया के कुछ लोग अभी भी पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं किंतु आज सरकार यूट्यूब पर दबाव बनाकर उन्हें या तो बंद करवाया जा रहा है या फिर डिमोनेटाइज किया जाने लगा है। बाकी बचे हुए कितने दिन तक बचे रहेंगे, इसके आशंका है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में लोकतंत्र को गर्क में ले जाने का प्रत्येक उपक्रम किया जा रहा है।
नेशनल डेस्क : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि अगर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है, तो कोई भी लोकतंत्र,, सामाजिक न्याय और संविधान को नहीं बचा सकता है। कावेरी डेल्टा जिलों के पार्टी के बूथ-स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद किसे सत्ता पर कब्जा करना चाहिए इसके बजाय सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केंद्र में किसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा कि यदि विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट नहीं हुईं तो संभव है कि ‘अगली बार देश में चुनाव ही न हो’।आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में यह दावा भी किया कि 'जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आय कर विभाग) के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेन्द्र मोदी 2024 में (फिर से) प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित हैं, वह इस देश के राजा रहेंगे। और इस देश की आजादी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, खो जाएगी।' 'जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आय कर विभाग) के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेन्द्र मोदी 2024 में (फिर से) प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित हैं, वह इस देश के राजा रहेंगे। और इस देश की आजादी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, खो जाएगी।' शीर्ष द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश का गठन करने वाले मौलिक विचारों को नुकसान पहुंचाया है और ‘‘हमें आगामी संसदीय चुनावों में इस पर पूर्ण विराम लगाना होगा, अन्यथा केवल तमिलनाडु ही नहीं, कोई भी पूरे भारत को नहीं बचा सकता।'' आप के ही भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर 2024 BJP जीतीतो देश में आगे से नहीं होगा कोई चुनाव। और नरेंद्र मोदी बन जाएंगे ‘नरेंद्र पुतिन'।
दैनिक भास्कर के हवाले से लगभग दो महीने पहले केजरीवाल ने कहा था, ‘ कि पहले लोग कहते थे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन अब ‘INDIA’ गठबंधन पर सबकी नजर बनी हुई है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दिल्ली में पार्टी स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने BJP पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा - भाजपा 2014 और 2019 में ऐतिहासिक वोटों से जीतोथी। अगरवे चाहते तो देश में प्रगति कर सकते थे, मगर फेल हुए। ऐसे में 2024 में होने वाले चुनावों में हमें एक साथ आकर भाजपा को हराना है। उन्होंने विपक्षी दलों और जनता को आगाह करते हुए कहा कि 2024 में BJP को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी।‘
BJP के फैसलों की आलोचना करते हुए केरजीवाल बोले- केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वे फैसले क्यों लिए हैं। 2016 में नोटबंदी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई। लोगों की नौकरियां, व्यवसाय और कारखाने बंद हो गए। BJP सरकार द्वारा लाए गए GST की भी आलोचना की और इसे इतना जटिल बताया कि कोई इसे समझ ही नहीं पाया है। उन्होंने आगे केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा - ये ED और CBI मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। भाजपा ने ED और CBI को कई बड़े बिजनेसमैन तथा विपक्षी दलों के अनेक नेताओं के पीछे लगा दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर व्यक्तियों और व्यापारियों ने अपनी भारतोय नागरिकता छोड़ दी और विदेशी नागरिकता हासिल कर ली। यह बहुत गंभीर मामला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा उन सभी के लिए शरणस्थली है जो किसी भी तरह के गलत काम में शामिल हैं। उन्होंने कहा, "अगर चोरी या उत्पीड़न में शामिल कोई भी व्यक्ति उनकी पार्टी में शामिल होता है, तो कोई भी जांच एजेंसी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करती। गुंडे और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले, सभी उनकी पार्टी में हैं। दिल्ली के CM ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं।
विदित हो कि संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब तक कुल 141 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया सांसदों (लोकसभा-33, राज्यसभा-45) को निलंबित किया गया था।
पिछले कुछेक वर्षों से ये भी देखा गया है कि बीजेपी के अनेक नेता बार-बार हिंदुओं को खतरे में होने की बात को बिना किसी तर्क के जोर शोर से प्रचारित करती रहते हैं। तो क्या आपकी नजरों में भी हिंदू खतरे में हैं? हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था, ना ही कभी रहेगा। आज तक जो शासक थे, अभी 70 साल में तो हिंदू ही थे, और आज भी ज्यादातर हिंदू ही हैं फिर हिंदू खतरे में हैं, यह बयानबाजी कितनी तर्कसंगत है? हाँ! ये जुमला हिंदुओं के वोट हासिल का सार्थक हथियार जरूर हो सकता है। वोटर लोकतंत्र की पक्ष में अपनी भूमिका निभाने के बदले सामप्रदायिकता के पक्ष में बटन दबाते हैं ...किसी भगवान या धर्म के लिए बटन दबाते हैं। तो आप भविष्य के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर रहे हैं,। खैर! यह मानने में कोई शंका नहीं है कि नेता वही करते हैं जो उनकी राजनीति को बनाए रखने में हितकर हो, यह भी किसमाज जिस तरह का होता है, वह उसी तरह का नेता भी चुनता है। तो समाज का भविष्य किस तरह का किस तरह का बनेगा, इसका फैसला आपको करना है किंतु ये काम कतई सहज नहीं है।
यथोक्त के आलोक में, यूँ तो माहिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक अवहेलना, इलेक्ट्रोरल बोंड्स के जरिए बड़े-बड़े उद्योग घरानों से धन उगाही, पीएम केयर फंड के जरिए एकत्र फंड का जनता के सामने हिसाब-किताब न रखना, आर एस एस अर्थात बीजेपी की पैत्रिक संस्था की तर्ज पर समाज में हिंदु-मुसलमान का विद्वेष उत्पन्न करना, सरकारी जाँच एजेंसियों का बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष के विरोध में अनैतिक रूप से प्रयोग करना, चुनाव आयोग को बेदम करना जैसे जाने कितने ही मसले हैं जो बीजेपी सरकार की नीयत की पोल खोलने का काम करते दिख रहे हैं लेकिन इस सब समस्याओं का एक ही लेख में वर्णन करना व्यावाहरिक रूप से संभव नहीं हैं इसलिए इस मसलों पर आगे किन्ही अन्य लेखों में करने का प्रयास किया जाएगा। इस लेख में बस इतना ही।
0000
भला! घुट-घुटकर जीवन यापन करने की बाध्यता शादी ही क्यों हो?
आम धारणा है कि देर से शादी एक ऐसा कारक है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। हालाँकि कुछ लोग देर से शादी करना पसंद करते हैं और कुछ लोगों के पास उपयुक्त उम्र में शादी करने का अवसर नहीं होता है, दोनों को देर से शादी के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जो ज्ञात है उसके विपरीत, देर से विवाह में केवल नुकसान या फायदे शामिल नहीं होते हैं। यह इन दोनों को लोगों के जीवन में जोड़ता है। आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों ही देर से शादी करना पसंद करते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण चाहते हैं। इसके अलावा, यदि ये लोग विश्वविद्यालयों में या मास्टर या पीएचडी के लिए पढ़ते हैं, तो उनकी शादी की उम्र देर से होगी। दूसरी ओर, करियर लक्ष्य के कारण लोग अपनी शादी में देरी करते हैं, भले ही उनके जीवन में कोई साथी हो। जब वे अपनी शादी की उम्र में देरी करते हैं, तो उन्हें फायदे का सामना करना पड़ सकता…। सबको अपनी स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। शादी नहीं करने से आपको अपनी ज़िन्दगी को अपनी मर्ज़ी से जीने का मौका मिलता है। आप अपने लाइफस्टाइल, करियर और व्यक्तिगत संबंधों को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं।
लड़का हो या लड़की शादी करने सेपहले हर किसी को शादी के मूलभूत लाभ और हानि को जरूर जान लेना चाहिए, नहीं तो बाद में होगा अफसोस...क्योंकि हर किसी की लाइफ में शादी के बाद कुछ आवशयक बदलाव आ जाते हैं। अगर आपकी भी शादी हो गई है तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी दिनचर्या/आपके हालात जैसे शादी के पहले थे, शादी के बाद वैसे नहीं रहे।
आजकलआपजबभी सोशलमीडिया पर जाते होंगे, तो दिखरहा होगा कि आप के दोस्त या पहचानवालों की शादियां हो रही है।वहीं कुछइंगेजमेंटतो कुछहनीमूनके भी फोटो शेयरकररहे हैं।उन्हें देखकरआपके परिवारवालों का भी आप से यही कहना होगा कि 'शादी करलो, नहीं तो उम्र निकलजाएगी'।लड़का हो या लड़की, हरकिसी की लाइफमें शादी के बादकुछदलावआ ही जाते हैं।इसबातको आपने भी महसूसकिया होगा कि जो दोस्तशादी से पहले रोजाना मिला करते थे, वे आजकममिलने लगे हैं।इसका कारणहै कि उनपरपारिवारिकजिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिसकारणवे अपने लिएकमसमयनिकालपाते हैं। अगर आप भी शादी करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अधोलिखित तथ्यों को जान लेना,मेरी दृष्टि में जरूरी जान पड़ती हैं
शादी की कहानी कोई नई थोड़ी है ...ना ही कोई नया रास्ता है ...चाहे-अनचाहे सभी इस रास्ते से गुज़रते हैं। ... किन्तु कमाल का सच ये है कि इस रास्ते में आई बाधाओं के क़िस्से चुटकलों के ज़रिए तो सुनने/पढ़ने को ख़ूब मिलते हैं किन्तु इस सच को कोई भी पति अथवा पत्नी व्यक्तिश: स्वीकार नहीं करता। क्यों ...? लोक-लज्जा का डर, पुरुष को पुरुषत्व का डर, पत्नी को स्त्रीत्व का डर ...डर दोनों के दिमाग़ में ही बना रहता है ...इसलिए पति व पत्नी दोनों आपस में तो तमाम ज़िन्दगी झगड़ते रहते हैं किन्तु इस सच को सार्वजनिक करने से हमेशा कतराते हैं ...यही भावना कष्टकारी है। ... महिला सशक्तिकरण का नाटक मुझे तो बड़ा ही बचकाना लगता है। मुझे तो महिला के मुक़ाबले कोई और सशक्त नहीं लगता ...महिला अपनी पर उतर आए तो क्या नहीं कर सकती? ...बेटा-बेटी के अलावा पति की क्या मजाल कि उसके सामने कोई भी बोल पाए ...।
दोस्तो एक समय था कि जब शादी के मामले में लड़के और लड़की की इसके अलावा कोई भूमिका नहीं होती थी कि वो दोनों आँख और नाक ही नहीं अपितु साँस बन्द करके माँ-बाप की इच्छा के अनुसार शादी के लिए तैयार हो जाएँ। इसके पीछे समाज का अशिक्षित होना भी माना जा सकता है। किन्तु जैसे –जैसे समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ तो नूतन समाज के विचार पुरातन विचारों से टकराने लगेऔरअब शादी के मामले में लड़के और लड़की की इच्छाएँ भी पुरातन संस्कृति के आड़े आने लगीं हैं। फलतः पिछले कुछ दशकों से यह देखने को मिला है कि शादी के परम्परागत पहलुओं के इतर शादी से पहले लड़के और लड़की को देखने का प्रचलन ज़ोरों पर है। पहले यह उपक्रम केवल शहरों-नगरों तक ही सीमित था किन्तु आजकल तो यह उपक्रम दूरस्थ गाँवों तक भी पहुँच गया है। झुग्गी–झोंपड़ीयाँ तक इस प्रथा की ज़द में आ गई हैं। इसमे कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ एक सवाल का उठना बड़ा ही जायज़ लगता है कि पंद्रह-बीस मिनट की मुलाक़ात में लड़का, लड़की और लड़की, लड़के के विषय में क्या और कितना जान पाते होंगे। सिवाय इसके कि एक दूसरा, एक दूसरे की चमड़ी भर को ही देख ले। दोनों एक दूसरे की नक़ली हँसी को किसी न किसी हिचकिचाहट के साथ दबे मन से स्वीकार कर लें। इस सबका कोई साक्षी तो होता नहीं है। अगर हो भी तो उनका इस प्रक्रिया में कुछ भी कहने का कोई अधिकार यदि होता है। वह केवल लड़के और लड़की को केवल शादी के लिए तैयार करना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता।
कहना अतिशयोक्ति न होगा कि दो अनजान चेहरों के बीच पहली बैठक में बात शुरू करने में कुछ न कुछ तो हिचकिचाहट होती ही है। अमूनन देखा गया है कि शादी के बन्धन में बन्धने जा रहे जोड़े को प्राय: दूसरी मुलाक़ात का मौक़ा दिया ही नहीं जाता। धार्मिक/सामाजिक बाधाएँ इस सबके सामने खड़ी कर दी जाती हैं। हमको इस धार्मिक उपक्रम ने इस हद तक कमज़ोर और क़ायल बना दिया है कि हम सारा समय लड़के और लड़की की कुंडलियाँ मिलाने में गवाँ देते हैं। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि शादी की पुरातन रीति आज की रीति से भिन्न है? हाँ! इतना अंतर अवश्य है कि पहले समय में लड़के और लड़की का मिलान करने में दोनों ही पक्षों के माता-पिता की सीधी जवाबदारी होती थी और आजकज इस जवाबदारी का एक बड़ा हिस्सा लड़के और लड़की पर डाल दिया जाता है, नूतन संस्कृति के चलते माँ-बाप की ये मजबूरी भी है। वह इसलिए कि आजकल के पढ़े-लिखे बच्चों के माता-पिता इसलिए असहाय हैं कि वो बच्चों की स्वीकृति के बिना ‘हाँ’ या ‘ना’ कहने की स्थिति में नहीं होते। दूसरे, बच्चों की शिक्षा का स्तर और कामयाबी के चलते माँ-बाप की मर्ज़ी के कोई मायने नहीं रह गए हैं। और हों भी क्यों? लड़का और लड़की को कामयाब होने के बाद भी अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि नहीं?
व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो यह क़तई सच है कि प्रथम दृष्टि में, आजकल लड़के और लड़की को शादी से पूर्व मिलने का मौक़ा तो अवश्य दिया जाता है किन्तु उसके बाद उन्हें फोन पर भी बातचीत करने का मौक़ा न दिए जाने तक की क़वायद होती है। यह बात अलग है कि आज के तकनीकी युग में लड़का–लड़की चोरी-छिपे फोन, वाटसेप, इंटरनेट या फिर फ़ेसबुक के ज़रिए बराबर बात करते रहते हैं। किन्तु फोन, वाटसेप, इंटरनेट या फिर फ़ेसबुक के ज़रिए बात करने का वो अर्थ तो नहीं हो सकता जो साक्षात् बात करने में होता है। क्योंकि फोन, वाटसेप, इंटरनेट या फिर फ़ेसबुक के ज़रिए बात करने में बॉडी-लेंगुएज का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता जबकि इसके उलट साक्षात् मुलाक़ात में बॉडी-लेंगुएज बहुत कुछ कह जाती है। किन्तु हम बच्चों को शादी से पूर्व एक से ज़्यादा बार मिलने का मौक़ा ही नहीं देते। और तो और बच्चों के माता-पिता ही दोबारा ऐसा कोई मौक़ा लेने का प्रयास करते हैं। बस! घड़ी-भर का मिलना पूरे जीवन का बन्धन बना दिया जाता है। यह कहाँ तक उचित है? सच तो ये है कि जीवन का यह एक ऐसा अकेला सौदा है जो एक-दो दिन की मुलाक़ात में ही तय मान लिया जाता है जबकि एक टीवी या फ़्रिज जैसी दैनिक उपयोग की चीज़ें ख़रीदने की क़वायद में सप्ताह, हफ़्ता ही नहीं, यहाँ तक की कई-कई महीने तक लग जाते हैं।... कौन सी कम्पनी का लें? इसकी क्या और कितने दिनों की गारंटी है? ...इसका लुक औरों के मुक़ाबले कैसा है? ...न जाने क्या-क्या ...न जाने कितने मित्रों से इसकी जानकारी हासिल की जाती है ...इतना ही नहीं, सब्ज़ी तक दस दुकानों की ख़ाक छानने के बाद भाव-मोल करने के बाद ही ख़रीदी जाती है।... किन्तु लड़का-लड़की के बीच जीवन-भर का रिश्ता बनाने में जान-पहचान के बजाय बच्चों की शिक्षा के स्तर और उनकी आमदनी के विषय में ही ज़्यादा सोचा जाता है ... और कुछ नहीं। लगता है कि यही प्रक्रिया आजकल के रिश्तों में टूटन का कारण ख़ास कारण है ...बच्चों की कमाई इसका कारण है, एक दूसरा एक दूसरे की कमाई पर हक़ जताने की ज़िद में हमेशा उलझे रहते हैं । … लड़का और लड़की के घर वाले भी इस क़वायद में कम भूमिका नहीं निभाते ।
लड़का और लड़के के घर वाले लड़की की कमाई को हर-हाल हथियाने की कोशिश में लग रहते हैं, और लड़की अपनी कमाई को लड़के के नाम क्यूँ करदे, इसी उलझन में फँसी रहती है ...पड़े भी क्यूँ न? जो लड़की अपने माँ-बाप के घर को छोड़कर लड़के के साथ उसके घर में रहने के लिए बाध्य होती है तो क्या वह अपनी कमाई से ससुराल वालों को पालने के लिए बाध्य है? हाँ! मान-सम्मान अता करने की बात अलग है। इस जद्दो-जहद के चलते लड़का और लड़की के बीच मतभेद हो न हो, घर वाले दोनों के बीच में दीवार खड़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। केवल माँ-बाप ही लड़का और लड़की के बीच की दीवार नहीं बनते, अपितु अनेक बार लड़का और लड़की भी अपने बीच दीवार खड़ा करने में पीछे नहीं रहते। इसी कश-म-कश के चलते, यह देखा गया है कि शादी हो जाने के बाद पति-पत्नी एक दूसरे को निभाने, या यूँ कहूँ कि पति-पत्नी के सामने इस रिश्ते को ढोने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं रह जाता।
जहाँ तक कुंडलियों के मिलान का सवाल है, यह एक ढोंग है जो सदियों से होता आ रहा है और पता नहीं भविष्य इस परिपाटी को कब तक ढोने को बाध्य होगा। क्या कुंडली-मिलान रिश्तों के अमरत्व की कोई गारंटी देता है? क्या कुंडली-मिलान वाले जोड़ों के बीच कभी कोई दरार नहीं पड़ती? क्या उनका जीवन-भर साथ बना रहता है? क्या उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आती? जैसी कुंडली मिलाते समय आशा की जाती है। नहीं, क़तई नहीं। मुझे लगता है कि इसके इतर यह अच्छा होगा कि लड़के और लड़की की चिकित्सीय कुंडली का मिलान भी किया जाय। मेरी इस बात के महत्त्व को खुशवंत सिंह की पुस्तक ‘दिल्ली’ में उद्धृत शेख़ सादी के इस बयान से जाना जा सकता है कि यदि औरत बिस्तर से बेमज़ा उठेगी तो बिना किसी वजह के ही मर्द से बार-बार झगड़ेगी-शेख़ सादी का शेर है – “स्त्री बिस्तर से ग़र उट्ठेगी बेमज़ा, वो मर्द से झगड़ेगी ही रह-रहके बेवजह”। किन्तु ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी पुरुष अथवा औरत मानने वाली नहीं है ...किन्तु ऐसा होता है। रिश्तों की खटास में यह भी एक बड़ा कारण है। इस कारण के बाद आता है ...दौलत का सवाल शृंगारिक संसाधनों की उपलब्धता ...गहनों की अधिकाधिक रमक ...आदि ...आदि। क्या इस ओर कुंडलियाँ मिलाते समय ध्यान दिया जाता है? होता ये है कि इन तमाम कारणों के चलते रिश्तों में खटास आ जाने के कारण या तो बिछोह हो जाता है, या फिर जीवन-भर दम्पति को एक दूसरे को हारे-मन ढोते रहने को बाध्य होना पड़ता है। पति-पत्नी की एक-दूसरे से कमर भिड़ी रहती है ...और इसी कश-म-कश में जीवन तमाम हो जाता है। हाँ! ये बात अलग है कि समाज का एक बड़ा वर्ग, ख़ासकर इस व्यवस्था से पीड़ित पति/पत्नी सरेआम इस बात को स्वीकार करने से कतराते हैं ...क्योंकि उनके सामने समाज में सिर उठाकर जीने का सवाल हमेशा बना रहता है। चेहरे पर चेहरा लगाए रहते हैं । कोई और पहल करे ...तो वो भी करे ...यह मौक़ा कभी आता ही नहीं ...क्योंकि जन-सामान्य उस मुखौटे को उतारने का साहस कर ही नहीं पाते, जो भिरूता हमें विरासत में मिली है। इसी इंतज़ार में अपने मन की बात को मन में दबाए रहते हैं ...क्या नहीं?
नवभारत टाइम्स–(06।02।2015) के ज़रिए एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया कि ज़्यादातर दम्पत्तियों के बीच शादी वाला प्यार शादी होने के पहले दो सालों में ही फुर्र हो जाता है । ...कुछ का तीन सालों बाद ...और जिनका बचा रहता है ...वो किसी न किसी प्रकार की सामाजिक मजबूरी ही होती है। ... ये पहले कभी होता होगा कि पति-पत्नी बुढ़ापे में एक दूसरे के मददगार बने रहते होंगे ...आज समय इतना बदल गया है कि बुढ़ापा आने से पहले ही सारा खेल बिगड़ जाता है। ... पहला बच्चा पैदा होने के साथ ही पत्नी का प्रेम पति के प्रति इतना कम हो जाता है कि पति उसके लिए उधार की चीज़ बन जाता है। ... ऐसा उधार कि जिसे वो उतार तो नहीं सकती ...बस! ढोने भर के लिए बाध्य होती है।
पति की हालत भी कमोवेश यही होती है। यहाँ भी लोक-लाज ही ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए आड़े आती है ...इस विछोह के पीछे एक और जो कारण होता है ...वो है–लगभग 80/90 प्रतिशत पति अपनी पत्नी को ही अपनी जायज़ या नाजायज़ सम्पत्ति का मालिक बनाने का काम करते हैं ...कारण चाहे जो भी हों ...और जब और जैसे ही पत्नी को इस सच का पता चल जाता है, वैसे ही वो पति पर सवार हो जाती है और उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देती है ...उसे अक़्ल जब आती है, तब उसकी अपनी औलाद ख़ासकर बेटा/बेटे अपना असली रूप दिखाने की हालत में आ जाते हैं ...यानी उसके सिर पर एक और चोटी उग आती है ...माने उनकी शादी हो जाती है ।
... अब घर में बहू का दख़ल भी शामिल हो जाता है। ... बेटियाँ तो अपने घर यानी ससुराल चले जाने के बाद भी अपने माँ-बाप के प्रति किसी न किसी प्रकार अपने अपनत्व का निर्वाह करती ही रहती हैं ...बेटों के बारे में क्या कहा जाए ...आप सब इस यर्थाथ से परिचित ही होंगें। ... फिर भी पता नहीं ...प्रत्येक दम्पत्ति के मन में बेटा पैदा करने की जिज्ञासा ज़्यादा ही बनी रहती है ...क्यों?
एक और सार्वभौम सत्य है कि 70 से 80 प्रतिशत औरतों के पति उनसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फलतः पत्नियों को ऐसा पीड़ा भरा असहाय जीवन जीना पड़ता है जिसकी कल्पना करना भी दूभर होता है। एक उपेक्षित जीवन जीना ...और वहशी आँखों की किरकिरी बने रहना ...उसकी नियति हो जाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि विधवा की देखभाल के लिए क्या उसके बच्चे नहीं होते। इस सवाल का उत्तर वो ज़िन्दा लोग अपने गिरेबान में झाँककर खोजें कि उनके स्वयं के बच्चे उनका कितना ध्यान रखते हैं।
दान-दहेज की बात के इतर इस ओर कभी किसी का ध्यान शायद ही गया हो। लगता तो ये है कि इसके कारणों को खोजने का प्रयत्न भी शायद नहीं किया गया जो अत्यंत ही शोचनीय विषय है। मुझे तो लगता है कि समाज में ये जो प्रथा है कि लड़का उम्र के लिहाज़ से लड़की से प्रत्येक हालत में कम से कम पाँच वर्ष बड़ा होना ही चाहिए, इस प्रकार की सारी विपदाओं के लिए ज़िम्मेदार है। शायद आप भी इस मत से सहमत होंगे कि उम्र के इस अंतर को मिटाने की ख़ासी आवश्यकता है। लड़का-लड़की की उम्र यदि बराबर भी है तो इसमें हानि क्या है? या फिर शादी के एवज़ पारस्परिक रिश्तों को क्यूँ न स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए ...विछोह तो आगे ...पीछे होना तय है ही ...भला घुट-घुटकर जीवन यापन करने की बाध्यता शादी ही क्यों हो?
इस सबसे इतर, नवभारत टाइम्स दिनांक 23/05/2015 के माध्यम से अनीता मिश्रा कहती हैं कि शादी सिर्फ़ आर्थिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने भारत का माध्यम नहीं है। लड़कियों को ऐसे जीवन साथी की तलाश रहती है जो उन्हें समझे। उनकी भावनात्मक ज़रूरतें भी उनके साथी के महत्त्वपूर्ण हों। वो फ़िल्म ‘पीकू’ में एक संवाद का हवाला देती हैं ...“शादी बिना मक़सद के नहीं होनी चाहिए।” फ़िल्म की नायिका का पिता भी पारम्परिक पिताओं से हटकर है। वह कहता है, “मेरी बेटी इकनामिकली, इमोशनली और सेक्सुअली इंडिपेंडेंट है, उसे शादी करने की क्या ज़रूरत?” मैं समझता हूँ कि यह तर्क अपने आप में ही इमोशनल है। फिर भी यह आम जन का ध्यान तो आकर्षित करता ही है।
अनीता जी आगे लिखती हैं कि यहाँ एक सवाल यह भी है कि विवाह संस्था को नकारने का क़दम स्त्रियाँ ही क्यों उठाना चाहती है? शायद इसके लिए हमारा पितृसत्तात्मक समाज दोषी है। वर्तमान ढाँचे में विवाह के बाद स्त्री की हैसियत एक शोषित की हो जाती है। आत्मनिर्भर स्त्री के भी सारे निर्णय उसका पेशंट या उसके परिवार वाले ही करते हैं। शादी होने के बाद उसका पति मालिक की तरह ही व्यवहार करता है। ऐसे में स्त्री के लिए दफ़्तर की ज़िन्दगी और घरेलू ज़िन्दगी में तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। कहा जा सकता है कि ज़्यादातर स्त्रियों को दफ़्तर में काम करने के बाद भी घर में एक पारम्परिक स्त्री की तरह ख़ुद को साबित करना होता है। किसी भी स्त्री को जब सफलता मिलती है तो यह भी जोड़ दिया जाता है कि उसने करियर के साथ सारे पारवारिक दायित्व कितनी ख़ूबी से निभाए। जबकि पुरुषों की सफलता में सिर्फ़ उनकी उपलब्धियाँ गिनी जाती है। कामकाजी लड़कियों के लिए शादी के बाद इतनी सारी चीज़ों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन विवाहेतर संबंधों में खटास आ जाती है। यहाँ तक की तलाक़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी मिसालें देखकर आज कई लड़कियाँ शादी नहीं करने का निर्णय ले रही हैं। वे अपनी आज़ादी को पूरी तरह जीना चाहती हैं और अपने व्यक्तित्व और सम्पत्ति की मालिक ख़ुद होना चाहती हैं।
यहाँ यह सवाल उठना भी लाज़िमी है कि शादी समाज की एक ज़रूरी व्यवस्था रही है किन्तु आज़ादी चाहने वाली लड़कियाँ शादी को एक बन्धन की तरह देखती हैं। फिर मानव समाज की दृष्टि से एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर विवाह का विकल्प क्या है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बदलते परिवेश में स्त्री शादी का विकल्प ख़ुद खोजे? ज़ाहिर तौर पर अब तक पुरुषों की आर्थिक स्वनिर्भरता और सक्षमता ने केवल उन्हें ही निर्णय लेने का अधिकार दे रखा था। अब अगर महिलाएँ भी इसी हैसियत में पहुँचने के बाद अपनी ज़िन्दगी की दिशा तय करने वाला फ़ैसला ख़ुद लेने लगी हैं तो इसमें ग़लत क्या है? फिर क्यों न आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम महिला को शादी करने, न करने का फ़ैसला ख़ुद लेने दिया जाए?
उपर्युक्त के आलोक में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी के प्रश्न का हल एक लम्बी प्रक्रिया से होकर गुज़रेगा। आनन-फ़ानन में कुछ भी नहीं होने वाला है। किन्तु इस प्रकार की बहसों का जन्म लेना सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति तो प्रदान करता ही है।
0000
राजनीति रोजगार/व्यवसाय का हिस्सा बनती जा रही है
भारतीय राजनीति में विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म यूँही नहीं हुआ, इसका कारण केवल और केवल यह है कि ब्राह्मणवाद के चलते पहले से ही वर्चस्वशाली राजनीतिक पार्टियां अलोकतांत्रिक होती जा रही हैं। अलोकतांत्रिक होती जा रही इन वर्चस्वशाली राजनीतिक पार्टियों के गिरते राजनीतिक आचरण के कारण विभिन्न क्षेत्रीय दलों का न केवल जन्म हुआ अपितु उनमें से कई पार्टियां सत्ता तक भी पहुंचीं। विगत और वर्तमान राजनीतिक फलक इस बात का साक्षी है। आज समय है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने भरोसे चुनाव लड़ने से कतरा रहे है। हो ये रहा है कि छोटे-छोटे विभिन्न दलों को लेकर गठबंधन की राजनीति को बल मिल रहा है। यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो भाजपा के एन डी ए के गठबंधन में कहने तो लगभग 38 राजनीतिक दल शामिल हैं और ज्यादातर ऐसे दल है जिनका न तो कोई विधायक है और न ही सांसद। विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन में अपना-अपना वजूद रखने वाले लगभग 26/27 दल शामिल हैं किंतु इस गठबंधन के सामने जो सवाल मुंह बाए खड़ा है, वो है अपने-अपने वर्चस्व को बनाए रखने का।
किंतु पिछले छह/सात दशक में पहली बार राजनीतिक अस्मिता खतरे से बाहर नजर नहीं आ रही। राजनीतिक अस्मिता ही नहीं, जातीय अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता, परिवार की या कोई और कुछ भी तो सुरक्षित नहीं रहा है। आज के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर न केवल अस्मिता की राजनीति को धता बता ‘आकांक्षा’की राजनीति को खड़ा करने का सफल प्रयास किया है, अपितु राजनीतिक अस्मिता/राज-धर्म को रसातल में पहुँचा दिया है। इसका अफसोस गए समय में तो नहीं हुआ था किन्तु भाजपा का ऐसा आचरण आज साफ तौर पर देखा जा सकता है।सत्ता पक्ष ने राजनीतिक अस्मिता/राज-धर्म को किनारे करके लोकशाही में तानाशाही में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।आगे आने वाले दिनों में मोदी के चहेतों को इस सत्य का एहसास जरूर होगा, इसमें दो राय नहीं।
दरअसल, पिछले वर्षों में भाजपा की प्रतिष्ठा का ग्राफ इतना गिर चुका है कि गए दिनों में भाजपा कै शासन में हुए राज्यों के चुनावों में भाजपा की जो फज़ीती हुई है, इसके चलते भाजपा और इसके समर्थक समर्थक दलों और पैत्रिक संस्थाआर आर एस को यह तो सोचना ही होगा कि लोकसभा के चुनावों में भाजपा के हक में हुआ बदलाव महज एक हीबार की बात है या फिर स्थाई। गौर तलब है ऐसे परिवर्तन राजनीति में ज्यादा दूर तक का सफर तय नहीं कर पाते। वही हालत आज भाजपा की है। भाजपा की पैत्रिक संस्था की असल चिंता यह है कि यदि 2024 के आम चुनावों में भाजपा सरकार नहीं बना पाती है तो उसके सामाजिक/धार्मिक सभी एजेंडे कहीं दरक न जाएं। इसलिए आर एस एस भाजपा के समर्थन में खुलकर आगे आ गई है। और समाज के हाशियाकृत तबकों/जातियों से सीधे संपर्क साधने की भूमिका में आ गई है।
यथोक्त के आलोक में यह स्मरण रखने की जरूरत है कि आजकल भाजपा के अनेक नेता कोविंद जी के आवास पर निरंतर दौरा करने पर लगे हुए हैं। विदित हो कि 4 जून 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तीन जून को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव कानपुर देहात के परौंख गांव पहुंचे। इस मौक़े पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पहली बार अपने पैतृक गाँव पहुँचे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति कोविंद प्रोटोकॉल तोड़तेहुए ख़ुद हेलीपैड तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि राष्ट्रपति कोविंद की इस गर्मजोशी ने उन्हें 'हैरान' कर दिया और वो 'शर्मिंदगी' महसूस कर रहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मोदी जी ने राम कोविंद जी के राष्ट्रपति हुए कभी भी वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान राम कोविंद जी ने मोदी जी को दिया। इस प्रकार मोदी जी द्वारा कोविंद जी की प्रशंसा करना महज एक राजनीतिक कारण है, मनोभाव का नहीं।
प्रधानमंत्री ने परौंख की एक सभा में कहा, “ ये कहना कि परौंख की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं, उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है और मैं आज देख रहा था कि एक ओर संविधान और दूसरी तरफ़ संस्कार। और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकलकर के मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर मुझे रिसीव करने आए। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। उनके पद की एक गरिमा है, एक वरिष्ठता है।" मोदी जी के इस कथन का क्या आशय है। क्या इस कथन में किसी जमीनी सोच का प्रमाण मिलता है। शायद नहीं, क्योंकि यह कथन केवल और केवल एक राजनीतिक कथन है। यह एक औपचारिकता भर है। पी एम की इस दौरे का मकसद केवल और केवल कोली समाज की मत बैंक पर नजर है। कोली समाज को मोदी जी की कोविंद जी के यहाँ के दौरे को समाज के प्रति हितों के हक में मानने का गुनाह न करे, तो भला।
12 NOV 2023:ये भी कि प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द से भेंट कर उन्हें सपरिवार दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मोदी जी के इस दौरे पर एक इंटरव्यु में लखनऊ के ख्याति प्राप्त प्रेफेसर ने साफ-साफ कहा कि मोदी जी का कोविंद जी के यहाँ दौरे का मकसद महज कोंविंद जी की उपयोगिता का लाभ उठाने का है। वे आगे कहते हैं कि मुझे इस अवसर पर हर्ष तो इसलिए हो रहा है कि मैं भी उसी कोली समाज से आता हूँ जिससे कोविंद जी आते है और विषाद इस लिए है कि कोविंद जी ने कभी भी अपने समाज के हित में कोई भी काम नहीं किया, यहाँ तक अपने गाँव में भी। कोविंद जी ने राष्ट्रपति रहते सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण पर बिना कोई टिप्पणी किए चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। आपको यह जानकर यह अफसोस होगा कि नए संसद भवन के भूमिपूजन के समय कोविंद को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। । एक दलित राष्ट्रपति का इतना अपमान कोविंद जी चुपचाप सहकर रह गए। यही हाल वर्तमान जनजाति वर्ग के राष्ट्रपति माननीय द्रोपदी मूर्मू का भी है, उन्हें भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी नहीं बुलाया गया। लगता तो ये है कि किसी भी दलित को राष्ट्रपति बनाने के पीछे मोदी जी का महज एक ही मकसद रहा कि कोई भी दलित राष्ट्रपति मोदी जी के किसी सही/गलत काम पर आवाज न उठा सकें। यही हालत भाजपा के बैनर के तले चुने गए दलित/ओबीसी के सांसद मुँह न खोलने के लिए मजबूर है।
असल में सबसे बड़ी बात ये है कि पिछ्ले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति एक रोजगार/व्यवसाय का हिस्सा बनती जा रही है। इसका जीता जागता प्रमाण है। भारतीय राजनीति में जड़ जमाता/जन्मता परिवारवाद/वंशवाद। दरअसल वंशवाद अथवा परिवारवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह से एक के बाद एक कई शासक बनते चले जाते हैं। यह भाई-भतीजावाद की परिपाटी लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो है ही, अधिनायकवाद को जन्म देने वाली हो सकती है। आदर्श तो ये है कि लोकतंत्र में वंशवाद के लिये कोई स्थान नहीं है किन्तु भारत में लोकतंत्र की शुरुआत से ही परिवारवाद की राजनीति हावी रही। प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वंशवाद/परिवारवाद निम्न स्तर का असंवैधानिक आरक्षण है। इसे राजतंत्र/ एकतंत्र का एक सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता है। वंशवाद,आधुनिक राजनैतिक सिद्धान्तों एवं प्रगतिशीलता के विरुद्ध है। पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि लोकतंत्र पूंजीवाद हावी हो गया है। सरकार को विपक्षियों की सही/गलत कमजोरियां तों दिखती हैं, अपने दल के नेताओं की नहीं। यहाँ तक कि विपक्षी राजनैतिक दलों के कथित भ्रष्टाचारी यदि भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो भाजपा की वाशिंग मशीन में साफ-सुथरा करके उपमुख्य मंत्री अथवा अन्य किसी लाभकारी पद पर आसीन कर दिया जाता है।
कहना न होगा कि जातीय/क्षेत्रीय अस्मिता, दोनों ही भावनात्मक छोर की ओर ले जाती हैं। यद्यपि अस्मिता की राजनीति लोगों को ज्यादा गुणकारी लगती है, तथापि भारत में जातिवाद और क्षेत्रवाद का भाव लोगों को लामबन्द कर देते हैं। और वोटिंग के समय मतदाता देश तो क्या, यहाँ तक कि अपने निजी और सामाजिक हितों को भी ताक पर उठाकर रख देते हैं। राज्य से निकलकर क्षेत्रीय दल राजनीतिक गठबन्धन के चलते केंद्र की सत्ता में तक पहुंच गए। इस प्रकार कई जातीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का सशक्तीकरण हुआ। यह कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि यह राजनीतिक बदलाव समाज के निचले तबके को रास आने लगा। किंतु दुख की बात तो ये है कि समाज के निचले वर्ग की समस्याएं जहाँ की तहाँ हैं। क्योंकि यह क्षेत्रीय दलों की यह नाकामी रही किवे क्षेत्र और जाति की अस्मिता को उचित प्रतिनिधित्व देने में सफल न हो सके। और राष्ट्रीय पटल पर अपना कोई वर्चस्व कायम न कर सके। दलित और पिछड़े वर्ग से आए नेता अपने ऐशो-आराम की जिन्दगी जीने के जुगाड़ मेंमशगूल हो गए । कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय और जातीय दलों के उभार का सामाजिक स्तर पर इतना तो फायदा हुआ कि अब निचली माने वाली जातियां बिना राजनीतिक संरक्षण के भी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लामबन्द होने लगी हैं। लेकिन शासन के स्तर पर इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि निचली माने वाली जातियों के राजनेता सत्ता के विर्मश और सामाजिक विकास से जैसे बाहर हो गए। कारण कि वे अपने वर्चस्वशाली राजनीतिक आकाओं के सामने मुंह न खोलने को बाध्य हैं। उसकी कीमत पूरे दलित और पिछड़े समाज को चुकानी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनके भले के लिए इस राजनीति का दावा किया जा रहा था।
हैरत की बात है कि आजकल मतदाता भी पूरी तरह से भ्रमित है। इसलिए वह किसी व्यक्ति के गुण-दोष देखकर वोट नहीं करती अपितु सबके अपने-अपने राजनितिक दल हैं फलत: वो प्रत्याशी को नहीं, राजनीतिक दल विशेष को वोट करता है। यह भी कि यदि लोकतंत्र में किसी भी राजा की व्यक्ति पूजा आरम्भ हो जाती है तो राजा तानाशाही प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। ऐसे में माननीय काशीराम का ये कहना कतई भी भ्रामक नहीं है कि लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं अपितु कमजोर सरकार की जरूरत है। इसका मुख्य कारण ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार न केवल समाज के हाशियाकृत समाज की उपेक्षा करने लगती है अपितु देश के पूंजीपतियों की ग्रफ्त में आकर केवल और केवल पूंजिपतियों के काम करती है। कारण कि पूंजीपति ही राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन की आपूर्ति करते हैं। यही सब आज के भारत में हो भी रहा है।
ज्ञात हो कि पूर्ण बहुमत की सरकार धर्म और असामाजिक गतिविधियों से जुड़े एजेंडे को साधने के लिए सामाजिक हितों को सूली पर चढ़ा देते हैं। आज आम मतदाता केवल इस बात से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है कि वोट मांगने वाला उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र का है। लेकिन राजनीतिक गुंडातत्व जाति, धर्म या क्षेत्र को ज्यादा महत्त्व देता है। आम मतदाता को लगता है कि अस्मिता की राजनीति भूमिगत हो गई है। मतदाता अस्मिता की राजनीति की अपील करता है। वह परिवर्तन के लिए प्रयोग करने को तैयार है। शायद इसलिए कि अस्मिता की राजनीति दिन प्रति दिन खत्म होती जा रही है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि अस्मिता की राजनीति खतरे में है।
इन हालातों में यदि गहनता से विचार करें तो आम मतदाता को चाहिए कि कोशिश ये की जाय कि देश किसी एक दल को सत्तारूढ़ न कर गठबंधन की सरकार बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि सरकारें सत्ता में बने रहने के लिए मतदाताओं के हितों के लिए काम करें। पूर्ण बहुमत की सरकार ने जनता के हितों की अनदेखी करके एक एक राजनीतिक कारोबार का रूप ले लिया है। पी एम का ये कहना कि देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का वितरण किया जाता है, इस बात का प्रमाण है। राजनीति के गलियारों में परिवारवाद के खिलाफ कितनी ही भी हायतौबा की जाती हो लेकिन भारतीय राजनीति के व्यवहार/आचरण से परिवारवाद दिन पर दिनबढ़ता ही जा रहा है। परिवारवाद की राजनीति से कोई भी राजनीतिक दल अछूता हो, ऐसा नहीं है। तमाम राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति का खुला खेल रहे हैं। अब चुनाव लोकसभा के हों अथवा राज्यों की विधान सभाओं के धरती-पकड़ नेता अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को आगे लाने में लगे रहते हैं।
जैसा किपहले कहा गया है कि राजनीति में दशकों से परिवारवाद कायम है। नई बात यह हुई है कि नेहरू परिवार के बाहर के राजनीतिक शिखर पुरुष अपने-अपने नौसिखिया बेटे/बेटियों को राजनीतिक दंगल में जिस उन्मुक्ता से उतारे हुए हैं, वह सिर्फ इसलिए कि राजनीति का क्षेत्र हरेक तरह से सुरक्षित है। कुछ भी करो, खुलकर कब्बडी खेलो, इसको मारो... उसको मारो या मरवाओं...खुलकर लूट मचाओ...देश की प्रशासनिक व्यवस्था तो शासन की अधीन होती ही है। न्याययिक प्रणाली के साथ-साथ प्रशासनिक शक्तियों का भी कोई डर नहीं।
स्मरण रहे कि एक समय हुआ करता था कि जब देश की लोकसभा में 75% सांसद ब्राहम्ण और बनिया वर्ग के हुआ करते थे, आज 67% सांसद अनुसूचित /जन-जाति और पिछड़े वर्ग से चुनकर लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। किंतु सांसद या मंत्री बनते ही वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय समाज के दलित/दमित वर्ग के लिए उनका कोई दायित्व भी है। भारतीय समाज के दलित/दमित वर्ग की कमोवेश आज भी वो ही हालत है... जो विगत में थी, कुछ मोडरेट जरूर हो गई है। भेदभाव के नए तौर-तरीके... अत्याचार के तौर-तरीकों में आया नयापन राजनेताओं को ‘विकास’ नजर आता है। आज के भारत में भाजपा सरकार के चलते जितना हिंसक अत्याचार दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, शायद ही कभी पहले इस दर्जे की क्रूर क्रियाएं हुई हों। किंतु सत्ता पक्ष में बैठे इस वर्ग से आए सांसदों और मंत्रियों की जुबान को जैसे लकवा मार गया हो, किसी का भी मुंह नहीं खुला। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि पालतू कुत्ता मालिक की सोटी खाकर भी केवल पूंछ ही हिलाता है... भौंक सकने की ताकत वह खो चुका होता है।
संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में डा. अम्बेडकर ने जिस सामाजिक लोकतंत्र की कल्पना की थी, उसे आज पूरी तरह से भुला दिया गया है। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज देश की राजनीति पर भाजपा की पैत्रिक संस्था आर आर एस जैसे परम्परागत संस्कृतिवादी संस्थाओं का कब्जा है। तर्क इनकी समझ से परे है और मिथ्याआस्था इनके खून में है। संस्कृति और धर्म की आड़ में समाज विरोधी राजनीति करना इनकी आदत में सुमार है। यद्यपि समाज का बहुसंख्यक वर्ग इनकी विचारधारा को पसंद नहीं करता किंतु आज का टी आर पी पसंद मीडिया और प्रचार के दूसरे माध्यम इनकी राजनीति को शिखर पर ही रखते हैं और सरकार से अच्छा-खासा पैसा कमाते हैं। जिसके चलते धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मसले प्राय: इनके पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं। धर्म और जाति केन्द्रित राजनीति भारतीय समाज के लिए एक कलंक ही है। जाहिरहैकिआजकामीडियाभीकारोबारीहोगयाहै।
लेकिन लोकतंत्र में संख्याबल के जो मायने है। उसका जायजा इस बात से लिया जा सकता है कि यदि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ओर 51 गधे और दूसरी ओर 49 घोड़े जीतकर लोकसभा में पहुँचते हैं तो सरकार 51 गधों की ही बनेगी। इस तर्क के मद्देनजर समाज का दलित/दमित वर्ग अपने आप को वर्चस्वशाली वर्गों, जिनपर सवर्णों का कब्जा है और जिनका न्याय, समानता, वर्गहीन समाज और समग्र विकास में साझेदारी जैसे कामों में कोई विश्वास नहीं होता, के साथ स्वार्थपूर्ण गठबन्धन कर उनके हवाले कर देता है। और दलित-दमित समाज के तथाकथित नेता जीतने के बाद उस दलित/दमित समाज की अनदेखी कर देता है जिसके भले की दुहाई देकर वो सत्ताशीन होता है। ऐसे में विचार और सामाजिक परिवर्तन की राजनीति केवल एक सवाल बनकर रह जाती है।यद्यपि लोकतंत्र में जनता को निर्णायक शक्ति माना जाता है, किंतु लोकतंत्र में जनता को अपना अधिकार दिखाने का हक पाँच साल में केवल एक बारही मिलता है और राजनेताओं को जनता को लूटने का अधिकार पूरे पाँच साल के लिए मिल जाता है। अब कोई तो बताए कि लोकतंत्र में राजनीति की अस्मिता जनसेवक की नहीं....एक कारोबारी की है। यहाँ यह कहना भी तर्कसंगत ही होगा कि एक बार सत्ता में आने के बाद राजनेता जिस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं... किसी से छुपा नहीं हैं। क्या आज की राजनीति लोकतंत्र की कारोबारी राजनीति नहीं?
0000
सरकार सोशल मीडिया से इतना क्यों घबराती है
बड़े ही दुख की बात है कि सिनेमाई दुनिया के तथाकथित हीरो/ बड़े-बड़े लोग जुआ जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को जोर-शोर से प्रमोट कर रहे हैं।…..यूट्यूब पर विज्ञापनों के जरिए मोटी-मोटी राशि वसूल रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कैसा ही भी वीडियो नहीं बना रहा। और न ही ऐसे लुभावने विज्ञापनों पर सरकार ही कोई ध्यान देती है। परिणामत: मोबाइल पर रोज किसी भीं समय जुआ खेलना शुरू हो जाता है। बच्चों/लोगों में यूट्यूब पर जुआ खेलने की ऐसी लत लग जाती है कि जुआ कीदुनिया के जुआरी कर्ज में डूब जाते हैं। और वे लोग क्रेडिट कार्ड का अधिक प्रयोग करते हैं। ... एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से भरते हैं और दूसरे का बिल तीसरे क्रेडिट कार्डे से। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा… इस बुराई के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया जा रहा। उल्टे इसे प्रमोट कर रहे हैं। हाँ! इतना जरूर है कि सिगरेट और शराब की बोतलों पर लिखी चेतावनी “ सिगरेट/शराब सेहत के लिए हानिकारक है” जैसी चेतावनी देकर अपने कर्तव्य की खानापूरी जरूर पूरी कर दी जाती है। बच्चों/बड़ों को ...”जुआ खेलने की आदत लग जाती है इसमें आर्थिक जोख़िम भी शामिल है”। लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? मेरी उन सभी लोगों से जिनकी बात लोग सुनते हैं...मानते हैं और जुआ खेलने के इस खेल को/ बुराई को इस देश में बहुत बड़े इशू के रूप में देखते हैं और उनके पास अगर ऑडियंस है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे जुआरियों की लत में पड़े लोगों से उन बातों पर भी आप बात करें जिससे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। आपको पता है कि देश में रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। किंतु तंबाकू की, दारू की ऐड खुलेआम चल रही है। इलायची के नाम पर जाने क्या-क्या बेचा जा रहा है और इसका विज्ञापन बड़े जोरों से किया जाता है। पूरा का पूरा पंजाब, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश और बहुत बड़े दो तीन स्टेट पूरे के पूरे ड्रग्स की चपेट में बताए जाते हैं।
याद रहे कि जुआ खेलने का विकार एक दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो जुआरी के जीवन को कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। यह एक व्यवहारिक लत है जो तब होती है जब आप अपने जुए के व्यवहार पर नियंत्रण खो देते हैं। क्या आपने कभी लॉटरी की टिकट खरीदा है? क्या आपने अपनी पसंदीदा टीम पर कुछ पैसों की शर्त लगाई है? वास्तव में इन आदतों को जुआ कहते हैं। यह एक ऐसा काम है जिसमें अधिकतर लोग किसी न किसी तरह संलिप्त हैं। वास्तव में यह लत एक ऐसा वायरस है जो आपको धीरे-धीरे खोखला बना देती है। इससे आदमी कर्जदार बन सकता है और उस व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो सकती है। जुआ ऐसी कुछ चीज है जो आपको कुछ चीजों को हासिल करने के लिए मजबूर करता है और आखिर में आपको खतरे में डाल सकता है। परंपरागत जुआ गतिविधियों में लॉटरी, घुड़दौड़, सट्टेबाजी और कार्ड गेम शामिल रहे हैं। यह एक व्यापक गतिविधि है और कम से कम 86 फीसदी युवक जुए की किसी ना किसी गतिविधि में शामिल हैं जबकि 52 फीसदी वयस्क लॉटरी में भाग लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश बहुत बड़ी आबादी जुआ खेलने के आदी हैं।
लोग जुआ क्यों खेलते हैं? इस बारे में साइकेट्रिस्ट डॉ. अरुण जॉन के अनुसार, 'यह जोखिम का रोमांच है, जो लोगों को जुए के लिए खींचता है।' शुरुआती भाग्य के मिथक को खारिज करते हुए डॉक्टर जॉन कहते हैं कि पहली बार जुआरी दांव बढ़ाकर, वे पहले कुछ समय के लिए जीतते हैं। जब आप शुरुआत में जीतते रहते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है और उसके बाद आप हारना शुरू कर देते हैं। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए फिर और ज्यादा बड़ी शर्त लगाते हैं। लॉटरी के मामले में छोटी जीत भी आत्मविश्वास पैदा करती हैं। यहां तक कि पुरस्कार राशि के रूप में मिलने वाले रुपये भी आपके दिल में भविष्य में बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद पैदा कर देते हैं। और इस जुआरी को जुए की लत पड़ जाती है। जुआ की लत किसी को भी नहीं छोड़ती है। आदत को रोकने के दोहराए गए प्रयास विफल होने लगते हैं। आमतौर पर उन लोगों को जुए में रत देखा जाता है जो कि 18-35 आयु वर्ग के होते हैं। यह वह उम्र है जब पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है। जुआरीजुआ का विरोध करने की कोशिश करते वक्त बेचैन या चिड़चिड़ा महसूस करता है। और जुआ पलायनवाद का एक रूप बन जाता है। यह भी माना जाता है कि लोग असहायता, चिंता, अपराध या अवसाद की भावनाओं को भूल जाने के लिए जुआ खेलते हैं। जुए की लत के चलते जुआरी आदत को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या गबन जैसे आपराधिक व्यवहार में शामिल हो जाता है।जुआ के लिए नौकरी या रिश्तों को खतरे में डालना। आदत को बढ़ावा देने के लिए दूसरों से धन उधार लेना।जुआ जुआरी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जुआरी जीतने के उत्साह, हताशा, अवसाद, चिंता के बीच घिरा रहता है। जुआ खेलने की लत का कोई सफल इलाज भी हो सकता है, यह गफलत की बात है।
आज के तकनीकी युग में जुए ने भी नया रूप ले लिया है जिसे अक्सर ओनलाइन गैम्बलिंग (Online Gambling) या ओनलाइन गेमिंग के रूप में जाना जाता है। अक्सर लोगों के मन में Online Gambling और Betting Apps को लेकर कई भ्रम होते हैं और जानकारी के अभाव के कारण लोग वित्तिय जोखिम में पड़ जाते हैं। यहाँ यह समझने की बात है किभारत में online betting को लेकर कानून क्या कहता है और ये कहां वैध है ... कहां अवैध। भारत में Online Gambling और Betting Apps को लेकर भ्रम बना रहता है। कई लोगों के जहन में सवाल रहता हैकि क्या ये एप्स India में लीगल हैं।क्या इन्हें इस्तेमाल करना सुरक्षित है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब खोज पाना थोड़ा मुश्किल है। एक ओर तो भारत सरकार है जो लगातार इन एप्स के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर रही है, तो वहीं कुछ राज्य सरकारें हैं, जिनके द्वारा इन online gaming and gambling को लीगल बताया गया है। ऐसे में ये एक उलझन भरा मसला है। भारत में ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर तो कोई एक कानून नहीं है, जो पूरे देश में इसे रेगुलेट करता हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे जरूर हैं, जिनके द्वारा खुद कुछ कानून बनाकर बैटिंग लीगल की गई है।
बताया तो ये जाता है कि भारत में, ऑनलाइन गेम खेलना गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि सरकार ऑनलाइन गेम को "एक ऐसा गेम है जो इंटरनेट पर पेश किया जाता है और जिसे उपयोगकर्ता कंप्यूटर संसाधन या मध्यस्थ के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट तक पहुंच और दूरदराज के गांवों में स्मार्टफोन का उपयोग करने की प्रवृत्ति ने गेमिंग उद्योग में एक अलग स्तर पर बदलाव ला दिया है। केपीएमजी इंडिया द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2024 तक 25।3 बिलियन रुपये का उद्योग बनने के लिए तैयार है।
अजीब बात है कि यह समाज विरोधी खेल उभरते हुए उद्योग के बाद बाजार को तेजी से बढ़ा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक माना जा रहा है।भारत में गेमिंग उद्योग में पैदा होने वाले भ्रम से बचने के लिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए व्यापक कानून नहीं है। इस विषय में तर्क दिया जाता है कि ऑनलाइन गेम मानव बुद्धि यानी कौशल का उपयोग करके और 'कौशल का खेल' के कारण खेला जाता है, और जो भारत में कानूनी है। इसके विपरीत, मौका का उपयोग करके खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम जहां मानव बुद्धि का उपयोग किए बिना संयोग से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, वह 'मौका का खेल' है जो भारत में कानूनी नहीं है। यही कारण है कि भारतीय राज्यों में जुआ और सट्टेबाजी कानूनी नहीं है। दूसरी ओर online and offline betting, gambling संबंधित कानून कहीं न कहीं लोगों को वित्तीय नुकसान, लत और मानसिक आघात से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए बिना किसी तनाव या डर के खेलने के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु क्या यह संभव है? वैसे अप्रैल 2023 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य कानूनों की खामियों को देखने के बाद, ऑनलाइन गेमर्स को लत और हानिकारक परिणामों से बचाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है इन विनियमों को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") में संशोधन किया गया है। यह मुख्य रूप से ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर गौर करेगा। कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया है। तब यह सभी के ध्यान में लाया गया कि प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करने के लिए, सरकार को जुआ वेबसाइटों और पोर्टलों को ब्लॉक करने की आवश्यकता है।
सर्वे में शामिल लोगों से पहला सवाल पूछा गया था कि वे कौन सा ऑनलाइन गेम सबसे ज्यादा खेलते हैं? जिसके जवाब में पहले नंबर पर अधिकतर लोगों ने पबजी खेलने की बात मानी थी जबकि दूसरे नंबर परफ्री फायर और फोर्टनाइट तीसरे नंबर पर था। और आजकल क्रिकेट से जुड़ा गेम “अपनी टीम बनाओ” जैसे कई खेल सुर्खियों में हैं। आजकल तो यह गेमिंग बच्चों में ज्यादा प्रचलित हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। कई बार चोरी की लत लग सकती है। इससे बच्चों की सोशल स्किल्स खराब होती हैं। गेमिंग के चक्कर में बच्चे परिवार से दूर हो जाते हैं। स्कूल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इतना ही नहीं बच्चे आत्महत्या का रुख अपनाने लगे है। खबर है कि एक बच्चे ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी है। उसमें लिखा है कि उसने गेम के चक्कर में उसने 40 हज़ार रुपए बर्बाद कर दिए। अंग्रेजी और हिंदी में लिखे सुसाइड नोट में उसने यह भी लिखा है कि अवसाद के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। स्मार्ट फोन के आने के बाद अक्सर ओनलाइन गैम्बलिंग (Online Gambling) या ओनलाइन गेमिंग का दायरा इतना बढ़ गया है कि यूट्यूब पर आने वाले विज्ञापन धड़ाधाड़ आ रहे हैं और सरकार की ओर से ओनलाइन गैम्बलिंग (Online Gambling) या ओनलाइन गेमिंग से जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगाने की मंशा दिखाई नहीं देती। सरकार ने कहा है कि स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन गेमिंग बड़े अवसर के रूप में सामने आया है। सरकार ने सट्टेबाजी और गैंबलिंग से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा न दिया जाए। किंतु सरकार इस काम को करने में गंभीर दिखाई नहीं देती।
Apr 12, 2024 : जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मोदी जी को अपनी छवि की काफी चिंता सताने लगी है। क्योंकि ज़मीन पर जो खास मुद्दे हैं, वो हैं महंगाई, बेरोज़गारी, नौकरी, भ्रष्टाचार, चुनावी बांड। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग ज़मीन पर तो बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी हर दिन कुछ न कुछ नई बातें करके मौजूदा मसलों के इतर अपनी नई छवि दिखाते हैं। वहीं हाल में मोदी जी ने देश के मशहूर गेमर्स यानी गेमिंग इंडस्ट्री के मशहूर लोगों से बातचीत की है। और आज इसका एक छोटा सा ट्रेलर सामने आया है जिसमें सभी गेमर्स मोदी जी को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। और इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं कि मोदी जी का इसे अपना मास्टरस्ट्रोक मान रहे हैं। दूसरे ट्वीट पर नजर डालें तो पता चलता है कि पीएम ने शीर्ष भारतीय गेमर्स यानी गेमिंग इंडस्ट्री के शीर्ष लोगों से बातचीत ही नहीं की अपितु मोदी जी ने उनके साथ गेम भी खेला यानि उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में वर्चुअल रियलिटी गेम्स पर अपना हाथ रख दिया है। और उन्हें एक नाम भी दिया गया है, नमो ओपी, नमो प्रबल। गेमिंग इंडस्ट्री में हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग नाम हैं, इसलिए उन्हें नमो ओपी का एक नया नाम भी मिल गया है, यानी नमो ओवरपावर्ड।
जाहिर सी बात है कि चुनाव के दौरान मोदी की छाया को बढ़ाना... उनकी जनसंपर्क टीम का कर्तव्य है। ताकि लोगों को लगे कि वे इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आज भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। तो पीएम मोदी की गेमर्स से इस बातचीत का चुनाव में क्या फायदा होगा? वह देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब देश के सामने गेमर्स को लेकर गंभीर मुद्दे हैं तो इसके पीछे का तर्क क्या है? पीएम की टीम में चाहे सलाहकार हों, सलाहकार हों, ट्रोलर हों, आईटी के लोग हों, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या उन्हें लगता है कि लोग अब जनता से कट गये हैं? वहीं मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी लगातार मोदी सरकार के बारे में एक ही बात कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब देश की जनता को मोदी जी को हटाना होगा। ध्रुव राठी का यह बहुत छोटा वीडियो है, एक मिनट से भी कम, लेकिन उस वीडियो से देखा जा सकता है। और अंत में ध्रुव राठी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना जरूरी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ाए।
इस चुनाव में पैसा कहां से आ रहा है? इसे कैसे खर्च किया जा रहा है? यह सब गलत है तो ये भी एक पहलू है। वह पैसा भी इन गेमर्स से लिया जा रहा है। हमें यह सोचना ही होगा कि क्या यह गेम देश के लिए उपयुक्त है।क्या यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा है? क्या युवाओं का भविष्य मजबूत होगा? हमारे देश में ये चिंता का विषय है। ऐसे वर्चुअल गेम खेलने से, जो कहीं से भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं करता, हमारी बुद्धि में सुधार नहीं करता, तरह-तरह के विकार पैदा करता है। बच्चे लगातार ऐसे खेलों से जुड़ रहे हैं। और ये हर परिवार के लिए चिंता का विषय है। बच्चे अपने अभिभावकों से छिपते हैं। और रात भर गेम खेलते हैं। और दिन भर मन ऐसा ही रहता है। इसलिए ऐसे गेमिंग को हतोत्साहित करने की जरूरत है न कि इसे प्रोत्साहित करने की। अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए किसी भी अनैतिक बात को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। एक और बात आपको याद होगी। जब चुनावी बांड खुल रहे थे। गेमिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ने कई सौ करोड़ का दान दिया। शायद यह 400 करोड़ से ज्यादा की रकम बताई जा रही है। दान देने वालों ने टैक्स चोरी भी की। उन्होंने सैकड़ों करोड़ टैक्स का पैसाबचाया।
आनलाइन गेमिंग से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जिससे अभिभावक की चिंता बढ़ गयी है। किंतु प्रधान मंत्री की वीडियो गेमर्स के साथ बातचीत से तो यही लगता है कि सरकारी स्तर पर इसे रोकने के बजाय बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। जाहिर है कि यदिआप फुटबॉल को बढ़ावा देते हैं तो इससे वोट नहीं मिलेगा। यदि आप कबड्डी और हॉकी को बढ़ावा देते हैं तो इससे भी राजनेताओं को वोट नहीं मिलेगा। फिर कोई कबड्डी , तिरंदाजी जैसे खेलों को कौन प्रोत्साहित क्यों करे? होना तो ये चाहि़ए कि युवकों में खेल भावना पैदा की जाए। ऐसे सभी खेलों को प्रमोट किया जाए जिनसे युवकों के बीचदोस्तीऔरभाईचारे को बढ़ावा मिले। सत्य है कि मिलजुल कर रहने की कला ऐसे शारिरिक श्रम के खेलों से ही प्राप्त होती है। किंतु आनलाइन गेमिंग हमें हर स्तर पर नष्ट कर रही है। किंतु नेताओं को क्या? जब यह गोदी मीडिया द्वारा संचालित चुनाव है। फिर चुनाव के प्रचार में नमक-मिर्च लगाना एक आवश्यक अवयव बन गया है। ताबड़तोड़ बंद होने लगे यूट्यूब चैनल से यह तो सिद्ध होता ही है कि सोशल मीडिया की ताकत से राजा डर गया है? कई महीनों, कहें तो सालों से जिस बात का डर था, वो होने लगा है। अभी खबर मिली है कि कई यूट्यूब चैनल गायब हो गए हैं जो सवाल करते थे, जो जूते पॉलिश नहीं करते थे, जो आंखें दिखाकर सवाल करते थे। इन सभी को समय-समय पर हटाया जा रहा है। किसी का मुद्रीकरण समाप्त किया जा रहा है। ईवीएम से जुड़े मसलों पर सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया का भी मुद्रीकरण खत्म कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि यूट्यूब चैनलस/सोशल मीडिया पर झगड़े व दंगे दिखाए जाते हैं; गालीयां दी जाती हैं; ये झूठ परोसते हैं। बहाना कुछ भी हो सरकार मेन स्ट्रीम के गोदी मीडिया की तरह ही सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाना चाहती है।
सोशल मीडिया को तमाशाई कहा जाता है।देश में सैकड़ों चैनल हैं, सैकड़ों गुंडे हैं जो दिन-रात नफरत उगलते हैं। दस साल में क्या आपने सुना है कि किसी चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया हो? क्या आपको पता चला कि किसी गुंडे के मुंह पर ताला लगा हो, जो दिन-रात जहर उगलता है, जो दिन-रात हिंदू-मुसलमान करता है, जो दंगे भड़काते हैं।गोदी मीडिया सत्ता के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया ऐसा नहीं करते। वे सवाल करते हैं। इसीलिए चुनाव से पहले आप देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और जो स्वतंत्र आवाजें हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, उनके चैनलों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है।
पिछले दिनों आर्टिकल 19, नेशनल दस्तकसहित कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर प्रतिबंध लगाने का काम किय जा रहा है। ताजा खबर आई है कि ‘बोलता हिंदुस्तान’ नाम के यूट्यूब चैनल को तो हटा दिया ही गया है और ‘’ लोकहित इंडिया‘ चैनल का मोनेटाइजेशन हटा दिया गया है। संभव है कि अगले एक-दो दिन में कई और चैनल गायब ही कर दिया जायें। यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनी भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। इसे कोई देखने वाला नहीं है।
आप इसे लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं? किसान आंदोलन के दौरान लगातार सभी ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। उन्हें निलंबित कर दिया गया। जो भी सवाल उठ रहे थे, उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा था। कहीं खुलेआम तो कहीं छुपकर। किसी को जेल में डालो। किसी का चैनल बंद करो। किसी चैनल का मुद्रीकरण हटाएँ। कुछ नहीं मिला तो बस आर्थिक झटका मारो। आप कुछ भी करें आवाज बंद होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्र आवाजें चुप नहीं होने वाली हैं, ऐसा लगता है। कुछ साल पहले देश के सबसे बुजुर्ग पत्रकारों में से एक रवीश कुमार ने कहा था कि जब चैनल पर प्रतिबंध लगेगा तो हम सड़कों पर खड़े होकर खबरें पढ़ेंगे। सड़कों पर खड़े होकर लोगों को जानकारी देंगे। और सड़कों पर उतरने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। हम उन सभी दरवाजों पर दस्तक देंगे जहां से हमें न्याय की उम्मीद है। आखिरी उम्मीद अब भी सुप्रीम कोर्ट ही बची है। हम भी वहां जाएंगे। जाहिर है कि हानिकारक का मतलब हानिकारक होता है। यह किसके लिए हानिकारक है? आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर हजारों वीडियो हैं। मतलब साफ है कि अगर यूट्यूब को लगता है कि कंटेंट हानिकारक है तो यह सत्ता के लिए हानिकारक है। और अगर यूट्यूब पावर के लिए काम करता है तो हमारे वीडियो निश्चित रूप से हानिकारक हैं। क्योंकि हमारा काम जनता के लिए बोलना है, सत्ता के लिए नहीं। विदित है कि मंत्रालय ने जिन 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है। उनकी कुल व्यूअरशिप 260 करोड़ से अधिक बताई जाती थी। पिछले साल फरवरी में आईटी रूल्स, 2021 के आने के बाद से यह पहली बार है जब भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की गई है। इन्हें मिलाकर दिसंबर 2021 से अब तक सूचना प्रसारण मंत्रालय कुल 78 यूट्यूब आधारित न्यूज चैनलों और दूसरे कई सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर चुकी है।
अभी तक यूट्यूब ने कुछ भी गलत नहीं देखा है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, जैसे ही कायर राजा साहब को लगा कि ये पोल खुल रही है, सब बहुत-बहुत बातें कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खुल रहा है, मेरी संपत्ति, मेरी रंगदारी, मेरी रिश्वतखोरी, सब खुल रही है। तब रज़ा साहब घबरा गये। और वो इतना डर गए कि अब यूट्यूब चैनल एक-एक करके गायब होते जा रहे हैं। उनका मुद्रीकरण ख़त्म किया जा रहा है। इससे अधिक कायरतापूर्ण बात और क्या हो सकती है? 10-12 साल से जिन लोगों ने पूरे देश की मीडिया पर कब्ज़ा कर रखा है, जो चाहे वो कहलवाते हैं, जितना चाहे जहर उगलवाते हैं, वो लोग सोशल मीडिया से भी इतना डरते हैं।प्रचार तंत्र ये जानकारी भी मिल रही है कि दरबारी मीडिया चैनलों के दर्शक निरंतर कम हो रहे हैं।
0000
अपने ही जाल में फंसता जा रहा है बहुजन समाज
जाति व्यवस्था के बारे में यह कहना एक प्रासंगिक प्रश्नचिन्ह ही होगा कि जाति से मुक्ति अथवा उन्मूलन की कोई ठोस और कारगर परियोजना के तहत संभव है। दरअसल यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से ही निरुत्तर रहा है। ज्यों-ज्यों और जब-जब जाति-रूपी साँप ने जोरों से फुफकारना शुरु किया है, जाति के उन्मूलन हेतु नाना प्रकार के आन्दोलनों का आव्हान भी हुआ है किंतु जाति का मर्ज घटने के बजाह और बड़ा ही है, ये सही हो न हो किंतु ये सही है कि जातिगत मर्ज की प्रकृति जरूर बदलती रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जाति आधारित उत्पीडन के सवाल पर हुए आंदोलनों ने निश्चित रूप से असर किया है, जो हमें कम से कम शहरों में तो देखने को मिलता ही है। गांवों की सामाजिक संरचना के साथ-साथ उत्पीड़न के तौर-तरीकों में भी खासा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस आधार पर यह मान लेना कि जाति समाप्त होती नजर आ रही है, एक भ्रमजाल में फंसना ही माना जाएगा।
कोई माने न माने ब्राहम्णवादी व्यवस्था के वर्चस्व में किसी प्रकार की कमी के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ! प्रकृति में बदलाव जरूर झलकता है। जिसका मूल कारण समूचे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रहे प्रचार- प्रसार में निहित है। इस प्रकार का बदलाव केवल भारत में ही है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रहे प्रचार-प्रसार से यह तो माना जा सकता है कि समाजके दलित और दमित वर्ग में जागरूकता का ज्वार आया है। दूसरे ....भारत की सैंवाधानिक व्यवस्था से भारतीय राजनीति में जातियों को एकजुट और तो और .....और पुष्ट होने का प्रभाव बढ़ा है। चुनावी व्यवस्था में दलित जातियों के आरक्षण के चलते विधायिका में दलित-पिछड़े और आदिवासियों की संख्या बढी है, लेकिन भारतीय समाज के दलित-दमित वर्ग में जातीय अलगाव भी तेजी से बढ़ा है। जिसके चलते अनुसूचित/अनुसूचित जनजातियों का ध्रुवीकरण होने के बदले बिखराव ही उत्पन्न हुआ है.....प्रत्येक व्यक्ति में सत्ता में कुर्सी पाने का लालच इस कदर शीर्ष हुआ है कि वर्चस्वशाली राजनीतिक दलों की चाटुकारिता करके सत्ता में कुर्सी तो हासिल कर लेता है किंतु निजी स्वार्थों के चलते सामाजिक-स्वार्थ गर्क में चले जाते हैं। इस तरह राजनीतिक-सत्ता दलित और दमितों के बिखराव के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों वाली दलितों और पिछड़ों क लिए सभी तालों की चाबी नहीं रह गयी है। सत्ता की 'मास्टर की' न केवल ब्राहम्णवादी शक्तियों के हाथों में बल्किअब तो कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली गई है। इस प्रकार राजनीति में अनुसूचित/अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व तो है किंतु उसका सत्ता के संचालन में हस्तक्षेप नहीं के बराबर ही है।
जहाँ तक इतिहास में जाति से मुक्ति के लिए चले आंदोलनों का सवाल है तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं कि जाति से मुक्ति के लिए सदियों से अनेक आन्दोलन चलते रहे हैं किंतु समय के साथ-साथ सारे आन्दोलन साम, दाम, दण्ड और भेद वाली नीतियों के शिकार होते रहेहै । हाँ! भारतीय समाज में लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व बौद्ध दर्शन ने ब्राह्मणवाद और जातियों से मुक्ति का मार्ग जरूर प्रशस्त किया जिसकी छाया/प्रतिछाया आज भी देखने को मिलती है। किंतु बुद्ध के निर्वाण के साथ ही केवल 300/400 वर्षों में ही बौद्ध संस्थाएं जातिवाद और ब्राह्मणों द्वारा अपनी श्रेष्ठता कायम रखने के लिए रचे गए सामाजिक-आर्थिक कुचक्रों के जाल में फंसकर मृतप्राय: हो गईं। यह कहना अतार्किक न होगा कि भारतीय समाज के कुटिल, बौद्दिक रूप से सम्भ्रात ब्राहम्णवादी शाक्तियाँ जाति से मुक्ति के प्रत्येक आन्दोलन के ताप को ठंडा करके अपने प्रभाव में ले लेती हैं।
जाति और धर्म से मुक्ति के सवालों को कबीर , रैदास, दादू, चोखामेला जैसे संत कवियों ने जिस शिद्दत से समाज के सामने रखा, वैसी मिसाल अन्य जगह कम ही देखने को मिलती। उनके साहित्य को किसी न किसी रूप में जाति से मुक्ति के लिए एक परियोजना माना जा सकता है किंतु अन्य विभिन्न साहित्यिकारों/ लेखकों के लेखन में जाति से मुक्ति की लिए आवाज उठाने का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस हेतु काम को किसी परियोजना का हिस्सा माना जा सकता है। आमजन की रुचि के साहित्यिक कर्म को साहित्यकार/लेखक/कवि विशेष की रुचि के रूप में भी देखा जा सकता है। उसकी अपनी रुचि के अनुसार उपजे साहित्य में यदि जाति मुक्ति के लिए कोई विशेष संदर्भ देखने को मिलते हैं तो यह एक संयोग ही माना जाएगा। हाँ! इतना अवश्य माना जा सकता है कि तथाकथित दलित साहित्य में ऐसे प्रकरण मिलते तो जरूर हैं किंतु वो समाज की दशा को ही ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन उस दशा से उबरने या जाति से मुक्ति के सवाल या तो केवल कटाक्ष के रूप में या फिर केवल आलोचना के रूप में ही ज्यादा उभर हैं। तथाकथित दलित साहित्य के रचनाकारों की तो सबसे ज्यादा त्रिसादी ये रही है कि वे “दलित” शब्द को इतनी जोर से जकड़कर पकड़े हुए हैं कि यदि दलित शब्द को कहीं छोड़ दिया तो उनका साहित्यिक अस्तित्व व सामाजिक अस्मिता का ही ह्रास हो जाएगा। यदि ये कहा जाए कि ज्यादातर दलित साहित्यकार “दलित” शब्द के प्रयोग को ही अपनी मुक्ति का मार्ग मानते हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सामाजिक/धार्मिक/आर्थिक बराबरी के लिए दलित जिस मैली-कुचैली जातीय चादर को उतार कर फैंक देना चाहते हैं, उसी मैली-कुचैली जातीय चादर को अपने साहित्य पर डालकर साहित्यिक क्षेत्र में शिखर पुरुष होने का मार्ग तलाशने में संघर्षरत हैं।
इतना ही नहीं दलित साहित्यकार आजकल जातियों के खैमों में संगठित हो रहा है जिससे जातियों के और पुष्ट होने के प्रमाण ही मिलते हैं। इस खैमेबाजी के चलते “ दलित लेखक संघ” में भी टूट पड़ गई और “दलित लेखक संघ” की स्थापना का मूलभाव तमाशा बनकर रह गया है। ऐसे साहित्यकारों के इतर आजकल कुछ ऐसे दलित साहित्यकार भी सामने आए हैं जो दलितों के साहित्य को “दलित साहित्य” के रूप में स्वीकार न करके इसे “अम्बेडकरवादी साहित्य” के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने को सामान्यत: “दलित-साहित्य” और “अम्बेडकर साहित्य” के प्रेरणा स्त्रोत केवल और केवल बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ही हैं। कहना न होगा कि आज दलित-समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ही अपने समाज की अनदेखी करने में देखा जा रहा है।
इस कड़ी में विभिन्न सामाजिक नायकों, नामचीन लेखकों और चिंतकों के स्वतंत्र लेखन और उनके द्वारा नाना प्रकार से किए गए कामों को निश्चित रूप से जाति से मुक्ति के लिए स्वतंत्र परियोजना का नाम दिया सकता है। इस संबंध में संत परंपरा से लेकर जोतिबा फुले, डा. अम्बेडकर, स्वामी अछूतानंद, पेरियार जैसे महानायकों की एक बड़ी जमात है जिसका उल्लेख करना जरूरी जान पड़ता है किंतु डा. अम्बेडकर ने जिस व्यवस्थित व व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तन के जो मानदंड और आदर्श प्रस्तुत किए, वैसे उदाहरण कहीं और मिलना असंभव जान पड़ता है। इनके द्वारा किए गए कामों में जाति से मुक्ति के लिए किया गया प्रत्येक संघर्ष मिलता है।
जहाँ तक मेरे अपने साहित्यिक कर्म में जाति से मुक्ति का मार्ग तलाशने के बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि आत्मालोचना करना किसी भी साहित्यकार के लिए एक जोखिम भरा कार्य है। फिर भी इतना तो कह ही सकता हूँ कि मेरी अपनी लेखन शैली अमूमन दलित साहित्यकारों से अलग और गाली-गलौज से परे की लेखन-शैली है। जिस कारण से जनसासान्य में मेरे लेखन के प्रति शायद खिन्नता नहीं उपजती अपितु सामाजिक जुड़ाव का भाव ही उत्पन्न होता है। शायद इसलिए ही मैं साहित्यिक क्षेत्र में खैमेंबाजी से दूर अलग-थलग पड़ा दिखता हूँ।
कमोबेश यही हालत दलित राजनीति की भी है।बहुजन समाज में बसपा के अतिरिक्त अनेक राजनीतिक दल भी मैदान उतरने का दम भर रहे हैं। विदित हो कि रिपब्लिक पार्टी के बाद बसपा ने बहुजनों के लिए जो काम किया, वैसा अन्य कोई अन्य बहुजन समाज को एक करने के बजाय अन्यंय राजनीतिक दल बनाकर बहुजनों के वोटों को छितराने का काम कर रहे हैं। और यही कांग्रेस और भाजपा चाहती भी है। यह भी कि बहुत से बहुजनों को कुछ न कुछ लोभ देकर बहुत सी जेबी राजनीतिक पार्टियों का सृजन कराने का काम करती हैं ताकि बहुजनों और ओबीसी के वोट बैंक कहीं एकजुट न हो जाएं।कमाल की बात तो ये है कि बहुजनों के राजनीतिक दल आपस में ही एक दूसरे की टाँग खिचने में लगे रहते हैं। या यूं कहें कि बहुजन समाज के जेबी राजनीतिक दल ही बहुजनों को बाँटने पर तुले हैं।
उपरोक्त के आलोक में मेरे लिए तो यह कहना अति कठिन कार्य है कि मौजूदा कालखण्ड की राजनीतिक/ साहित्यिक गतिविधियों में समाहित जातिगत उटा-पटक से भारतीय समाज में जातियां कमजोर हो रही हैं........उल्टे और मजबूत हो रही हैं। कारण है कि मौजूदा राजनीति केवल और केवल धर्म और जातियों की गुटबन्दी/जुगलबन्दी पर आधारित है। इस प्रकार ब्राह्मणवाद का उद्देश आज भी स्थाई बना हुआ है। केवल उसका वर्चस्व और उसकी रणनीति समय के साथ बदलती रहती है। साम, दाम, दण्ड और भेद वाली नीतियां आज भी जिन्दा हैं। किंतु दलित राजनीति बिखरती जा रही है। ये भी कहा जा सकता है बहुजन समाज अपने ही जाल में फंसता जा रहा है।
0000
राजशाही के शिकंजे में कसमसाती लोकशाही
किसी भी देश अथवा स्थान पर शासन करने की प्रणालियों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र तथा तानाशाही इत्यादि कई सारी शासन प्रणालियां हैं। ऐसी प्रणाली कि जिसमें केवल एक व्यक्ति ही शासन का अधिकारी होता है, ऐसे शासन प्रणाली को राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र में राजा ही प्रजा का सर्वेसर्वा होता है। अगर दुनिया में सबसे पुराने शासन पद्धतियों के बात की जाए, तो उसमें राजतंत्र सबसे प्राचीन है। आधुनिक युग में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत में भी आज से दशकों पहले राजतंत्र हुआ करता था। कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्राचीन समय में लगभग हर देश में राजतंत्र कायम था, जो आज कुछ प्रतिशत में लोकतंत्र में परिवर्तित हो चुका है। राजतंत्र को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें राजशाही तथा पूर्ण राजशाही का समावेश होता है। पूर्ण राजशाहीतानाशाही का ही एक रूप माना जा सकता है।
जिस प्रकार लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था सीधे जनता के हाथ में होती है और लोग ही देश के तथाकथित तौर पर सर्वे सर्वा माने जाते हैं। उसी तरह राजतंत्र में भी शासन केवल राजा के हाथों में होती है। आज भी दुनिया के कई देशों में राजशाही शासन व्यवस्था है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यह वाक्य अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र के परिभाषा के रूप में कहीं गई सबसे प्रसिद्ध वाक्य है। इसके विपरेत राजतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केवल राजा को ही शासन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। राजतंत्र में प्रजा की कोई भी भागीदारी सत्ता में नहीं होती है।
विदित हो कि लोकतंत्र में सत्ता को चुनने के लिए एक चुनाव प्रणाली होती है जिसके तहत जनता ही मतदान करके अपने नेताओं को चुनते हैं, जो केंद्र में सरकार बनाते हैं। और राजतंत्र में प्रजा अपने राजा को नहीं चुनती है। यहां कोई भी मतदान प्रणाली नहीं होती, जिससे कि प्रजा अपने शासक को चुन सके। यह सिर्फ राजवंशों द्वारा ही तय किया जाता है कि राजा कौन बनेगा।
लोकतंत्र में चुनाव में जीते हुए लोग जब शासन व्यवस्था संभालते हैं, तो वे ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान करते हैं, जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। इन नियम कानूनों के लिए सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होती है। किंतु राजतंत्र में राजाओं की कोई भी जवाबदेही अपने प्रजा के प्रति नहीं होती है। वह जब चाहे तब कोई भी नियम कानून बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं, इसमें प्रजा की कोई भी भूमिका नहीं होती।
इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि लोकतंत्र में शासन करने वाली सरकार पूरी तरह से लोगों के प्रति उत्तरदाई होती है। यदि सरकार किसी भी अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती है, तो उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा यदि लोग चाहे तो शासकों को अपने पद से हटवा भी सकते हैं। किंतु राजतंत्र में राजा अथवा रानियां किसी भी प्रकार से प्रजा के प्रति उत्तरदायि नहीं होती। यहां तक कि लोगों को इतनी शक्ति नहीं होती, कि वह राजा को उसके पद से हटा सके।
लोकतंत्र में सामान्यत: सभी की भागीदारी एक समान होती है, चाहे वह किसी भी तबके का हो। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाता और सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। राजतंत्र में समानता नहीं देखी जाती है। यहां अधिकतर उन्हीं लोगों को सम्मान दिया जाता है, जो राजवंश से ताल्लुक रखते हैं अथवा अमीर घराने के होते हैं। आम जनता को उतनी समानता प्रदान नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन के चार प्रमुख स्तंभ हैं - न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया।
इनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, ताकि सभी को निष्पक्ष न्याय मिल सके। लेकिन राजतंत्र में राजा ही कानून बनाने वाला, उसे लागू करने वाला और लोगों को न्याय देने वाला होता है। कई बार इसी कारण राजा निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाता है। देश का शासन संभालने के लिए लोकतंत्र में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, जिसमें कई पार्टियां अथवा पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक साथ सत्ता में बने रहते हैं। इस तरह शासन का बागडोर स्थिर नहीं रहता है। लेकिन राजशाही शासन व्यवस्था में राजा का शासन पर एकाधिकार होता है। और राजवंश से ताल्लुक रखने वाले लोग ही अगले शासक चुने जाते हैं।
स्मरणीय है कि भाजपा नीत भारत सरकार को अपने पहले टर्म में आर्थिक मसलों, खासकर महंगाई के मोर्चे पर अधिक सवालों का सामना नहीं करना पड़ा था। किंतु भाजपा की सरकार फिलहाल रोजी-रोटी के मसले से पूरी तरह से घिर गई है तब ही तो पी एम मोदी ने एलान किया है कि फ्री में मिलने वाला राशन अब अगले 5 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है जिसका देश के 80/81करोड़ जरूरतमंदों को भोजन की गारंटी देने वाली इस योजना का लाभ होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी भूख से लड़ने को मजबूर है। क्या इस पर यह सवाल करना नहीं बनता कि भारत में अति गरीब लोगों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। फिर हमारे प्रधान मंत्री जी इस प्रकार की घोषणाएँ करके किस प्रकार का एहसान जताने का प्रयास करते हैं? क्या उन मतदाताओं पर जिनके मतों के बल वो प्रधान मंत्री पद पर आसीन हो पाए हैं? क्या गरीबों को दिए जाने की कीमत की भरपाई जनता से वसूले करों से नहीं की जाती?
रही किसानों की बात तो भारत में किसानों की आत्महत्या 1990 के बाद पैदा हुई स्थिति है जिसमें प्रतिवर्ष दस हज़ार से अधिक किसानों के द्वारा आत्महत्या की रपटें दर्ज की गई है। 1997 से 2006 के बीच 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या की थी। विदित हो कि भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है तथा मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलों का नष्ट होना किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का मुख्य कारण माना जाता रहा है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां समस्याओं के एक चक्र की शुरुआत करती हैं। बैंकों, महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्र में फँसकर भारत के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने आत्महत्याएँ की है। ऐसा कहा जाता है कि सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूक रहा। देश में हर महीने 70 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को आत्महत्या की दशा तक पहुँचा देने के मुख्य कारणों में खेती का आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होना तथा किसानों के भरण-पोषण में असमर्थ होना है।
हाल मेंकिसानों द्वारा एम एस पी को कानूनी दायरे में लाने के लिए आयोजित आंदोलन को कमजोर करने के लिए हरियाणा राज्य और केंद्रीय सरकार ने पूरा जाल बिछा रखा है। किसानों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जैसा कि किसी दुश्मन पड़ोसी देश के साथ किया जाता है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कों पर न केवल बड़ी-बड़ी सिमेंटिड दीवारें खड़ी कर दी गई, अपितु सड़कों पर जगह-जगह सरियों के कांटे बिछा दिए गए हैं। क्या इसे किसी तानाशाह के व्यवहार से अलग करके देखा जा सकता है?
उल्लेखनीय यह भी है कि खेती आजकल घाटे का धंधा बन गई है। दुनिया का और कोई धंधा घाटे में नहीं चलता, पर खेती हर साल घाटे में चलती है। अत: किसानी के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। किसान अब किसानी करना नहीं चाहता। इस सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान को अपनी उपज का यथोचित दाम नहीं मिलता क्योंकि उसकी उपज की कीमत सरकार तय करती है जो वर्षों से की भी नहीं गई। किसानों का आंदोलन भी सरकार की मनमानी के चलते जैसे पूरी तरह से विफल हो गया। इसके ठीक उलट, पूंजीपतियों/ उद्योगपतियों अपने उत्पाद की कीमत अपने स्तर पर मनमानी कीमत करते हैं। सरकार का जैसे इस बारे कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीपतियों/उद्योगपतियों के उत्पादों की बढ़ी किमतों का भार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम पायदान के उपभोक्ता पर ही पड़ता है। यही कारण है कि किसान हमेशा घाटे में और पूंजीपति/उद्योगपति लाभ में रहता है। दलितों / महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार की गिनती करना जैसे संभव ही नहीं है। सरकार है कि इस ओर से मुँह मोड़े हुए है। मणीपुर की घटना का तो उल्लेख ही क्या किया जाए?
भाजपा के शासन काल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बैंकों का कर्ज चुकाए बिना ही विदेश भाग गए और बैंक मुँह ताकते रह गए। और सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करने का मन नहीं रखती। 8 वर्ष पहले विजय माल्या 9000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग गए या भगाए गए? माल्या ने कर्ज न लौटाने का दोष उलटे बैंकों पर ही मढ़ दिया ,''बैंकों ने उस खतरे को भांपने के बाद ही लोन दिया था। लोन देने का फैसला बैंकों का था, हमारा नहीं । ईडी ने 17 बैंकों को नोटिस देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करदी। हैरत की बात है कि राज्यसभा सांसद के रूप में ये माल्या का दूसरा टर्म है। पहली बार 2002 में और इसके बाद 2010 में। दूसरी बार वो कर्नाटक से बतौर इंडिपेंडेट कैंडिडेट इलेक्ट हुए थे। एक पंक्ति में कहें तो भारत के 25 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर (Willful Defaulters) ( पूंजीपतिओं) पर देश की विभिन्न बैंकों का लगभग 58,958 करोड़ रुपये बकाया है। उल्लेखनीय है कि देश के अनेक पूंजीपतियों पर अपना बकाया वसूलने के लिए न तो बैंक ही दवाब बनाते हैंऔर न ही सरकार। बड़े लोन वाले पूंजीपतियों के लोन को या तो सरकार माफ कर देती है या फिर कर्ज लेकर विदेश भाग जाने का उपक्रम करते हैं। ऐसे जाने कितने ही मामले है। सत्तासीन राजनीतिक दल इस लिए भी शांत रहता है क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए पूंजीपति ही तो आर्थिक मदद करते हैं। विदित हो कि बैंकों में जमा अधिकतर धन उन गरीब लोगों का ही होता है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी बचत को बैंकों में जमा करते हैं।
"प्लेटो सत्ता के शीर्ष पर जिन विशेषज्ञों को चाहते थे, वे विशेष रूप से प्रशिक्षित दार्शनिक होने चाहिए। उन्हें उनकी ईमानदारी, वास्तविकता की गहरी समझ (आम लोगों से कहीं ज़्यादा) के आधार पर चुना जाना चाहिए।" किंतु लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर मतदाता अपना नेता चुनते समय उम्मीदवार के रूपरंग, जाति, समुदाय, राजनीतिक दल विशेष आदि को नहीं भुला पाते। फिर होता यह है कि लोकतंत्र में धीरे-धीरे सत्ता का स्वरूप बदलता जाता है और लोकतंत्र में तानाशाही पनपने लगती है। और इस तरह की सरकार का स्वरूप अभिजात्य वर्ग का शासन कायम हो जाने का डर बना रहता है। फिर होता यह हे कि सत्ता जनता की हितों को साधने और “बेहतरीन लोगों की सरकार" चुनने में बेअसर होती चली जाती है। उल्टे होता ये है कि सत्ताधारी पक्ष सता में आने के तुरंत बाद अगले चुनाव को जीतने और अपनी पूरी ज़िंदगी नेता बनने के लिए तैयारी करने में व्यस्त रहते हैं। और सत्ता गणतंत्र को चलाने की ज़िम्मेदारी को सार्थक रूप से न ही तोनिभा पाती और न ही समाज के लिए बुद्धिमतापूर्ण फ़ैसले नहीं ले पाती है। यदि जनता के हक में कुछ निर्णय लिए भी जाते हैं तो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के भाव से लिए जाते हैं। परिणामत: आदर्श समाज हमेशा पतन की कगार पर खड़ा रहता है।
यथोक्त के आलोक में गंभीरता से देखा जाय तो आज हमारे लोकतंत्र की स्वायतता तानाशाही में बदलती जा रही है। सरकार पर किसी का कोई अंकुश नहीं रह गया है। सरकार बिना पगाह के बैल की तरह आरचरण करने में लगी है। स्वतंत्र कहे जाने वाली तमाम सरकारी ईकाइयां सरकार के इशारे पर केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर ही दंण्डात्मक कार्यवाही करने पर उतारू रहती है। हाँ! अपवाद स्वरूप सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी एक-दो केस दायर कर विपक्ष के इस आरोप को नकारने का असफल प्रयास करती है कि सरकार की ई डी, सी बी आई, आयकर जैसे आदि विभाग सत्तापक्ष पर भी नजर रखते हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसी ईडी ने लगातार सक्रियता दिखाई है। वह एक के बाद एक कई छापे मार रही है और गिरफ्तारियां भी कर रही है। हालांकि ईडी के निशाने पर लगभग सारे विपक्षी नेता और राजनीतिक दल ही रहे। इसी वजह से इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई। विपक्षी दल ईडी को सरकार और बीजेपी का टूल बताने लगे हैं। सरकार ईडी को स्वतंत्र एजेंसी बताकर उसके कदमों को डिफेंड तो कर रही है, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि ईडी की ओर से की गई कार्रवाई में बाढ़ सी आ गई है। विपक्ष के अधिकाधिक कद्दावर नेताओं को ईडी के जरिए जेलों में डाला जा रहा है। हैरत की बात ये है कि सत्ताधारी पक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ ईडी का कोई भी उदाहरण नहींहै।
सरकार और बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं पर कसते ईडी के शिकंजे को करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में प्रॉजेक्ट कर रही है। वहीं विपक्षी दल इस मसले पर जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इसे अपने नेताओं को परेशान करने या विपक्ष शासित राज्य को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा बता रहा है। कुल मिलाकर संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में ईडी की तमाम कार्रवाई अगले आम चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि क्या चुनावों में भ्रष्टाचार निर्णायक मुद्दा बन सकता है? इसका परिणाम क्या होगा या जनमानस पर इसका असर क्या होगा? इस मामले में अब तक के ट्रेंड विरोधाभासों से भरे रहे हैं। 2014 के बाद विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना उछाल पाकर , 95 फीसदी का आंकड़ा छू गया है। ईडी (ED) की केसबुक में विपक्षी राजनेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसा मत आम है। विपक्षी नेता भी लगातार इसे लेकर आवाज उठाते रहे हैं।
तानाशाही, सरकार का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति होती है। तानाशाही , सरकार का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति होती है। तानाशाही शब्द लैटिन शीर्षक तानाशाह से आया है , जो रोमन गणराज्य में एक अस्थायी मजिस्ट्रेट को नामित करता था जिसे राज्य संकटों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती थीं। हालाँकि, आधुनिक तानाशाह प्राचीन तानाशाहों के बजाय प्राचीन तानाशाहों से मिलते जुलते हैं। ग्रीस और सिसिली के अत्याचारों के बारे में प्राचीन दार्शनिकों के वर्णन आधुनिक तानाशाही को चित्रित करने की दिशा में बहुत आगे जाते हैं। तानाशाह आमतौर पर निरंकुश राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए बल या धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, जिसे वे धमकी, आतंक और बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता के दमन के माध्यम से बनाए रखते हैं । वे अपने सार्वजनिक समर्थन को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार की तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते पाँच महीनों से जारी हिंसक संघर्ष के बीच गत दिनों मणिपुर की दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह घटना क्रम सबने देखा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने भी मणिपुर की घटना का ज़िक्र करते हुए केवल कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। लेकिन मणीपुर का दौरा आज तक नहीं किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के न बोलने को लेकर लंबे समय से सवाल उठा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट द्वार इलेक्ट्रोरल बाँड पर रोक लगाने के बाद भाजपा की भौंए तन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि इलेक्तट्रोरल बोंड के जरिए राजनीतिक दलों को पूंजीपतियों द्वारा दिए गये चंदे के बारे में यह जानना चाहिए कि कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा दे रही है। उसका मालिक किसका दोस्त कहा जाता है। उस कंपनीयों को मोदी सरकार ने अपनी नीतियों से क्या-क्या दिया? चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भाजपा द्वरा की गई खुल्ल्म्खुल्ला हेराफेरी , क्या राजशाही की मार्ग प्रशस्त नहीं करती? सरकार की इस प्रकार की गतिविधियों के चलते यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अगर 2024 में BJP जीती तो 2024 का आमचुनाव अंतिम चुनाव होगा। 2024 के बाद आने वाले वर्षों में शायद ही कोई आमचुनाव होगा और नरेंद्र मोदी जी ‘नरेंद्र पुतिन' बन जाएंगे। इस प्रकार की सोच केवल राजनीतिक दलों की ही नहीं अपितु आम जनता का भी ऐसा ही विचार है।
अफसोसनाक सत्य है भाजपा सरकार आम चुनाव 2024 को जीतने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और फौजी अफसरों का राजनीतिक प्रयोग करने में नहीं हिचक रही है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कुकृत्य पर कोई एक्सन लेने में मौन दिखाई देती है। क्या सरकार के इस तरह के प्रयोग तानाशाही की ओर बढ़ते कदम के रूप में नहीं देखे जाने चाहिएं?
यथोक्त के आलोक में आजकल भारतीय लोकतंत्र में धीरे-धीरे सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री में राजशाही के गुण अवतरित होते जा रहे हैं। राजतंत्र की तरह लोकतंत्र की राजा भी यह सोचने लगा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे 95% जनता को भिखारी बना दें और उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता को अपने हाथ से न जाने दे। कहा तो ये भी जाता है कि जब सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने कुछेक विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें और 95% जनता को भिखारी बना दे।उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। ऐसा आजके भारत में होता हुआ भी दिख रहा है। यूं भी कहा जा सकता है कि भाजपा के शासन काल में भारतीय लोकतंत्र राजशाही की बाहों में फंसकर बुरी तरह कसमसा रहा है।
0000
संविधान को बदलकर भाजपा कर रही है मनुवाद से राष्ट्र को चलाने की साजिश
रोजमर्रा की दिनचर्या में न जाने कितनी प्रकार के अर्थात भिन्न-भिन्न प्रकृति के ख़याल आते-जाते हैं, इतना ही नहीं नित्य-प्रति न जाने कितनी ही घरेलू और देश की विभिन्न समस्याओं से रुबरू होना पड़ता है। चिंतन-मनन की रह-रह कर सुलझती और उलझती गुत्थियों में अनायास ही समाधान के उत्कृष्ट तरीके बनते /बिगड़ते नज़र आते हैं। बहुत से मूल्यवान निष्कर्ष जब कागज पर नहीं लिखे जा पाते हैं, तो उनकी अकालिक मृत्यु मन को दुखा जाती है। लेकिन यदि कागज पर उतर आते हैं तो समाज को जितना अब तक समझा जा चुका है, उससे आगे सोचने का मार्ग प्रशस्त होता है। नित्य-प्रति समाज और देश से जुडना, नित्य-प्रति समाज और देश से निजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुलाकातें और नित्य-प्रति की नई वैचारिक उधेड़-बुन, जब आगे तक जाती हैं, तो अपनी सही और व्याप्क भूमिका अदा करती हैं।
एक सच्चे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के मत/वोट का बराबर एक मूल्य होता है । इसका निर्धारण मतदाता की जाति, धर्म, लिंग, भाषा, या सामाजिक -आर्थिक स्थिति से नहीं किया जाता । लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता कानून का शासन (rule of law) है। जिसके लिए लोकतंत्र की एक अहम शर्त यह है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों।
किंतु आज के भारत में जैसे लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है। देश की लोकशाही पर तानाशाही हावी होती जा रही है। फलत: जनता और सत्ता के बीच अलगाव जैसी स्थिति बनती जा रही है।सत्ताधारी भाजपा और इसकी पैत्रिक संस्था येन-केन प्रकारेण संविधान को बदलने की जुगत लगाती रहती है। यूँ तो संविधान को बदलने का आर. एस. एस का कोई नया एजेंडा नही है। भारतीय संविधान भारत की शान है, लेकिन अब इसी संविधान को बदलने की मांग उठने लगी है। लेकिन अब सरकार में बैठे कुछ बड़े पदों पर बैठे लोग भी संविधानको बदलने की मांग करने लगी है।भारतीय संविधान को बदलने की मांग करने वाला व्यक्ति विवेक देबरोय है।लोग इसे बाबा साहेब के संविधानपर हमले की तरह देख रहे हैं,क्योंकि ये मांग करने वाले व्यक्ति गली का कोई गुंडा नहीं है, कोई छोटा व्यक्ति भी नहीं है, संघी मानसिक्ता का व्यक्ति है। पिछले दिनों में ऐसे कुराफाती लोगों द्वारा संसद भवन के बाहर भारतके संविधान की प्रतियां भी जलाई गई थी, लेकिन उन पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है। ये व्यक्ति कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, जो इस तरह की हरकत कर रहा हो।विवेक देबरोय व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री की सलाकार समिति का अध्यक्ष है, वो Economic Advisory Council का चेरमेन भी है। इसलिए ये मामला बेहद अहम हो जाता है कि भारतीय संविधान को बदलने की मांग कहां से हो रही है।
आप सब जानते होंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी संविधान समीक्षा के बहाने एक समिति बनाई थी और उसको ये काम सोंपा गया थाकि वो भारतीय संविधान की समीक्षा करे ताकि संविधान को बदला जा सकेकिंतु बाद में उनकी सरकार चली गई । इस प्रकार उनका काम अधूरा रह गया। लेकिन भारतीय संविधान को आज भी बदलने की कोशिशें जारी हैं। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान सभी को समानता, न्याय की गारंटी देता है, सबको मताधिकार देता है, सबको हर काम करने, अपने मन से घुमने-फिरने, अपनी वाणी की अभिव्यक्ति धर्म की आस्थाकी आजादी देता हैजो भाजपा और भाजपा की पैत्रिक संस्था आर एस एस उसको बदलना चाहती है। संघी सोच के लोग भारत के संविधान को मानते ही नहीं हैंलेकिन भारत का संविधान इस देश का सबसे बड़ा कानून हैकितु संघ परिवार संविधान को बदल देना चाहता है। यहां तक कि बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व की राजनीती करने वालेकटरपंथी लोग हैं, वो तो ये भी दावा करते हैंकि मनुस्मृति को लागू किया जाना करना चाहिए जो हिंदु धर्म के पैरोकारों का विवादित ग्रंथ है।
संविधान को बदलने की बात को लेकर भड़के विपक्ष ने कहा- बीजेपी-RSS की घृणित सोच आई सामने आई है। इस पर न तो आर एस एस की कोई टिप्प्णी आई है और न ही भाजपा सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने देश को नया संविधान दिए जाने की जरूरत बताई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय के संविधान को लेकर लिखे एक लेख पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जेडीयू और आरजेडी ने लेख को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा, बिबेक देबरॉय ने जो कहा है उसने बीजेपी, RSS के घृणित सोच को फिर सामने ला दिया है। राजीव रंजन ने कहा, इस तरह की कोशिशों को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने भारत के संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया और कहा कि बिबेक देबरॉय सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा, बिबेक देबरॉय कभी भी आर्थिक नीतियों पर विचार व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन दूसरे क्षेत्रों के विषयों पर चर्चा करते हैं जिसकी जानकारी उनको नहीं है। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, ये बिबेक देबरॉय की ज़ुबान से बुलवाया गया है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा हो रही तो और डालो और फिर कहो कि अरे! ये मांग उठने लगी है। मनोज झा ने कहा, संवैधानिक मूल्य पूर्णतः अधिनायकवाद का लाइसेंस इन्हें नहीं दे रहा है इसलिए खटक रहा है। संशोधन और पूरा संविधान बदलने में अंतर हैं। आरजेडी नेता ने कहा, मोदी जी के देश में असामनता चरम पर है। विधान बदलने की ज़रूरत है संविधान बदलने की नहीं। झा ने आगे कहा, ये चाहते हैं कि वैसा कानून बने, जहां के राजा के मुख से निकला शब्द ही कानून हो। माला डाल देने से विचार आत्मसात नहीं होते जब से केंद्र में बीजेपी सरकार सत्तारूढ़ हुई है, उसके मंत्री, जन प्रतिनिधि और नेता समय-समय पर अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। कभी कोई देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कभी कोई संविधान के बारे में कुछ भी बोल देता है तो कभी कोई समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक तबकों को धमका देता है। इस प्रकार की मौखिक अराजकता को लेकर दिख रही चुप्पी गैर-जिम्मेदार लोगों का हौसला बढ़ा रही है। ऐसा लगता है जैसे देश में राजतंत्र चल रहा हो और बीजेपी के नेता यहां जीवन भर अपना शासन चलाने के लिए अधिकृत कर दिए गए हों। आश्चर्य है कि इनकी अनर्गल बयानबाजी को कोई नियंत्रित करने वाला भी नहीं है। एकाध बार प्रधानमंत्री ने घुमा-फिराकर इसकी आलोचना जरूर की, पर उसके बाद वह प्राय: चुप ही रहे हैं। दरअसल संविधान पर पुनर्विचार आरएसएस का 'हिडेन एजेंडा' है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित हैं और इसे बदले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद इस पर ग़ौर किया जाना चाहिए। 'संविधान पर पुनर्विचार आरएसएस का 'हिडेन एजेंडा' है'। संघ का तर्क है कि संविधान तो बीच-बीच में बदला जाता है, कई बार इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस किस तरह के बदलावों की बात कर रहा है वो सेक्यूलर संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसकी तो इजाज़त ही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई फ़ैसलों में कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। चाहे उनके पास दो तिहाई बहुमत ही क्यों ना हो, संविधान को इस तरह से नहीं बदला जा सकता कि उसके मूल आधार ही ख़त्म हो जाए। धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल स्तंभ माना गया है।
किंतु देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने गए दिनों में जयपुर में जिस तरह से विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण का सवाल उठाया, वह सामान्य नहीं है। दोनों ने पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही कि जिस तरह से विधायिका न्यायिक फैसले नहीं दे सकती, उसी तरह न्यायपालिका को भी कानून बनाने का अधिकार हड़पने की कोशिशों से बचना चाहिए। ध्यान रहे, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खुद एक अच्छे वकील रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ऐसे में उनका यह कहना मायने रखता है कि संविधान की बुनियादी संरचना की अक्षुण्ता से जुड़े बहुचर्चित केशवानंद भारती मामले में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत परंपरा स्थापित करता है। उनकी दलील है कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है। ऐसे में संसद में पारित किए गए कानून को कोई दूसरी संस्था अमान्य करार दे तो फिर संसदीय सर्वोच्चता रह कहां जाती है।
दूसरी बात यह है कि चाहे संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत हो या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में, इन सबका मूल स्रोत देश का संविधान ही है। शासन के सभी महत्वपूर्ण अंग संविधान से ही शक्ति लेते हैं। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता असंदिग्ध और निर्विवाद है। न्यायपालिका इसी संविधान की संरक्षक है। संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाली गई है। जाहिर है, सरकार के किसी फैसले या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को संविधान की कसौटी पर कसना न्यायपालिका का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। किसी भी दलील से उसे इस जिम्मेदारी से रोकने की कोशिश उचित नहीं कही जाएगी।
मूल संरचना सिद्धांत पर जोर देते हुए चिदंबरम ने कहा, “मान लीजिए कि संसद ने बहुमत से संसदीय प्रणाली को खत्म करते हुए राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने के लिए वोट कर किया या अनुसूची VII से राज्य सूची को निरस्त कर दिया और राज्यों की अनन्य विधायी शक्तियों को खत्म कर दिया। ऐसे में क्या ये संशोधन मान्य होंगे? पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने यह दावा भी किया कि धनखड़ की टिप्पणी के बाद संविधान से प्रेम करने वाले हर नागरिक को आगे के खतरों को लेकर सजग हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “असल में सभापति के विचार सुनने के बाद हर संविधान प्रेमी नागरिक को आगे के खतरों को लेकर सजग हो जाना चाहिए।”
यह कोई नई बात नहीं है जब से मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केन्द्रीय सरकार बनी है, तब से ही संविधान की अवमानना के मामलों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। हाल ही में मोदी सरकार के मंत्री अनंत हेगड़े ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बैंग्लोर में एक कार्यक्रम के दौरान अनंत हेगड़े ने कहा कि 'बीजेपी सत्ता में संविधान बदलने के लिए ही आई है।' इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष और बुद्धिजीवी मानते हैं, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती। (कर्नाटक)। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा कि संविधान में संशोधन के लिए पार्टी को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करना होगा। हेगड़े ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "संविधान में संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियों और अनावश्यक रूप से जोड़ी गई चीजों को हटाने के लिए भाजपा को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। भाजपा को इसके लिए 20 से अधिक राज्यों में भी सत्ता में आना होगा।" इससे पूर्व भी उत्तर कन्नड़ से 5 बार लोकसभा सांसद रहे अनंत हेगड़े ने सोमवार को कहा कि 'मुझे खुशी होगी कि अगर कोई गर्व के साथ ये दावा करे कि वो मुस्लिम, ईसाई, ब्राह्मण या हिंदू है, क्योंकि वो अपनी रगों में बह रहे खून के बारे में जानता है।' उन्होंने आगे कहा कि 'लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्हें क्या कहकर बुलाया जाए, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। ' कोप्पल जिले के कूकानूर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अनंत हेगड़े ने कहा कि 'वो लोग जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन वो बुद्धिजीवी होते हैं।'
अनंत हेगड़े ने आगे कहा कि 'मैं आपके आगे सिर झुकाउंगा, क्योंकि आपको अपनी रगों में बहने वाले खून का पता है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, तो आप कौन हैं, इसको लेकर संदेह पैदा होता है।' उन्होंने आगे कहा कि 'हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में संविधान बदला जाएगा। हम संविधान बदलने ही आए हैं। हेगड़े ने संविधान की प्रस्तावना पर सीधा हमला किया है। कर्नाटक के कोप्पल ज़िले में रविवार को ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यक्रम में बोलते हुए 'सेक्युलरिज़्म' का विचार उनके निशाने पर था। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या सरकार 'सेक्युलर'शब्द को संविधान से हटा सकती है? जैसी इच्छा केंद्रीय राज्य मंत्री अनंतकुमार हेगड़े ने जताई है? माना कि अब तक संविधान में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन क्या संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके?
विदित हो कि 1973 में पहली बार यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। मुख्य न्यायाधीश एस। एम। सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था। यह केस था- 'केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरला', जिसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली थी। संविधान के आर्टिकल 368 के हिसाब से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसकी सीमा क्या है? जब 1973 में यह केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो जजों की राय बंटी हुई थी। लेकिन सात जजों के बहुमत से फैसला दिया गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ़ नहीं हो सकता है।
यह केस इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसने संविधान को सर्वोपरि माना। न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा कहा और साफ़ किया कि संसद की शक्तियां संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकतीं। संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है और पूरा संविधान इसी पर आधारित है। यूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी एक बार 1976 में संशोधन किया गया है जिसमें 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को शामिल किया गया। लेकिन इससे पहले भी ‘पंथनिरपेक्षता’ का भाव प्रस्तावना में शामिल था। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता हमेशा से है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार पहले से ही लिखित है। 1976 के 42वें संशोधन में 'सेक्युलर' शब्द को जोड़कर सिर्फ इसे ही स्पष्ट किया गया था।
नवभारत टाइम्स के मत से कि जब देश के नीति-निर्माता सरकारी मंचों से अपराधियों की भाषा बोलने लगें तो फिर देश का भविष्य क्या होगा?, कत्तई सहमत हुआ जा सकता है। एक समय था यदि कोई नेता संविधान या व्यवस्था को लेकर जरा भी हल्की बात कह देता तो लोग उस पर आपत्ति करते थे। लेकिन अभी लोग भी चुप हैं। उनको समझना होगा कि यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब संविधान से मिले अधिकारों पर कैंची चलाने की कोशिशें गंभीरता से शुरू हो जाएंगी।
दरअसल आर एस एस और भाजपा को संविधान की आत्मा से कोई खास परहेज नहीं है। इनकी दिक्कत ये है कि संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहेब डा। अम्बेडकर का नाम संविधान से जुड़ा है। ये मौके-बेमौके दलित बस्तियों में समरसता भोज तो आयोजित करते हैं लेकिन छूआछूत और शोषण की पैरोकार वर्णव्यवस्था के ख़िलाफ़ चुप क्यों रहते हैं? संविधान समीक्षा करने के बहाने आर एस एस का जो मूल मकसद है, वो है - भारतीय संविधान के रचियता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम होना। आर एस एस अथवा समस्त हिन्दूवादी संगठन केवल इस बात को लेकर ही ज्यादा परेशान हैं इसलिए नहीं कि संविधान अच्छा या बुरा है।
यथोक्त की आलोक में समाज के बहुजनों/अल्पसंख्यकों और संविधान में विश्वास रखने वालो लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर संविधान को बचाने के लिए काम करना होगा। और वह काम है – 2024 के आमचुनावों में वर्तमान सत्ताधारी राजनीतिक दल को सता से बाहर करना। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस और संविधान दिवस पर जो हजारों प्रकार की यात्राएं; संविधानको घर घर बांटना; संविधान को बचाने के लिए बड़-बड़े सम्मेलन करना; संविधान बचाओ के नारे लगाना; संविधान बचाओ संघर्ष समिति गठित करना; संविधान का ये, संविधान का वो क्या। किंतु इस पर तरह तरह से गहराई से कोई बात नहीं करना चाहता। संविधान बचाने का एक नया काम मिल गया है लोगों को। पैसा इकट्ठा करने का, अपने संगठन के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्यक्रम लगाने का, अपनी नेतागिरी चमकाने की, चुनाव लड़्ने के अपने टिकट पक्का करने का, अपनी फोटो खिंचवाने का, संविधान के साथ अपना फोटो के साथ लगाने का, अपनी-अपनी करनी नाकरनी की चर्चा करने का, एक नया काम और मिल गया। कुछ दिन पहले तक यही लोग आरक्षण बचा रहे थे। अभी आरक्षण बचाने का जिक्र कोई नहीं करता। आरक्षण बचाओ, संघर्ष समिति, आरक्षण बचाओ मेला, आरक्षण बचाओ अभियान, आरक्षण ऐसा।।। आरक्षण वैसा करना सब कुछ भूल गए।
अब संविधान को बचाने का नया काम आ गया। जो लोग पुराने हैं उन्हें याद होगा कि इससे पहले लोग एट्रोसिटीज़/ उत्पीड़न बचाने के लिए उत्पीड़न विरोधी आंदोलन, उत्पीड़न विरोधी सम्मेलन, इकट्ठे होने का आह्वान करने तथा इसके लिए संगोष्ठियां सारे काम करते थे। आए रोज नेता नए नए मुद्दों को पकड़ लेते हैं। जैसे आरक्षण नहीं बचा, वैसे ही संविधान भी नहीं बचेगा अगर संविधान खतरे में है। तो पता कर लेना चाहिए कि संविधान खतरे में है या नहीं है? संविधान बचेगा तो कैसे बचेगा इस प्रकार की बात करते नजर आते है। भारत में इस बात के लिए जितने संगठन है आपस में बैठकर बात करने की वकालत करनी होगी। अलग-अलग छोटे-छोटे मुद्दों को भुलाकर आपस में एक दूसरे से उलझने से बचना होगा ताकि तमाम संगठन आपस मिलकर संविधान को बचाने के लिए काम किया जा सके। अन्यथा समाज के दलित/दमित/अल्पसंख्यकों/ अन्य समाज के गरीब तबकों को मनुस्मृति में उल्लिखित समाज विरोधी प्रावधानों का पुन: शिकर होना पड़ेगा।
भाजपा सरकर और संघ परिवार द्वारा संविधान बदलने की साजिश की जा रही। भाजपा सरकार में देश का संविधान खतरे में है। दलितों के आरक्षण पर सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है। समाजवादियों को इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। उक्त विचार सपा कार्यालय पर सपा बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल ने व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का चुनावएक चुनौती है। जिसका समाज के बहुजनों और संविधान प्रेमियों को भाजपा की संविधान बदलने की साजिश का डटकर मुकाबला करना चाहिए।
सिद्धांत रूप में संसद मतदाताओं को धोखे में नहीं रख सकती। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि यदि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो उसे संविधान को संशोधित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। सरकार को उस कानून को बदलने का अधिकार नहीं मिल जाता जिसके बल पर संसद मैं पहुँची है। बहुमत से निर्वाचित हो जाने मात्र से ही किसी को संविधान बदलने की ताकत नहीं मिल जाती।सारांशत: ऐसा लगता है कि संविधान को बदलने के बहाने देश में मनुवाद को थोपना भाजपा का मनत्व है और साथ ही साथ भाजपा मंशा देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलने की लग रही है।
0000
भारतीय राजनीति अब भगवानों को भी जमीन पर उतार लाने में सक्षम
आम विचारधारा है कि अमीर व्यीक्ति सोचता है कि हर बुराई की जड़ गरीबी है। और आम आदमी सोचता है कि पैसा हर बुराई की जड़ है। एक औसत कमाई वाले व्यक्ति की सोच है कि अमीर आदमी खुशकिस्मत या बेईमान होता है। यह जगजाहिर है कि पैसा खुशियों की गारंटी नहीं देता, उससे जिदंगी आसान जरूर हो जाती है। अमीर कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले अपना फायदा देखता है, जबकि गरीब मन की शांति को प्राथमिकता देता है। अमीर व्यक्ति दिमाग से काम लेता है जबकि गरीब व्यक्ति दिल से काम लेता है। गरीब व्यक्ति मौके को नहीं पहचान पाता जबकि अमीर व्यक्ति इसे बहुत जल्दी पहचान जाता है। इस माने में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अखाड़ों की कलाबाजी पर बात के जाए तो वर्तमान में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों का तत्कालीन और समकालीन आचरण खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है कि भारत में ‘’भगवान’ कैसे बनाए गए है या फिर बनाए जाते हैं।
तत्कालीन और समकालीन दोनों ऐसे शब्द हैं जिनके मूल्य सदा एक जैसे नहीं रहते। तत्कालीन मूल्य परम्परागत मूल्यों का हिस्सा हो जाते हैं और समकालीन मूल्य तत्कालीन मूल्यों का हिस्सा हो जाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। परम्परागत मूल्य किसी एक तत्व का सापेक्ष मूल्य नहीं होता। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक यानी सभी मान्य सिद्धांतों के अपने अपने परम्परागत मूल्य होते हैं। यहाँ पर केवल कुछेक परम्परागत राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा करने का मन है। परम्परागत राजनीतिक-सिद्धान्त में मूल्यों, आदर्शों व परम तत्वों को, बेशक वो बदल भी गए हों, सर्वोपरि स्थान ही दिया जाता है। परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त का निर्माण सिद्धान्त निर्माताओं की मान्यताओं से जुड़ा हुआ होता है। इनके सामने नूतन तथ्यों, जांच, प्रमाण तथा अवलोकन का कोई महत्व नहीं माना जाता। परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त में ही नहीं समकालीन राजनीति में भी ‘चाहिए’ शब्द का महत्व सदा बना रहता है।राजनीति सिद्धांत हमेशा एक जैसे नहीं रहते अपितु सत्ताधारी राजनीतिक दलों की मान्यताओं के अनुसार समर्थन पाते हैं या फिर विरोध का साधन बनते रहते हैं। इतना ही नहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के मतों को विरोध के जरिए ही दबाना पसंद करते हैं। सच तो ये है कि परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त में मूल्यों व मान्यताओं को इतना महत्व दिया जाता है कि राजनीतिक सिद्धान्त में निहित मानवीय मूल्यों व मान्यताओं में सकारात्मकता और नकारात्मकता का अंतर ही शेष नहीं रहता। यही कारण है कि समस्याओं का समाधान न करके पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर निरंतर सवाल दागता रहता है। जाहिर है कि विपक्ष का काम तो सत्ता से सवाल पूछने का एक संवैधानिक अधिकार है, इसके अलावा विपक्ष के पास शायद ही कोई और काम होता हो। आपातकालीन परिस्तिथियों में जरूर उसकी प्राथमिकता बदल जातो है। किंतु अफसोस तो तब होता है कि जब सत्ता पक्ष अपनी नाकामियों पर परदा डालने के लिए विपक्ष पर सवालों के गोले दागता है। वर्तमान में सवाल का उत्तर खोजने के बजाए पिछली सरकारों के इतिहास में झाँकने का निरर्थक उपक्रम करने लगते है।
पिछ्ले कुछ वर्षों में इस प्रवृति ने कुछ ज्यादा ही पैर जमाए हैं। और तो और राजनीतिक भक्तगण मौके-बेमौके नए-नए भगवानों को जन्म देतो रहते हैं। सेंट्रल डेस्क: June 22, 2020: की एक खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘Surender Modi’ वाले ट्वीट पर भारतोय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए जेपी नड्डा जी जोश में होश खो गए और बड़बोलेपन के जादूगर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही ‘Surender Modi’ हैं यानी वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों (देवताओं) के भी नेता हैं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा रविवार को यहाँ तक कह गए कि आप (कांग्रेस) के साथ तो भगवान भी नहीं हैं।’ अब तो कांग्रेस को भगवान की भाषा समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरेन्द्र मोदी कह रहें हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी सिर्फ इंसानों के ही नेता नहीं बल्कि भगवानों के भी नेता हैं।
इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि राजनीति अब निराकार भगवानों को भी जमीन पर उतार लाने में सक्षम हो गई है। यह बड़े ही दुख की बात है कि राजनीति का मूल काम लोकतंत्र की रक्षा व जनता की समस्याओं को मज़बूतो के साथ हल करना है किंतु हो इसका उलट रहा है। राजनीति को न लोकतंत्र की चिंता है और न जनता की चिंता, अगर कुछ चिंता है तो वह बस सत्ता पर बने रहने की है। यही कारण है कि आज की राजनीति बिगड़े बोलों के बल पर ही जिन्दा है। जरूरी तो ये है कि राजनीतिकभक्तगण अपने नेता या नायकोंको ज़मीन पर ही रहने दें, उसमें 'अवतरत्व' का रोपण न करें... यानी उन्हें भगवान होने का तमगा न दें। यदि ऐसा किया जाता है तो यह लोकतंत्र व संविधान के साथ विश्वासघात है। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस प्रकार की प्रवृति हिन्दू धर्म के अनुयाई भक्तजनों में ही ज्यादा पाई जातो है। अन्य धर्मों में शायद इस प्रकार की प्रवृति का नितांत अभाव है।
“संवैधानिक और कानूनी उपायों के बावजूद लोकतंत्र को कुचलने वाली शक्तियां आज पहले से अधिक मज़बूत हैं। मैं यह नहीं कहता कि राजनैतिकनेतृत्व परिपक्व नहीं है। लेकिन कुछ कमियों के कारण मुझे यह भरोसा नहीं है कि आपातकाल फिर से नहीं होगा…! (भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ;इंडियन एक्सप्रेस; 28 जून,2015) समय, शासन और सत्तारूढ़ अध्यक्षों में विभिन्नता के बावजूद असाधारण महिमा मंडन की अभिन्न मानसिकता की अविच्छन्न निरंतरता को देखकर हैरत होना स्वाभाविक है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमतो इंदिरा गाँधी ने ‘इमरजेंसी या आपातकाल’ देश पर थोपा था। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के तब के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने प्रधानमंत्री का यशोगान करते हुए एक नायाब नारे का आविष्कार किया था - “इण्डिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया”… पूरे आपातकाल के दौरान यह नारा कोंग्रेसियों की जबान पर देश भर में ताण्डव करता रहा। भारत और इंदिरा एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए या ‘एकमेव‘ हो गए। याद रखना चाहिए, विराट बहुलतामुखी जनसमूह, संस्कृति-सभ्यता-आकांक्षा- निश्चित भूभाग की चरम अभिव्यक्ति है देश व राष्ट्र। जबकि प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष का पद केवल संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। इस पद पर व्यक्ति आते-जाते रहते हैं, लेकिन देश शेष रहता है। इसलिए भारत और इंदिरा एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते।” लगता है कि आज के अन्धभक्तगण यथोक्त सत्य को नकारने का काम ज्यादा कर रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो आते-जाते रहेंगे, किंतु देश सदैव रहेगा। इसलिए अपने राजनीतिक आकाओं को भगवानों की पंक्ति में खड़ा करना न तो दल विशेष का ही भला कर सकता और न ही देश का।
कुछ वर्षों पूर्वराजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को देवी बनाने की कवायद चल रही थी। इसी तरह की एक कोशिश महाराष्ट्र में भाजपा के एक विधायक ने की है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को भगवान बनाने का यह पहला मामला है। जैसी मेरी जानकारी है, फिल्मी कलाकार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आदि के मंदिर पहले से ही बने हुए हैं। भाजपा के वर्तमान शासनकाल में नाथूराम गोडसे का मन्दिर बनाने की बात भी जोरों पर है। शायद कहीं बना भी दिया गया हो, पता नहीं। इनके पीछे के तर्कशास्त्र को भी अपने-अपने तरीके से ईजाद किया जा चुका है, जैसा कि तर्क दिया जा रहा है कि वसुंधरा का अर्थ धरतो माता होता है। यही नहीं वोहरा सिंधिया को मंदिर के माध्यम से मां कल्याणी के रूप में भी स्थापित करने जा रहे थे।।।लगता है कि हमारे देश में भगवान बनाने की परम्परा आज भी बदस्तूर जारी है और यही गुलामों की असली पहचान है।
13/10/2018 : एन डी टी वी के हवाले से खबर आई थी कि महाराष्ट्र के भाजपा प्रवक्ता अवधूत वाध ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का ‘ग्यारहवां अवतार’ बताया है। जिसका विपक्ष ने मजाक उड़ाया और कांग्रेस ने देवताओं का ‘अपमान’ करार दिया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अवधूत वाघ ने ट्वीट किया, ‘सम्मानीय प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का ग्यारहवां अवतार हैं।’ एक मराठी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘देश का सौभाग्य है कि हमें मोदी में भगवान जैसा नेता मिला है।’ उल्लेखनीय कि आज तक आर एस एस और भाजपा भगवान बुद्ध को विष्णु का दसवां अवतार बताते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि विष्णु के कितने अवतार होंगे? क्या यह आर एस एस और भाजपा की नजरों में उनके देवी-देवताओं का अपमान नहीं है? क्या यह भाजपा की राजनीतिक जमीन को हासिल करने की कवायद नहीं है? वैसे तो भाजपा प्रवक्ता अवधूत वाघ की इस टिप्पणी को ज्यादा तवज्जों देने की बात नहीं है किंतु भाजपा की संस्कृति के निम्नस्तर की झलक है, इसलिए इस टिप्पणी पर दिमाग देने की जरूरत तो है। अवधूत वाध की इस टिप्पणी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने तो यहाँ तक कहा, ‘वाघ वीजेटीआई से अभियांत्रिकी स्नातक हैं। अब इस बात की जांच करने की जरुरत है कि उनका (डिग्री) सर्टिफिकेट असली है या नहीं। ऐसी उनसे आशा नहीं थी।’ वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट (वीजेटीआई) एशिया में सबसे पुराने अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में एक है। यह वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट के शिक्षा स्तर पर भी यह एक दाग है। बताते चलें कि वीरमाता जिजाबाई तकनीकी संस्थान (वीजेटीआई) मुंबई में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1887 में स्थापित, यह एशिया के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। इसे 26 जनवरी, 1997 को अपना वर्तमान नाम अपनाए जाने तक विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान के रूप में जाना जाता था। एक मराठी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘देश का सौभाग्य है कि हमें मोदी में भगवान जैसा नेता मिला है।’ ...अब कोई वाध से पूछे - अब तक बनाए गए देवी देवता और भगवानों के बल पर देश का कितना भला हुआ है?...अथवा देश कितना सुरक्षित रहा है?...तो शायद अवधूत वाघ आसमान की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे।
यह विडंबनापूर्ण संयोग है कि देश की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपनी पुश्तैनी विरोधी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बरुआ से सौ कदम आगे बढ़ गए। कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष राहुल गाँधी की भाषा से खिलवाड़ करते हुए उन्होंने घोषित कर दिया कि मोदी जी ‘सुरेंद्र‘ हैं। हालाँकि बताया जाता है कि राहुल का मंतव्य था ‘सरेंडर मोदी’ या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं ‘समर्पण मोदी’।राहुल गाँधी ने मज़ाकिया ढंग में ‘सरेंडर’ की स्पेलिंग ‘सुरेन्डर’ लिख दी। नड्डा भी इस मामले में पीछे कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने राहुल के ‘सरेंडर’ को ‘सुरेंदर’ बना दिया। सुरेंद्र का दूसरा नाम ‘इंद्र’ या देवताओं के राजा। नड्डा जी द्वारा मोदीजी के लिए प्रयुक्त यह संज्ञा नड्डा जी पर ही उलटी पड़ गयी। जिसका अपभ्रंश हो गया ‘भगवानों का ईश्वर‘ अर्थात मोदीजी इंसानों के ही नहीं, देवताओं या भगवानों के भी नेता हैं। भाषा का मनोविज्ञान है कि व्यक्ति की उपचेतना में चिंतन-संस्कार-क्रिया-प्रतिक्रिया के अभिव्यक्ति-लोक का निर्माण होता रहता है। शब्द या भाव ‘सुरेंद्र‘ शब्द अकस्मात अभिव्यक्ति हुआ हो ऐसा नहीं है बल्कि लम्बे समय से निर्मित हुई अभिव्यक्ति-लोक की क्रिया है। स्वामी भक्ति, चाटुकारिता, चारणवृति, पदलोलुपता, व्यक्ति-पूजा जैसी प्रवृतियां व्यक्ति की विवेचनात्मक चेतना का अपहरण सबसे पहले करतो हैं। उसे विश्लेषण व तर्क शून्य बना डालतो हैं। इसके विपरीत समर्पण के भाव को बढ़ातो व गाढ़ा करतो रहतो हैं। यदि सतर्क न रहें, तो फासीवाद-नाज़ीवाद-नस्लवाद-मोबलिंचिंग जैसी मानव-विरोधी घटनाओं में इनकी परिणीति होतो रहतो है। अर्थात त्रासदियां घटतो रहतो हैं जिसका खामियाजा जन-साधारण को भोगना पड़ता है। राजनैतिक आकाओं और भक्तगणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता। हैरत की बात तो ये कि राजनैतिक आका विशेष अपने आप को भगवान के रूप में देखने ही नहीं लगता अपितु अपने आप को ईश्वर मान ही बैठता है।
इसका यह अर्थ नहीं है कि बरुआ या नड्डा इन त्रासदियों के समर्थक हैं। लेकिन, इतिहास में मानव विभीषिकाएँ इसलिए घटतो रही हैं क्योंकि प्रवृतियों की संस्थागत स्थापना होने लगतो है। भक्तजनों की प्रवृति से नेता और राज्य का वैसा ही चरित्र बन जाता है। शासक के रूप में व्यक्ति अपने आप को ईश्वरीय प्रवृतियों को आत्मसमर्पित हो जाता है। जैसे–जैसे वो ईशवरीय माया-जाल में फंसता चला जाता है, वैसे-वैसे वह जनता से अथवा जनता उससे दूर होतो चली जातो है। आखिर राजसत्ता को तो एक न एक दिन किसी दूसरे हाथ में जाना ही है। लोकतंत्र की यही एक ऐसी विशेषता है। तब ईश्वर बनाने वालों को नए आकाओं की खोज करनी होगी और ऐसे ही उनकी उम्र तमाम हो जाएगी। औरों को भगवान बनाते-बनाते खुद भगवान को प्यारे हो जाएंगे किंतु भगवान बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा।
नड्डा जी ने मोदीजी के साथ कुछ नया किया है, ऐसा भी नहीं है। अनेक नेता प्रधानमंत्री मोदी को विगत में ‘अवतार‘ घोषित कर चुके हैं। यहाँ ऊपर इसका सिलसिलेवार हवाला दिया गया है। इतना ही नहीं, कतिपय बुद्धिजीवी भी उन्हें अवतारी पुरुष कह चुके हैं। कांग्रेस से भाजपा में जानेवाले एक प्रख्यात भारतविद ने तो प्रवेश के साथ मोदी जी को ‘भगवान् का अवतार’ घोषित कर दिया था। कथित भारतविद के पिता प्रख्यात भाषाविद व पूर्व जनसंघ के वरिष्ठ नेता भी थे। सच तो ये है कि सत्ता के लालची नेता मोदी जी में ‘ईश्वरत्व’ रोप देते हैं। उन्हें ‘डेमी गॉड’ बना देते हैं। और अब तो मोदी जी ने स्वयं ये कहा है कि वो बायलोजीकल प्रोड्क्ट नहीं है, बल्कि उन्हें भगवान ने जनकल्याण करने के लिए सीधे पृथ्वी पर अवतरित किया है।
माना जाता है कि वास्तव में पिछड़े समाजों व देशों में जनता नेताओं को काफी हद तक भूमि पर देवताओं के रोल मॉडल के रूप में देखतो है। शातिर राजनीतिक दलमिथकीय मिसालों, प्रतोकों, बिम्बों, रूपकों, उपमाओं, कथाओं का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके वह मतदाताओं की भावनाओं को जाग्रत कर और फिर उसका दोहन करते हैं। मिथकों की बाढ़ में विवेक, तर्क, विश्लेषण, विवेचना बहते चले जाते हैं, शेष रह जातो है ‘भावना’ और भक्तगण इसका अकूत दोहन कर सत्ता पर काबिज़ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में लोकतंत्र हाशिये पर खिसकता चला जाता है।
राजनीतिक बुद्धिजीवियों के इस वर्तमान प्रकरण में, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बुद्धिजीवियों के विषय में लिखी गई कुछेक पंक्तियां याद आ रही हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है। वह भले ही शासक वर्ग न रहा हो। बुद्धिजीवी वर्ग वह है, जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग धोखेबाजों का गिरोह या संकीर्ण गुट के वकीलों का निकाय भी हो सकता है, जहां से उसे सहायता मिलतो है। अब आप स्वयं सोचिए कि आज की भारतोय राजनीति में क्या हो रहा है? आप ऐसे नेताओं को बुद्धिजीवियों की कौन सी श्रेणी में रखना चाहेंगे? क्या धर्म व संस्कृति के ठेकेदारों को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? कहने की जरूरत नहीं कि स्वार्थी तत्वों व अवसरवादियों ने सदैव धर्म का दुरुपयोग किया है। आतंकवाद भी धर्म के दुरुपयोग का एक बेहद घिनौना रूप है। यूं कहने को सब ये ही कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता किंतु आतंकवाद का मुख्य बिन्दु धर्म ही है, इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है।
हाल हीं माइ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खऱगे जी का यह कथन यथोक्त सोच और बल देता है। खऱगे जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अब भगवान विष्णु का 11 वां अवतार बनना चाहते हैं। खऱगे ने कहा कि सुबह उठते ही लोग अपने भगवान या गुरुओं का चेहरा देखते हैं लेकिन अब हर जगह मोदी दिखाई देते हैं। मोदी अब 11 वां अवतार बनने निकले हैं। मोदी पर धर्म और राजनीति को मिलाने का आरोप लगाते हुए खऱगे ने कहा कि जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो अच्छे और बुरे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर वोट लेना देश के साथ गद्दारी है।
सारांशत: भगवान बनने व बनाने वालों को थोड़ी चिंता इसकी भी होनी चाहिए। यह कवायद हमें सोचने पर विवश करतो है, क्या किसी व्यक्ति का नाम ही वह कसौटी है, जिसके आधार पर देवी-देवता व भगवान बनाए जाते हैं? क्या यह देवी-देवता व भगवान बनाने की प्रक्रिया इस हकीकत को पुख्ता नहीं करतो है कि अन्य देवी-देवता व भगवान भी संभवतः इसी प्रकार बनाए गए होंगे।कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजनीतिक आकाओं को भगवान बनाने की यही विकृत मानसिकता राजनैतिक सागर में जहर घोलने का काम करतो है।
0000
आमचुनाव 2024 जीतने के लिए भाजपा सरकार देश में सब कुछ बदल देना चाहती है
इस तथ्य का शुरूआत में ही उल्लेख कर देना शायद तर्कसंगत ही होगा कि आज के भारत में नित समाज विरोधी नई-नई घटनाएं घट रही हैं। इस हालत में लेखक के सामने एक द्वंद्व पैदा हो गया कि न चाहकर भी अलग-अलग घटनाएं , सांकेतिक रूप से ही सही,किसी भी लेख में परिलक्षित हो जाती हैं। शायद पाठकों को इस लेख में भी ऐसा कुछ एहसास होना मुमकिन है।
प्लेटो ने क्यों कहा था, लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है? टीम बीबीसी (1 मार्च 2021) के जरिए आदर्श राठौर ने बताया कि लोकतंत्र की पालक कहे जाने वाले एथेंस के दार्शनिक प्लेटो ने अब से 2400 साल पहले अपनी किताब 'द रिपब्लिक' के छठवें अध्याय में जो सवाल उठाया था वो ये है - “क्या ये बेहतर नहीं होगा कि चुनाव के माध्यम से नेता तय करने की जगह राज्य का नेतृत्व करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को तलाश किया जाए?” यहाँ यह देखने की बात है कि वर्तमान की दुनिया में लोकतंत्र के मुखिया तानाशाही की प्रवृति के शिकार होते जा रहे हैं। चीन और रूस इस तथ्य के प्रमाण हैं जहाँ ‘एक देश एक मुखिया’ की राजशाही विद्यमान है। लगता है आज भारत भी इनकी राह पर चलती नजर आ रही है। तानाशाह अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए अनेकानेक समाज विरोधी प्रावधान करने का साजिश रचते ही रहते हैं। इस हेतु सबसे बड़ी विडंअबना है कि तानाशाह हमेशा चाहता है,“ जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने दो तोन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें. 95% जनता को भिखारी बना दें। लोकतंत्र की प्रशासनिक ईकाइयों जैसे देश के मीडिया, तमाम जाँच एजेंसियों, चुनावी व्यवस्था, और तो और न्यायिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया जाय और उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी।
यथोक्त के आलोक में आज की भाजपा सरकार देश में सबकुछ बदल देना चाहती है, वह भी शिक्षा प्रणाली/विषयों के माध्यम से...सड़कों के नाम, इमारतों के नाम यानी कि इतिहास को बदलने की कवायद। पर ये सफल होने वाली कवायद नहीं है।...हिम्मत है तो बदलो...इंडिया गेट का नाम, तोड़ सकते हो तो तोडो...लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पुराना किला, तुगलक की मजार, मीर की मजार, गालिब की मजार, देश का सर्वोच्च भवन..’संसद भवन’, साथ ही राष्ट्रपति भवन जो भारतीय सम्पदा तो है किंतु देन तो मुगलों और अंग्रेजों की ही है।...भारत कुछ अपने द्वारा बनाई गई सम्पदा के नाम तो गिनाए?...भारत के नेताओं ने तो केवल धर्मिक और जातीय दुराव फैलाने के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं...। यहाँ तक कि गांधीजी द्वारा लिखित किताब ‘स्वराज हिन्द’ न केवल समाज विरोधी है अपितु देश के विकास में एक अवरोधक भी है। शायद भाजपा और गांधी जी के मनसूबों में सामाजिक हितों को साधने का कर्म शामिल ही नहीं है। मीडिया सत्ता की गोदी में बैठकर केवल हिन्दू-मुसलमान करने में लगा है। सत्ता से प्रश्न करने के बदले विपक्ष से सवाल करके अपने दायित्व की इतिश्री कर लेता है। जनता के सरोकार तो आजकल जैसे मीडिया के विषय नहीं रह गए हैं। राम मन्दिर के जिस अंकुर को कांग्रेस ने रोपित किया था भाजपा उसी के पालने पोसने में लगी हुई है। अब जबकि राम मन्दिर के निर्माण का मार्ग भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है तो भाजपा और नए नए एजेंडों की तलाश में लग गई लगती है। कोरोना की आगत ने सत्ता को धन जुटाने और जनता को भूखों मरने का मार्ग प्रशस्त कर ही दिया है। सरकार नाना प्रकार से केवल और केवल धन जुटाने में लगी है...इस हेतु “पी एम केयर फंड” खाता खोल दिया गया जबकि “प्रधान मंत्री राहत कोष” नामक खाते का पहले से ही प्रावधान है। हैरत की बात तो ये है कि “पी एम केयर फंड” को चलाने वाले ट्रष्ट में केवल तीन ही सदस्य हैं...प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। इस ट्रस्ट में विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं है। ज्ञात हो कि “प्रधानमंत्री राहत कोष” के संचालन के लिए छ: सदस्य हैं जिनमें तीन सत्ता पक्ष के और तीन विपक्ष के। “प्रधानमंत्री राहत कोष” का केग द्वारा आडिट किया जा सकता है किंतु “पी एम केयर फंड” और ‘इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं। “पी एम केयर फंड” और ‘इलेक्टोरल बॉन्ड्स’ के जमा-खर्च का ब्यौरा देना तो दूर की कौड़ी है। ये दोनों ही फंडस को आर टी आई की परिधि से बाहर रखा गया है। जो संविधान संगत नहीं मानी जा सकती।
यहाँ इस बात का खुलासा करना शायद विषयांतर पैदा नहीं करेगा कि 2018 से भारत एक ‘चुनावी तानाशाह’ राष्ट्र बना हुआ है। वी-डेम रिपोर्ट 'डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूज़िंग एट द बैलट (चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार)' शीर्षक वाली रिपोर्ट वी-डेम इंस्टिट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2024 में कहा गया है कि भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है।
आज देश में ताजा मसला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। विदित हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सवाल उठाते हुए एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), कॉमन कॉज़ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत पांच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार करते हुए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए मिली धनराशि की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देनी होगी। ये जानकारी चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इस पर ए डी आर के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफ़ेसर जगदीप छोकर कहते हैं, "ये फैसला क़ाबिल-ए तारीफ़ है इसका असर ये होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम बंद हो जाएगी और जो कॉरपोरेट्स की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता था जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था, वो बंद हो जाएगा। इस मामले में जो पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ने ख़त्म की थी वो वापस आ जाएगी।" इस जानकारी के सार्वजनिक होने पर ये साफ़ हो जाएगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा और किसे दिया।
किंतु स्टेट बैंक इस बाबत मामले को लटकाने का भरसक प्रयत्न किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक की बाजुओं को जोर से मरोडा तो स्टेट बैंक ने चुनावी बाण्ड की तमाम जानकारी दिनांक 21 मार्च तक चुनाव आयुक्त को मुहैया करा दिया। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदे गए थे और इसमें से ज़्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी।
स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध आँकड़ों को जब चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया तो जो आँकड़े प्रकाश में आए, वह बहुत ही चौकाने वाले हैं। प्रसारित आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी को अप्रैल-2019 से जनवरी-2024 तक चुनावी बॉन्ड के ज़रिए ₹6,061 करोड़ का चंदा मिला। इस दौरान टीएमसी को ₹1,610 करोड़,कांग्रेस को ₹1,422 करोड़, बीआरएस को ₹1,215 करोड़ और बीजेडी को ₹776 करोड़ मिले। 'आप को ₹65 करोड़, जेडीएस को ₹44 करोड़, एसएडी को ₹7 करोड़ और आरजेडी को ₹1करोड़ मिले। रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में यह प्रश्न बलवता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का चुनावी फंडिंग पर क्या असर होगा?
विगत पर नजर डालें तो आपको याद होगा, मोदी जी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा करके आय थे। लेकिन हालात ये हो गई है कि देश कर्ज के बोझ तले दबता ही जा रहा है। 67 साल तक 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलाकर कुल जितना कर्ज लिया, मोदी सरकार ने उस कुल कर्ज का भी 3 गुना कर्ज लेकर अनूखा रिकॉर्ड बना दिया है। बी बी सी के अनुसार 2014 के बाद देश पर कर्ज तेजी से बढ़ा है। कर्ज का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। IMF ने भारत को चेतावनी दी है कि उसका सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में उसके सकल घरेलू उत्पाद , यानि कि GDP के 100% से अधिक हो सकता है।
लगता है कि आज के राजनीतिक आचरण को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। सब जानते हैं कि भारत में सरकार तो भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी की भी बनी थी...बेशक झटके खा-खाकर। किंतु अटल जी ने चुनावी भाषणों में कांग्रेस के कार्यकाल की निन्दा तो जरूर की थी जो चुनावी प्रचार का हिस्सा था किंतु सरकार बनने के बाद वाजपेई जी ने खुले मन से स्वीकार किया कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कांग्रेस के शासनकाल में देश हित में जो भी काम किए, उन्हें भुलाया जा ही नहीं सकता।..उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
किंतु भाजपा के ही मोदी जी के आज के शासन में क्या हो रहा है? हिन्दू को मुसलमान से भिड़ाना/लड़ाना, किसानों के हक में भाषण तो करना,किंतु करना कुछ नहीं, नौकरियां देने की एवज पकौड़े तलने के सुझाव, अतार्किक रूप से अचानक नोटबन्दी लागू करना, देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और चौकसी को बा-ईज्जत देश से बाहर चले जाना ही आज की भाजपा सरकार की उपलब्धियां हैं। ...कमाल तो ये है - जो शार्मनाक है, सब उसकी वकालत कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह के तानाशाही रवैये के आगे भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं का नतमस्तक हो जाना, भाजपा के लिए तो अंतिम यात्रा जैसा ही सिद्ध होगा। बेहतर है भाजपा के ये तथाकथित शीर्ष नेता राजनीतिक मैदान से बाहर ही हो जाएं, अन्यथा इनका नाम लेवा तक भी कोई नहीं बचेगा। यह बात मोदी सरकार के आज के आचरण से प्रमाणित होती नजर आ रही है। यह भी कि जसवंत सिन्हा हों, शत्रुघन सिन्हा हों, सिद्धु जी हों...न जाने और भी कितने ही भाजपाई हैं जो मोदी जी और शाह के रवैये से परेशान होकर भाजपा से बाहर निकले गए। अब वो सुविधाभोगी मानसिकता से परे होकर भाजपा का विरोध करने का साहस जुटा पाए हैं। और यही मानसिकता लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है।
आज की भाजपा सरकार सब कुछ बदल देना चाहती है। वो ये सिद्ध करना चाहती है कि भारत में सबसे पहले लोहपथगामिनी (ट्रेन) लाने वाली भाजपा है, मोदी जी! की सरकार से पहले इस देश में हवाई जहाज भी नहीं दिखाई देते थे, वो तो मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद ही सम्भव हो पाया है...और महत्त्वपूर्ण तो ये है कि नेहरू के बाद केवल मोदी जी ही ऐसे शानो-शौकत वाले प्रधान मंत्री हुए है जो पिछ्ड़ी जाति के होते हुए भी नेहरू से भी बढ़तर शानो-शौकत वाली जिन्दगी जीने वाले भारतीय प्रधान सेवक जाने जाते रहेंगे। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अब तो ये लगने लगा है कि जिस व्यक्ति को अपने घर, अपने परगने, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश के हितों के इतर केवल अपनी और अपनी ही शानो-शौकत बनाए रखने की चिंता हो, तो ऐसा आदमी एक तानाशाह के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। जो राजा शानो-शौकत के लिए दिन में चार-पाँच बार लाखों-करोड़ो के लिबास बदलता हो, वह देश का बफादार कैसे हो सकता है? मोदी जी की इस प्रकार हर मौके पर बार-बार नए लिबास बदलने की प्रवृत्ति के चलते माइकल नास्त्रेडाम्स (एक यूरोपियन दार्शनिक) की यह उक्ति याद आती है कि यदि किसी भी देश का शासक अपनी जनता से ज्यादा अपने वस्त्रों पर ध्यान दे तो समझ लीजिए कि उस देश की बागडोर एक बेहद कमजोर, सनकी और डरे हुए इंसान के हाथों में है।
अब मैं अपनी बचपन की बात कर रहा हूँ कि जब मैं बचपन के दौर से गुजर रहा था तो गाँवों में होली-दीवाली पर अलग-अलग तरह के केलेंडर अथवा पोस्टर देखने को मिला करते थे...उसमें इंगित होता था किजो पर स्त्री गमन करेगा, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, जो अपने माँ-बाप का अपमान करेगा, उसे नर्क प्राप्त होगा, जो गरीबों को सताएगा, उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी और जो राजा जनता पर अन्याय करेगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा।... क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार का डरावनी घोषणाएं केवल और केवल कमजोर वर्गों में तथाकथित भगवान का डर बनाए रखने के लिए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि मोदीजी इस सब कथनों की परवाह किए बिना जैसे चाहें राजशाही का उपभोग कर रहे हैं। इस माने में, मोदी जी सच्चे ईश्वर विरोधी हैं। उनकी दिनचर्या, कार्यप्रणाली और जुल्मो-सितम भरी तानाशाही इसका प्रमाण है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि मोदी जी हिन्दुत्व की इस धारणा को भी नकारते हुए लगते हैं कि जो जैसे अपराध करेगा, उसे वैसा ही दंड मिलेगा। शायद मोदी जी को पुनर्जन्म वाली धारणा में कोई विश्वास नहीं है (...होना भी नहीं चाहिए) । तभी तो मोदी जी किसी अच्छे-बुरे की परवाह किए बिना कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं।
कहा तो यह भी जाता है कि मोदी जी बेशक तानाशाह बनते हों किंतु वो हैं तो आर एस एस के दम पर ही...वो केवल और केवल आर एस एस के मुखौटे भर हैं और यह भी कि आर एस एस तभी तक भारत में शासन में देखे जा सकते हैं, तब तक मोदी जैसे चाटुकार और स्वहित साधने वाले ही नहीं, आर एस एस को मूर्ख बनाने वाले मोदी जैसे लोग मिलते रहेंगे...कोई शक? किंतु मोदी जी आज की असंवैधानिक गतिविधियों के चलते यह शंका होती है कि अब मोदी जी अपनी ही पैत्रिक संस्था आर एस एस को भी नकारने की मानसिकता से ओतप्रोत हैं।
यहाँ यह बताते चलें किवी-डेम (वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी) इंस्टिट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2024 के अनुसार, विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही (Electoral Autocracy) वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा, जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। आज न केवल केन्द्र में अपितु देश के 20-22 राज्यों में भाजपा का शासन है।...इस पर भाजपा इतरा रही है। भाजपा को याद रखना चाहिए कि इसके मान्यवरों की भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में कोई भागीदारी नहीं रही है। सो वो ज्यादा इतराए नहीं। देश का वोटर इतना भी सुसुप्त नहीं है कि देर तक किसी को सहन कर पाए।
चलते-चलते बतादूँ कि सरकार की ई. डी. जैसी विभिन्न जांच एजेंसियां अब तक अलग-अलग मामलों में हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इनमें तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे जयललिता, चुके हैं। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। शिबू सोरेन, चंद्रबाबू नायडू, मधु कोड़ा, ओपी चौटाला और बीएस येदियुरप्पा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। (short by Monika Sharma / 03:46 pm on Friday, 22 March, 2024 ) यथोक्त के आलोक में मोदी सरकार के कुछ कारनामों के विषय में, मैं समझता हूँ,, सोशल मीडिया के जरिए अधिकतर जनता को अच्छी तरह से मालूम है। इस लेख में उन सबका का उल्लेख करना मुझे प्रासंगिक नहीं लग रहा है, किसी और लेख में उनका विस्तार से उल्लेख करने का प्रयास करूँगा
यथोक्त के आलोक में यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि देश में चुनावों का एलान हो गया है। प्रैस कॉर्मफ्रेंस आपने ध्यान से दिखली होगीऔर खास तौर पर जो सवाल जवाबपत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग के साथ किये गए। इस पूरे सत्र के बाद यकीन से कहा जा सकता है कि अबकी बार देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है।ये चुनाव आयोग और ये चुनावी व्यवस्था भारत के आम आदमी को यह सोचने को मजबूर करती है कि इस देश मेंकभी भी इस देश के लोगों को उनकी सरकार नहीं मिल सकती। जनता सरकार चुनने के लिए वोट तो देगी लेकिन सरकार शायद उनकी नहीं हो सकती। अब जो भी सरकार बनेगी जनता की नहीं होगी। सरकार के वर्तमान संविधान विरोधी कार्यकलापों से तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव लोकतंत्र के कलेजे पर एक करारा प्रहार सिद्ध होंगे। शेष भविष्य तय करेगा।
0000
सत्ता और राजनीति के दबाव में गायब हो रहे हैं मानवाधिकार के प्रश्न
मानवाधिकार पर बात करने से पूर्व यह जानना अत्यावश्क है कि मानवाधिकार क्या है। एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं।
आज जहाँ विश्वभर में राजनैतिक/ धार्मिक/ सामाजिक/ आर्थिक अराजकता का माहौल है, समाज में मानवाधिकारों का विमर्श उग्र होता देखाई दे रहा है। यह बात अलग है कि मानवधिकारों का यह विमर्श कोई सकारात्मक जगह नहीं बना पा रहा है। अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि जिन देशों में राजनैतिक/ धार्मिक/ सामाजिक/ आर्थिक अराजकता का माहौल नगण्य होता है और वे देश जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं एवं अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तीव्र गति से आर्थिक विकास करते हैं जबकि धर्मांधता को प्रश्रय देने वाले देशों में आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और निर्धनता बढ़ने लगती है। क्या देश के मौजूदा आर्थिक संकट का संबंध भी हमारी बढ़ती धार्मिक संवेदनशीलताओं से है?...क्या मानवाधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता किसी ताकतवर राष्ट्र की पहली पहचान है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा तभी मजबूत हो सकती है जब हम मानवाधिकारों के प्रश्न को गौण बनाते हुए मुट्ठी भर आतंकवादियों या अलगाववादियों के खात्मे के लिए लाखों आम लोगों के साथ भी वैसा ही कठोर व्यवहार करें जैसा किसी संदिग्ध अपराधी के साथ किया जाता है? क्या हमारा आदर्श धार्मिक कानून के द्वारा संचालित होने वाले वे देश हैं जिनका रिकॉर्ड मानवाधिकारों के संबंध में अत्यंत खराब रहा है? क्या हमारी प्रेरणा वे देश हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं? ऐसे सवालों का उठना स्वाभाविक ही है।
खबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में बढ़ रही हिंसा और बलात्कार की घटनाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव के मामलों, एक्टिविस्टों पर भीड़ के हमलों व इनकी पुलिस प्रताड़ना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों की ज्यादतियों को संरक्षण दिए जाने की प्रवृत्ति पर अनेक बयान जारी किए हैं। किंतु भारत सरकार इन रिपोर्टों और बयानों को दुर्भावनापूर्ण बताकर ख़ारिज करती रही है और इसे देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताती रही है। सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं।...किंतु सरकार के तर्क तर्कसंगत ही हों, ये जरूरी तो नहीं।
कहा तो ये भी जाता है कि दरअसल राजनीतिक नेतृत्व की असफलता का खामियाजा आम लोगों और सुरक्षा बलों दोनों को भुगतना पड़ता है। चाहे वे आतंकवादी या अलगाववादी हों या नक्सली-यह सभी आम लोगों को डरा धमकाकर उनका समर्थन हासिल करते हैं और आम लोगों के बीच जा छिपते हैं। यह आम लोगों में व्याप्त असंतोष को अपनी हिंसा की विचारधारा के समर्थन में प्रयुक्त करने में निपुण होते हैं। सुरक्षा बलों को ऐसी परिस्थितियों में काम करने को कहा जाता है जो उनके लिए सर्वथा अपरिचित होती हैं। उनके लिए निर्दोष आम आदमी, नक्सली या आतंकी की स्पष्ट पहचान करना कठिन हो जाता है। आतंकवादी और नक्सली आम लोगों को सामने रख अपनी गतिविधियां करते हैं ताकि आम लोग मारे जाएं और सुरक्षा बलों की बदनामी हो तथा जनता में असंतोष फैले।
कुल मिलाकर यह राजनीतिक नेतृत्व की असफलता का परिणाम होता है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन अथवा धार्मिक सांस्कृतिक भेदभाव के कारण हिंसा और अलगाववादी ताकतों को जमीन मिलती है। जब चर्चा, विमर्श और संवाद का सेतु भंग होता है तो सुरक्षा बलों का प्रयोग अपने ही देश के नागरिकों पर करने की नौबत आती है। जब हिंसा होती है तो उभय पक्षों द्वारा सीमाएं लांघी जाती हैं। सरकार के आदेशों का पालन सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक है। आम लोग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय सुरक्षा बलों को एक पृथक इकाई की भांति देखते हैं जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें ऐसी कठिन परिस्थितियों में कार्य करने को सरकार द्वारा बाध्य किया जाता है जिसमें गलतियों की संभावनाएं अधिक होती हैं। जब हम सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की चर्चा करते हैं तो उस सरकार की मंशा और नीतियों पर भी बहस होनी चाहिए जिसके अधीन ये कार्य कर रहे हैं।
जब हम मानवाधिकारों की रक्षा पर विमर्श करते हैं तो न्याय पालिका हमें अंतिम शरण स्थली के रूप में दिखाई देती है। किंतु पिछले कुछ समय से कुछ राजनीतिक दलों, धार्मिक-सांस्कृतिक संगठनों और सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ समूहों द्वारा न्याय पालिका पर भी यह निरंतर दबाव बनाने की चेष्टा की जा रही है कि वह ऐसे फैसले ले जो बहुसंख्यक वर्ग को स्वीकार्य हों, सरकार विरोधी न हों और सरकार की देशहित और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा से संगत हों।
स्थिति ऐसी बन जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मानो यह बीड़ा उठाते हैं कि अपनी सेवा निवृत्ति के पहले राम-जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुना देंगे, जनहित के अन्य अनेक मुद्दों पर वरीयता देते हुए लगातार 40 दिनों तक 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करती है और जब फैसला बहुसंख्यक समुदाय की आशाओं और उम्मीदों के अनुसार आता है तो मीडिया इन न्यायाधीशों का प्रशस्तिगान करते करते इन्हें रामभक्त की संज्ञा देने की सीमा तक पहुंच जाता है, लेकिन हमें इस पूरे घटनाक्रम में कुछ भी असंगत नहीं लगता। हम पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि हम न्यायपालिका से एक खास निर्णय की अपेक्षा करने लगते हैं। ऐसा ही दबाव न्यायाधीशों पर भी बनाया जाता है कि वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय दें। पता नहीं वे इस दबाव का सामना किस प्रकार करते होंगे। न्याय यदि लोकप्रियता की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहे और सरकारी फैसलों का समर्थक बन जाए तो उसे अन्याय में बदलते देर नहीं लगेगी। जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना नेताओं के लिए आवश्यक हो सकता है, न्यायाधीशों को तो न्याय की कसौटी पर ही खरा उतरना होता है।
वर्तमान परिदृश्य चिंताजनक है और मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए हमें गहन आत्ममंथन करना होगा। क्या हम एक ऐसे धैर्यहीन, हिंसाप्रिय और आक्रामक तथा अराजक समाज में बदलते जा रहे हैं जिसका विश्वास लोकतंत्र और न्याय प्रक्रिया में नहीं है। हो सकता है कि हमारी न्याय प्रणाली दोषपूर्ण हो, यह भी संभव है कि भ्रष्टाचार का दीमक हमारी संस्थाओं को खोखला कर रहा हो, यह भी हो सकता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धनबल और बाहुबल का आधिपत्य स्थापित हो गया हो किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकार दें और स्वयं कानून और पुलिस का स्थान ले लें अथवा स्वयं को अनुशासित करने के लिए किसी तानाशाह की तलाश करने लगें जिसे लोकतांत्रिक स्वीकृति देकर हम और निरंकुश बना दें। मॉब लिंचिंग की बढ़ती प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि हम अराजक कबीलाई समाज बनने की ओर अग्रसर हैं।
विदित हो कि हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जोधपुर के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि न्याय कभी भी आनन-फानन में किया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि न्याय बदले की भावना से किया जाए तो अपना वह अपना मूल चरित्र खो देता है। यह देखना एक भयंकर अनुभव था कि किस प्रकार हमारा सभ्य समाज इस एनकाउंटर को लेकर आनंदित था। चाहे वह दिल्ली का निर्भया कांड हो या कठुआ, उन्नाव, मुजफ्फरपुर और हैदराबाद में हुई बलात्कार की घटनाएं, इन सब में क्रूरता की सीमाएं लांघी गई हैं। न्याय प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण रेप पीड़ितों को न्याय मिलने में विलंब हुआ है।
कई बार आरोपियों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी मिला है। रेप पीड़ित युवतियों की सामान्य पृष्ठभूमि के कारण धन और शक्ति के समक्ष शरणागत होने वाले पुलिस तंत्र ने आरोपियों को सजा दिलाने से अधिक उन्हें संरक्षण देने में रुचि दिखाई है। यदि आरोपी रसूखदार हैं तो उन्होंने पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों पर हिंसक और जानलेवा हमले भी किए हैं और उनकी हत्या तक की है। लेकिन इस विषम परिस्थिति का किसी फिल्मी क्लाइमेक्स की भांति सरल और सस्ता हल नहीं निकाला जा सकता। इस तरह की प्रायोजित मुठभेड़ों को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा देना जल्दबाजी और भोलापन है। मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा किसी घटना विशेष को लेकर लोगों की संवेदनाओं को कृत्रिम रूप से उद्दीप्त करना और फिर उन्हें गलत दिशा देकर हिंसा को स्वीकारने और महिमामंडित करने के लिए प्रेरित करना चिंतनीय और निंदनीय है।
ऐसा लगता है कि लोगों को सुनियोजित रूप से हिंसा का आश्रय लेने के लिए मानसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिंसक भीड़ को एक जाग्रत समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और भीड़ की हिंसा को जनक्रांति की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसा की अभ्यस्त इस भीड़ का प्रयोग किया जाएगा, इस भीड़ का निशाना निर्दोष लोग होंगे-शायद वे तर्कवादी हों, धार्मिक अल्पसंख्यक हों, वंचित समुदाय के लोग हों या वैचारिक असहमति रखने वाले बुद्धिजीवी या शायद वे हमारी आपकी तरह सीधी राह पर चलने वाले डरे-सहमे, हताश, हारे हुए शहरी हों। तब हम इन घटनाओं का विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि हमारी सोच को हिंसा करने, हिंसा देखने और हिंसा सहने के लिए कंडिशन्ड कर दिया गया होगा।
भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार में डूबा है। आदिवासियों तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रकाश पहुंच नहीं पाया है और यदि पहुंचा भी है तो उसका लाभ लेकर पुराने छोटे शोषकों का स्थान लेने नए कॉरपोरेट शोषक वनों तक पहुंच गए हैं जो आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन सब उनसे छीनने पर आमादा हैं। लाखों वंचितों के लिए अभी भी सामंतशाही का दौर समाप्त नहीं हुआ है। शोषण और दमन के वे इस तरह अभ्यस्त हैं कि स्वतंत्रता और सहानुभूति मिलने पर वे घबरा जाते हैं कि कहीं यह मालिक की कोई नई रणनीति तो नहीं। हमारी पूरी व्यवस्था पर पितृसत्ता की गहरी पकड़ है। चाहे शोषक वर्ग हो या शोषित वर्ग-स्त्री की नियति में कोई विशेष अंतर नहीं देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी जाग्रत और अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग समाजों के मुद्दे ही उठाता है। कई बार मानवाधिकारों के विमर्श के पीछे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलता और कुटिलता छिपी हुई होती है। किंतु पीढ़ियों से शोषित हो रहे उन लोगों की चर्चा कभी नहीं होती जिनके मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन होता है।व्यापक दृष्टिकोण से देर्खें तो प्रशासन की जो जनविरोधी भूमिका होती है, उसमें सिर्फ प्रशासन का ही दोष नहीं होता अपितु प्रशासन राजनीतिक दबाव में ही मानवाधिकार का हनन करता है।
0000
मोदी जी पद की गरिमा के प्रतिकूल बातें क्यों करते हैं
आज की सामाजिक / राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, जब मैं अपने शिक्षाकाल पर नजर डालता ह