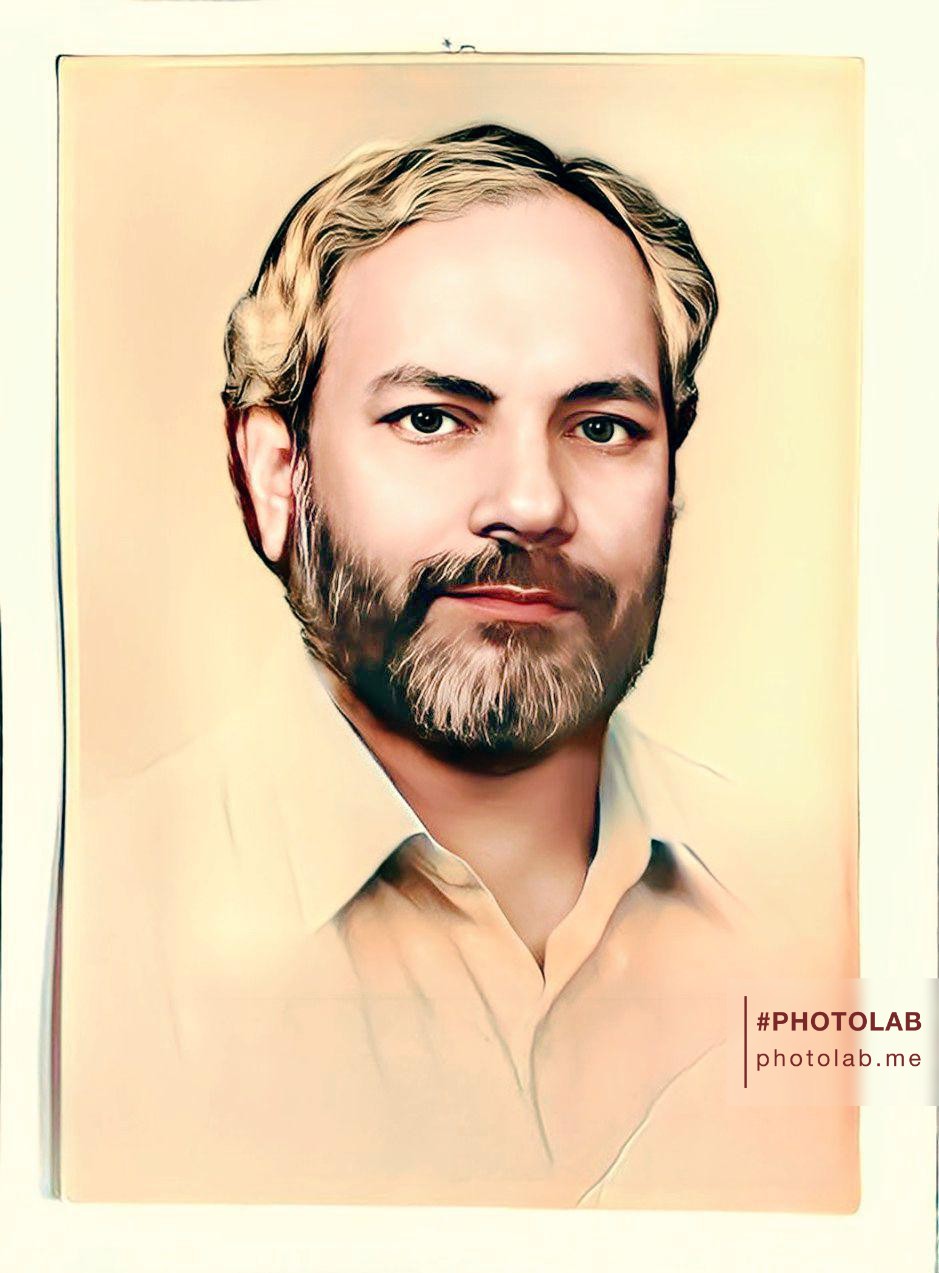प्रस्तुति - तेजपाल सिंह 'तेज'
अम्बेडकरवादी कसौटी और दलित लेखन
ईश कुमार गंगानिया
अम्बेडकरवादी कसौटी पर ‘दलित लेखन का मूल्यांकन’ मेरे लिए ऐसा है जैसाकि स्पाइन या ब्रेन की सर्जरी जैसे जोखिम को निमंत्रण देना। कहने की जरूरत नहीं कि दलित लेखन में असहमतियों के लिए ना के बराबर स्पेस है। साहित्य की यह मुहिम कमोबेश वर्तमान निजाम की तर्ज पर चल रही है, जहां सत्ता के सुर में सुर मिलाओ तो सब ठीक, वरना कुछ भी ठीक नहीं, यानी पूर्वाग्रही दुश्मनी। डा. धर्मवीर से आजीवक को लेकर वैचारिक असहमति बनी तो शांति स्वरूप बौद्ध ने ‘गद्दार सत्ता : भाग 1, मक्खलि गोसाल के मानसपुत्र’ जैसी पुस्तक संपादित कर डाली। इसमें लिखने वालों ने प्रतिशोध के चलते आजीवक को लेकर वह सब लिख डाला, जिसमें कुछ भी रचनात्मक नहीं था और नहीं लिखना चाहिए था। कंवल भारती और डा. धर्मवीर के बीच वैचारिक विवाद हुआ तो कंवल भारती ने ‘डा धर्मवीर का फासिस्ट चिंतन’ नामक पुस्तक लिख डाली। डा. धर्मवीर और ओमप्रकाश वाल्मीकि के बीच कुछ हुआ तो डा. धर्मवीर ने ‘जय भंगी, जय चमार (खण्ड एक) ‘जूठन’ का लेखक कौन?’ की श्रृंखला ही शुरु कर दी। ऐसे हालात में सार्थक संवाद या ‘बदलाव की स्थिति’ के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई खास स्पेस बचता है, लेकिन फिर भी अंधेरे के खिलाफ नई रोशनी की तलाश हर जिम्मेदार नागरिक का पहला कर्तव्य है। जाहिर है, मेरा भी है।
जोखिम इसलिए कहा कि विषय बेहद गंभीर है और मेरी पहचान विवादित, क्योंकि मैं दलित साहित्यकार नहीं हूं और आज मैं कह सकता हूं कि मैं विशुद्ध रूप से अम्बेडकरवादी साहित्यकार भी नहीं हूं। लेकिन हां, मैं अम्बेडकरवादी वैचारिकी का संवाहक जरूर हूं। मैं किसी ‘वाद’ का मोहताज रहकर अपनी वैचारिक उड़ान को बाधित/सीमित करने का पक्षधर नहीं हूं। गौरतलब है कि यह जज्बा भी मैंने अम्बेडकरी वैचारिकी से पाया है। इसलिए मेरा वर्तमान लेखन ‘न कोई वाद, न कोई विवाद, सिर्फ और सिर्फ ‘समय से संवाद’ के भाव का पक्षधर है। मैं यह मान कर चल रहा हूं कि वर्तमान चर्चा के विषय ‘अम्बेडकरवादी कसौटी और दलित लेखन’में प्रयुक्त शब्द ‘दलित लेखन’ मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए स्पेस बनाता है क्योंकि मैं भी दलित समाज से आता हूं। भले ही मेरी स्थिति दलित साहित्य में हीरा डोम ‘अछूत’ जैसी है, मगर मैं हीरा डोम की तरह शिकायत नहीं, हस्तक्षेप कर रहा हूं। मेरा हस्तक्षेप वर्ग-विहीन व जाति-विहीन समाज के निर्माण के लिए है। मेरा हस्तक्षेप सभी प्रकार के शोषण-उत्पीड़न के विरुद्ध समता, स्वतंत्रता और बंधुता के दम पर संत रैदास के ‘बेगमपुरा’ जैसे समाज/देश निर्माण में सहभागिता का हस्तक्षेप है।
जहां तक साहित्य की वर्तमान दशा का प्रश्न है, मुझे लगता है ‘साहित्य’ दो सांडों के बीच एक झुंड की तरह फंसा है। एक सांड दलित (स्त्री, आदिवासी आदि) का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा परंपरावादी/वर्चस्ववादी जातियों का। मगर एक तीसरा सांड भी है, वह दोनों से अलग खड़ा जुगाली कर रहा है। उसकी जुगाली से कितना साहित्य सृजन हो रहा है, यह अपने आप में अलग से शोध का विषय है। ऐसा लगता है, इन सांडों के बीच पूर्वाग्रही दुश्मनी के चलते संवाद, सृजन, और समाज निर्माण के लिए कोई खास स्पेस नहीं बचा है। वर्तमान साहित्य को इस स्पेस के विस्तार की जरूरत है ताकि आपसी सकारात्मक संवाद के लिए अधिक से अधिक स्पेस बने। तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले, और डा. अम्बेडकर ने भी ऐसे ही स्पेस का इस्तेमाल किया है और आज ये विश्व पटल पर छाए हुए हैं। इसे किसी सीमा तक मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं। स्पेस का सदुपयोग अम्बेडकरवाद की प्रमुख पहचान है, जो अपने पक्ष की वैज्ञानिकता, नैतिकता, सृजन और निर्माण के रूप में जानी जाती है। लेकिन वर्तमान दलित साहित्य के बारे में ऐसा कोई ठोस दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक अंधभक्त की तरह डा. अम्बेडकर और उनके साहित्य के शरणागत है, इसका प्रचारक है, मगर मुझे इसका अम्बेडकरवाद से कोई खास वास्ता नजर नहीं आता।
प्रश्न है, साहित्य में ये दो या तीन ध्रुव क्यों हैं और इनके आपसी टकराव की वजह क्या है? अगर अपवाद को छोड़ दें, परंपरावादी यानी जातिवादी समाज से जुड़ा साहित्यकार अपने जातीय वर्चस्व और इसकी पोषक परंपराओं को बनाए रखना चाहता है। इसमें इसके और इसके समाज के हित सुरक्षित हैं, जिसके चलते दलित समुदाय में इंसान के सामान्य जीवन जीने और आगे बढ़ने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं है। यह टकराव शोषक और शोषित यानी परंपरागत वर्चस्व को वंचितों की चुनौती से उपजा टकराव है। इसलिए शोषित समाज अपनी सम्मानजनक अस्मिता व वजूद के लिए संघर्षरत है। लेकिन अफसोस ‘दलित’ शब्द को अपनी अस्मिता मान बैठा है, जिसका तर्क-विवेक और वैज्ञानिकता से कोई वास्ता नहीं है। हैरत की बात है कि यह लड़ाई अम्बेडकरवाद को ठीक से समझे बगैर, इसके बैनर तले लड़ी जा रही है। जाने-अनजाने यह डा. अम्बेडकर की वैचारिकी को बोना करने के उपक्रम बनकर रह गया है। इस आलेख को लिखने के पीछे मेरा मकसद ‘दलित’ के मिथक से मुक्ति, समाज निर्माण की परिस्थितियों के लिए स्पेस बनाना और इसके सदुपयोग के विकल्प तलाशना है। गौरतलब है, ‘दलित’ शब्द है और रहेगा भी, समाज के स्तर पर भी ‘दलित समाज’ का प्रयोग भी रहेगा लेकिन इनकी हर गतिविधियों के साथ ‘दलित’ शब्द को जोड़कर इसका महिमामंडन तर्कसंगत नहीं है।
बाबा साहब स्वयं ‘दलित’ शब्द के पक्षधर नहीं थे। वे ‘नामकरण’ शीर्षक के अंतर्गत ‘दलित’ को पहचान के रूप में अस्वीकार करते हुए कहते हैं-‘एक अति उत्तम अवसर है कि दलित वर्ग का एक उचित और उपयुक्त नामकरण किया जाए।’’1 वे इसकी ठोस वजह भी बताते हैं-‘दलित वर्ग एक निम्न और असहाय समुदाय है जबकि वास्तविकता यह है कि हर प्रांत में उनमें से अनेक सुसंपन्न और सुशिक्षित लोग हैं; और समूचे समुदाय में अपनी आवश्यकताओं के प्रति चेतना जागृत हो रही है। उसके मन में भारतीय समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त करने की प्रबल लालसा पैदा हो गई है, और वह उसे प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इन सब कारणों के आधार पर ‘दलित वर्ग’ शब्द अनुपयुक्त और अनुचित है।’2
इस सबके बावजूद, दिन-रात बाबा साहब डा. अम्बेडकर का राग अलापने वाले हमारे एक विद्वान साथी चंद्रभान प्रसाद ‘दलित’ शब्द की स्थापना की दीवानगी के चलते, जीवन में जो कुछ भी है, उससे पहले दलित शब्द जोड़ कर चलने को ही दलित समाज की प्रगति का मार्ग समझते हैं। वे रोजमर्रा प्रयोग में आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे अचार, मसाले, रेड़ीमेड गारमेंट्स, बैंक, स्टॉकएक्सचेंज आदि के साथ ‘दलित’ शब्द चस्पा करते हैं और इसके चलते दलित अचार, दलित मसाले, दलित रेड़ीमेड गारमेंट्स, दलित बैंक, दलित स्टॉक एक्सचेंज जैसा नया शब्दकोश ईजाद करते हैं। FICCI (Federation of Indian Chambers of commerce and Industry) की तर्ज पर उन्होंने दलितों के परिप्रेक्ष्य में DICCI - Dalit Indian Chambers of Commerce and Industryदेश में मौजूद है। उनकी इस भावना को किसी प्रकार का राजनीतिक रंग देने की मेरी कोई मंशा नहीं है, अपितु एक संदर्भ रूप में उद्धृत किया गया है।
इसी प्रकार दलित साहित्य के पैरोकार भी साहित्य की हर विधा के नाम से पूर्व ‘दलित’ शब्द जोड़कर परंपरागत साहित्य से अलगाते हैं और इसे अपने साहित्य की विरासत बनाते हैं। इसके चलते दलित साहित्यकारों द्वारा लिखी गई कविता-दलित कविता, कहानी-दलित कहानी, उपन्यास-दलित उपन्यास, संस्मरण-दलित संस्मरण, आत्मकथा-दलित आत्मकथा आदि ‘दलित साहित्य’ की अलग-अलग विधाओं की पहचान के रूप में मौजूद हैं। कांचाइलैया इसे विस्तार देते हुए बताते हैं-‘अब खुद धर्म का इतिहास भी अपने अंत पर पहुंच रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि अपने समग्र समाज का दलितीकरण करें। दलितीकरण ही सारे भारतीय समाज में एक नए समतावादी भविष्य की स्थापना करेगा।’’3वी.टी राजशेखर इस विस्तार को दूसरा कलेवर देते हैं-‘दलित होने, इस प्राचीन धरती के मूलनिवासी होने में गर्व महसूस करो। आओ! सिर ऊंचा करके चलें। दलित संस्कृति पर गर्व करें। जो काला है वह सुंदर है।’’4 विचित्र है, मगर फिर भी ‘हिन्दू’ धर्म की तर्ज पर ‘दलित’ शब्द को स्थापित करने के पीछे ऐसी दीवानगी है कि ‘दलित’ शब्द को अस्मिता, संघर्ष व उपलब्धियों के प्रतीक की तरह प्रचारित-प्रसारित करने की होड़ लगी है। हिन्दूवाद की तर्ज पर ही इन्होंने बाबा साहब को मार्गदर्शक की बजाए एक नया अवतार/ईश्वर बना कर रख छोड़ा है। यह किन्हीं मायनों में हिन्दूवादी मोनोपॉली की तर्ज पर दलित साहित्यकारों की मोनोपॉली का नया संस्करण है।
डा. कर्दम दलित मोनोपॉली के सशक्त हस्ताक्षरों में से एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। वे ‘प्रो. तुलसीराम के ‘राष्ट्रीय सहारा’ अखबार में प्रकाशित एक आलेख के हवाले से बताते हैं-संगठित रूप से सबसे पहले गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था विरोधी अभियान चलाया था। अतः प्राचीन बौद्ध साहित्य ही वर्तमान दलित साहित्य की जननी है।’5 वे पर्सेप्सन के आधार पर इसे और आगे बढ़ाते हैं-‘तुलसीराम की इस धारणा के अनुसार बौद्ध साहित्य के पदों या श्लोकों को ‘दलित कविता’ का प्रारंभ माना जा सकता है।’6 अंतत: अपनी स्थापना देते हैं-‘कुछ दूसरे विद्वानों के अनुसार दलित कविता का प्रारंभ सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं से है, तो कुछ के अनुसार कबीर और रैदास की वाणी दलित साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं हैं। इस दृष्टि से दलित कविता का उद्भव कबीर और रैदास की रचनाओं से होता है।’7
डा. कर्दम के द्वारा पहले तथागत बुद्ध और उसके बाद सिद्ध और नाथ, फिर कबीर और रैदास की कविता को दलित कविता के उद्भव के रूप में प्रचारित करना, एक प्रकार की जबरदस्ती है। ऐसा साहस साहित्य की विश्वसनीयता को भी संदिग्ध बनाता है। नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी स्थापना या निष्कर्ष में तथ्यात्मकता और इनकी सार्वभौमिकता के तत्व मौजूद होते हैं, जो इन्हें स्वीकार्य बनाते हैं। इन तत्वों की उपेक्षा कर हमें किसी विरासत को अपना बनाने की ऐसी किसी भी मुहिम से बचना चाहिए। दलितपन के जुनून में दलित साहित्य का अगर कोई पुरोधा कल ‘बौद्ध साहित्य’ को भी दलित साहित्य का हिस्सा घोषित करने लग जाए, तो हैरत नहीं होनी चाहिए?
जहां तक संतों का सवाल है, संत रैदास खुद को ‘खलास चमारा’ कह कर संबोधित करते हैं। क्या उन्हें मात्र जाति के आधार पर दलित साहित्य की खेमेबंदी का हिस्सा बनाना उचित है? मेरा प्रश्न है-क्या रैदास को ‘बेगमपुरा’ और संत कबीर को ‘अमरदेसवा’ के साथ किसी जाति या ‘दलित’ की कोठरी में बंदी बनाकर रखा जा सकता है? क्या सिद्धों, नाथों और संतों के बहुआयामी वैचारिक कैनवास को मात्र दलित जातियों तक सीमित कर ‘दलित साहित्य’ के खूंटे से बांधने की कवायद तर्कयुक्त है? इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सभी शख्सियतें जाति और धर्म की संकीर्ण दीवारों से परे, विशुद्ध मानवतावादी सोच से ओतप्रोत थीं और इसे अपने बेबाक अंदाज में अभिव्यक्त भी करती थीं। यह अच्छी बात है कि वर्तमान दलित साहित्यकारों की तरह सिद्ध-नाथो और संतों के सामने पाठ्यक्रम में शामिल होने की कोई अफरातफरी नहीं थी, मगर वे बराबर सिलेबस का हिस्सा हैं, आखिर क्यों? दलित साहित्यकारों को इस प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
एक प्रश्न और, अगर हमारे महा नायकों के जीवन में पुरस्कार पाने और किन्हीं संगठनों की मठाधीशी के लिए लालसा होती, तो भी क्या वे किसी तिकड़मबाजी के शिकार हो सकते थे? निस्संदेह नहीं, क्योंकि उनका संघर्ष और साहस बताता है कि अवसरवाद जैसी बीमारी उनके जहन को छू तक नहीं गई थी। मेरा आग्रह है कि दलित साहित्यकार अगर तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले, बाबा साहब आदि की विरासत बनने के लिए वास्तव में गंभीर हैं तो उनके चिंतन-दर्शन की तर्ज पर अपने चिंतन-दर्शन-लेखन के प्रति भी सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाएं, तथ्यों के प्रति निष्पक्ष व ईमानदार बनें, बस इतना-सा ही तो काम है और क्या? इसके बाद जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तिकड़मबाजी की जरूरत नहीं रह जाएगी।
डा. धर्मवीर की ‘अवसरवाद के अवसाद’ और ‘दलित्व’ के योजनाबद्ध तरीके से उन्मूलन की रणनीति काफी सार्थक लगती है। उनकी चाहत थी कि हिन्दी में दलित लेखकों की पांच सौ पुस्तकें आएं। वे इसकी वजह बताते हैं कि ‘इसके लिए दो काम करने पड़े। पहला, जो दलित कौमें बाबा डॉ. अम्बेडकर के नाम और कामों से परिचित नहीं थी, उन्हें परिचित कराया गया। दूसरी, जो दलित विद्वान मार्क्सवाद और जनवाद में फंसे पड़े थे, उन्हें वापस उनकी जड़ों के पास लाया गया।...’अब कुछ और बढ़ाना है पाये-तलब को...।’ अब देखें क्या-क्या जुड़ता है और कैसी-कैसी उपलब्धियां होती हैं।’8 आंदोलन को समग्रता में देखने वाली डा. धर्मवीर की यह दृष्टि प्रशंसनीय है। लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है कि बाद के दिनों में डा. धर्मवीर खुद अपने मार्ग से भटक गए और जार सत्ता के बखान में उलझ कर रह गए। अंततः वे ‘आजीवक धर्म’, जो मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, की स्थापना व पैगंबर बनने के चक्कर में, जो कुछ भी उन्होंने बौद्धिक जगत में उल्लेखनीय कमाया था, उसे भी गंवा बैठे।
बेशक, डा. धर्मवीर की हसरत हार जाती है, मगर अपनी इस हार की जो वजह वे बताते हैं, वह काबिल-ए-गौर है-‘दलित लेखकों के बीच एक दूसरे से खुफियागिरी चल रही है। पुरस्कार न हो गया, दलित लेखकों के बीच एक खलनायक पैदा हो गया है। यदि यह पुरस्कार बंद कर दिया जाए तो दलित लेखक आपस में बंटने बंद हो जाएंगे। कम से कम इसके बंद होने से दलित लेखकों को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उन्हें यह मिल ही नहीं रहा है।’9 लेकिन आजकल पुरस्कार मिल रहा है। अगर डा. धर्मवीर जिंदा होते तो वे अपने स्टेटमेंट को जरूर क्वालीफाई करते। पुरस्कार पाने की खलनायकी की श्रेणी में छपास की भूख, पाठ्यक्रम में शामिल होने की ललक, जेबी संगठन का मोह और लोकप्रियता के लिए चारणगिरी को एक साथ जोड़ लें अगर, तो साहित्य के प्रति खलनायकी की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है, क्या नहीं? मेरी मान्यता है, जब व्यक्ति साहित्य और समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित होगा तो अपनी विरासत की श्रृंखला बनाने के लिए उसे किसी तिकड़मबाजी की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसका अपना सृजन स्वत: समृद्ध विरासत का प्रबल संवाहक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सिद्धों, नाथों और संतों जैसा सतत संघर्ष और इंसानी कर्तव्य के प्रति समर्पण जरूरी है। नहीं भूलना चाहिए कि किसी फल की लालसा/प्राथमिकता सारे किए धरे को गुड़-गोबर कर डालती है।
‘दलित’ से जुड़ी ऐसी बहस का कोई अंत नहीं है। फिलहाल, साहित्यिक पक्ष पर लौटते हैं और दलित लेखन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं। दलित साहित्य में ‘जो देखा, जो सहा-वही कहा’, यह एक तर्क आधारभूत सूत्र का काम करता है। इस संबंध में गंगाधर पानतावणे की टिप्पणी काबिल-ए-गौर है-‘दलित साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। जो हमने देखा, अनुभव किया, भोगा, जाना, समझा, उसका अंकन उत्कृष्टतापूर्ण हुआ। दलित्व का निर्मूलन हमारे साहित्य का हथियार है, इसलिए सर्वव्यापी क्रांति का वह आह्वान करता है।’10 यह दलित्व के निर्मूलन की सोच काबिल-ए-तारीफ है। यह सोच अम्बेडकरवादी चिंतन-दर्शन की पोषक है और समय की मांग भी है। निस्संदेह, साहित्य सृजन में इन पहलुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसे ‘जैसे का तैसे’ परोस देना साहित्य नहीं हो जाता-‘साहित्य में जीवन का यथार्थ ज्यों का त्यों नहीं आता, बल्कि वह पुनर्सृजित होकर आता है। इसलिए ‘साहित्य’ के सृजन का पुनर्सृजन होता है।’11पुनर्सृजन होना चाहिए लेकिन कैसे? इसे तय करने के लिए जरूरी नहीं है कि परंपरागत साहित्य के मौजूदा टूल ही इकलौते विकल्प हैं। दलित साहित्य के सृजनकार परंपरागत साहित्य से जुदा, अपने नए और कोई भी तर्कयुक्त टूल ईजाद कर सकते हैं, जो उनकी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए सार्थक ही नहीं, अग्रगामी भी हों।
ऐसा नहीं है कि दलित साहित्य में सृजन व पुनर्सृजन नहीं हुआ है, जरूर हुआ है। अगर इसे कविता के संदर्भ में देखें तो पाते हैं दस में एक कविता सृजन या पुनर्सृजन की कसौटी से गुजरी हुई नजर आती है। शेष इश्तिहार जैसी सपाट-बयानी, आक्रोश की फतवेबाजी, उत्पीड़न का उद्गार या समाचार पत्रों की कतरने जैसी बनकर रह गई हैं। इनके उदाहरण प्रस्तुत करना जोखिम का काम है। इसलिए बानगी के लिए सृजन व पुनर्सृजन की श्रेणी में आनी वाली कुछ सहज सुलभ कविताओं पर बात करते हैं। (क) ’वर्ण-धर्म की वैचारिकी के/सुडोलउरोजों का/जहरीला दूध पीकर/ विखंडन के खप्पर भरने वाली डायन है/हमारे देश की जाति-प्रथा।’12 (ख) ‘हमारे गांव में भी/ कुछ हरि होते हैं/कुछ जन होते हैं/ जो हरि होते हैं/ वे जन के साथ/न उठते हैं/ न बैठते हैं/ न खाते हैं/ न पीते हैं/ यहां तक कि जन की/ परछाई तक से परहेज करते हैं।’13(ग) ‘जिस दिन/ संगीनों के सामने/ खड़ा होना/ सीख जाओगे/ जेलों को/ अपना घर/ समझने लगोगे/ समझ लो/ उस दिन/ उनके गढ़े किले/ध्वस्त हो जाएंगे।’14
इस कड़ी में पवन करण की कविता का उल्लेख करना जरूरी महसूस हो रहा है। इस कविता में एक पिता अपनी कम उम्र की पुत्री को न डराता है और न ही उसे किन्हीं प्रतिबंधों से लादता है। वह उसके स्वाभाविक जीवनयापन के लिए उसका मार्गदर्शन कुछ ऐसे करता है: ‘मेरी बेटी प्रेम करे तो थोड़ा रुक कर/क्योंकि प्रेम करने की सही उम्र नहीं यह/ मेरी बेटी कांपते हुए और डरते हुए नहीं/इस डर पर/संभल कर चलते हुए करे प्रेम/अपने भीतर अद्भुत स्वाद लिए बैठे इस प्रेम के फल को/ हड़बड़ी में नहीं/धैर्य के नमक के साथ चखे।’…’यदि इस सब के बावजूद उससे कोई गलती होती है/तो हो जाए/ इसके पीछे उसे बचाने के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूंगा।’15यह कदम साहित्यिक जिम्मेदारी और समाज में पिता की बेबसी के कलंक को साफ करता है। लेकिन लगभग पचास वर्ष से अधिक की साहित्यिक यात्रा के बावजूद आज भी ‘जो सहा, वही कहा’ का हर विधा पर कब्जा, समसामयिक विचारणीय मसला है। इसके चलते इस साहित्य के प्रति उदासीनता व इसकी धार का कुंद होना स्वाभाविक है। ऐसी उदासीनता ही ‘विचारधारा के अंत’ की घोषणा जैसे विचार को जन्म देती है। यह साहित्य पर भी अक्षरशः लागू होती है।
जो देखा, सहा-वही कहा’ के समर्थन में अक्सर ‘स्वानुभूति’ को भी एक अन्य प्रमुख टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस विषय पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव ‘स्वानुभूति’ के आधार पर बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन यह गंभीर विचारणीय विषय है कि ‘जो देखा, सहा-वही कहा’ के सूत्र को साहित्य की हर विधा की गुणवत्ता का मूलाधार माने जाने की जिद/जबरदस्ती और इसके पक्ष में दिए जाने वाले अजीबोगरीब तर्क निराश करते हैं, परेशान करते हैं। इस संबंध में मेरा मात्र एक ही सवाल है-‘क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर, कोई शिक्षक, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री धारक कोई व्यक्ति अपनी कहानी, कविता, उपन्यास आदि के संबंध में इस सूत्र को मात्र दलित होने (जातीय पहचान) के दम पर अपनी रचना की गुणवत्ता का प्रमुख पैमाना बनाने का विशेषाधिकार रख सकता है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी विवेकशील व्यक्ति को इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि ऐसा बराबर हो रहा है। निस्संदेह, इस विषय पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।
‘स्वानुभूति’ की इस कड़ी में डॉ. कर्दम कहते हैं-‘ब्राह्मणवाद-विरोध दलित साहित्य की पहचान है।...‘तमाम विरोधों के बीच एकता का एक बड़ा सूत्र है ब्राह्मणवाद एवं सामंतवाद का विरोध।’16 इस वक्तव्य की रोशनी में कोई व्यक्ति यदि सवाल पूछ बैठे-‘कोई ब्राह्मण यदि ब्राह्मणवाद व सामंतवाद का ईमानदार विरोध करे तो क्या उसे दलित साहित्य में स्वीकार्यता मिलेगी? हम इसका उत्तर जानते हैं, मगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और वैचारिक अंतर्विरोध को समझने के लिए पुन: डा. कर्दम द्वारा डा. सुदर्शन मजीठिया के कई प्रश्नों में से एक, के उत्तर को बानगी के रूप में समझते हैं। मजीठिया-‘क्या विधवा पर कविता लिखने के लिए विधवा होना चाहिए? डा. कर्दम का उत्तर-‘सवाल यह है कि विधवा पर लिखने वाला व्यक्ति कौन है? उसकी सोच कैसी है? वह विधवा को किस नजर से देखता है? क्या वह विधवा के बिखरे हुए केश, सफेद वस्त्र, श्रृंगार विहीन चेहरे और आंसुओं को देख द्रवित होता है और उसके प्रति करुणा व्यक्त करता है? या उसके उद्धार के नाम पर उसके साथ विवाह कर समाज का हीरो और उसका देवता बन उसका दोहन करना चाहता है? या उसको ‘ईजी गोइंग’ (सहज उपलब्ध) मानकर उसके रूप-लावण्य पर मोहित होता है या समाज द्वारा उस पर किए गए अन्याय के विरोध में उसके पक्ष में खड़ा होकर समाज से लड़ता है, और उसको भी इस दकियानूसी और रूढ़ समाज की विसंगतियों को ढोने की बजाए उनके खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है? यही अंतर ‘दलितों पर लेखन’ और ‘दलित लेखन’ में है।’17
इस जवाब के चलते प्रश्न उठता है, लिखने की पात्रता तय करने की यह कवायद सबके लिए एक समान है या दलित समाज का लेखक इससे बाहर है? वैसे उत्तर जानते हुए ऐसे प्रश्न के कोई मायने ही नहीं रह जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ‘जाति’ के आधार पर किसी भी व्यक्ति की नैतिकता, ईमानदारी व उसका चरित्र-चित्रण करना भारतीय समाज का परंपरागत कोढ़ है। परंपरागत समाज इस प्रवृत्ति का बड़ा अपराधी है और दलित साहित्यकार/समाज भले ही इससे पीडि़त है, मगर वह भी इस अपराध से मुक्त नहीं है। क्योंकि वह भी उसी समाज का अनुसरण करता है जो सामाजिक असमानता, उत्पीड़न व अन्याय के सारे विवादों की जड़ है। अनैतिकता और जातिवाद के कोढ़ को बाबा साहब के शब्दों में समझते हैं-‘हिंदुओं में इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वे अपनी जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सकें। गुणों की सराहना तभी होती है, जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उनकी पूर्ण नैतिकता इतनी ही निम्न कोटि की है, जितनी जंगली जातियों की होती है। आदमी कैसा भी हो, सही या ग़लत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए।’18
कहने की जरूरत नहीं कि दलित साहित्य का ‘स्वानुभूति’ का बैरोमीटर ‘जाति’ के आधार पर ही काम करता है और इसके अनुकूल या प्रतिकूल रीडिंग देता है। साहित्यकार दलित है तो उसकी सोच ठीक, और गैर-दलित है तो संदिग्ध/गलत। जातिवादी लाठी से जबरन सबको हांकना कहां तक जायज है? इस कसौटी पर अगर दलित जातियों के अंदर मौजूद ब्राह्मणवाद को परखें तो तस्वीर कम डरावनी नहीं है। क्या दलित साहित्यकारों ने अपने साहित्य में लेखन की पात्रता के लिए दलित वर्ग के अंदर आने वाली जातियों को ही अंतिम पैमाना नहीं बना लिया हैं? जरा सोचिए, वर्ग-विहीन व जातिविहीन समाज-निर्माण का यह ‘जाति आधारित यानी जातिवादी फार्मुला’ कितना तर्कयुक्त है और कितना लोकतांत्रिक? क्या यह वर्णवादियों की तर्ज पर साहित्य में एकाधिकार व वर्चस्ववाद का नया संस्करण नहीं है? क्या दलित साहित्यकारों की नैतिकता का आधार भी परंपरावादी समाज की तर्ज पर ‘जाति’ तक सिमट कर नहीं रह गया है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है- ‘दलित साहित्यकारों की नैतिकता भी कट्टर हिन्दुओं जैसी ही जातिवादी है, जैसा ऊपर उल्लिखित बाबा साहब की कोटेशन बताती है और ‘साहित्य की जंग’ जातियों के दो अलग-अलग समूहों की जंग है, जिसमें सृजन व समाज निर्माण की संभावनाएं ना के बराबर हैं।
‘स्वानुभूति’ को केंद्र में रखकर जैसे तर्क डा. कर्दम ने विधवा पर लिखने के संबंध में दिए हैं, कमोबेश ऐसे ही तर्क हर दलित साहित्यकार के एकाधिकार/विशेषाधिकार के रूप में पेटेंट हो गए हैं। आइए, नैतिकता व विज्ञानवाद की कसौटी पर दलित/जाति आधारित ‘स्वानुभूति’ की अवधारणा का थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करते हैं। (क) क्या कोई पुरुष दलित साहित्यकार, चूंकि वह स्त्री नहीं है, स्त्री पर लिखने की पात्रता रखता है? (ख) क्या दलित समाज के अंतर्गत आने वाली किसी एक जाति का व्यक्ति अन्य किसी भी दूसरी जाति पर लिखने का नैतिक आधार रखता है? (ग) क्या खेती-किसानी से जुड़ा व्यक्ति पशुओं की खाल उतारने वाले समुदाय के जीवन पर लिख सकता है? (घ) क्या गटर के अंदर घुसकर काम करने वाले के जीवन पर वह व्यक्ति लिख सकता है, जो सिर्फ सड़कों या गली-मुहल्ले की सफाई तक सीमित है? (ड़) क्या कोई गटर में काम करने वाला व्यक्ति उस परिवार के दर्द पर लिख सकता है, जिस परिवार के सदस्य की मौत गटर में हुई है? कहने की जरूरत नहीं, ‘दलित’ अपने आप में कोई एक जाति नहीं है, यह अनेक जातियों का समुच्चय है और इन जातियों के स्वानुभूति के स्वर व स्तर निस्संदेह अलग हैं, क्या नहीं हैं? क्या डा. कर्दम का लेखन की पात्रता तय करने का पैमाना अपने आप में अ-तार्किक व भ्रामक नहीं है? ‘स्वानुभूति’ को लेकर दलित साहित्यकारों द्वारा स्थापित दबंगई को लेकर जितने तर्क गढ़े गए हैं, उनके विरुद्ध अनेक तर्क दिए जा सकते हैं, और प्रश्नों की ऐसी उत्तर-श्रृंखला साहित्यकार को अपनी पूरी जाति पर लिखने तक से अलगाकर अंतत: मात्र खुद पर लिखने तक सीमित कर सकती है, क्या नहीं? क्या दलित साहित्य के पैरोकारों को यह चुनौती स्वीकार है या फिर...?
स्वानुभूति व संवेदना का यह एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो और अधिक गहन चिंतन की मांग करता है। जिस स्वानुभूति या संवेदना की बात ऊपर कही जा रही है, वह लेखक की संवेदना है, पीडि़त की नहीं। अगर यह पीडि़त की संवेदना होती तो पीडि़त कभी का अपनी पीड़ा की दीवारों को तहस-नहस कर चुका होता जैसा बाबा साहब दावा करते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वह अपनी गुलामी की जंजीरें खुद-ब-खुद तोड़ डालेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेखन में पीडि़त की संवेदना न होना, लेखक और पीडि़त को दो अलग-अलग छोर पर लाकर खड़ा कर देता है। इसे राजनेता और आम जनता के आपसी संबंध के रूप में बेहतर समझ सकते हैं।
जिस प्रकार कोई राजनेता जनता के दुख-दर्द और इसके निवारण के लिए बड़ी-बड़ी बातें/वादे बड़े उत्साह और चालाकी से करता है, दलित साहित्यकार भी वैसा ही कुछ करता है। जिस प्रकार बड़ी-बड़ी बातों के दम पर राजनेता राजसी ठाटबाट का अधिकारी हो जाता है और जनता पहले से बुरे हाल। ऐसे ही साहित्यकार अपने शब्दजाल के दम पर स्टार बन जाता है, सिलेबस का हिस्सा हो जाता है और पुरस्कारों का स्वामी/पात्र हो जाता है और पीडि़त अपनी पुरानी अवस्था में ही खटता रहता है। दोनों के बीच का स्पेस घटता नहीं, बढ़ता दिखता है। साहित्य की भूमिका समाज के बीच निरंतर बढ़ रही आपसी खाई को पाटना है, सेतु बनाना है और दूरियां मिटाना है। यही सृजन और समाज निर्माण की बेहतर युक्ति है। लेकिन दलित साहित्यकार जो अपने को सामाजिक खाई को पाटने हेतु सेतु बनाने का दम भरता है, वह दलितों के बीच नए वर्ण जैसा हो गया है, जिसके अपने हित सर्वोपरि हैं, क्या नहीं?
जिस प्रकार आग से आग नहीं बुझ सकती, ठीक उसी प्रकार जातिवाद के उन्मूलन का टूल ‘जाति’ नहीं हो सकता। डा. तेजसिंह की मानें तो दलितवाद और जातिवाद से मुक्ति का विकल्प अम्बेडकरवाद हो सकता है। ‘जातिवाद’ से जातीय चेतना से खत्म नहीं किया जा सकता, मजबूत ही किया जा सकता है।’19 दरअसल, ‘जाति चेतना’ ने दलित साहित्य को जाति की सीमा में कैद कर दिया है और जातिवाद से लड़ते-लड़ते खुद जातिवादी बनते चले जा रहे हैं।’20 दलित पैंथर का दावा रहा है कि यह आंदोलन अम्बेडकरवादी था, लेकिन उससे भी बड़ा दावा दलित साहित्यकार कर रहे हैं। डा. तेजसिंह दोनों के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं-‘इन्होंने ‘विचार’ और ‘विचारधारा’ में कोई भेद नहीं किया और विचारों को ही विचारधारा मान बैठे। विचार और विचारधारा में अंतर होता है। सामाजिक परिवर्तन विचारों से नहीं विचारधारा से आता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए उनका प्रभाव क्षणिक होता है और विचारधारा का प्रभाव स्थाई होता है।’21
वे इससे एक कदम और आगे बढ़कर घोषणा करते हैं-‘विचारों का इतिहास नहीं होता, विचारधारा का होता है।’…विचार उसी वक्त विचारधारा का रूप लेते हैं जब वे ऐतिहासिक प्रक्रिया में सामाजिक-आर्थिक संरचना कराते हैं।’…अम्बेडकरवादी विचारधारा केवल डॉ. अम्बेडकर के विचारों तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें बुद्ध और जोतिबा फुले के विचारों का भी समावेश है।’22 वे दलित साहित्य के समर्थन में उपलब्ध तर्कशास्त्र से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। वे इसे ‘जाति’ की परिधि से मुक्ति के लिए इसके कैनवास को व्यापक करते हुए व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखे जाने की वकालत करते हैं। वे सारी संकीर्णताओं को लांघते हुए इसे अम्बेडकरवादी साहित्य की संज्ञा देते हुए स्पष्ट करते हैं-‘अम्बेडकरवादी साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करना रहा है, जिसमें जाति, लिंग, धर्म, वर्ण, और समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है।’23 उनके संपादन में निकलने वाली आलोचना की त्रैमासिक पत्रिका ‘अपेक्षा’ में इस मुद्दे को लेकर लम्बे-लम्बे लेख लिखे गए, विशेषांक निकाले गए और एक आंदोलन जैसा खड़ा हो गया लेकिन परिणाम ‘वही ढाक के तीन पात’। जैसाकि पहले संकेत दिया गया है कि ‘दलित’ आज कुछ लोगों के वजूद का सवाल बन गया है। इसे बनाए रखने के लिए उनका अपना एक ढर्रा है, तर्कशास्त्र है और एक खास किस्म की दबंगई है। मजे की बात है कि सभी पक्के अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं लेकिन वे मात्र अपनी पुरोहिताई के लिए भगवान बने रहने तक सीमित हैं।
‘स्वानुभूति’ के आधार पर साहित्य के खंडन-मंडन की जो मुहिम चली, उसमें मराठी दलित आत्मकथा/आत्मवृत की आंधी जैसे बवंडर में बदल गई। इसने दलित जीवन को सार्वजनिक पटल पर लाकर परंपरावादी समाज की खोखली संस्कृति के कोढ़ में जबरदस्त खाज का काम किया और आत्मकथा की कामयाबी ने दलित उत्पीड़न को कामयाबी का चोला पहना दिया। गैर-दलित साहित्यकारों ने इसे चिंता व आत्ममंथन का विषय बनाने की अपेक्षा साहित्य की सफलता का मानदंड बना दिया। परिणामस्वरूप, शौहरत और साहित्य का शिखर पुरुष बनने की होड़ में आत्म-उत्पीड़न की अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति के नए-नए कीर्तिमान बनने लगे। आज तस्वीर कुछ ऐसी है कि दलित साहित्य की हर विधा आत्म-उत्पीड़न और इसके प्रतिकार के दो ध्रुवों के बीच सिमट रही है। इनकी अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति ने साहित्य की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया और संवेदना को कृत्रिमता का दोषी बना छोड़ा है। डा. कुसुम वियोगी अपने एक साक्षात्कार में इस स्टारडम के शार्ट-कट फार्मुले में आत्मकथा की भूमिका को रेखांकित करते हुए टिप्पणी करते हैं-‘दलित आत्मकथाओं में जो सामाजिक उत्पीड़न और पारिवारिक गंद परोसी गई है, उसे बड़े नमक मिर्च लगाकर कर चटखारेदार बना, गैर-दलित आलोचकों ने चाट बनाकर साहित्य में परोसा और दलित लेखक चतुर्वर्ण के जाल में फंस गदगद महसूस करने लगा और आत्मकथा लिखने की होड़ सी लग रही है!’24
काफी हद तक कुसुम वियोगी की बात से सहमत हुआ जा सकता है। इसके लिए कुछ नामचीन साहित्यकारों के बयानों/टिप्पणियों की रोशनी में इसे समझने की कोशिश करते हैं। नैमिशराय-‘गांवों में तो दलित समाज की महिलाओं पर खूब जुल्म और अत्याचार होता था। उसमें घासवालियों पर खूब कहर ढाया जाता था। नाड़े तोड़ना सवर्ण अपना पैदाइशी अधिकार समझते थे।’’25 शायद नैमिशराय जी के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। अगर इसे कुसुम वियोगी के चश्में से देखें तो नैमिशराय ने इसे और अधिक चटखारेदार बनाने के लिए लिख डाला-‘हमारी बस्ती की औरतें जंगल जाती हैं। एक टोकरी गोबर पर बिक जाती हैं। उनके पांव दबाती हैं। उनका बिस्तर बनती हैं।’26 नैमिशराय जी का स्त्री के प्रति गैर-जिम्मेदाराना अभिव्यक्ति का तूफान गांवों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लेखक के साथ शहर में भी तबाही मचाता है। लेखक इस तबाही को इस प्रकार बयां करता है–‘शहर की अन्य दलित बस्तियों की तरह हमारी बस्ती से भी ढेर सारी औरतें जंगल जाती थीं। उन्हें अकेला पा उनके शरीर को नोचने के लिए गिद्ध तैयार बैठे रहते थे।’27
इस कड़ी में प्रो. तुलसीराम को बीच में लाना जरूरी महसूस हो रहा है। वे अपनी मां के बारे में लिखते हैं-‘मेरी मां बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करतीं तो पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते। पिताजी अक्सर मां को फरुही से मारने दौड़ पड़ते। एक बार उन्होंने मां को मारने के लिए फरुही उठाया कि मैंने पिता को एक तमाचा मारा। उस घटना के बाद पिताजी मां को मारने से बचने लगे।’28विषयांतर व निजता पर चर्चा से बचने के लिए सिर्फ इतना कहना है कि नवीं कक्षा का छात्र मां को न्याय दिलाने के लिए पिता को तमाचा मार देता है, लेकिन सवाल जब अपनी पहली पत्नी के विरुद्ध खुद के असीम अन्याय का आता है तो संवेदना और न्याय का पहाड़ रहस्यमय ‘ब्लैक-होल’ हो जाता है। छोडि़ए! मेरा फोकस समस्या पर बात करना है, व्यक्ति की निजता पर नहीं। समस्या यह है कि किसी भी छिटपुट उदाहरण या घटना को पूरे समाज/समुदाय का सच या प्रवृत्ति बना देना और उसके आधार पर कुछ भी फतवे जारी कर देना किसी भी नजरिए से उपयुक्त नहीं है। स्त्री अस्मिता पर कीचड़ उछालने और उसके बारे में घृणित यानी नकारात्मक छवि गढ़ना क्या समाज में स्त्री को परंपरावादी अंधकारमय कोठरी में वापस धकेलने जैसा कृत्य नहीं है?
लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। आज आधुनिकता की पहचान के रूप में महिलाओं की एक ऐसी जमात तैयार हो गई है जो अंग प्रदर्शन, छोटे कपड़े पहनने, सिगरेट-शराब पीने, लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने, किसी भी स्तर पर शारीरिक संबंध बनाने को जीवन की सामान्य व स्वाभाविक गतिविधियों के रूप में देखती हैं। वे बिना किसी लाग-लपेट और मुखरता के साथ इसके समर्थन में बात करती हैं। कुछ मामलों में महिला खुद महिला होने और अपने सौंदर्य को सफलता की सीढ़ी बनाने को स्वाभाविक व विशेषाधिकार के रूप में देखती हैं। इसकी चर्चा यहां इसलिए की जा रही है कि हमें दलित साहित्य में स्त्री जीवन के हर पक्ष को स्थापित पितृसत्तात्मक नजरिए की अपेक्षा, स्त्री के नजरिए से देखने की जरूरत है। जरूरत यह भी है कि जब स्त्री की प्रगतिशीलता या उसकी रेवोल्यूशनरी एप्रोच पर बात करें तो बराबरी के स्तर पर बात करें, संवाद करें। स्त्री को किसी दूसरे दर्जे के नागरिक या अपने अधीन किसी पालतू जीव-जंतु के रूप में देखने का दुस्साहस न करें।
यह मसला साहित्य व समाज के प्रति रचनात्मक भूमिका निभाने का है। अगर ‘हंस’ के संपादक राजेन्द्र यादव जैसा कोई व्यक्ति बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर यह कहे-‘धर्म की दिग्विजय का झंडा औरत की योनि में गाड़ा जाता है।’ तो हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम राजेन्द्र यादव बनने की होड़ में स्थापना देने पर उतर आएं कि ‘ठीक इसी तरह जातीय प्रतिशोध या अहं का हर खूंटा भी स्त्री की योनि में गाड़ा जाता है।’29 लेकिन दया पवार स्त्री संबंधी ऐसे मसलों को गंभीरता से लेते हैं और पुरुष को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। वे समस्या के व्यापक कैनवास को ध्यान में रखकर बात करते है-‘औरतों को लेकर भारतीय पुरुष समाज बहुत ही शंकालु है। पुरुषों के बारे में, उनके लफड़ों के बारे में, किसी को कुछ नहीं लगता। परन्तु अपनी औरत के बारे में मात्र शंका भी हो जाये तो कितनी बड़ी ‘रामायण’ घटित होती है। वह सबको मालूम है।’30
किसी शंका, संदेह, अफवाह आदि को लेकर किसी समुदाय, किसी जाति व लिंग विशेष के प्रति उल्टी-सीधी स्थापना के मसले संबंधों की मधुरता और स्वस्थ्य समाज के निर्माण में बाधक हैं। दया पवार जिसे रामायण की संज्ञा दे रहें हैं, का सीधा-सा मतलब है विवादों का अंतहीन हो जाना। इसे समझने के लिए हम अमृत लाल नागर के उपन्यास ‘नाच्यौ बहुत गोपाल’ के पीछे की शरारत व आधारहीन स्थापना की साजिश को समझने का प्रयास करते हैं। यह उपन्यास बताता है कि एक ब्राह्मण युवती का मेहतर युवक के साथ प्रेम संबंध होता है जो शादी के अंजाम तक पहुंचता है। उसके उपरांत ब्राह्मणी से मेहतरानी बनने और फिर उसका जीवन जीने की यातना और संघर्ष पर इसका अंत होता है। यह एक काल्पनिक उदाहरण या किसी अपवाद पर आधारित है, किसी समाज का यथार्थ नहीं। यह उपन्यास दलित का चरित्र हनन, घिनौनी इमेज-बिल्डिंग और उसका सार्वभौमीकरण करके गैर-दलितों को यह मैसेज देता है कि अंतरजातीय विवाह के ऐसे भयावह परिणाम होते हैं। फिल्म ‘पी के’ भी ऐसी ही पूर्वाग्रही प्रवृत्ति की पुष्टि करती है, जिसमें धर्म का एक पुरोधा स्थापना देता है-‘मुसलमान धोखा देता है’। कहने की जरूरत नहीं कि समाज में ऐसी आधारहीन मान्यताएं मौजूद हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, मगर समाज में जहर घोलने के लिए बराबर मौजूद हैं। ऐसी स्थापनाएं दलित और गैर-दलित दोनों तरफ से हो सकती हैं। इस लिए इस साहित्य के साहित्यकार को नैतिक, ईमानदार और पूर्वाग्रह मुक्त होकर बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने की जरूरत है।
माना कि ‘आक्रोश’ दलित साहित्य की मौलिक व प्रभावशाली कसौटी है। लेकिन ‘आक्रोश’ को अंजाम देने के लिए तर्क-विवेक की हत्या ही कर डालें, तो ‘आक्रोश’ किस काम का? अब श्याम सुंदर सिंह चौहान की कहानी ‘गुबार’ को देखें तो मानसिक दिवालियापन का एक अद्भुत नमूना है। इस कहानी में चंदो (दलित पात्र) जूठन खिलाने की परंपरा का प्रतिशोध लेती है। वह अपने यहां अपहृत एक पंडित, ‘वाजपेयी’ से शारीरिक संबंध बनाती है, गर्भवती होने पर बदला लेने के तरीके को कुछ ऐसे बताती है-‘मेरी कोख से तेरी संतान पैदा होगी, वह जीवन भर जूठन खाएगी। दो-मैंने तुझे जूठा कर दिया है, अब तेरी ब्याहता, जिसे तू सात फेरे डालकर लाएगा, सारी जिंदगी मेरी जूठन का ही स्वाद लेती रहेगी।’ इस कहानी में तथाकथित प्रतिशोध लेने वाली महिला दलित है और तथाकथित पीडि़त व्यक्ति पंडित है। इस कहानी के मर्म को समझने में मदद करने वाला एक प्रश्न अनुत्तरित है-महिला के इस प्रतिरोध में उसके और उस पंडित के सेक्सुअल प्लेजर की प्राथमिकता व जीवंतता की भूमिका कितनी थी?31
इसके बरक्स कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें महिला गैर-दलित है। यदि ऐसी कहानियों को ‘हीनताबोध से राहत के लिए प्रतिशोध’ की श्रेणी में रखें तो अनुचित नहीं होगा। ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें गैर-दलित महिलाएं संतान प्राप्ति या सेक्सुअल प्लेजर के लिए दलित पुरुष से संबंध बनाती हैं। इस श्रेणी में चन्द्रभान प्रसाद की कहानी ‘चमरियामईया का शाप’, में स्त्री ठाकुर है, वह पति की अक्षमता के कारण, दलित पुरुष से बच्चा चाहती है। गिड़गिड़ाते हुए कहती है-‘मुझ पर दया करो...मुझे मुक्ति दो। मुझे मां बनना है...।’ दया की भीख मांगती है, यह ‘स्त्री विवशता की समस्या’ झकझोर देने वाली है। दूसरी कहानी ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘बिरम की बहू’ है। इसमें भी स्त्री ठाकुर ब्रह्म सिंह की पत्नी है। वह पति की अक्षमता से परेशान है और मां बनने की लालसा में सूर्य ग्रहण की रात अनाज मांगने आए वाल्मीकि युवक से सहवास करती है और मां बनती है। रतन कुमार सांभरिया की कहानी ‘शर्त’ में बहन के बलात्कार के बदले, न्याय के लिए, मुखिया की बेटी के दलित समाज के किसी लड़के के साथ रात गुजारने की शर्त रखी जाती है।
इन कहानियों में फ्रस्ट्रेशन, प्रतिशोध, वैर-भावना को छोड़कर यह देखना पहली जरूरत है कि इन कहानियों में समस्याओं के सकारात्मक निवारण की कवायद कितनी है; और जातीय फ्रस्ट्रेशन के मुक्ति का उपक्रम कितना? इनमें बेहतर समाज के निर्माण की जद्दोजहद कितनी है और अपनी ईगो की संतुष्टि का मसला कितना? माना कि दलितों का उत्पीड़न एक भयावह समस्या रही है लेकिन साहित्य न राजनीति का अखाड़ा है और गली-मुहल्ले की लठैती का। यह कोर्ट-कचहरी का भी मसला नहीं है। यह बेहद संवेदनशील व जिम्मेदारी का मसला है। इसे ईंट का जवाब पत्थर यानी आंख के बदले आंख की तर्ज पर हल करेंगे तो क्या पूरा समाज ही अंधा व लहूलुहान नहीं हो जाएगा? साहित्यिक मॉब-लिंचिंग, जो आज चल रही है, क्या यह समाज निर्माण का विकल्प हो सकती है? बेशक नहीं। अब इस साहित्य के साहित्यकार खुद तय करें कि बदलाव का स्वरूप क्या हो जो ‘जातियों की जंग’ से हुई क्षति भरपाई कर सके।
कहने की जरूरत नहीं, साहित्य की कोई भी विधा हो, उसमें ‘विश्वसनीयता’ लेखकीय ईमानदारी, कुशलता और नैतिकता की एक सशक्त कसौटी होती है। दलित साहित्य में इसकी परख के लिए ओमप्रकाश वाल्मीकि, जो साहित्य में बड़े किरदार हैं, के साहित्य से कुछ पन्ने पलटते हैं। वे अपनी आत्मकथा जूठन में मां की आंखों में दुर्गा के अवतरण की बात करते हैं। इस घटनाक्रम में मां सुखदेव त्यागी से कहती है-‘चौधरी जी, इब तो सब खाणा खा के चले गए...म्हारे जातकों...कू भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो। वो बी तो इस दिन का इंतजार कर रे ते।’32 सुख देव सिंह-‘टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है...ऊपर से जाकतों के लिए खाणा मांग री है? अपनी औकात में रह चूहड़ी। उठा टोकरा और चलती बन।’33 ‘उसी रोज मेरी मां की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। मां का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। मां ने टोकरी वहीं बिखेर दिया था। सुखदेव सिंह से कहा था-इसे ठाके अपने घर में धर ले। कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देणा।’34 अगर ऐसे प्रसंग किसी उपन्यास या कहानी की विषयवस्तु होते तो प्रेरणादायक व स्वागत योग्य हो सकते थे। लेकिन ये प्रसंग आत्मकथा के हैं जो संभवत: मराठी आत्मकथाओं का प्रतिबिंब हैं।
आत्मकथा में ‘विश्वसनीयता’ की दरकार बराबर बनी रहती है। उपरोक्त घटनाक्रम में वाल्मीकि जी मां को खुद्दारी और स्वाभिमान की प्रतीक, अन्याय को रौंद देने वाली दुर्गा बना देते हैं। अगर इसे सच माने लें तो सवाल उठता है-क्या मां को सुख देव त्यागी के जातीय चरित्र का पता नहीं था? पता था तो वे सुखदेव त्यागी के घर क्यों गई थी? इस दिन का इंतजार क्यों कर रही थी? क्यों जूठन को टोकरे में भर रखा था? बच्चों के लिए खाना क्यों मांग कर रही थी? ऐसे अनेक सवाल हैं जो विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाते हैं। सिक्के का दूसरा पक्ष इसे और संदिग्ध बनाता है। यहां त्यागी के घर से कुछ मिलना अधिकार नहीं था, बल्कि कुछ भी मिलना त्यागी के रहमोकरम पर निर्भर था। यहां मां दुर्गा बन भी गई थी अगर, तो यहां उसे दुर्गा बनने की जरूरत क्या थी। उसे दुर्गा बनने की जरूरत उस स्कूल में थी जहां स्कूल का हेडमास्टर कलीराम ओमप्रकाश वाल्मीकि को पढ़ाई के अधिकार से वंचित कर, उस पर कहर ढा रहा था, कह रहा था-‘...चूहड़े, का है?...ठीक है...वह शीशम का पेड़ खड़ा है। चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाडूं बना ले...और पूरे स्कूल कू ऐसा चमका दे, जैसा शीशा। तेरा तो खानदानी काम है।...अबेचूहड़े के, मादर चोद कहां घुस गया...अपनी मां...जा लगा पूरे मैदान में झाडू। नहीं तो गांड में मिर्ची डाल के स्कूल से बाहर काढ़ (निकाल) दूंगा।’35
यह स्कूल किसी कलीराम के पिता जी का नहीं था, सरकार का था, जो जनता के पैसे से चलता था और आज भी चलता है। यहां ओमप्रकाश वाल्मीकि के पिता भी श्रीराम या हनुमान, कुछ भी बन सकते थे और अधिकारपूर्वक कलीराम की खटिया खड़ी कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निस्संदेह, ऐसा होता अगर, मां के दुर्गा वाला घटनाक्रम सच्चाई का द्योतक होता। स्पष्ट है कि वाल्मीकि जी का परिवार शोषण-उत्पीड़न का शिकार था और इसी लिए सुखदेव त्यागी की दबंगई अपने समाज की हकीकत साफ बयां करती है। ऐसे में जबरन स्टारडम दिखाने के कोई मायने ही नहीं है। यहां इस घटनाक्रम की चर्चा इसलिए की जा रही है कि दलित साहित्य का एक बड़ा भाग झूठे स्टारडम के चक्कर में साहित्य में नैतिकता और ईमानदारी खून कर रहा है।
मसले की गंभीरता को समझने के लिए वाल्मीकि जी के एक और घटनाक्रम से रूबरू होते हैं। वाल्मीकि जी सन् 1970-71 में, उम्र लगभग बीस वर्ष, दसवीं पास, आर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग संस्थान, अंबरनाथ छात्रावास महाराष्ट्र में थे। गांव में भयंकर जातीय उत्पीड़न झेलने के बाद और पूना के एक गांव में सवर्णों द्वारा गंवई बंधुओं की आंखें फोड़ी जाने का ऐपीसोड लोगों में आक्रोश भर रहा था और इसी बीच वाल्मीकि जी दलित साहित्य की ओर आकर्षित हो रहे थे।...सविता कुलकर्णी वाल्मीकि जी को ब्राह्मण समझ उनसे बेहद प्यार करती है। इस प्यार की परिणति यानी दामाद बनने की पूर्व सीढ़ी के विषय में वाल्मीकि जी लिखते हैं-‘मिसेज कुलकर्णी ने बारी-बारी से हम तीनों (कुलकर्णी, अजय और वाल्मीकि जी) को उबटन और तेल लगाया था। तेल से मोहक सुगंध आ रही थी। मैंने कच्छे के ऊपर तौलिया लपेट रखा था। मिसेज कुलकर्णी ने तौलिए को अलग रखने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे संकोच होता है। मिसेज कुलकर्णी ने तौलिया छीनते हुए कहा, ‘तुम मेरे बेटे अजय जैसे हो। फिर मां से कैसी शर्म!’36
सविता कुलकर्णी वाल्मीकि जी के साथ समय बिताती है, उनके निवास/हास्टल में किताबें भी टेबल पर व्यवस्थित करती है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वे कैसी किताबें पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी इतने भोले कि दलित उत्पीड़न के मामले में अग्रणी रहने वाले महाराष्ट्र के बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं रहा। सविता यह भी जानती है कि वाल्मीकि जी कभी मंदिर प्रवेश नहीं करते, बाहर पुलिया पर बैठते थे। लेकिन सविता को बाल्मीकि जी के पंडित होने पर कभी शक ही नहीं हुआ। आखिर में वाल्मीकि जी का स्टारडम जाग उठता है और वे सविता को अपनी जाति बता देते हैं, कोई विवाद नहीं होता और सविता से छुटकारा पा लेते हैं। मुझे इस घटनाक्रम के विषय में इतना ही कहना है जो दूध का जला हो, क्या वो सविता कुलकर्णी जैसे पेट्रोल बम को गले में बांधना तो दूर, ऐसा सोचने तक साहस कर सकता है? लेकिन वाल्मीकि जी ने किया। वे भूल गए कि यह किसी फिल्म की स्क्रीप्ट नहीं, साहित्य है, वह भी आत्मकथा, जिसमें हर बिंदु पर सत्यता और ईमानदारी की प्रमाणिकता की दरकार होती है। खैर...
विश्वसनीयता/प्रमाणिकता को वाल्मीकि जी के नजरिए से समझते हैं-‘दलित साहित्य’ ‘आशय’ को महत्व देता है। अभिव्यक्ति और शिल्प दूसरे स्थान पर आता है। जीवन अनुभवों की प्रमाणिकता ‘आशय’ को अर्थ गंभीर बनाती है।37 इस गंभीरता की परख के लिए पुन: ‘जूठन’ के एक प्रसंग को देखते हैं-ओम प्रकाश वाल्मीकि बस्ती के ‘पहले हाई स्कूल पास’ होने पर पिता ने पूरी बस्ती को दावत दी और किसी त्यौहार जैसा माहौल था। उस दिन ’एक और विशेष बात हुई थी।चमन लाल त्यागी मेरे पास होने की बधाई देने हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई त्यागी चूहड़ों के घर बधाई देने आया था। बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह हुई थी कि चमन लाल त्यागी मुझे अपने घर ले गए थे। बेहद आत्मीयता के साथ पास बैठाकर दोपहर का खाना खिलाया था। वह भी अपने बर्तनों में। छुआछूत के माहौल में यह एक विशेष घटना थी।’38